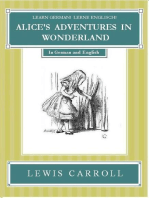Professional Documents
Culture Documents
New PDF
New PDF
Uploaded by
Ff Account0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views3 pagesOriginal Title
New pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views3 pagesNew PDF
New PDF
Uploaded by
Ff AccountCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 3
मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंध
21वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में मीडिया की भूमिका को लेकर एक
विचारोत्तेजक बहस काफी असरे से चल रही है। इसकी शुरूआत 20वीं शताब्दी में
(1970 वाले दशक में) ही आरंभ हो चुकी थी जब नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था
(न्यू इंटरनेशल इन्फॉरमेशन ऑर्डर) की मांग जोर पकड़ने लगी थी। यह वह समय
था जब नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के गठन के लिए तीसरी दुनिया में दबाव बढ़
रहा था। दोनों ही मांगों के पीछे समान तर्क थे । औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के
विलय के बाद और अफ्रीका एशिया के "बहुत सारे देशों के स्वाधीन हो जाने के
बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय समाज में विषमता घटी नहीं थी। हकीकत तो यह थी कि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समय बीतने के साथ-साथ अमीर और गरीब तथा
ताकतवर और कमज़ोर के बीच की खाई और भी गहरी हो गई थी। शीतयुद्ध के दौर
में जिन सैनिक संधि-संगठनों का निर्माण किया गया था उनके कारण कई छोटे-
छोटे राज्य पराश्रित और परजीवी वन गए. थे। आन्द्रे गुन्दर फ्रांक और समीर अमीन
जैसे विद्वानों ने इस स्थिति को पर-निर्भरता का नाम दिया, जिसके कारण पश्चिमी
देशों का उन पर प्रभुत्व निरंतर बढ़ता जा रहा था। वैसे 1960 के दशक के मध्य में
ही इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्र पति सुकर्णो ने अपने अफ्रो-एशियाई साथियों को
नव-उपनिवेशवाद और आर्थिक साम्राज्यवाद के खतरे के प्रति सतर्क करना आरंभ
कर दिया था। बहरहाल जिस बात की ओर विद्वान ध्यान दिला रहे थे वह यह थी
कि जिस तरह आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाकर पूर्व औपनिवेशिक
ताकतें नवोदित राज्यों की स्वाधीनता को बधिया कर रही थीं वैसे ही नव-
उपनिवेशवादी ताकतों की मीडिया सांस्कृ तिक साम्राज्यवाद को जड़े मजबूत कर
रही थी।
शीतयुद्ध के दौर में मीडिया का प्रयोग विरोधी को और उसकी विचारधारा को
बदनाम करने के लिए निरंतर किया जाता रहा। शुरू-शुरू में वॉयस ऑफ अमेरिका
और रेडियो फ्री यूरोप जैसी संस्थाओं ने इस काम में हिस्सा बंटया पर आगे चलकर
मीडिया राजनय ने एक परिष्कृ त रूप लिया। यह कहा जाने लगा कि जनतंत्र का
घनिष्ठ नाता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीन वर्जना रहित संचार साधनों से
है। जिस समाज में मीडिया बेड़ियों में जकड़ा हो उससे सिर्फ दमन और उत्पीड़न
की ही उम्मीद की जा सकती है। सोवियत संघ में स्टालिन के काल में और उसके
बाद भी असहमति का स्वर मुखर करने वाले असंतुष्ट तत्वों को अराजक
असामाजिक शुत्र करार दे उनका बर्बरता से दमन किया जाना आम बात थी ।
इसका शिकार न के वल पास्तरनाक जैसे कवि हुए, शोलजेनित्सिन जैसे
उपन्यासकार और साखारोव जैसे वैज्ञानिक भी बरसों नजरबंद रखे गए। पश्चिमी
मीडिया में इन सभी प्रसंगों को जोर-शोर से उछाला और जब इन्हें नोबेल पुरस्कार
के सम्मानित किया तो फिर एक बार इनके तिरस्कार और प्रताड़ना को सुर्खियों में
स्थान दिया।
इसी दौर में कु छ मीडिया विश्लेषकों ने पश्चिमी मीडिया की स्वाधीनता स्वतंत्रता,
और असलियत की पड़ताल शुरू कर दी। इनमें सबसे पहला नाम जो याद आता है
वह वांस पेकार्ड का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक दि हिडन परसुएडर्स में इस बात का
खुलासा किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष समझे जाने वाले मीडिया भी विज्ञापनों के
माध्यम से पाठकों दर्शकों और स्त्रोताओं को किस तरह प्रभावित अनुकू लित करते
हैं। एक और पुस्तक सेडक्शन ऑफ दि इनोसेंट में भी इस बात को रेखांकित
किया गया कि हमारे दिल और दिमाग को अपनी इच्छानुसार रंगने का काम सिर्फ
अखबार और टेलिवीजन या रेडियो ही नहीं करते बल्कि कॉमिक्स, फिल्में और
उपन्यास भी इसमें काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शीतयुद्ध के युग में
प्रकाशित जॉन लेकार के जासूसी उपन्यास द स्पाए हू के म इन फ्रॉम द कोल्ड तथा
इयान फ्लेमिंग के जेम्स बॉण्ड शृखंला के उपन्यासों का उदाहरण विद्वान इसी तर्क
को पुष्ट करने के लिए देते रहे हैं। जब 1960 में अमेरिका के राष्ट्र पति पद के चुनाव
के लिए निक्सन के मुकाबले कै नेडी मैदान में उतरे तो यह बात किसी से छिपी न
रही कि अपने करिश्माई आकर्षक व्यक्तित्व और युवा दिलेर छवि के कारण कै नेडी
टेलिविज़न का उपयोग अपने पक्ष में बखूबी करने में अपने प्रतिपक्षी की तुलना में
कही अधिक कामयाब रहे। आगे चलकर विलियम मैन्वेस्टर ने सेलिंग ऑफ द
प्रेसिडेंट में इस प्रसंग का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया।
दूसरी ओर मार्शल मैनकलुहान ने मीडिया के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के सामाजिक
सांस्कृ तिक प्रभावों का गहन विचारोत्तेजक विश्लेषण कर समाजशास्त्रियों को
अभिभूत कर दिया। उनकी अनेक स्थापनाएं क्रांतिकारी और बेहद विचारोत्तेजक
थीं, जिनमें कु छ ने गागर में सागर भरने वाले सूत्र वाक्यों का रूप ले लिया,
'माध्यम ही संदेश है' तथा 'माध्यम गर्म और ठण्डे होते हैं ', ' कै मरा आंख का
विस्तार है
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20108)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20479)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsFrom EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsRating: 4 out of 5 stars4/5 (6863)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasFrom EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasRating: 4 out of 5 stars4/5 (9991)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7503)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2487)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9975)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (3829)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionFrom EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (9765)
- The Happiness Project: Or, Why I Spent a Year Trying to Sing in the Morning, Clean My Closets, Fight Right, Read Aristotle, and Generally Have More FunFrom EverandThe Happiness Project: Or, Why I Spent a Year Trying to Sing in the Morning, Clean My Closets, Fight Right, Read Aristotle, and Generally Have More FunRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (1182)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6703)
- Getting to Yes: How to Negotiate Agreement Without Giving InFrom EverandGetting to Yes: How to Negotiate Agreement Without Giving InRating: 4 out of 5 stars4/5 (660)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishFrom EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (5620)






















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)