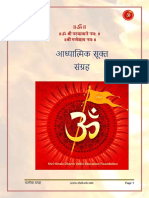Professional Documents
Culture Documents
0%(1)0% found this document useful (1 vote)
972 viewsकाल गणना
काल गणना
Uploaded by
Arun UpadhyayAncient measures of time in India
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You might also like
- Mahan NariDocument30 pagesMahan NariRajesh Kumar Duggal100% (3)
- भारत की काल गणनाDocument17 pagesभारत की काल गणनाSanjeev SaxenaNo ratings yet
- श्रुति स्मृति पुराणDocument16 pagesश्रुति स्मृति पुराणraghavendradas100% (1)
- संपूर्ण पंचांग ज्ञान 1Document327 pagesसंपूर्ण पंचांग ज्ञान 1forslowmovideosNo ratings yet
- यम सूक्तDocument2 pagesयम सूक्तMahavir Mandir PatnaNo ratings yet
- देश और काल (स्वामी माधवतीर्थजी)Document392 pagesदेश और काल (स्वामी माधवतीर्थजी)Skishna1980100% (2)
- तुरंत फल देता है सूर्याष्टक का पाठDocument1 pageतुरंत फल देता है सूर्याष्टक का पाठपं सुशील शर्मा 'सरल'No ratings yet
- षोडश मातृकाDocument4 pagesषोडश मातृकाKamalakarAthalyeNo ratings yet
- श्रवण मनन निदिध्यासनDocument3 pagesश्रवण मनन निदिध्यासनraghavendradasNo ratings yet
- Gurutva Jyotish Jun-2011 (गुरुत्व ज्योतिष)Document72 pagesGurutva Jyotish Jun-2011 (गुरुत्व ज्योतिष)CHINTAN JOSHINo ratings yet
- शिव पुराण PDFDocument845 pagesशिव पुराण PDFniranjanchou100% (1)
- ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सिद्धांतDocument138 pagesब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सिद्धांतRohit Sahu100% (2)
- स्वस्तिवाचनDocument12 pagesस्वस्तिवाचनShobhitNo ratings yet
- महामृत्युंजय मंत्रDocument30 pagesमहामृत्युंजय मंत्रbhadrakaaliNo ratings yet
- Nandi Shraddha VidhiDocument4 pagesNandi Shraddha VidhioompbhNo ratings yet
- TotkenDocument15 pagesTotkenram_krishna70No ratings yet
- Chakra Devi HindiDocument6 pagesChakra Devi HindiShaaradd P.No ratings yet
- तुलसी विवाह पद्धतिDocument28 pagesतुलसी विवाह पद्धतिPavan VoraNo ratings yet
- बालग्रह तथा पूतनाDocument9 pagesबालग्रह तथा पूतनाdindayal maniNo ratings yet
- Adhyatmik Sookt 1Document30 pagesAdhyatmik Sookt 1Rishav DikshitNo ratings yet
- सर्वतोद्रद्र मंडंलDocument9 pagesसर्वतोद्रद्र मंडंलShashanka PandaNo ratings yet
- Sandhya Deep MantraDocument3 pagesSandhya Deep MantraADITYA_PATHAKNo ratings yet
- मांगलिक दोष निवारण का उपाय अध्ययन एवं शोध की गयीं बातेंDocument3 pagesमांगलिक दोष निवारण का उपाय अध्ययन एवं शोध की गयीं बातेंRomani BoraNo ratings yet
- गजेन्द्र मोक्ष स्त्रोतDocument9 pagesगजेन्द्र मोक्ष स्त्रोतMehul Bhatt100% (1)
- श्री शम्भु गीताDocument220 pagesश्री शम्भु गीताAkashNo ratings yet
- पंचमहायज्ञविधिDocument54 pagesपंचमहायज्ञविधिDaleep KumarNo ratings yet
- महामृत्युंजय जपDocument9 pagesमहामृत्युंजय जपManish Kalia100% (1)
- नाड़ी ज्योतिष के रहस्यDocument2 pagesनाड़ी ज्योतिष के रहस्यravi goyalNo ratings yet
- वैधव्य योगDocument1 pageवैधव्य योगJan Jyotish MitraNo ratings yet
- Vivah SanskarDocument95 pagesVivah SanskarDeep Pandya0% (1)
- ॐ नमः शिवायःDocument4 pagesॐ नमः शिवायःjitendraktNo ratings yet
- कुबेर साधना BY महाकाली तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति साधनाDocument7 pagesकुबेर साधना BY महाकाली तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति साधनाPrime PlexNo ratings yet
- श्री शिक्षाष्टकम्Document2 pagesश्री शिक्षाष्टकम्Surya BabaNo ratings yet
- Shakambhari-Kavach-V1-2020-07-31 - To ShareDocument6 pagesShakambhari-Kavach-V1-2020-07-31 - To ShareNK SharmaNo ratings yet
- All SahasranamamDocument1,044 pagesAll SahasranamamDev79 Sreekar NandiNo ratings yet
- वासवदत्ता में आदर्श राजनैतिक व्यवस्थाDocument4 pagesवासवदत्ता में आदर्श राजनैतिक व्यवस्थाvishal sharma100% (1)
- WhatsApp Chat with सूर्य यंत्र ज्योतिषDocument213 pagesWhatsApp Chat with सूर्य यंत्र ज्योतिषhasraj thoratNo ratings yet
- भैरव रक्षा कवचDocument2 pagesभैरव रक्षा कवचअखिलेश कैलखुराNo ratings yet
- अप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्रDocument2 pagesअप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्रSushilSharmaNo ratings yet
- Laghu ChandiDocument55 pagesLaghu ChandiMayank Bhardwaj0% (1)
- Vedic Sahitya Aur Sanskriti - Aacharya Baldev Upadhyay - MergedDocument533 pagesVedic Sahitya Aur Sanskriti - Aacharya Baldev Upadhyay - MergedNirmala DhakalNo ratings yet
- All Mantra 3Document12 pagesAll Mantra 3niteshshah007No ratings yet
- 001 - बृहद् पराशर होरा शास्त्र - पूर्वार्धम - अध्याय १ - वर्णनाध्याय - सृष्टी आरम्भ और अवतार अद्ध्यायDocument14 pages001 - बृहद् पराशर होरा शास्त्र - पूर्वार्धम - अध्याय १ - वर्णनाध्याय - सृष्टी आरम्भ और अवतार अद्ध्यायSunilkumar DubeyNo ratings yet
- जय श्रीराम हनुमान कवचDocument13 pagesजय श्रीराम हनुमान कवचSandeepNo ratings yet
- घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षणDocument12 pagesघर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षणshrinath_chauhanNo ratings yet
- सरल गोपूजन विधिDocument12 pagesसरल गोपूजन विधिPriyanshuNo ratings yet
- गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्रDocument8 pagesगजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्रJagdish Prasad JoshiNo ratings yet
- Shubh Ashubh muhurtBAJY-202Document254 pagesShubh Ashubh muhurtBAJY-202Adhyayan GamingNo ratings yet
- कर्ज मुक्ति का अनुभूत मन्त्र प्रयोगDocument11 pagesकर्ज मुक्ति का अनुभूत मन्त्र प्रयोगRaju KumarNo ratings yet
- सिद्ध भैरवी चक्र साधना का मूल स्वरूप और साधना विधान क्या है -Document1 pageसिद्ध भैरवी चक्र साधना का मूल स्वरूप और साधना विधान क्या है -Riddhesh PatelNo ratings yet
- सर्प पूजनDocument20 pagesसर्प पूजनVikas kaushikNo ratings yet
- आसन शुद्धिDocument10 pagesआसन शुद्धिVashishth ArunNo ratings yet
- Gurutva Jyotish Dec-2010Document73 pagesGurutva Jyotish Dec-2010Bhoj KhojNo ratings yet
- Shri Guru GitaDocument47 pagesShri Guru GitaAkashNo ratings yet
- तंत्र साहित्य (भारतीय) - विकिपीडियाDocument17 pagesतंत्र साहित्य (भारतीय) - विकिपीडियाKANHAIYA VERMANo ratings yet
- ओड़िशा परिचयDocument85 pagesओड़िशा परिचयArun UpadhyayNo ratings yet
- ईशावास्योपनिषद्Document42 pagesईशावास्योपनिषद्Arun Upadhyay100% (1)
- श्री सूक्तDocument9 pagesश्री सूक्तArun UpadhyayNo ratings yet
- व्यक्ति और विश्व का सम्बन्धDocument7 pagesव्यक्ति और विश्व का सम्बन्धArun UpadhyayNo ratings yet
- आदि शङ्कराचार्य कालDocument5 pagesआदि शङ्कराचार्य कालArun UpadhyayNo ratings yet
काल गणना
काल गणना
Uploaded by
Arun Upadhyay0%(1)0% found this document useful (1 vote)
972 views11 pagesAncient measures of time in India
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentAncient measures of time in India
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0%(1)0% found this document useful (1 vote)
972 views11 pagesकाल गणना
काल गणना
Uploaded by
Arun UpadhyayAncient measures of time in India
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 11
काल गणना
-अरुण कु मार उपाध्याय, भुवनेश्वर
सारांश-भारत में देश काल की माप कई प्रकार की थी तथा बहुत सूक्ष्म थी। काल के अर्थ और प्रकार की जितनी व्याख्या भारत में थी, उतनी अभी तक
आधुनिक विज्ञान में नहीं हो पायी है। भारत में ४ प्रकार के काल, ९ प्रकार के कालमान तथा ७ प्रकार के युग हैं। देश की माप के लिये ७ प्रकार के योजन थे
तथा आकाश के माप जितनी सूक्ष्मता से किये गये थे उतना आज तक नहीं हो पाआ है। यह आधुनिक विज्ञान में भी अनुसन्धान को एक नयी दिशा देता है।
काल की माप कई प्रकार से देश (दूरी) की माप से सम्बन्धित है-प्रकाश किरण की गति माध्यम से या काल खण्ड तथा आकाश खण्डों की संख्या की
समानता। अभी तक ऐसा विचार आधुनिक विज्ञान में नहीं किया गया है। इन विषयों को मूल उद्धरणों के साथ यथा सम्भव सरल रूप में दिया जा रहा है।
१. काल की परिभाषा -भारत में विभिन्न दर्शनों में काल की परिभाषा कै प्रकार से दी गयी है। इनका संकलन श्री वासुदेव पोद्दार की पुस्तक विश्व की कालयात्रा
में है (अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, के शव कुं ज, नयी दिल्ली-५५, २०००)। इनका सारांश है-
परिवर्तन का आभास काल है।
परिवर्तन क्या है-किसी स्थान पर एक वस्तु थी, वह अन्य स्थान पर चली गयी-यह गति या क्रिया है।
एक वस्तु जिस रूप में थी, वह अन्य रूप में दीखती है।
कई वस्तुओं का संग्रह एक स्थिति में था, अन्य स्थिति में दीखता है।
इनको परिणाम, पृथक् भाव या व्यवस्था क्रम कहा है-
परिणामः पृथग् भावो व्यवस्थाक्रमतः सदा। भूतैष्यद्वर्त्तमानात्मा कालरूपो विभाव्यते॥
(सांख्य कारिका, मृगेन्द्रवृत्ति दीपिका, १०/१४)
इस प्रकार देश-काल-पात्र या ज्योतिष में दिक् -देश-काल परस्पर सम्बन्धित हैं।
दिक्कालावकाशादिभ्यः (कपिल सांख्य सूत्र, २/१२) २. काल के भेद-विश्व को जितने प्रकार से देखते हैं, काल उतने ही प्रकार का है। वेद में मनुष्य, विश्व या
उसकी कोई वस्तु-सभी को पुरुष कहते हैं। पुरुष वह है जो किसी पुर (नगर) अर्थात् सीमा के भीतर दिखे।
विश्व और उनके काल के प्रकार हैं-
(१) क्षर पुरुष-जिसका हमेशा क्षय होता रहता है, तथा अन्त में पूरा विनाश हो जाता है। यह एक ही दिशा में है, जो बूढ़ा है वह पुनः युवक या बच्चा नहीं हो
सकता। आग से धुंआ निकलता है, वह वापस अपने स्रोत में नहीं आ सकता है। इसके काल को नित्य काल कहते हैं, जिसका एक अर्थ मृत्यु भी है। इसे
आधुनिक भौतिक विज्ञान के थर्मोडाइनेमिक्स में एण्ट्रोपी हैं-कोई भी वस्तु या संहति सदा अधिक अव्यवस्था की दिशा में जाती है। तीन पुरुष गीता, अध्याय
१५-द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कू टस्थोऽक्षर उच्यते॥१६॥
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥१७॥
अजोऽपि अन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। (गीता ४/६)
नित्य काल- कालोऽस्मि लोक क्षयकृ त्प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिहप्रवृत्तः। । (गीता १०/३२)
सूर्य सिद्धान्त (१/१०) में २ प्रकार के काल कहे गये हैं-अन्तकृ त् या नित्य काल, कलनात्मक या जन्य।
लोकानामन्तकृ त् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते॥१०॥
(२) अक्षर पुरुष-क्षरण या क्षय के बाद भी किसी वस्तु का नाम, रूप गुण प्रायः वैसा ही बना रहता है। बूढ़े होने पर भी हमारा वही नाम और परिचय रहता है
जो जन्म के समय था। इसी प्रकार कु छ परिवर्तन प्रायः एक चक्र में होते हैं। जैसे हर २४ घण्टे में किसी स्थान पर सूर्योदय हो जाता है। इससे हम दिन या
उससे छोटे समय की माप करते हैं। प्रकृ ति के मुख्य चक्र हैं-दिन, मास, वर्ष। इसी के अनुसार हम काम तथा उत्पादन करते हैं। अतः इसे जन्य (जन्म देने
वाला, उत्पादक) काल कहते हैं इसी से या इसके खण्डों या बड़े गुणकों से समय की माप होती है। इसी के अनुसार विज्ञान के सभी माप और गणित हैं। अन्य
गणना से यह अधिक कठिन है। यान्त्रिकी में द्रष्टा के अनुसार गति होती है। पर प्रकाश या विद्युत् प्रभाव की गति हर द्रष्टा के लिये समान होती है। अतः भगवान्
ने कलन (गणना) में सबसे कठिन इसी को कहा है। जन्य काल-कालः कलयतामहम् । (गीता १०/३०),
(३) अव्यय पुरुष-यदि किसी पूरी व्यवस्था को देखें तो उसके एक वस्तु में जो कमी होती है, उतना अन्य में बढ़ जाता है। कु ल योग उतना ही रहता है। इसके
लिये भौतिक विज्ञान में ५ प्रकार के संरक्षण नियम हैं। अन्ततः यह पूरे विश्व का काल है। इस अक्षय काल को ही विश्व का स्रोत (मुख) या धारण करने वाल
कहा है।
अक्षय काल-अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः (गीता १०/३३)
(४) परात्पर पुरुष-बहुत छोटे या बहुत बड़े स्तर के विश्व का अनुभवनहीं किया जा सकता। या, वह सब जगह समान होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
अतः इसे परात्पर पुरुष तथा इसके काल को परात्पर काल कहते हैं।
भागवत पुराण (३/११) कै वल्यं परममहान् विशेषो निरन्तरः॥२॥
एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम॥ संस्थानभुक्ता भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः॥३॥
काल का वर्णन भागवत पुराण, स्कन्ध ३, अध्याय ११ तथा अथर्ववेद, शौनक शाखा, काण्ड १९, सूक्त ५३, ५४ में है।
३. काल की माप-३ प्रकार के काल का वर्णन हर भाषा में प्रचलित है।
नित्य काल-आयु बीत रही है। उसका काल (मृत्यु) आ गयी।
जन्य काल-कितना समय हुआ (किसी निश्चित विन्दु से कितना वर्ष, मास, दिन हुआ या कितना घण्टा/मिनट/सेकण्ड हुआ)।
अव्यय काल-अभी समय ठीक नहीं है।
परात्पर काल-काल की गति कौन जानता है?
इनमें प्रथम २ काल का वर्णन स्टीफे न हाकिं स ने अपनी पुस्तक ’ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम’ में किया है। इसमें कलनात्मक या जन्य काल का वर्णन पूर्ण नहीं
है। हम यान्त्रिकी तथा प्रकाश के लिये एक ही काल का प्रयोग गणित सूत्रों में करते हैं, पर सिद्धान्त रूप में वे अलग हैं।
काल माप की कई प्रकार की इकाइयां हैं। इनके २ कारण हैं-
(१) बड़े-छोटे माप-आणविक स्तर की क्रियाओं में बहुत सूक्ष्म समय लगता है; उनके लिये बहुत छोटी इकाई चाहिये। मनुष्य जीवन से सम्बन्धित इकाइयां
दिन-मास-वर्ष से सम्बन्धित हैं जो सूर्य चन्द्र की दृष्ट गति से सम्बन्धित प्राकृ तिक चक्र हैं। दिन के छोटे अंशों घण्टा-मिनट-सेकण्ड का प्रयोग होता है। आकाश
में ग्रह गति में परिवर्तन, सूर्य चन्द्र का निर्माण आदि के लिये बहुत बड़े माप की जरूरत है।
(२) काल की विभिन्न प्राकृ तिक इकाइयों में सरल सम्बन्ध नहीं है। सभी दिन बराबर नहीं हैं। सौर या चान्द्र मास में दिनों की संख्या पूर्ण अंक नहीं है और ये
बदलते रहते हैं। इसी प्रकार सौर या चान्द्र वर्ष में दिन संख्या पूर्ण नहीं है।
इनके समाधान के लिये प्रकृ ति में ९ प्रकार के निर्माण चक्रों (पुराण में सृष्टि के सर्ग) के लिये ९ प्रकार के काल मान हैं। वर्ष से बड़ी अवधि की माप के लिये ७
प्रकार के युग हैं जो दो या अधिक कालमानों के योग से बने हैं। सूर्य सिद्धान्त (१४/१) के अनुसार ९ प्रकार के काल हैं-
ब्राह्मं पित्र्यं तथा दिव्यं प्राजापत्यं च गौरवम्। सौरं सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वै नव॥
बड़े मान से आरम्भ कर इनका क्रम है-ब्राह्म, प्राजापत्य, दिव्य, गुरु, चान्द्र, सौर, सावन, नाक्षत्र।
ये सभी कलनात्मक होने के कारण जन्य काल हैं, अतः सृष्टि के ९ सर्गों के अनुसार हैं। सभी सर्गों की निर्माण अवस्था १ -१ मेघ है, अतः बाइबिल में ९ मेघ
कहे गये हैं।
४. कालमान-९ प्रकार के कालमान तथा उनकी परिभाषा नीचे दी जा रही है-
(१) ब्राह्म-अव्यक्त से व्यक्त की सृष्टि को ब्रह्मा का दिन तथा उसके लय को रात्रि कहा गया है-
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥
अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ (गीता, अध्याय ८)
पुराणों और सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार १२,००० दिव्य वर्षों का युग होता है। एक दिव्य वर्ष ३६० सौर वर्षों का है। अतः
ब्रह्मा का दिन या कल्प = १००० युग = १००० x ३६० x १२००० = ४३२ कोटि वर्ष।
उतने ही मान की रात्रि है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार दृश्य जगत् की सीमा प्रायः उतनी ही है जितनी दूर तक ब्रह्मा के अहो-रात्र में प्रकाश जा
सकता है, अर्थात् ८६४ कोटि प्रकाश वर्ष त्रिज्या का क्षेत्र। ब्रह्मा के अहोरात्र मान से ३० दिनों का मास, १२ मासों का वर्ष तथा १०० वर्ष की परमायु है।
अर्थात् ब्रह्मा की आयु ७२,००० कल्प है-
= ७२००० x ४३२ x १०७ x ३६० = प्रायः १.१२ x १०१७ दिन।
ज्योतिष में कल्प तक की ही गणना की जाती है। के वल वटेश्वर सिद्धान्त में मन्दोच्चगति की गणना ब्रह्मा के १०० वर्षों में की है। ब्रह्मा की आयु में १ परार्ध दिन
होते हैं, अतः उसे या उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अभी ब्रह्मा का परार्ध या ५० वर्ष पूर्ण हो चुके है, ५१ वें वर्ष का प्रथम कल्प श्वेतवराह चल रहा है,
जिसमें ६ मन्वन्तर बीत चुके हैं, ७ वें मे २७ युग बीत चुके हैं, २८वें का कलियुग १७-२-३१०२ ई.पू. में आरम्भ हुआ। ब्रह्मा से बड़े काल मान विष्णु, शिव
तथा पराशक्ति के हैं-
विष्णु पुराण, अध्याय (१/३)-काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम। काष्ठास्त्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मौहूर्तिको विधिः॥८॥
तावत्संख्यैरहोरात्रं मुहूर्त्तैर्मानुषं स्मृतम्। अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः॥९॥
तैः षड्भिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे। अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम्॥।१०॥
दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु कृ तत्रेतादिसंज्ञितम्। चतुर्युगं द्वादशभिस्तद् विभागं निबोध मे॥११॥
प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने॥१५॥ ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुर्दश॥१६॥
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः॥२२॥
अध्याय (६/५) द्विपरार्धात्मकः कालः कथितो यो मया तव। तदहस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते॥४७॥
व्यक्ते च प्रकृ तौ लीने प्रकृ त्यापुरुषे तथा। तत्र स्थिते निशा चास्य तत्प्रमाणा महामुने॥४८॥
(२) प्राजापत्य-ब्रह्म का क्रियात्मक रूप प्रजापति कहते हैं। मनुष्य रूप में प्रजा का पालन करनेवाला राजा भी प्रजापति है। आकाश में यज्ञ या निर्माण कार्य
ब्रह्माण्ड के निर्माण से हुआ। उसका चक्र-भ्रमण ही ब्रह्माण्ड का प्रथम यज्ञ है। अतः यह प्राजापत्य काल हुआ। ब्रह्माण्ड विराट् मन की सबसे बड़ी प्रतिमा है,
अतः इसे मनु तत्त्व कहते हैं। इसका अक्ष-भ्रमण मन्वन्तर है। ब्रह्माण्ड मन की प्रतिमा हमारा मन है जिसके कण (कोषिका) की संख्या उतनी ही (१०११) है
जितनी ब्रह्माण्ड के कण (तारा)। व्यक्ति में भी वही मनु तत्त्व होने के कारण उसे मनुष्य कहते हैं। यह गणना शतपथ ब्राह्मण में है।
पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के दिन में १४ मन्वन्तर हैं। अतः
१ मन्वन्तर = १००० युग/१४ = ७१.४३ युग।
गणना में हम १ मन्वन्तर = ७१ युग लेते हैं। ६ युग बचते हैं जिनको हम १५ सन्ध्या में बांट देते हैं, जो दो मनु के बीच का सन्धिकाल हैं तथा मन्वन्तर के
आरम्भ और अन्त में आते हैं।
प्रत्येक सन्धिकाल = ६/१५ = ४/१० युग। युग के १० भाग करने पर उसके ४ खण्ड सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि क्रमशः ४, ३, २, १ भाग हैं। अतः प्रत्येक
सत्य युग = ४/१० युग, जो मन्वन्तरों के बीच की सन्ध्या हैं। अतः
१ मन्वन्तर = ७१ युग = ७१ x ४३२०००० = ३१,६८,००,००० वर्ष।
आधुनिक मान से भी ब्रह्माण्ड का अक्ष-भ्रमण काल प्रायः इतना ही ३२ कोटि वर्ष होना चाहिये। के न्द्रसे २/३ त्रिज्या दूरी पर सूर्य ब्रह्माण्ड के न्द्र की परिक्रमा
प्रायः २०-२५ कोटि वर्ष में करता है, बाहरी भाग का परिभ्रमण धीमा होगा तथा प्रायः ३२ कोटि वर्ष होना चाहिये।
आर्यभट ने स्वायम्भुव मनु की परम्परा में कल्प तथा युग दोनों के समान विभाग माने हैं। इसमें युग वही है ४३,२०, ००० वर्ष पर उसके ४ समान विभाग हैं-
सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि-प्रत्येक का मान १०,८०,००० वर्ष है। प्रति मन्वन्तर भी ७१.४३ के बदले पूर्ण ७२ युग का लिया है, अतः १ कल्प = ७२ x १४
=१००८ युग। वटेश्वर ने भी यही मन्वन्तर तथा कल्प माना है।
(३) दिव्य मान-सूर्य के उत्तरायण-दक्षिणायन गति चक्र या वर्ष (ऋतु वर्ष) को दिव्य दिन कहते हैं। ऐसे ६० दिव्य दिन अर्थात् ३६० सौर वर्ष का दिव्य वर्ष
होगा। यह ३ प्रकार से परिभाषित है-
वायु पुराण के २८ व्यासों की सूची में इसे परिवर्त युग कहा गया है, अर्थात् यह ऐतिहासिक परिवर्तन का चक्र है। १०० कोटि योजन के लोकालोक भाग (सूर्य
के चारों तरफ ग्रहकक्षा का क्षेत्र) की सीमा पर यदि कोई काल्पनिक ग्रह हो तो उसका परिभ्रमण काल भी प्रायः ३६० वर्ष होगा। के प्लर सिद्धान्त के अनुसार
इसकी त्रिज्या = (३६०) २/३ = ५०.६०६ ज्योतिषीय इकाई , अर्थात् ११८.६१ कोटि योजन व्यास होगा। इस नियम के अनुसार परिभ्रमण काल का वर्ग,
ग्रह की दूरी (बृहद् अक्ष) के घन के अनुपात में होता है। तीसरा अर्थ है कि सूर्य की उत्तर-दक्षिण गति को ही दिव्य दिन कहते हैं जैसे उदय-अस्त का चक्र दिन
कहलाता है। पुराण तथा ज्योतिष ग्रन्थों में उत्तरायण को देवों का दिन तथा असुरों की रात्रि कही गयी है (उद्धरण ब्राह्म मान में हैं), अतः ३६० दिनों के सावन
वर्ष की तरह ३६० दिव्य दिनों का दिव्य वर्ष होगा।
(४) गुरु मान-गुरु ग्रह १२ वर्ष में सूर्य की १ परिक्रमा करता है। मध्यम गुरु १ राशि जितने समय में पार करता है वह ३६०.०४८६ दिन (सूर्य सिद्धान्त,
अध्याय १४) का गुरु वर्ष कहा जाता है। दक्षिण भारत में पैतामह सिद्धान्त के अनुसार सौर वर्ष को ही गुरु वर्ष कहा गया है। रामदीन पण्डित द्वारा संग्रहीत-
बृहद्दैवज्ञरञ्जनम्, अध्याय ४ में इनका संग्रह है।
(५) सौर मान-सूर्य की १० अंश गति १ दिन, ३०० अंश (१ राशि) गति १ मास तथा ३६०० अंश गति (पूर्ण भगण या चक्र) १ सौर वर्ष होता है। इस प्रकार
के वल सौर वर्ष तथा सौर मास की गणना होती है। सौर मास के अनुसार ही ऋतु की गणना होती है। यह ऋतु वर्ष है, जो नाक्षत्र सौर वर्ष से थोड़ा कम होता है,
क्योंकि पृथ्वी का अक्ष शंकु अकार में २६,००० वर्षों में विपरीत गति से घूम रहा है। इस चक्र को ब्रह्माण्ड पुराण में मन्वन्तर कहा गया है। ऋतु वर्ष के ही भागों
को ऋतु कहा गया है जो दीर्घकालिक अन्तर को छोड़ देने पर सौर संक्रान्ति (राशि परिवर्तन) से आधारित होता है। २-२ सौर मास की १ ऋतु, ३ ऋतु या ६
मास का १ अयन है। इन सौर मासों के नाम हैं-
मधुश्चमाधवश्च, शुक्रश्च शुचिश्च, नभश्च, नभस्यश्च, ईषश्चोर्जश्च, सहश्चसहस्यश्च, तपश्च तपस्यश्चोपयाम गृहीतोऽसि संसर्पोऽस्यहंस्पत्याय त्वा॥
(तैत्तिरीय संहिता १/४/१४)
मधुश्चमाधवश्च वासन्तिकावृतू। शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मावृतू। नभश्च, नभस्यश्च वार्षिकावृतू। ईषश्चोर्जश्च शारदावृतू। सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतू। तपश्च
तपस्यश्च शैशिरावृतू॥ (तैत्तिरीय संहिता ४/४/११)
वर्ष में ५ या ३ ऋतुओं के विभाजन भी सौर मास के ही आधार पर हैं-
द्वादशमासाः पञ्चर्तवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन। (ऐतरेय ब्राह्मण १/१)
(६) चान्द्र मान-सूर्य की तुलना में चन्द्र गति अर्थात् चन्द्रमा की कला (प्रकाशित भाग) का चक्र प्रायः २९.५ दिन का होता है, जो चान्द्र मास कहा जाता है।
अमावास्या (एक साथ वास) में सूर्य-चन्द्र एक ही दिशा में होते हैं, उसके बाद चन्द्र आगे बढ़ने पर वह दीखना शुरु होता है, जिसे दर्श कहते हैं। दर्श से पूर्णिमा
तक शुक्ल पक्ष में १५ तिथि (प्रायः १५ दिन) तथा उसके बाद पूर्णिमा से दर्श तक कृ ष्ण पक्ष में १५ तिथियां होतीं हैं। इस चक्र के अनुसार प्रायः सभी यज्ञ-
चक्रों को वेद में दर्शपूर्ण-मास यज्ञ कहा गया है। १२ चान्द्र-मास में प्रायः ३५४ दिन होते हैं जबकि सौर वर्ष में ३६५.२५ दिन होते हैं, अतः प्रायः ३१ मास के
बाद वर्ष में १ अधिक मास जोड़कर उसे सौरमास या ऋतु-चक्र के समतुल्य करते हैं। अधिक मास में सूर्य उसी राशि में रह जाता है जिसमें वह पूर्व मास में था,
चन्द्रोदय से आगामी चन्द्रोदय को भी तिथि कहा जाता था-
यां पर्यस्तमयादभ्युदयादिति सा तिथिः। (ऐतरेय ब्राह्मण ३२/१०)
(७) पितर मान- चन्द्र के ऊपरी (विपरीत भाग जो नहीं दीखता है) में पितर रहते हैं। अतः चान्द्र-मास को पितरों का दिन कहा गया है। विपरीत भाग (पृथ्वी
से दूर) में रहने के कारण कृ ष्ण पक्ष पितरों का दिन तथा शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है। ३० चान्द्रमास का पितर मास तथा ३० चान्द्र वर्ष का पितर वर्ष
होता है।
(८) सावन मान-सूर्योदय से आगामी सूर्योदय का सावन दिन, ३० दिन का मास तथा १२ मास का वर्ष होता है। इसे सौर मास के समतुल्य करने के लिये
इसमें ५ दिन जोड़ते हैं (पाञ्चरात्र) या ४ वर्षों के अन्तर पर ६ दिन (षडाह) जोड़ते हैं।
(९) नाक्षत्र मान-स्थिर नक्षत्रों की तुलना में पृथ्वी का अक्ष-भ्रमण काल २३ घण्टा ५६ मिनट) नाक्षत्र दिन है। उसके हिसाब से ३० दिनों का मास, ३६०
दिनों का वर्ष होता है।
४. युगमान-२ प्रकार के चक्रों के योग से युग होता है, जैसे-
(१) सौर-चान्द्र मासों का योग-५ या १९ वर्ष का युग।
(२) सौरवर्ष + दिन का योग-४ वर्ष का लीप वर्ष का चक्र या गोपद युग।
(३) ग्रहण युग-सूर्य + राहु चक्रों का योग = १८ वर्ष १०.५ दिन
(४) बृहस्पति तथा सौर वर्षों का चक्र-१२ वर्ष युग।
(५) बृहस्पति + शनि का चक्र-६० वर्ष का बार्हस्पत्य युग।
(६) सौर वर्ष+ सप्तर्षि चक्र=सप्तर्षि वत्सर या युग।
(७) सौर वर्ष + पृथ्वी अक्ष का भ्रमण -२६००० वर्ष का ऐतिहासिक मन्वन्तर
(८) रोमक सिद्धान्त युग- १९ वर्ष युग x १५० = २८५० वर्ष।
(९) अयनाब्द युग-मन्दोच्च का दीर्घकालिक चक्र + पृथ्वी अक्ष का चक्र
(१०) शनि तक की ग्रह कक्षाओं (सहस्राक्ष= १००० सूर्य व्यास तक) का चक्र-ज्योतिषीय युग
(११) तपः लोक, सृष्टि के प्रसार संकोच का चक्र = कल्प
मुनीश्वर ने सिद्धान्त सार्वभौम में ५ प्रकार के युग बताये हैं-
(१) ५ वर्ष, (२) १२ x ५ = ६० वर्ष, (३) १२ x ६० = ७२० वर्ष, (४) ६०० x ७२० = ४३२०,००० वर्ष का कलियुग, (५) कलि x १० = १
युग।
७ प्रकार के योजन की तरह ७ प्रकार के युग होने चाहिये। वस्तुतः अधिक प्रकार के युगों का उदाहरण ऊपर दिया गया है, किन्तु यज्ञ या सृष्टि क्रिया की पूर्णता
के अनुसार इनके ७ वर्ग हैं-
(१) संस्कार युग-४ से १९ वर्षों में शिक्षा के क्रम पूरे होते हैं। यह ५ प्रकार के हैं-
(क) गोपद युग-४ वर्ष के लीप ईयर की पद्धति में ३६५ १/४ वर्ष की दिन संख्या पूर्ण होती है। यह दिन और वर्ष के चक्रों का योग है तथा ऐतरेय ब्राह्मण के
निम्नलिखित श्लोक पर आधारित है-
कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृ तं सम्पद्यते चरन्॥ (७/१३)
प्रथम वर्ष (कलि = गणना का आरम्भ) की गोधूलि वेला यदि १ जनवरी सन्ध्या ६ बजे से हो, तो वह द्वितीय वर्ष १ जनवरी को रात्रि १२ बजे पूरा होगा। अतः
कलि को सोया हुआ कहते हैं (इसकी पूर्णता के समय अर्द्ध रात्रि)। द्वितीय या द्वापर वर्ष तीसरे वर्ष २ जनवरी को प्रातः ६ बजे होगा जब लोग उठने लगेंगे। अतः
द्वापर को सञ्जिहान (जागने का समय) कहते हैं। तृतीय वर्ष त्रेता ४थे वर्ष २ जनवरी दिन १२ बजे पूरा होगा जब लोग खड़े होंगे (या सूर्य ऊपर खड़ा होगा)।
चौथा वर्ष कृ त (पूर्ण) २ जनवरी सन्ध्या ५ बजे समाप्त होगा जब लोग घर लौटते होंगे।
इन ४ वर्षों में १ लीप ईयर होगा जिसमें १ दिन अधिक होगा। अतः ४ वर्ष का युग उसी दिन १ जनवरी को पूर्ण होगा।
(ख) पञ्चवर्षीय युग-याजुष ज्योतिष में ५ वर्षों का युग माना गया है जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होता था क्योंकि उसी तिथि में सूर्य चन्द्र की वासव
(इन्द्र) के नक्षत्र ज्येष्ठा में युति होती थी-
माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृ ष्णसमापिनः। युगस्य पञ्चवर्षस्य कालज्ञानं प्रचक्षते॥५॥
स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं स वासवौ। स्यात् तदाऽऽदियुगं माघस्तपः शुक्लोह्ययनं ह्युदक् ॥६॥
प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्यचन्द्रमसावुदक् । सार्पार्धे दक्षिणार्क स्तु माघश्रवणयोः सदा॥७॥ (याजुष ज्योतिष ५-७)
इन वर्षों के नाम वत्सर में सम्, परि, इदा, अनु, इत्-उपसर्ग लगाने से होते थे। सिर्फ वत्सर या इद् वत्सर का अर्थ ३६० दिनों का सावन वर्ष है।
(ग) १२ वर्षीय युग-गुरु का परिभ्रमण काल है। चान्द्रमास के अनुकरण पर १२ वर्षीय युगों के नाम चैत्र वैशाख आदि हैं।
गुरुभगणा राशिगुणास्त्वाश्वय्जाद्या गुरोरब्दाः॥ (आर्यभटीय ३/४)
= गुरु के भगण में १२ से गुणा करने पर अश्विनी से आरम्भ होने वाले गुरु वर्षों की संख्या आती है।
१ राशि में गुरु के संचार का काल १ गुरु वर्ष है
राशि के अनुसार गुरुवर्षों के नाम हैं-
१, मेष-आश्वयुक् (अश्विनी), २. वृष-कार्तिक, ३. मिथुन-मार्गशीर्ष, ४. कर्क -पौष, ५. सिंह-माघ, ६. कन्या-फाल्गुन, ७. तुला-चैत्र, ८. वृश्चिक-वैशाख,
९. धनु-ज्येष्ठ,१०. मकर-आषाढ, ११. कु म्भ-श्रावण, १२. मीन-भाद्रपद।
(घ) १९ वर्षीय युग-प्रभाकर होले की पुस्तक-वेदाङ्ग ज्योतिष (आप्टे भवन, नागपुर, १९८५) के अनुसार ऋक् ज्योतिष का युग १९ वर्ष का होता है। यहां
‘पञ्चसम्वत्सरमयं युगं’ (ऋक् ज्योतिष का प्रथम श्लोक) का अर्थ है कि १९ वर्षीय युग में ५ वर्ष सम्वत्सर होते हैं, बाकी १४ वर्ष परिवत्सर आदि अन्य ४
प्रकार के हैं। याजुष ज्योतिष में भी ५ युगों के ५ x ५ = २५ वर्षों में ६ क्षय वर्ष होने से १९ वर्षों का युग होता है-
क्षयं सम्वत्सराणां च मासानां च क्षयं तथा॥ (महाभारत, शान्ति पर्व ३०१/४६)।
(ङ) ग्रहण युग-सूर्य-राहु की संयुक्त गति से १८ सौर वर्ष १०.५ दिनों में ग्रहण चक्र पूर्ण होता है। यह २२३ चान्द्रमास का सरोस चक्र कहलाता है (सुमेरियन
ज्योतिष का नाम)। इसका आधा ३३३९ तिथि का भी अर्ध-चक्र है जो दूसरे अर्ध चक्र के समान है। अतः वर्ष की ३७१ तिथियों को प्रत्येक में ९ भांश कर वर्ष
में ३३३९ भांश किये गये हैं, जो वेद में क्रान्ति-वृत्त के देवता कहे गये हैं-
त्रीणि शतानि त्रीसहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चा सपर्यन्। (ऋक् ३/९/९, १०/५२/६, वा. यजु. ३३/७)
(२) मनुष्य युग-(क) ६० वर्ष-मनुष्य जीवन का कर्म समय प्रायः ६० वर्षों का होता है जो गुरु वर्षों का चक्र है। इसमें गुरु की ५ तथा शनि की २ परिक्रमायें
होती हैं। यह सभी ज्योतिष ग्रन्थों तथा पुराणों में है। इसे वेद में अङ्गिरा काल कहा गया है-
आदित्याश्च ह वा आङ्गिरसश्च स्वर्गे लोके स्पर्धन्त-वयं पूर्वे एष्यामो वयमिति। ते हाऽऽदित्याः पूर्वे स्वर्गं लोकं जग्मुः , पश्चेवाङ्गिरसः, षष्ट्यां वा वर्षेषु। (ऐतरेय
ब्राह्मण १८/३/७)
आदित्याश्चाङ्गिरसश्च सुवर्गे लोके ऽ स्पर्धन्त .... त आदित्या एतं पञ्चहोतारमपश्यन्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण २/२/३/५)
यहां, आदित्य = १२, पञ्च होता = ५ x १२ = ६० वर्ष।
(ख) १०० वर्ष-शताब्दी काल में सप्तर्षि १ नक्षत्र चलते हैं। ऋक् ज्योतिष के १९ वर्षीय युग समाप्त होने पर पुनः वही नक्षत्र आता है। ५ युगों के १९५ वर्षों के
बाद ५ वर्षों का याजुष युग लेने पर चन्द्रमा भगण से १ नक्षत्र अधिक चलता है। कल्हण की राजतरङ्गिणी में इसे लौकिक वर्ष कहा गया है।
(ग) १२० वर्ष-३६० वर्षों के दिव्य वर्ष का १/३ भाग १२० वर्ष की ग्रह दशा भी मनुष्य की आयु मानी गयी है (विंशोत्तरी दशा) ।
(३) परिवर्त युग-१ दिव्य वर्ष या ३६० सौर वर्ष में ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। अतः यह परिवर्त युग कहा गया है। वायु पुराण (२३/११४-२२६) में २८
व्यासों की गणना के समय कभी उसे द्वापर, कभी परिवर्त कहा गया है। अतः युगों का विभाग इन्हीं परिवर्त खण्डों में है। इन्हें ही १० वां या १५वां त्रेता आदि भी
कहा गया है। इसी प्रकार का वर्णन कू र्म (अध्याय ५२) ब्रह्माण्ड पुराणों मे भी है। ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/२९/१९) में २६००० वर्षों का युग कहा गया है। उसे ही
(१/२/९/३६,३७) में ७१ युगों का मन्वन्तर कहा गया है-
षड्विंशति सहस्राणि वर्षाणि मानुषानि तु। वर्षाणां तु युगं ज्ञेयं ... (१/२/९/१९)
तस्यैकसप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते। (१/२/९/३७)
७१ x ३६० = २५,५६० या प्रायः २६,००० वर्ष।
(४) सहस्र युग-(क) भागवत प्राण (१/१/४) में शौनक ऋषि के १००० वर्ष के सत्र का वर्णन है। एक मनुष्य १०० वर्ष तक ही जीता है, पर धर्म, संस्कार
आदि के मापदण्ड हजारों वर्षों तक चलते हैं। शौनक सत्र के बाद पुराणों का पुनः सम्पादन ३००० वर्षों के बाद विक्रमादित्य के समय हुआ जो अभी २०००
वर्षों से चल रहा है। (भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व ४-१/१-४)
(ख) प्रायः सहस्र वर्ष २ दिव्य वर्षों (७२० वर्ष -मुनीश्वर वर्णित युग) या ३ दिव्य वर्षों (१०८० वर्ष) का होगा।
(ग) २७०० दिव्य वर्ष या ३०३० मनुष्य वर्ष का सप्तर्षि युग होता है-
त्रीणि वर्ष सहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः ।
त्रिंशदधिकानि तु मे मतः सप्तर्षि वत्सरः॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२९/१६, वायुपुराण, ५७/१७)
सप्तविंशति पर्यन्ते कृ त्स्ने नक्षत्र मण्डले ।
सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ते पर्यायेण शतं शतम्॥ (वायु पुराण, ९९/४१९, ब्रह्माण्ड पुराण २/३/७४/२३१)
यहां, मानुष वर्ष = चन्द्र परिक्रमा वर्ष = २७.३ दिन चन्द्र परिक्रमा x १२ = ३२७.५३६४ दिन।
३०३० मानुष वर्ष = २७२७ सौर वर्ष (३६५.२५ दिन का)
तारा प्रायः स्थिर होते हैं अतः उन्हें नक्षत्र (क्षत्र = चलना) कहा जाता है। किन्तु सप्तर्षि मण्डल के पूर्व भाग में स्थित पुलस्त्य, क्रतु तारों को मिलाने वाली रेखा
विपरीत गति से नक्षत्र को १०० वर्षों में पार करती है-
सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वो दृश्येते ह्युदितौ दिवि। तयोऽस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यस्तमं निशि॥१०५॥
तेन सप्तर्षयो युक्ता तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्॥
(विष्णु पुराण ४/२४/१०५, वायु पुराण ९९/४२१, ४१२, ब्रह्माण्ड पुराण २/३/७३/२३३, २३४)
(घ) रोमक सिद्धान्त का युग २८५० वर्षों का है जो ऋक् ज्योतिष के १९ वर्षीय युग का१५० गुणा है।
रोमकयुगमर्के न्द्वोर्वर्षा-‘ण्याकाशपञ्चवसु पक्षाः’ (२८५०)
’खेन्द्रियदिशो’ (१०५०) ऽधिमासाः ’स्वरकृ तविषयाष्टयः’ (१६,५४७) प्रलयाः॥ (पञ्चसिद्धान्तिका १/१५)
(५) ध्रुव या क्रौञ्च युग-यह सप्तर्षि युग का ३ गुणा या अयन चक्र (२६,०००) वर्ष का प्रायः १/३ भाग है। इसमें ९०९० मानव वर्ष या ८१०० सौर वर्ष होंगे-
नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषानि तु। अन्यानिनवतिश्चैव ध्रुवः सम्वत्सरः स्मृतः॥
(ब्रह्माण्ड पुराण १/२/२९/१८, वायु पुराण ५७/१८ में क्रौञ्च सम्वत्सर)
प्रायः इसी आकार का गुरु महायुग माना जा सकता है। सौर मत से मध्यम गुरु गति का गुरु वर्ष लेने पर ८५ सौर वर्ष में १ अधिक अर्थात् ८६ गुरु वर्ष होते हैं।
६० वर्षों का चक्र ८६ बार लेने पर कु ल गुरु वर्ष = ६० x ८६ = ६० x ८५ सौर वर्ष = ५१०० सौर वर्ष होंगे। माया कै लेण्डर इतने ही वर्षों का बनाया गया
था (३११४ ई.पू. से २०१२ के अन्त तक) वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-जन्म की ग्रह स्थिति ११-२-४४३३ ई.पू. में थी, जब २४ वां त्रेता चल रहा
था। उस समय विष्णुधर्मोत्तर पुराण (८२/७, ८) के अनुसार सौर तथा पैतामह दोनों मतों से प्रभव वर्ष था। इसी प्रकार मत्स्य अवतार के समय भी दोनों मतों
से प्रभव वर्ष था। इस कारण प्रभव वर्ष से गुरुवर्ष का चक्र आरम्भ होता है जब गुरु कर्क राशि में होता है, उसके मेष राशि से चक्र नहीं आरम्भ होता। अर्थात्
मत्स्य अवतार राम से ५१०० वर्ष पूर्व ९५३३ ई.पू. में हुआ था। होमर के इलियड के अनुसार भी एटलाण्टिस का अन्तिम भाग ९५६४ ई.पू. में डू बा था।
पारसी गाथाओं के अनुसार जल प्रलय ९८४४ ई.पू. में हुआ था जब जमशेद (वैवस्वत यम, १० वें व्यास) का काल था।
वर्तमाने तथा कल्पे षष्टे मन्वन्तरे गते। तस्यैव च चतुर्विंशे राजंस्त्रेता युगे तदा॥६॥
यदा रामेण समरे सगणो रावणो हतः॥ लक्ष्मणेन तथा राजन् कु म्भकर्णो निपातितः॥७॥
माघशुक्ले समारभ्य चन्द्रार्कौ वासर्क्षगौ। जीवयुक्तो यदा स्यातां षष्ट्यब्दादिस्तदा स्मृतः॥८॥
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ८२)
बल्लालसेन ने अद्भुत् सागर, १/५ अध्याय में गुरु-सूर्य-चन्द्र की धनिष्ठा में युति १ कल्प में ५ बार मानी है। प्रति चक्र १ कल्प का १/५ भाग होगा जिसमें क्रम
से गुरु-सूर्य-चन्द्र की युति अश्विनी से आरम्भ कर २७ नक्षत्रों में होगी। कल्प आरम्भ में सभी ग्रह अश्विनी आरम्भ में थे, अतः धनिष्ठा में इन ३ ग्रहोंकी युति
२२/७ कल्प/५=४३२० x १०६ x २२/३५ = ७०४ x १०६ वर्ष में होगी। (धनिष्ठा २२ नक्षत्र पूर्ण होने के बाद २३ वां है) । इस समय प्रथम चक्र आरम्भ
हो कर कल्प के ५ वें भाग ८६४ x १०६ वर्ष के ४ चक्र होंगे। ५वें चक्र में कल्पान्त तक के वल १६० x १०६ वर्ष बचेंगे।
(६) अयनाब्द युग-(१) २४०००वर्ष का चक्र -२६००० वर्षों के अयन-चक्र को ही ब्रह्माण्ड पुराण में मन्वन्तर कहा गया है-षड् विंशति सहस्राणि वर्षाणि
मानुषाणि तु । वर्षाणां युगं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२९/१९)
स वै स्वायम्भुवः पूर्वं पुरुषो मनुरुच्यते। तस्यैकसप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ (ब्रह्माण्ड पुराण,१/ २/९/३६,३७)
यहां सौर वर्ष के दिनों को वर्ष मानने से वह दिव्य वर्ष का युग होता है-
७१ x ३६५.२५ = २५९३२.७५ या प्रायः २६००० वर्ष।
युग चक्र की गणना में सुविधा के लिये ३६५.२५ के बदले ३६० लिया जाता है, जो वत्सर के दिन होते हैं। इसमें ३० दिनों के १२ मास होंगे। वर्ष के बाकी ५
या ६ दिन पाञ्चरात्र या षडाह होंगे।
मत्स्य पुराण, अध्याय २७३ में भी कहा है कि स्वायम्भुव मनु के ४३ युग बाद वैवस्वत मनु हुये जिनके बाद २८ युग बीत चुके हैं -कलि आरम्भ (३१०२ ईसा
पूर्व) तक जब सूत द्वारा पुराणों का प्रणयन हुआ-
अष्टाविंश समाख्याता गता वैवस्वतेऽन्तरे। एते देवगणैः सार्धं शिष्टा ये तान्निबोधत॥७७॥
चत्वारिंशत् त्रयश्चैव भवितास्ते महात्मनः (स्वायम्भुवः)। अवशिष्टा युगाख्यास्ते ततो वैवस्वतो ह्ययम् ॥७८॥
भविष्य पुराण में भी स्वायम्भुव मनु को बाइबिल वर्णित आदम कहा है जिसके १६००० वर्ष बाद वैवस्वत मनु हुये-
आदमो नाम पुरुषो पत्नी हव्यवती तथा। ... षोडशाब्द सहस्रे च तदा द्वापरे युगे।
(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व १/४/१६, २६)
स्वायम्भुव मनु को ब्रह्मा या प्रथम व्यास कहा गया है। कृ ष्ण द्वैपायन या बादरायण २८ वें व्यास थे, उसके बाद अन्य कोई व्यास अभी तक नहीं हुआ है अतः
अभी भी २८वां युग ही माना जाता है। वैवस्वत मनु से परिवर्त युग की गणना लेने पर बादरायण का काल २८ युग बाद था।
स्वायम्भुव मनु से वैवस्वत मनु=१६००० वर्ष = ३६० x ४३
वैवस्वत मनु से कृ ष्णद्वैपायन व्यास तक सत्य, त्रेता, द्वापर का योग ४८००+३६००+२४०० = १०८०० होता है। इसमें ३६० वर्ष के ३० युग होंगे पर २
युग (७२० वर्ष) जल प्रलय में चले गये जो आधुनिक अनुमान के अनुसार १०००० ई.पू. में हुआ।
(२) तृतीय अयनाब्द २४००० वर्ष चक्र को भविष्य पुराण (प्रतिसर्ग १/१/३) में ब्रह्माब्द (अभी तीसरा दिन या युग) तथा वायु पुराण (३१/२९) में अयनाब्द
युग कहा गया है-
त्रेता युगमुखे पूर्वमासन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। ... ये वै ब्रजकु लाख्यास्तु आसन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। कालेन बहुनातीतायनाब्द युगक्रमैः (वायु पुराण ३१/३, २९)
कल्पाख्ये श्वेत वाराहे ब्रह्माब्दस्य दिनत्रये । (भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग १/१/३)
वेदों में भी देवों का काल ३ युग पूर्व कहा गया है-या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा।
(ऋग्वेद १०/९७/३, वाजसनेयि यजु १२/७५, तैत्तिरीय संहिता ४/२/६/१, निरुक्त ९/२८)
युग गणना वैवस्वत मनु से आरम्भ होने के कारण उनके पूर्व के चक्र में ब्रह्मा आद्य त्रेता में थे। ब्रह्मा से वर्तमान गणना वाला युग आरम्भ होता तो उनसे सत्य युग
का आरम्भ होता।
तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेता युगमुखे तदा (वायु पुराण ९/४६) त्रेता युगमुखे पूर्वमासन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। (वायु पुराण ३१/३) स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेता युगे
तदा। (वायु पुराण ३३/५)
(३) अयनाब्द चक्र के २ खण्ड- २४००० वर्षों के २ खण्ड किये गये हैं-अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी। इन विभागों का वर्णन जैन शास्त्रों में है किन्तु आर्यभट ने
भी उल्लेख किया है, अवसर्पिणी को अपसर्पिणी लिखा है। किसी भी चक्र गति को परिधि से देखने पर अर्ध भाग में दूर जाने की तथा बाकी भाग में निकट आने
की गति होती है। चान्द्र मास में भी सूर्य से दूर जाने पर शुक्ल पक्ष तथा पुनः उसके निकट जाने पर कृ ष्ण पक्ष होता है। किसी भी चक्र के इन विपरीत भागों को
चान्द्र मास की तरह दर्श-पूर्ण मास, निकट-दूर गति के कारण अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी, संकोच-प्रसार के अर्थ में उद्ग्राभ-निग्राभ कहा गया है।
उत्सर्पिणी युगार्धं पश्चादपसरिणी युगार्धं च। मध्ये युगस्य सुषमाऽऽदावन्ते दुष्षमेन्दूच्चात्॥ (आर्यभटीय, कालक्रियापाद २/९)
तद्यदेना उरसि (इन्द्रः) न्यग्रहीत तस्मान्निग्राभ्या नाम। (शतपथ ब्राह्मण ३/९/४/१५)
उद्ग्राभेणोदग्रभीत् (वाज.यजु.१७/६३, तैत्तिरीय संहिता १/१/१३/१, ६/४/२, ४/६/३/४, मैत्रायणी संहिता १/१/१३, ८/१३, ३/३/८, ४१/९, काण्व
संहिता १/१२, १८/३, २१/८, शतपथ ब्राह्मण ९/२/३/२१)
एष वै पूर्णिमाः। य एष (सूर्यः) तपत्यहरहर्ह्येवैश पूर्णोऽथैष एव दर्शो यच्चन्द्रमा ददृश इव ह्येषः। अथोऽइतरथाहुः। एष एव पूर्णमा यच्चन्द्रमा एतस्य ह्यनु पूरणं
पौर्णमासीत्याचक्षते ऽथैष एष दर्षो य एष (सूर्यः) तपति ददृश इव ह्येषः। (शतपथ ब्राह्मण ११/२/४/१-२) सवृत (= चक्रीय) यज्ञो वा एष यद्दर्शपूर्णमासौ।
(गोपथ उत्तर २/२४)
युग विभाग के प्रसंग में अवसर्पिणी का अर्थ है घटते मान वाले युग-क्रम-सत्य = ४८०० वर्ष, त्रेता = ३६००, द्वापर = २४००, कलि = १२०० वर्ष।
उत्सर्पिणी में युग विपरीत क्रम में बढ़ते हुये होंगे-कलि, द्वापर, त्रेता, सत्य युग। वैवस्वत मनु के काल से अवसर्पिणी क्रम लिया गया है। उसके पूर्व आद्य युग के
त्रेता में ब्रह्मा थे। ब्रह्मा से पूर्व साध्य, मणिजा आदि का काल था जो ब्रह्माब्द का प्रथम दिन कहा जा सकता है। आज की भाषा में यह प्रागैतिहासिक युग है। इसमें
अभी तीसरा दिन चल रहा है। देव युग के पूर्व साध्य युग का उल्लेख पुरुष सूक्त, ऋक् १६ में है-
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्तः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ (वाज. यजु. ३१/१६)
भास्कराचार्य-२ ने १२,००० वर्ष के चक्र में ही आगम अनुसार बीज संस्कार किया है, अर्थात् वैदिक मत के अनुसार इसी चक्र में काल गणना होती थी।
सिद्धान्त शिरोमणि, भूपरिधि (७-८)-
खाभ्रखार्कै (१२०००) हृताः कल्पयाताः समाः शेषकं भागहारात् पृथक् पातयेत्। यत्तयोरल्पकं तत् द्विशत्या (२००) भजेल्लिप्तिकाद्यं तत् त्रिभिः (३) सायकैः
(५) ॥ पञ्च (५) पञ्चभूमिः (१५) करा (२) भ्यां हतं भानु चन्द्रेज्यशुक्रे न्दुतुङ्गेष्वृणम्। इन्दुना (१) दस्र-बाणैः (५२) करा (२) भ्यां कृ तैर्भौमसौम्येन्दुपातार्कि षु
स्वं क्रमात्॥
स्वोपज्ञ भाष्य-अत्रोपलब्धिरेव वासना। यद्वर्षं सहस्रषट्कं यावदुपचयस्ततोऽपचय इत्यत्रागम एव प्रमाणं नान्यत् कारणं वक्तुं शक्यत इत्यर्थः।
(७) ज्योतिषीय युग-३६० सौर वर्षों का दिव्य वर्ष मानकर १२,००० दिव्य वर्षों का ज्योतिषीय युग सभी पुराणों तथा ज्योतिष पुस्तकों में वर्णित है। इस की
३ व्याख्यायें हैं- (क) भास्कराचार्य -२ ने भगणोपपत्ति ग्रन्थ में कहा है कि इस काल में सभी ग्रह (शनि तक) अपना भगण (परिक्रमा) पूर्ण करते हैं।
(ख) एक अन्य मत है कि पृथ्वी का उत्तर ध्रुव वर्तमान पामीर से उत्तर ध्रुव तक गया है। इसका विषुव रेखा से उत्तर ध्रुव जाने का चक्र के ४ खण्ड कलि द्वापर,
त्रेता, कृ त युग हैं। चुम्बकीय ध्रुवों का परिवर्तन भी प्रायः इसी काल में होता है। ज्योतिषीय काल में महाद्वीपों की उत्तर दिशा में गति दीख रही है। इसका एक
कारण है कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। घूर्णन के कारण विषुव भाग थोड़ा फै ल गया है। यह फै लाव घूर्णन धीमा होने के कारण कम होता जा रहा है। अतः
उभरे भाग के द्वीप उत्तर खिसक रहे हैं। ध्रुव तथा द्वीप गतियां अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण भी हैं।
(ग) पृथ्वी की कक्षा का छोटा -बड़ा होना या उसका आकार दीर्घवृत्त से प्रायः वृत्ताकार होने का चक्र भी प्रायः इसी अवधि का है। इन मतों का आधुनिक
ज्योतिष में अभी तक सटीक अध्ययन नहीं हुआ है, के वल अनुमान मात्र हैं।
ज्योतिषीय युग ४३,२०,००० वर्षों का है। इसके ४ खण्ड सदा अवरोही क्रम में हैं-सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि जिनके मान ४, ३, २, १ अनुपात में हैं। किन्तु
आर्यभट (३६० कलि = २७४२ ई.पू.) ने इनको बराबर माना है। दोनों मतों से कलियुग का आरम्भ ३१०२ ई.पू. में हुआ है, अतः इनको ऐतिहासिक युग
मानने की भूल होती है। १००० युगों का ब्रह्मा का कल्प या दिन है। इतने ही मान की रात्रि है।
३६० अहोरात्र का ब्रह्मा का वर्ष है, तथा १०० वर्षों की ब्रह्मा की परमायु है। इस काल में प्रायः ३ x १०१७ दिन होते हैं, अतः १०१७ को परा कहते हैं। ब्रह्मा
की १०० वर्ष आयु पुरुष या विष्णु का दिन है, किन्तु कल्प से अधिक की कोई गणना नहीं होती है।
५. ऐतिहासिक युग-चक्र- इन चर्चाओं के आधार पर पुराणों का ऐतिहासिक युग चक्र बनाया जा सकता है। ब्रह्मा के पूर्व मणिजा जाति का उल्लेख वायु पुराण
आदि में है। उस काल में देवों को याम कहते थे। ४ वर्णों को साध्य, महाराजिक, आभास्वर तथा तुषित कहते थे जिनका अमरकोष में भी गण-देवता के रूप में
उल्लेख है-
आदित्य विश्व-वसवस्तुषिताभास्वरानिलाः। महाराजिक साध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः॥ (अमरकोष १/१/१०)
त्रेता युगमुखे पूर्वमासन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। देवा यामा इति ख्याताः पूर्वं ये यज्ञसूनवः॥
अजिता ब्राह्मणः पुत्रा जिता जिदजिताश्च ये। पुत्राः स्वायम्भुवस्यैते शुक्र नाम्ना तु विश्रुताः॥
तृप्तिमन्तो गणा ह्येते देवानां तु त्रयः स्मृताः। तुषिमन्तो गणा ह्येते वीर्यवन्तो महाबलाः॥
ते वै ब्रजकु लाख्यास्तु आसन् स्वायम्भुवेऽन्तरे। कालेन बहुनाऽतीता अयनाब्दयुगक्रमैः॥ (वायु पुराण ३१/३-२१)
टिप्पणी-(१) यहां जलप्रलय तथा शीत युग का चक्र आधुनिक अनुमानों के आधार पर है, जैसे मीर प्रकाशन, मास्को का The Earth है। इनसे यह स्पष्ट
है कि सभी जल प्रलय अवसर्पिणी (अवरोही) त्रेता में तथा शीत युग उत्सर्पिणी (आरोही) त्रेता में हैं। अतः भारतीय युग व्यवस्था आधुनिक मिलांकोविच
सिद्धान्त से अधिक शुद्ध है।
(२) मन्दोच्च का पूर्ण मान १ लाख वर्ष का चक्र लेने पर २१६०० वर्ष का जल-प्लावन चक्र आता है। २४००० वर्ष के चक्र के लिये २६००० वर्ष की अयन
गति में मन्दोच्च का ३१२००० वर्ष का दीर्घकालिक चक्र जोड़ना पड़ेगा।
१/२४००० = १/२६००० + १/३१२०००
मन्दोच्च का दीर्घकालिक चक्र के अतिरिक्त उसका बचा भाग सूर्य भगण में मिलाया गया है। उस मन्दोच्च गति की तुलना में सौर वर्ष थोड़ा कम होगा तथा अयन
गति कु छ अधिक होगी। अतः ५० विकला के बदले सूर्य सिद्धान्त में ६० विकला अयन गति ली गयी है। इन मानों को निकालने पर १ कल्प में मन्दोच्च का
३८७ भगण होता है-
प्राग्गते सूर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्नयः॥ (सूर्य सिद्धान्त १/४१)
इस युग-चक्र के अनुसार मयासुर का सूर्य-सिद्धान्त ९१०२+१३१=९२३३ ईसा पूर्व में हुआ, जब जलप्लावन समाप्त हुआ तथा उसके बाद ९१०२ ईसा पूर्व
में इसके अनुसार पंचांग आरम्भ हुआ।
(३) इस युग चक्र के अनुसार जल-प्रलय या हिमयुग आते हैं। अतः इसी के अनुसार युगों के ऐतिहासिक लक्षण दीखेंगे। महाभारत, शान्ति पर्व (२३२/३१-
३४ के अनुसार त्रेता में ही यज्ञ या उत्पादन का विकास होता है जैसा कि वर्तमान काल के त्रेता में १६९९ ईस्वी से दीख रहा है-
त्रेता युगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृ ते युगे। द्वापरे विप्लवं यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा।
त्रेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन् महाबलाः। सन्यन्तारः स्थावराणां जङ्गमानां च सर्वशः॥
ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/६) में भी पूर्व युग में देवताओं द्वारा विमान के प्रयोग का वर्णन है। सूर्य के अधिक दाह के कारण जल प्रलय तथा इस युग का अन्त
हुआ।
अस्मात् कल्पात्ततः पूर्वं कल्पातीतः पुरातनः॥ चतुर्युगसहस्राणि सह मन्वन्तरैः पुरा॥१५॥
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन् दाहकाल उपस्थिते। तस्मिन् काले तदा देवा आसन् वैमानिकस्तु वै॥१६॥
एकै कस्मिंस्तु कल्पे वै देवा वैमानिका स्मृताः॥१९॥आधिपत्यं विमाने वै ऐश्वर्येण तु तत्समाः॥३२॥
(४) सप्तर्षि या लौकिकाब्द का आरम्भ ३०७६ ई.पू. (कलि २५) में हुआ जब युधिष्ठिर का कश्मीर में देहान्त हुआ (राजतरङ्गिणी, तरङ्ग १)-कलैर्गतैः
सायकनेत्र (२५) वर्षैः युधिष्ठिराद्याः त्रिदिवं प्रयाताः।
राजतरङ्गिणी निर्माण के समय लौकिकाब्द २४ था जिसमें शताब्दी अङ्क नहीं लिखे जाते हैं। उस समय (शालिवाहन) शक आरम्भ से १०७० वर्ष बीते थे-
लौकिकाब्दे चतुर्विंशे शककालस्य साम्प्रतम्। सप्तत्याभ्यधिकं यातं सहस्र परिवत्सराः॥ (राजतरङ्गिणी १/५२)
शककाल ७८ ई. में हुआ, उसके १०७० वर्ष बाद ३०७६ + ७८ + १०७० = ४२२४ या शताब्दी वर्ष छोड़ने पर २४ वर्ष हुये थे। युधिष्ठिर देहान्त तक
सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे, उसके २७०० वर्ष बाद सप्तर्षि का १ चक्र पूर्ण हुआ। ३ सप्तर्षि चक्र या ८१०० वर्ष का ध्रुव वर्ष है। इस क्रम से ध्रुव वर्ष का आरम्भ
२७,३७६ ई.पू. में हुआ, जो ठीक लगता है क्योंकि वह स्वायम्भूव के पुत्र (वंशज) उत्तानपाद के पुत्र थे। उसके बाद १ चक्र पूर्ण होने के समय १९.२७६
ई.पू. में क्रौञ्च द्वीप के शासक बलि का प्रभुत्व था, अतः इसे क्रौञ्च युग भी कहा गया है। दूसरा ध्रुव चक्र पूर्ण होने के समय ११,१७६ ई.पू. में जल प्रलय की
स्थिति थी।
ऐतिहासिक युग चक्र
६. युग खण्ड-वायु पुराण (अध्याय ९८), कू र्म पुराण, अध्याय ५२ आदि में स्वायम्भुव मनु से कृ ष्ण द्वैपायन तक के २८ व्यासों की सूची दी गयी है जिन्होंने
अपने अपने समय में वेद मन्त्रों का संकलन किया। इसके अनुसार-
तृतीय त्रेता, द्वापर या परिवर्त-उशना या भार्गव शुक्राचार्य व्यास
चतुर्थ युग या त्रेता-हिरण्यकशिपु
सप्तम त्रेता युग-बलि-वामन अवतार-सप्तम व्यास शतक्रतु इन्द्र
इसी काल में वराह अवतार द्वारा समुद्र मन्थन- कार्त्तिके य द्वारा असुरों की पराजय (७ दीर्घजीवियों में बलि की गणना)
१०म त्रेता-दत्तात्रेय-त्रिधामा व्यास
१५ वां त्रेता-मान्धाता-त्र्यारुणि व्यास
१९वां त्रेता-परशुराम-भरद्वाज व्यास
२४वां त्रेता-राम द्वारा रावण का वध-ऋक्ष या वाल्मीकि व्यास।
वैवस्वत मनु के पूर्व १० युग = ३६०० वर्षों तक असुर प्रभुत्व कहा है। उसके ४र्थ युग में हिरण्यकशिपु हुआ। यह युग वैवस्वत मनु से ७ युग = २५२० वर्ष
पूर्व अर्थात् १३९०२ + २५२० = १६४२२ ई.पू. में आरम्भ हुआ।
सप्तम युग अर्थात् १५०३८२ ई.पू. से ३६० वर्ष के भीतर बलि हुये थे। इसी काल में समुद्र मन्थन, कार्त्तिके य द्वारा क्रौञ्च द्वीप विजय आदि हुआ।
वैवस्वत यम के काल में जल प्रलय का उल्लेख है। ब्रह्म पुराण (४३/७१-७७) के अनुसार यम के काल में जगन्नाथ की इन्द्रनील मणि प्रतिमा को बालू में छिपा
दिया गया और जल प्रलय के बाद वह पुनः मिली। जेन्द अवेस्ता में भी जमशेद (यम) के काल में जल प्रलय कहा है। जल प्रलय के २ योगों (७२० वर्ष) के
बाद दत्तात्रेय १० वें अर्थात् प्रलय मिला कर १२वें युग में हुए। उनका काल १२ x ३६० = ४३२० वर्ष बाद = १३९०२-४३२० = ९५८२ ई.पू. में पूरा
हुये युग में था।
मान्धाता १५ वें युग अर्थात् ८१४२-७७८२ ई.पू. में थे।
परशुराम १९वें युग अर्थात् ६७०२-६३४२ ई.पू. में थे। उनके निधन के बाद ६१७७ ई.पू. मे कलम्ब (के रल का कोल्लम) संवत् शुरु हुआ। इसमें हजार वर्षों
को नहीं लिखा जात है और अभी ८२४ ई. से गणना चल रही है जब ७००० वर्ष पूरा हो चुका था।
भगवान् राम २४वें त्रेता अर्थात् ४९०२-४५४२ ई.पू. में थे। वैवस्वत मनु से द्वापर अन्त के १०८०० वर्षों में ठीक २८ त्रेता लेने पर थोड़ा अन्तर होगा।
७. भारतीय पञ्चाङ्ग-शक और सम्वत्सर-
शक किसी निर्दिष्ट काल से दिनों की गणना है। १ की गिनती को कु श द्वारा प्रकट किया जाता है। इनका समूह शक्तिशाली हो जाता है, अतः इसे शक (समुच्चय)
कहते हैं। कु श आकार के बड़े वृक्ष भी शक हैं, जैसे उत्तर भारत में सखुआ (साल) तथा दक्षिण में शक-वन (सागवान)। मध्य एशिया तथा पूर्व यूरोप की बिखरी
जातियां भी शक थीं। पर यह जम्बू द्वीप का अंश था। शक द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में कहा गया है। यह आस्ट्रेलिया है जहां शक आकार के यूकलिप्टस वृक्ष
बहुत हैं। भारत में हिमालय का दक्षिणी भाग ही शक (साल) क्षेत्र है जहां जन्म होने के कारण सिद्धार्थ बुद्ध को शाक्यमुनि कहते थे। पर गोरखपुर से दक्षिण
पश्चिम ओड़िशा तक साल वृक्षों का क्षेत्र चला गया है जिसके दक्षिणी छोर पर राम ने ७ साल वृक्षों को भेदा था। यह भारत का लघु शक द्वीप है , जहां के ब्राह्मण
शाकद्वीपीय कहलाते हैं।
चान्द्र और सौर वर्ष का समन्वय सम्वत्सर है। चन्द्रमा मन का नियन्त्रक है अतं पर्व चान्द्रतिथि के अनुसार होते है। ऋतु से समन्वय के लिये उसे सौर वर्ष के
साथ मिलाया जाता है। इसके अनुसार समाज चलता है, अतः इसे सम्वत्सर कहते हैं। सम्वत्सर के अन्य कई अर्थ भी हैं-(१) पृथ्वी कक्षा, (२) सौर मण्डल
जहां तक सूर्य प्रकाश १ सम्वत्सर में जाता है-१ प्रकाश वर्ष त्रिज्या का गोला। (३) गुरु वर्ष जो प्रायः सौर वर्ष के समान है। (४) वेदाङ्ग ज्योतिष के ५ प्रकार
के वत्सरों में जो सौर वर्ष के सबसे निकट होता है उसे सम्वत्सर कहते हैं।
(१) स्वायम्भुव मनु काल-स्वायम्भुव मनु काल में सम्भवतः आज के ज्योतिषीय युग नहीं थे। यह व्यवस्था वैवस्वत मनु के काल से आरम्भ हुयी अतः उनसे
सत्ययुग का आरम्भ हुआ। यदि ब्रह्मा से आरम्भ होता तो ब्रह्मा आद्य त्रेता में नहीं, सत्य युग के आरम्भ में होते। अथवा सत्ययुग पहले आरम्भ हो गया, पर
सभ्यता का विकास काल त्रेता कहा गया। ब्रह्मा की युग व्यवस्था में युग पाद समान काल के थे जैसा ऐतरेय ब्राह्मण के ४ वर्षीय गोपद युग में या स्वायम्भुव
परम्परा के आर्यभट का युग है। वर्ष का आरम्भ अभिजित् नक्षत्र से होता था, जिसे बाद में कार्त्तिके य ने धनिष्ठा नक्षत्र से आरम्भ किया। कार्त्तिके य काल में
(१५८०० ई.पू.) यह वर्षा काल था। स्वायम्भुव मनु काल में यह उत्तरायण का आरम्भ था। किन्तु दोनों व्यवस्थाओं में माघ मास से ही वर्ष का आरम्भ होता
था। मासों का नाम पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा के नक्षत्र से था, जो आज भी चल रहा है। मास का आरम्भ दोनों प्रकार से था-अमावास्या से या पूर्णिमा से। यह
अयन गति के अन्तर के कारण बदलता होगा जैसा विक्रमादित्य ने महाभारत के ३००० वर्ष बाद शुक्ल पक्ष के बदले कृ ष्ण पक्ष से मासारम्भ कर दिया। दिन का
आरम्भ भी कई प्रकार से था जैसा आज है।
ब्रह्मा के काल में सौर ऋतु वर्ष की भी गणना थी। इसमें सूर्य की उत्तरायण-दक्षिणायन गतियों के योग से वर्ष होता था। विषुव के उत्तर तथा दक्षिण ३-३ वीथियों
में सूर्य १-१ मास रहता था। विषुव के उत्तर तथा दक्षिण में १२, २०, २४ अंश के अक्षांश वृत्तों से ये वीथियां बनती थीं। ३४० उत्तर अक्षांश का दिनमान सूर्य
की इन रेखाओं पर स्थिति के अनुसार ८ से १६ घण्टा तक होगा। अतः दक्षिण से इन वृत्तों को गायत्री (६ x ४ अक्षर) से जगती छन्द (१२ x ४ अक्षर)
तक का नाम दिया गया। यह नीचे के चित्र से स्पष्ट है। इसकी चर्चा ऋग्वेद (१/१६४/१-३, १२, १३, १/११५/३, ७/५३/२, १०/१३०/४), अथर्व वेद
(८/५/१९-२०), वायु पुराण, अध्याय २, ब्रह्माण्ड पुराण अ. (१/२२), विष्णु पुराण (अ. २/८-१०) आदि में है। इनके आधार पर पं. मधुसूदन ओझा ने
आवरणवाद में इसकी व्याख्या की है (श्लोक १२३-१३२)। बाइबिल के इथिओपियन संस्करण में इनोक की पुस्तक के अध्याय ८२ में भी यही वर्णन है।
(२) ध्रुव पञ्चाङ्ग-ध्रुव को स्वायम्भुव मनु का पौत्र कहा गया है, किन्तु उनमें कु छ अधिक अन्तर होगा। भागवत, विष्णु पुराणों के अनुसार ध्रुव को परम पद मिला
तथा उनके चारों तरफ सप्तर्षि भ्रमण से काल गणना शुरु हुई। उस काल से ८१०० वर्ष का ध्रुव संवत्सर शुरु हुआ जिसका तीसरा चक्र ३०७६ ई.पू. में पूर्ण
हुआ। ध्रुव काल ३ x ८१०० + ३०७६ = २७,३७६ ई.पू हुआ। कुं वरलाल जैन ने अपूर्ण वंशावली के आधार पर पृथु तक की काल गणना की है। संवत्सरों
के अनुसार इसके २ आधार हो सकतेहैं-स्वायम्भुव से वैवस्वत मनु तक के काल को ६ भाग में बांटने पर १-१ मन्वन्तर का काल आयेगा। यह प्रायः
१५,२००/६ = २५३४ वर्ष होगा। यह सप्तर्षि वत्सर के निकट है, अतः २७०० वर्ष का सप्तर्षि चक्र तथा उसका ३ गुणा ध्रुव वर्ष लेना अधिक उचित है। ध्रुव
काल के वर्णन में प्रायः २७०० वर्ष का लघु-मन्वन्तर तथा ८१०० वर्ष का कल्प हो सकता है। १९२७६ ई.पू. में क्रौञ्च द्वीप का प्रभुत्व था जिसपर बाद में
कार्त्तिके य ने आक्रमण किया।
(३) कश्यप-१७५०० ई.पू. में देव-असुरों की सभ्यता आरम्भ हुई। तथा राजा पृथु काल में पर्वतीय क्षेत्रों को समतल बना कर खेती, नगर निर्माण आदि हुये।
खनिजों का दोहन हुआ। इन कालों में नया युग आरम्भ हुआ पर उनका पञ्चाङ्ग स्पष्ट नहीं है।
(४) कार्त्तिके य पञ्चाङ्ग-पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की दिशा अभिजित् से हट गयी थी, अतः १५,८०० ई.पू. में कार्त्तिके य ने बह्मा की सलाह से धनिष्ठा से वर्ष
आरम्भ किया जो वेदाङ्ग ज्योतिष में चलता है।
ऋग् ज्योतिष (३२, ५,६) याजुष ज्योतिष (५-७)
माघशुक्ल प्रपन्नस्य पौषकृ ष्ण समापिनः। युगस्य पञ्चवर्षस्य कालज्ञानं प्रचक्षते॥५॥
स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ। स्यात्तदादि युगं माघः तपः शुक्लोऽयनं ह्युदक् ॥६॥
प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसावुदक् । सार्पार्धे दक्षिणार्क स्तु माघश्रवणयोः सदा॥७॥
प्रायः १६००० ईसा पूर्व में अभिजित् नक्षत्र से उत्तरी ध्रुव दूर हो गया जिसे उसका पतन कहा गया है। तब इन्द्र ने कार्त्तिके य से कहा कि ब्रह्मा से विमर्श कर
काल निर्णय करें-
महाभारत, वन पर्व (२३०/८-१०)-
अभिजित् स्पर्धमाना तु रोहिण्या अनुजा स्वसा। इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता॥८॥
तत्र मूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्युतम्। कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय॥९॥
धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः। रोहिणी ह्यभवत् पूर्वमेवं संख्या समाभवत्॥१०॥
उस काल में धनिष्ठा में सूर्य के प्रवेश के समय वर्षा का आरम्भ होता था, जब दक्षिणायन आरम्भ होता था। कार्त्तिके य के पूर्व असुरों का प्रभुत्व था, अतः
दक्षिणायन को असुरों का दिन कहा गया है-
सूर्य सिद्धान्त, अध्याय १-मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदह उच्यते॥१३॥
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्। षट् षष्टिसङ्गुणं दिव्यं वर्षमासुरमेव च॥१४॥
(५) विवस्वान् पञ्चाङ्ग-यह वैवस्वत मनु के पिता थे अतः इनका भी काल १३९०२ ई.पू. माना जा सकता है, जिसके बाद १२००० वर्ष का अवसर्पिणी-
उत्सर्पिणी चक्र तथा चैत्र शुक्ल से वर्ष आरम्भ हुये। इसके बाद सूर्य सिद्धान्त के कई संशोधन हुये। मयासुर का संशोधन जल प्रलय के बाद सत्ययुग समाप्ति के
अल्प (१२१ वर्ष) बाद रोमकपत्तन में हुआ।
सूर्य सिद्धान्त प्रथम अध्याय-अल्पावशिष्टे तु कृ ते मयो नाम महासुरः। रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम्॥२॥
वेदाङ्गमग्र्यखिलं ज्योतिषां गतिकारणम्। आराधयन्विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुष्करम्॥३॥
तस्मात् त्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानम् ददामि ते।
रोमके नगरे ब्रह्मशापान् म्लेच्छावतार धृक् ॥ (पूना, आनन्दाश्रम प्रति)
शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः। युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र के वलम्॥९॥
(६) इक्ष्वाकु काल से भी काल गणना आरम्भ हुई थी। महालिंगम के अनुसार उनका काल १-११-८५७६ ई.पू. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ। यह तंजाउर के
मन्दिरों की गणना के आधार पर है।
(७) परशुराम पञ्चाङ्ग-६१७७ ई.पू.-परशुराम के निधन पर कलम्ब (कोल्लम्) सम्वत्। इसका अन्य प्रमाण है कि मेगास्थनीज ने सिकन्दर से ६४५१ वर्ष ३
मास पूर्व अर्थात् ६७७७ ई.पू. अप्रैल मास में डायोनिसस का भारत आक्रमण लिखा है जिसमें पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी राजा बाहु मारा गया थ। उससे १५
पीढ़ी बाद हरकु लस (विष्णु) का जन्म हुआ। इस काल के विष्णु अवतार परशुराम थे। उनका काल प्रायः ६०० वर्ष बाद आता है जो १५ पीढ़ी का काल है।
मयासुर के ३०४४ वर्ष बाद ऋतु १.५ मास पीछे खिसक गया था अतः नये सम्वत् का प्रचलन हुआ।
(८) कलि के पञ्चाङ्ग-राम का जन्म ११-२-४४३३ ई.पू. में हुआ था पर उस काल के किसी पञ्चाङ्ग का उल्लेख नहीं है। परशुराम के ३००० वर्ष बाद कलियुग
आरम्भ में ही नये पञ्चाङ्ग की आवश्यकता हुयी। युधिष्ठिर काल में ४ प्रकार के पञ्चाङ्ग हुये-(क) युधिष्ठिर शक-यह उनके राज्याभिषेक के दिन १७-१२-३१३९
ई.पू. से हुआ। उसके ५ दिन बाद उत्तरायण माघशुक्ल सप्तमी को हुआ। अतः अभिषेक प्रतिपदा या द्वितीया को था। (ख) कलि सम्वत्-शासन के ३६ वर्ष से
कु छ अधिक बीतने पर १७-२-३१०२ ई.पू. उज्जैन मध्यरात्रि से कलियुग आरम्भ हुआ जब भगवान् कृ ष्ण का देहान्त हुआ। उसके २दिन २-२७-३०
घं.मि.से. बाद २०-२-३१०२ ई.पू २-२७-३० घं.मि.से. से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरम्भ हुआ। (ग) जयाभ्युदय शक-भगवान् कृ ष्ण के देहान्त के ६ मास ११
दिन बाद २२-८-३१०२ ई.पू. को जब विजय के बाद जय सम्वत्सर आरम्भ हुआ, तो युधिष्ठिर ने अभ्युदय के लिये सन्यास लिया। यह परीक्षित शासन से
आरम्भ होता है तथा जनमेजय ने इसी का प्रयोग अपने दान-पत्रों में किया है। (घ) कलि के २५ वर्ष बीतने पर कश्मीर में युधिष्ठिर का देहान्त हुआ जब सप्तर्षि
मघा से निकले। उस समय (३०७६ ई.पू. मेष संक्रान्ति) से लौकिक या सप्तर्षि सम्वत्सर आरम्भ हुआ जो कश्मीर में प्रचलित था तथा राजतरङ्गिणी में प्रयुक्त
है।
(९) भटाब्द-आर्यभट काल से के रल में भटाब्द प्रचलित था। महाभारत काल में २ प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित थे। पराशर मथ तथा आर्य मत। यहां पराशर मत
पराशर द्वारा लिखित विष्णुपुराण में है जो मैत्रेय ऋषि ने उनको खण्ड १ तथा २ में कहा है। यह सूर्य सिद्धान्त की परम्परा में है, अतः ऋषि को मैत्रेय (मित्र
=सूर्य, सौर वर्ष का प्रथम मास, उत्तरायण से) कहा गया है। द्वितीय मत आर्य मत है जो स्वायम्भुव मनु की परम्परा से था। इसकी परम्परा में कलि के कु छ
बाद (३६० वर्ष) आर्यभट ने आर्यभटीय लिखा। विवस्वान् या सूर्य पिता हैं, उनके पूर्व के स्वायम्भुव मनु ब्रह्मा या पितामह हैं। आज भी आर्य (अजा)का अर्थ
पटना के निकट तथा ओडिशा आदि में पितामह होता है।
(१०) जैन युधिष्ठिर शक-जिनविजय महाकाव्य का जैन युधिष्ठिर शक ५०४ युधिष्ठिर शक (२६३४ ई.पू.) में आरम्भ होता है। इसके अनुसार कु मारिल भट्ट
का जन्म ५५७ ई.पू. (२०७७) क्रोधी सम्वत्सर (सौर मत) में तथा शंकराचार्य का निर्वाण ४७७ ई.पू. (२१५७) राक्षस सम्वत्सर में कहा है।
यह पार्श्वनाथ का संन्यास या निधन काल है। उनका संन्यास पूर्व नाम युधिष्ठिर रहा होगा या वे वैसे ही धर्मराज या तीर्थङ्कर थे। भगवान् महावीर (जन्म ११-३-
१९०२ ई.पू.) में पार्श्वनाथ का ही शक चल रहा था। युधिष्ठिर की ८ वीं पीढ़ी में निचक्षु के शासन में हस्तिनापुर डू ब गया था- यह सरस्वती नदी के सूखने का
परिणाम था। उस समय १०० वर्ष की अनावृष्टि कही गयी है जब दुर्भिक्ष रोकने के लिये शताक्षी या शाकम्भरी अवतार हुआ। दुर्गा-सप्तशती (११/४६-४९)
(११) शिशुनाग काल-पाल बिगण्डेट की पुस्तक बर्मा की बौद्ध परम्परा में बुद्ध निर्वाण से अजातशत्रु काल में एक नये वर्ष का आरम्भ कहा गया है (बर्मी में
इत्यान = निर्वाण)। इसके १४८ वर्ष पूर्व अन्य वर्ष आरम्भ हुआ था जिसे बर्मी में कौजाद (शिशुनाग?) कहा है। बुद्ध निर्वाण (२७-३-१८०७ ई.पू.) से १४८
वर्ष पूर्व १९५४ ई.पू. में शिशुनाग का शासन समाप्त हुआ।
(१२) नन्द शक-महापद्मनन्द का अभिषेक सभी पुराणों का विख्यात कालमान है। यह परीक्षित जन्म के १५०० (१५०४) वर्ष बाद हुआ था। इसमें १५००
को पार्जिटर ने १०५० कर दिया जिससे कलि आरम्भ को बाद का किया जा सके ।
(१३) शूद्रक शक-यह ७५६ ई.पू. में आरम्भ हुआ। जेम्स टाड ने सभी राजपूत राजाओं को विदेशी शक मूल का सिद्ध करने के लिये उनकी बहुत सी
वंशावलियां तथा ताम्रपत्र आदि नष्ट किये तथा राजस्थान कथा (Annals of Rajsthan) में अग्निवंशी राजाओं का काल थोड़ा बदल कर प्रायः ७२५
ई.पू. कर दिया।
काञ्चुयल्लार्य भट्ट-ज्योतिष दर्पण-पत्रक २२ (अनूप संस्कृ त लाइब्रेरी, अजमेर एम्.एस नं ४६७७)-
बाणाब्धि गुणदस्रोना (२३४५) शूद्रकाब्दा कलेर्गताः॥७१॥ गुणाब्धि व्योम रामोना (३०४३) विक्रमाब्दा कलेर्गताः॥
इस समय असुर (असीरिया के नबोनासर आदि) आक्रमण को रोकने के लिये ४ प्रमुख राजवंशों का संघ आबू पर्वत पर विष्णु अवतार बुद्ध की प्रेरणा से बना।
इन राजाओं को अग्रणी होने के कारण अग्निवंशी कहा गया-परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चाहमान। भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व (१/६/४५-४९) । ४ राजाओं
का संघ होने के कारण यह कृ त संवत् भी कहा जाता है तथा इन्द्राणीगुप्त को सम्मान के लिये शूद्रक कहा गया-शूद्र ४ जातियों का सेवक है।
(१४) चाहमान शक-दिल्ली कॆ चाहमान राजा ने ६१२ ईसा पूर्व में असीरिया की राजधानी निनेवे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसका उल्लेख बाइबिल में
कई स्थानों पर है। इसके नष्टकर्त्ता को सिन्धु पूर्व के मधेस (मध्यदेश, विन्ध्य तथा हिमालय के बीच) का शासक कहा गया है।
http://bible.tmtm.com/wiki/NINEVEH_%28Jewish_Encyclopedia%29-
The Aryan Medes, who had attained to organized power east and northeast of Nineveh, repeatedly
invaded Assyria proper, and in 607 succeeded in destroying the city
Media-From BibleWiki (Redirected from Medes)-They appear to have been a branch of the Aryans,
who came from the east bank of the Indus, …
इस समय जो शक आरम्भ हुआ उसका उल्लेख वराहमिहिर की बृहत् संहिता में है तथा कालिदास, ब्रह्मगुप्त ने भी इसी का पालन किया है। वराहमिहिर-बृहत्
संहिता (१३/३)-
आसन् मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ। षड् -द्विक-पञ्च-द्वि (२५२६) युतः शककालस्तस्य राज्ञस्य॥
(१५) श्रीहर्ष शक (४५६ ईसा पूर्व)-इसका उल्लेख अलबरूनि ने किया है। शूद्रक के बाद ३०० वर्ष तक मालवगण चला-जिसे मेगस्थनीज ने ३०० वर्षों का
गणराज्य कहा है। लिच्छवी तथा गुप्त राजाओं ने इसका प्रयोग किया है पर इसे निरक्षर इतिहासकारों ने हर्षवर्धन (६०५-६४६ इस्वी) से जोड़ दिया है।
(१६) विक्रम संवत्-५७ ईसा पूर्व में उज्जैन के परमार वंशी राजा विक्रमादित्य (८२ ईसा पूर्व-१९ ईस्वी) ने आरम्भ किया। उनका राज्य (परोक्षतः) अरब तक
था तथा जुलिअस सीजर के राज्य में भी उनके संवत् के ही अनुसार सीजर के आदेश के ७ दिन बाद विक्रम वर्ष १० के पौष कृ ष्ण मास के साथ वर्ष का
आरम्भ हुआ।
History of the Calendar, by M.N. Saha and N. C. Lahiri (part C of the Report of The Calendar
Reforms Committee under Prof. M. N. Saha with Sri N.C. Lahiri as secretary in November 1952-
Published by Council of Scientific & Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi-110001, 1955,
Second Edition 1992.
Page, 168-last para-“Caesar wanted to start the new year on the 25th December, the winter solstice
day. But people resisted that choice because a new moon was due on January 1, 45 BC. And some
people considered that the new moon was lucky. Caesar had to go along with them in their desire to
start the new reckoning on a traditional lunar landmark.”
यहां बिना गणना के मान लिया गया है कि वर्ष आरम्भ के दिन शुक्ल पक्ष का आरम्भ था, पर वह विक्रम सम्वत् के पौष मास का आरम्भ था। के वल विक्रम वर्ष में
ही चान्द्र मास का आरम्भ कृ ष्ण पक्ष से होता है. बाकी सभी शुक्ल पक्ष से आरम्भ होते हैं। इसी विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, वराहमिहिर आदि ९ रत्न
विख्यात थे।
(१७) शालिवाहन शक-विक्रमादित्य के देहान्त के बाद ५० वर्ष तक भारत विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा। तब उनके पौत्र शालिवाहन ने उनको पराजित
कर सिन्धु के पश्चिम भगा दिया। उनके काल में प्राकृ त भाषाओं का प्रयोग राजकार्य में आरम्भ हुआ। इनके काल में ईसा मसीह ने कश्मीर में शरण लिया
(हजरत बाल) ।
(१८) कलचुरि या चेदि शक (२४६ इसवी)
(१९) वलभी भंग (३१९ ईस्वी)-गुप्त राजाओं की परवर्त्ती शाखा गुजरात के वलभी में शासन कर रही थी जिसका अन्त इस समय हुआ। निरक्षर इतिहासकार
इसके १ वर्ष बाद गुप्त काल का आरम्भ कहते हैं।
८. भारतीय पञ्चाङ्ग में समन्वय-भारत में दिन के सूक्ष्म निर्धारण के लिये ५ प्रकार से दिन संख्या गिनते हैं-तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अतः
ऐतिहासिक तिथियों में यदि ये सभी ठीक निकलें तब तिथि ठीक होगी।
दिन का आरम्भ कई प्रकार से मानते हैं-(१) ज्योतिषीय गणना के लिये अर्धरात्रि से दिन मानते हैं क्योंकि किसी देशान्तर रेखा के सभी स्थानों पर एक साथ
अर्ध्हरात्रि होगी। सूर्योदय अक्षांश के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा।
(२) लोग सूर्योदय के समय उठते हैं, अतः सूर्योदय से लौकिक दिन आरम्भ होता है।
(३) पितर काम या सूर्य छाया के अनुसार माप के लिये मध्याह्न से दिन का आरम्भ होता है। इस समय छाया का सिरा कु तुप (कु प्पी) आकार में घूमता है
अतः उस मुहूर्त्त को कु तुप कहते हैं। कु तुप आकार की छाया को मीन (२ वृत्तों का कटान) से विभाजित कर उत्तर दिशा निकालते हैं, अतः इसे कु तुप-मीन
(कु तुबमीनार) कहते हैं। ऐसा ही काम चुम्बकीय कम्पास से होतॆ है, अतः उसे कु तुबनुमा कहते हैं।
(४) ग्रह या तारा के वेध (दिशा देखना) के लिये सूर्यास्त से दिन का आरम्भ होता है।
मास का आरम्भ शुक्ल या कृ ष्ण पक्ष से होता है। पर अधिक मास की गणना के लिये अमावास्या के अन्त से गिनते हैं। उस मास में सूर्य संक्रान्ति (राशि
परिवर्तन) नहीं होने पर वह अधिक मास होता है।
वर्ष भी ४ प्रकार से आरम्भ होते हैं-विषुव संक्रान्ति (जब सूर्य विषुव रेखा पर लम्ब हो) चैत्र मास में पड़ती है अतः संक्रान्ति या चैत्र से वर्ष आरम्भ होता है।
उत्तरायण से दिव्य दिन या वर्ष आरम्भ होता है। वर्षा से मूलतः सम्वत् आरम्भ होता था, अतः उसे वर्ष कहा गया। एक वर्षा (मौनसून) का क्षेत्र भी वर्ष है।
दक्षिणायन में जब सूर्य विषुव रेखा पर लम्ब हो तब भी वर्ष आरम्भ होता है। उस समय भाद्र शुक्ल १२ को वामन ने बलि से इन्द्र का राज्य लिया था अतः
राजाओं का काल उसी दिन से गिनते हैं (ओड़िशा की अंक पद्धति)।
भारत में राशियों का स्थान देकने के लिये (आंख या दूरदर्शक से) स्थिर ताराओं के अनुसार है। इसे निरयण कहते हैं। पर ऋतु आदि की गणना के लिये जिस
विन्दु पर सूर्य उत्तर दिशा में विषुव रेखा को पार करता है उसे शून्य विन्दु मानते हैं। दोनों के शून्य विन्दु का अन्तर अयन या अयनांश है। यह विपरीत दिशा में
घूमता है अतः निरयण में अयनांश जोड़ने पर सायन राशि आती है।
You might also like
- Mahan NariDocument30 pagesMahan NariRajesh Kumar Duggal100% (3)
- भारत की काल गणनाDocument17 pagesभारत की काल गणनाSanjeev SaxenaNo ratings yet
- श्रुति स्मृति पुराणDocument16 pagesश्रुति स्मृति पुराणraghavendradas100% (1)
- संपूर्ण पंचांग ज्ञान 1Document327 pagesसंपूर्ण पंचांग ज्ञान 1forslowmovideosNo ratings yet
- यम सूक्तDocument2 pagesयम सूक्तMahavir Mandir PatnaNo ratings yet
- देश और काल (स्वामी माधवतीर्थजी)Document392 pagesदेश और काल (स्वामी माधवतीर्थजी)Skishna1980100% (2)
- तुरंत फल देता है सूर्याष्टक का पाठDocument1 pageतुरंत फल देता है सूर्याष्टक का पाठपं सुशील शर्मा 'सरल'No ratings yet
- षोडश मातृकाDocument4 pagesषोडश मातृकाKamalakarAthalyeNo ratings yet
- श्रवण मनन निदिध्यासनDocument3 pagesश्रवण मनन निदिध्यासनraghavendradasNo ratings yet
- Gurutva Jyotish Jun-2011 (गुरुत्व ज्योतिष)Document72 pagesGurutva Jyotish Jun-2011 (गुरुत्व ज्योतिष)CHINTAN JOSHINo ratings yet
- शिव पुराण PDFDocument845 pagesशिव पुराण PDFniranjanchou100% (1)
- ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सिद्धांतDocument138 pagesब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सिद्धांतRohit Sahu100% (2)
- स्वस्तिवाचनDocument12 pagesस्वस्तिवाचनShobhitNo ratings yet
- महामृत्युंजय मंत्रDocument30 pagesमहामृत्युंजय मंत्रbhadrakaaliNo ratings yet
- Nandi Shraddha VidhiDocument4 pagesNandi Shraddha VidhioompbhNo ratings yet
- TotkenDocument15 pagesTotkenram_krishna70No ratings yet
- Chakra Devi HindiDocument6 pagesChakra Devi HindiShaaradd P.No ratings yet
- तुलसी विवाह पद्धतिDocument28 pagesतुलसी विवाह पद्धतिPavan VoraNo ratings yet
- बालग्रह तथा पूतनाDocument9 pagesबालग्रह तथा पूतनाdindayal maniNo ratings yet
- Adhyatmik Sookt 1Document30 pagesAdhyatmik Sookt 1Rishav DikshitNo ratings yet
- सर्वतोद्रद्र मंडंलDocument9 pagesसर्वतोद्रद्र मंडंलShashanka PandaNo ratings yet
- Sandhya Deep MantraDocument3 pagesSandhya Deep MantraADITYA_PATHAKNo ratings yet
- मांगलिक दोष निवारण का उपाय अध्ययन एवं शोध की गयीं बातेंDocument3 pagesमांगलिक दोष निवारण का उपाय अध्ययन एवं शोध की गयीं बातेंRomani BoraNo ratings yet
- गजेन्द्र मोक्ष स्त्रोतDocument9 pagesगजेन्द्र मोक्ष स्त्रोतMehul Bhatt100% (1)
- श्री शम्भु गीताDocument220 pagesश्री शम्भु गीताAkashNo ratings yet
- पंचमहायज्ञविधिDocument54 pagesपंचमहायज्ञविधिDaleep KumarNo ratings yet
- महामृत्युंजय जपDocument9 pagesमहामृत्युंजय जपManish Kalia100% (1)
- नाड़ी ज्योतिष के रहस्यDocument2 pagesनाड़ी ज्योतिष के रहस्यravi goyalNo ratings yet
- वैधव्य योगDocument1 pageवैधव्य योगJan Jyotish MitraNo ratings yet
- Vivah SanskarDocument95 pagesVivah SanskarDeep Pandya0% (1)
- ॐ नमः शिवायःDocument4 pagesॐ नमः शिवायःjitendraktNo ratings yet
- कुबेर साधना BY महाकाली तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति साधनाDocument7 pagesकुबेर साधना BY महाकाली तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति साधनाPrime PlexNo ratings yet
- श्री शिक्षाष्टकम्Document2 pagesश्री शिक्षाष्टकम्Surya BabaNo ratings yet
- Shakambhari-Kavach-V1-2020-07-31 - To ShareDocument6 pagesShakambhari-Kavach-V1-2020-07-31 - To ShareNK SharmaNo ratings yet
- All SahasranamamDocument1,044 pagesAll SahasranamamDev79 Sreekar NandiNo ratings yet
- वासवदत्ता में आदर्श राजनैतिक व्यवस्थाDocument4 pagesवासवदत्ता में आदर्श राजनैतिक व्यवस्थाvishal sharma100% (1)
- WhatsApp Chat with सूर्य यंत्र ज्योतिषDocument213 pagesWhatsApp Chat with सूर्य यंत्र ज्योतिषhasraj thoratNo ratings yet
- भैरव रक्षा कवचDocument2 pagesभैरव रक्षा कवचअखिलेश कैलखुराNo ratings yet
- अप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्रDocument2 pagesअप्सरा रंभा के विलक्षण मंत्रSushilSharmaNo ratings yet
- Laghu ChandiDocument55 pagesLaghu ChandiMayank Bhardwaj0% (1)
- Vedic Sahitya Aur Sanskriti - Aacharya Baldev Upadhyay - MergedDocument533 pagesVedic Sahitya Aur Sanskriti - Aacharya Baldev Upadhyay - MergedNirmala DhakalNo ratings yet
- All Mantra 3Document12 pagesAll Mantra 3niteshshah007No ratings yet
- 001 - बृहद् पराशर होरा शास्त्र - पूर्वार्धम - अध्याय १ - वर्णनाध्याय - सृष्टी आरम्भ और अवतार अद्ध्यायDocument14 pages001 - बृहद् पराशर होरा शास्त्र - पूर्वार्धम - अध्याय १ - वर्णनाध्याय - सृष्टी आरम्भ और अवतार अद्ध्यायSunilkumar DubeyNo ratings yet
- जय श्रीराम हनुमान कवचDocument13 pagesजय श्रीराम हनुमान कवचSandeepNo ratings yet
- घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षणDocument12 pagesघर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षणshrinath_chauhanNo ratings yet
- सरल गोपूजन विधिDocument12 pagesसरल गोपूजन विधिPriyanshuNo ratings yet
- गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्रDocument8 pagesगजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्रJagdish Prasad JoshiNo ratings yet
- Shubh Ashubh muhurtBAJY-202Document254 pagesShubh Ashubh muhurtBAJY-202Adhyayan GamingNo ratings yet
- कर्ज मुक्ति का अनुभूत मन्त्र प्रयोगDocument11 pagesकर्ज मुक्ति का अनुभूत मन्त्र प्रयोगRaju KumarNo ratings yet
- सिद्ध भैरवी चक्र साधना का मूल स्वरूप और साधना विधान क्या है -Document1 pageसिद्ध भैरवी चक्र साधना का मूल स्वरूप और साधना विधान क्या है -Riddhesh PatelNo ratings yet
- सर्प पूजनDocument20 pagesसर्प पूजनVikas kaushikNo ratings yet
- आसन शुद्धिDocument10 pagesआसन शुद्धिVashishth ArunNo ratings yet
- Gurutva Jyotish Dec-2010Document73 pagesGurutva Jyotish Dec-2010Bhoj KhojNo ratings yet
- Shri Guru GitaDocument47 pagesShri Guru GitaAkashNo ratings yet
- तंत्र साहित्य (भारतीय) - विकिपीडियाDocument17 pagesतंत्र साहित्य (भारतीय) - विकिपीडियाKANHAIYA VERMANo ratings yet
- ओड़िशा परिचयDocument85 pagesओड़िशा परिचयArun UpadhyayNo ratings yet
- ईशावास्योपनिषद्Document42 pagesईशावास्योपनिषद्Arun Upadhyay100% (1)
- श्री सूक्तDocument9 pagesश्री सूक्तArun UpadhyayNo ratings yet
- व्यक्ति और विश्व का सम्बन्धDocument7 pagesव्यक्ति और विश्व का सम्बन्धArun UpadhyayNo ratings yet
- आदि शङ्कराचार्य कालDocument5 pagesआदि शङ्कराचार्य कालArun UpadhyayNo ratings yet