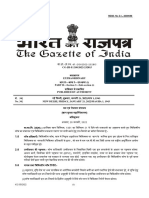Professional Documents
Culture Documents
Disaster Management For UPSC
Disaster Management For UPSC
Uploaded by
shivajiOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Disaster Management For UPSC
Disaster Management For UPSC
Uploaded by
shivajiCopyright:
Available Formats
VISIONIAS
www.visionias.in
Classroom Study Material
आपदा प्रबंधन
JOVIAL BOOK SHOP
9818869135
Copyright © by Vision IAS
2019
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without prior permission of Vision IAS.
विषय सूची
अध्याय-1 ____________________________________________________________________________________ 5
1. आपदा प्रबंधन का पररचय _______________________________________________________________________ 5
1.2. संकट (Hazard) क्या है? ____________________________________________________________________ 5
1.3. सुभेद्यता (Vulnerability) क्या है? _____________________________________________________________ 7
1.4. जोवखम (Risk) क्या है? _____________________________________________________________________ 7
1.5. क्षमता (Capacity) क्या है? __________________________________________________________________ 7
1.6. आपदाओं का िगीकरण (Classification of Disasters) _____________________________________________ 8
1.7. आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle) ______________________________________________ 8
1.7.1. आपदा से पहले (आपदा-पूिव) ______________________________________________________________ 8
1.7.2. आपदा के दौरान (आपदा का घरटत होना) _____________________________________________________ 9
1.7.3. आपदा के बाद (आपदा पश्चात्) ____________________________________________________________ 9
अध्याय-2 ___________________________________________________________________________________ 10
2. भारत में आपदा प्रबंधन ________________________________________________________________________ 10
2.1. पृष्ठभूवम (Background) ___________________________________________________________________ 10
2.2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 ________________________________________________________ 10
2.2.1. राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढााँचा ___________________________________________________________ 11
2.2.2. राज्य स्तर पर संस्थागत ढााँचा ____________________________________________________________ 15
2.2.3. वजला स्तर पर संस्थागत ढााँचा ____________________________________________________________ 15
2.2.4. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 के तहत वित्तीय व्यिस्थाएाँ _________________________________ 16
2.2.5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 की कवमयााँ ____________________________________________ 18
2.3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीवत, 2009 ____________________________________________________________ 19
2.4. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 ___________________________________________________________ 20
2.4.1. योजना के प्रमुख वबन्दु__________________________________________________________________ 20
2.4.2. राष्टरीय आपदा प्रबंधन योजना का महत्ि_____________________________________________________ 21
2.4.3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 की कवमयााँ _______________________________________________ 22
2.5. भारत में आपदा प्रबंधन चक्र _________________________________________________________________ 22
2.5.1. जोवखम न्यूनीकरण एिं प्रत्यास्थता में िृवि करना ______________________________________________ 22
2.5.2.आपदा तैयारी तथा अनुक्रक्रया _____________________________________________________________ 24
2.5.3. आपदा जोवखम शासन _________________________________________________________________ 28
2.5.4. सामान्य वस्थवत की बहाली एिं बेहतर पुनर्ननमावण ______________________________________________ 29
2.5.5. क्षमता विकास _______________________________________________________________________ 33
अध्याय-3 ___________________________________________________________________________________ 35
3. भारत में प्राकृ वतक संकट _______________________________________________________________________ 35
3.1. भारत: सुभेद्यता पररदृश्य ___________________________________________________________________ 35
3.2. प्राकृ वतक आपदाएं ________________________________________________________________________ 36
3.2.1. भूकंप (Earthquake) _________________________________________________________________ 36
3.2.2. सुनामी (Tsunami) __________________________________________________________________ 42
3.2.3. ज्िालामुखी (Volcano) ________________________________________________________________ 48
3.2.4. बाढ़ (Flood) _______________________________________________________________________ 49
3.2.5. शहरी बाढ़ (Urban Floods) ____________________________________________________________ 54
3.2.6. भूस्खलन ___________________________________________________________________________ 57
3.2.7. बादल फटना (Cloudburst)_____________________________________________________________ 60
3.2.8. चक्रिात (Cyclone) __________________________________________________________________ 62
3.2.9. सूखा (Drought) _____________________________________________________________________ 67
3.2.10. हीट िेि (Heat Wave)_______________________________________________________________ 76
3.2.11. शीत लहर (Cold Waves) ____________________________________________________________ 80
3.2.12. िनावि (Wild Fires) ________________________________________________________________ 83
3.3. मानि-जन्य आपदाएं (Man Made Disasters) __________________________________________________ 87
3.3.1. जैविक आपदा (Biological Disaster) _____________________________________________________ 87
3.3.2. औद्योवगक आपदाएाँ (Industrial Disasters) _________________________________________________ 91
3.3.3. नावभकीय संकट (Nuclear Hazards) _____________________________________________________ 95
3.3.4. भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) _____________________________________________________ 98
अध्याय-4 __________________________________________________________________________________ 103
4. अंतरावष्ट्रीय सहयोग तथा ितवमान घटनाक्रम _________________________________________________________ 103
4.1. आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु िैविक फ्रेमिकव ____________________________________________________ 103
4.1.1. ह्योगो फ्रेमिकव फॉर एक्शन 2005-2015: राष्ट्रों तथा समुदायों की प्रत्यास्थता का वनमावण __________________ 103
4.1.2. आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव ________________________________________________ 104
4.2. अंतरावष्ट्रीय एजेंवसयों के साथ साझेदाररयां _______________________________________________________ 106
4.2.1. संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण कायावलय _______________________________________________ 106
4.2.2. मानिीय मामलों के समन्िय हेतु संयुक्त राष्ट्र कायावलय __________________________________________ 107
4.2.3. आपदा न्यूनीकरण तथा सामान्य वस्थवत की बहाली हेतु िैविक सुविधा _______________________________ 107
4.2.4. साकव आपदा प्रबंधन कें द्र _______________________________________________________________ 107
4.2.5. दवक्षण एवशया आपदा संबंधी ज्ञान नेटिकव ___________________________________________________ 108
4.2.6. एवशयाई आपदा न्यूनीकरण कें द्र __________________________________________________________ 108
4.2.7. एवशयाई आपदा तैयारी कें द्र _____________________________________________________________ 108
4.2.8. आवसयान क्षेत्रीय मंच _________________________________________________________________ 108
4.3. भारत की नेतृत्िकारी पहलें _________________________________________________________________ 109
4.3.1. आपदा प्रत्यास्थ अिसंरचना पर प्रथम अंतरावष्ट्रीय कायवशाला, 2018 _________________________________ 109
4.3.2. वबम्सटेक राष्ट्रों के वलए प्रथम संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास, 2017 _________________________________ 109
4.3.3. आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर एवशयाई मंवत्रस्तरीय सम्मेलन, 2016 ________________________________ 109
4.3.4. UNISDR के साथ सहयोग (2016) ______________________________________________________ 110
4.3.5. आपदा प्रबंधन पर विक्स मंवत्रयों की बैठक, 2016 _____________________________________________ 110
4.3.6. साकव देशों के साथ प्रथम आपदा प्रबंधन अभ्यास, 2015 _________________________________________ 110
4.3.7. भारत-प्रशांत द्वीप समूह सतत विकास सम्मेलन _______________________________________________ 111
4.3.8. अन्य सुवनयोवजत पहलें ________________________________________________________________ 111
4.4. विवभन्न राष्ट्रों के साथ वद्वपक्षीय समझौते ________________________________________________________ 111
4.4.1. जापान ___________________________________________________________________________ 111
4.4.2. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) देश _______________________________________________________ 112
4.4.3. जमवनी____________________________________________________________________________ 112
4.4.4. इं डोनेवशया ________________________________________________________________________ 112
4.4.5. साकव देश (SAARC Countries) ________________________________________________________ 112
4.4.6. रूस _____________________________________________________________________________ 112
4.4.7. वस्िट्ज़रलैंड _______________________________________________________________________ 113
अध्याय 5 __________________________________________________________________________________ 114
5. विविध विषय _____________________________________________________________________________ 114
5.1. आपदा बीमा ___________________________________________________________________________ 114
5.2. समुदाय-आधाररत आपदा प्रबंधन _____________________________________________________________ 114
5.3. आपदा प्रबन्धन में मीवडया की भूवमका _________________________________________________________ 115
5.3.1. मीवडया के नकारात्मक प्रभाि ___________________________________________________________ 116
5.4. आपदा प्रबन्धन में सोशल मीवडया की भूवमका ____________________________________________________ 116
5.5. भिनों की रे रोक्रफटटग – समाधान इसके लचीलेपन में है ______________________________________________ 117
5.6. जलिायु पररितवन और आपदाएं ______________________________________________________________ 118
5.7. वनधवनता और आपदाएं ____________________________________________________________________ 118
5.8. विविध NDMA क्रदशा-वनदेश _______________________________________________________________ 119
5.8.1. संग्रहालय _________________________________________________________________________ 119
5.8.2. सांस्कृ वतक धरोहर स्थल और पररसर ______________________________________________________ 119
5.8.3 आपदाओं में मनो-सामावजक सहायता और मानवसक स्िास््य सेिाएं _________________________________ 120
5.9 पशुओं के वलए राष्ट्रीय आपदा योजना ___________________________________________________________ 121
अध्याय-1
1. आपदा प्रबं ध न का पररचय
(Introduction to Disaster Management)
आपदाएं (प्राकृ वतक या मानि-जन्य) विि भर में सामान्य हैं। ऐसा माना जाता है क्रक हाल के क्रदनों में
आपदाओं के पररमाण, जरटलता, बारं बारता और आर्नथक प्रभाि में िृवि हुई है। भारत, विि में
प्राकृ वतक संकटों के जोवखम के प्रवत सुभेद्यता के मामले में शीषव स्थान पर है।
1.1. आपदा (Disaster) क्या है?
आपदा शब्द की उत्पवत्त फ्रेंच शब्द “डेसास्त्रे” से हुई है। यह दो शब्दों ‘डेस’ (वजसका अथव है ‘खराब’) और
‘एस्टर’ (वजसका अथव है ‘वसतारा’) से वमलकर बना है। इस प्रकार यह शब्द ‘खराब या अमंगल वसतारे ’
को संदर्नभत करता है। क्रकसी आपदा को वनम्नवलवखत रूप में पररभावषत क्रकया जा सकता हैैः
“क्रकसी समुदाय या समाज के सुचारु रूप से कायव करने में एक ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौवतक,
आर्नथक, सामावजक या पयाविरणीय क्षवत उत्पन्न करती है और वजसके प्रभािों से वनपटना समाज द्वारा
अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए संभि नहीं होता है।”
आपदा क्षवत, आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत पश्चात् घरटत होती है। इसे सामान्यतैः भौवतक
इकाइयों (उदाहरण के वलए, आिास के वलए िगव मीटर, सड़कों के वलए क्रकलोमीटर आक्रद) में
मापा जाता है। यह प्रभावित क्षेत्र में भौवतक पररसंपवत्तयों के सम्पूणव या आंवशक विनाश,
आधारभूत सेिाओं में व्यिधान तथा आजीविका के स्रोतों में हुई हावनयों को वनरूवपत करती है।
आपदा प्रभाि, क्रकसी संकटपूणव घटना या आपदा के नकारात्मक प्रभािों (जैसे आर्नथक हावनयों)
और सकारात्मक प्रभािों (जैस,े आर्नथक लाभों) सवहत सम्पूणव प्रभाि को दशावता है। आपदा प्रभाि
में आर्नथक, मानिीय ि पयाविरणीय प्रभाि सवम्मवलत होते हैं तथा इसमें मृत्यु, चोटें, बीमाररयां
और मानि के शारीररक, मानवसक ि सामावजक स्िास््य पर पड़ने िाले अन्य नकारात्मक प्रभाि
सवम्मवलत हो सकते हैं।
आपदा, संकट, सुभद्य
े ता ि जोविम की संभावित पररवस्थवतयों को कम करने की अपयावप्त क क्षमता के
संयोजन का पररणाम होती है।
1.2. सं क ट (Hazard) क्या है ?
‘है़डव’ शब्द की उत्पवत्त प्राचीन फ्रेंच शब्द “हैसाडव” और अरबी के ‘अ़-़हर’ से हुई है, वजसका
अथव है ‘संयोग’ या ‘भाग्य’। संकट को “एक ऐसी खतरनाक वस्थवत या घटना के रूप में पररभावषत
क्रकया जा सकता है वजसमें जीिन को नुकसान पहुाँचाने अथिा संपवत्त या पयाविरण को क्षवत
पहुंचाने की क्षमता हो।”
कोई भी संकट, जैस-े बाढ़, भूकंप या चक्रिात, अपेक्षाकृ त अवधक सुभेद्यता (संसाधनों तक अपयावप्त क
पहुाँच, बीमार तथा िृि लोगों की उपवस्थवत, जागरूकता का अभाि आक्रद) िाले कारकों के साथ
वमलकर आपदा का कारण बन सकता है। आपदा से जान ि माल की अपेक्षाकृ त अवधक क्षवत होती
है। उदाहरण के वलए; एक वनजवन रे वगस्तान में आए भूकंप को एक आपदा नहीं माना जा सकता है,
चाहे िह क्रकतना भी शवक्तशाली और तीव्र क्यों न रहा हो। भूकंप के िल तब ही विनाशकारी होता
5 www.visionias.in ©Vision IAS
है जब यह लोगों, उनकी संपवत्तयों और गवतविवधयों को क्षवत पहुाँचाए। इस प्रकार, आपदा के िल
तब घरटत होती है जब संकट और सुभेद्यता का संयोजन होता है। साथ ही, व्यवक्त/समुदाय और
पयाविरण की इन आपदाओं का सामना करने की बेहतर क्षमता से संकट का प्रभाि कम हो जाता
है।
प्राकृ वतक संकट और आपदा के बीच अंतर
संकट (Hazard) आपदा (Disaster)
संकट (Hazard) एक संभावित आपदा आपदा एक घटना है। यह एक गंभीर दुघवटना,
है। संकट एक खतरनाक भौवतक वस्थवत त्रासदी या क्रकसी संकट का पररणाम है। जो
या घटना है। प्राकृ वतक संकट मानि जीिन और अथवव्यिस्था
को भारी क्षवत पहुंचाते हैं, उन्हें आपदाएं या
प्रलयकारी घटनाएाँ कहा जाता है। एक आपदा,
समाज की सामान्य कायवप्रणाली को बावधत कर
देती है।
जब तक भूकंप, बाढ़, ज्िालामुखी यह जान-माल को भारी क्षवत पहुंचाती है और
साथ ही साथ रोजगार के अिसरों को भी बावधत
विस्फोट, भूस्खलन, सूखा आक्रद के द्वारा
करती है।
जान-माल को भारी क्षवत नहीं पहुंचती
तब तक इन्हें प्राकृ वतक संकट कहा जाता
है।
इससे कम संख्या में लोग प्रभावित होते इससे अवधक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं।
हैं।
6 www.visionias.in ©Vision IAS
इससे चोट, जान-माल की क्षवत हो यह जान-माल की व्यापक क्षवत का कारण बनती
सकती है। है।
भूकंप, बाढ़, ज्िालामुखी, सुनामी, यह समाज को उस सीमा तक प्रभावित करती है
क्रक बाह्य सहायता ही हावनयों की भरपाई कर
भूस्खलन, सूखा आक्रद प्राकृ वतक संकट हैं।
पाती है।
1.3. सु भे द्य ता (Vulnerability) क्या है ?
सुभेद्यता को “भौवतक, सामावजक, आर्नथक और पयाविरणीय कारकों या प्रक्रक्रयाओं द्वारा वनधावररत ऐसी
पररवस्थवतयों के रूप में पररभावषत क्रकया जा सकता है, जो संकट के पररणामस्िरूप उत्पन्न प्रभािों के
प्रवत क्रकसी समुदाय की सुग्राह्यता में िृवि करती हैं।”
सुभेद्यता विवभन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे क्रक:
आर्नथक सुभद्य
े ता: वनधवन पररिारों को अनवधकृ त बवस्तयों में रहना पड़ सकता है क्योंक्रक िे
सुरवक्षत (अवधक महंगे) क्षेत्रों में रहना िहन नहीं कर सकते हैं।
भौवतक सुभद्य
े ता: लकड़ी के घर वजनकी एक भूकंप में ढहने की संभािना कम होती है, परन्तु ये
आग के प्रवत अवधक सुभेद्य होते हैं।
सामावजक सुभद्य
े ता: बाढ़ आने पर कु छ नागररक, जैसे क्रक बच्चे, बुजुगव और वनैःशक्तजन, स्ियं की
रक्षा करने में या आिश्यकता पड़ने पर आपदा प्रभावित स्थल से बाहर वनकलने में असमथव हो
सकते हैं।
1.4. जोवखम (Risk) क्या है ?
जोवखम “क्रकसी विवशष्ट समयािवध में क्रकसी वनर्ददष्ट क्षेत्र में संकट की घटना के कारण होने िाली
अनुमावनत हावन की माप है। जोवखम, क्रकसी विवशष्ट संकटपूणव घटना की तथा उससे होने िाली
हावनयों की संभािना का एक फलन (function) है।”
जोविम = संकट x सुभद्य
े ता
जोवखम का स्तर िस्तुतैः संकट की प्रकृ वत, प्रभावित हुए तत्िों की सुभेद्यता और उन तत्िों के
आर्नथक मूल्य पर वनभवर करता है।
1.5. क्षमता (Capacity) क्या है ?
आपदा जोवखम को प्रबंवधत एिं न्यूनीकृ त करने तथा प्रत्यास्थता को प्रबल बनाने के वलए क्रकसी
संगठन, समुदाय या समाज के भीतर उपलब्ध सभी साम्यों, विशेषताओं और संसाधनों के समुच्चय को
क्षमता कहते हैं। क्षमता में अिसंरचना, संस्थान, मानि ज्ञान ि कौशल, तथा सामूवहक विशेषताएं जैसे
क्रक सामावजक संबंध, नेतृत्ि और प्रबंधन आक्रद सवम्मवलत हो सकते हैं।
सामना करने की क्षमता (Coping capacity): यह उपलब्ध कौशलों ि संसाधनों का उपयोग
करते हुए प्रवतकू ल पररवस्थवतयों, जोवखमों या आपदाओं को प्रबंवधत करने की लोगों, संगठनों और
प्रणावलयों की क्षमता है। इस क्षमता के वलए सामान्य समय के साथ-साथ आपदाओं या प्रवतकू ल
पररवस्थवतयों में भी सतत जागरूकता, संसाधनों ि कु शल प्रबंधन की आिश्यकता होती है। आपदा
का सामना करने की ये क्षमताएं, आपदा जोवखमों के न्यूनीकरण में सहायक होती हैं।
7 www.visionias.in ©Vision IAS
1.6. आपदाओं का िगीकरण (Classification of Disasters)
आपदाओं को दो मुख्य श्रेवणयों नामतैः प्राकृ वतक और मानि-जन्य में विभावजत क्रकया जा सकता है।
प्राकृ वतक आपदाएं िे आपदाएं हैं जो प्राकृ वतक (मौसम संबंधी, भूगभीय या जैविक मूल की)
पररघटनाओं के कारण घरटत होती हैं। चक्रिात, सुनामी, भूकंप और ज्िालामुखी विस्फोट उन
प्राकृ वतक आपदाओं के उदाहरण हैं जो पूणत
व ैः प्राकृ वतक मूल की हैं। भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग
आक्रद सामावजक-प्राकृ वतक आपदाएं हैं क्योंक्रक ये प्राकृ वतक और मानि-जन्य दोनों ही कारणों से
घरटत होती हैं। उदाहरण के तौर पर, बाढ़ की वस्थवत अत्यवधक िषाव, भूस्खलन या मानि अपवशष्ट
के कारण जल वनकासी में व्यिधान के कारण उत्पन्न हो सकती है।
मानि-जन्य आपदाएं िे आपदाएं हैं जो मानिीय उपेक्षाओं या असािधानी के कारण घरटत होती
हैं। ये उद्योगों या ऊजाव उत्पादन इकाइयों से संबि होती हैं और इनमें विस्फोट, विषाक्त अपवशष्टों
का ररसाि, प्रदूषण, बांध का टू टना, युि या नागररक संघषव आक्रद सवम्मवलत हैं। इनमें से कई
आपदाएं प्रायैः घरटत होती रहती हैं जबक्रक कु छ कभी-कभी घरटत होती हैं।
1.7. आपदा प्रबं ध न चक्र (Disaster Management Cycle)
आपदा जोवखम प्रबंधन में िे सभी गवतविवधयां, कायवक्रम और उपाय सवम्मवलत हैं जो एक आपदा से
पहले, उसके दौरान और उसके पश्चात् अपनाए जा सकते हैं।
आपदा प्रबंधन की एक आदशव सतत प्रक्रक्रया में सवम्मवलत चरण हैं:
आपदा पूिव जोवखम प्रबंधन चरण, वजसमें रोकथाम, शमन और तैयारी सवम्मवलत हैं।
आपदा पश्चात् संकटकालीन प्रबंधन चरण, वजसमें राहत, अनुक्रक्रया, पुनिावस, पुनर्ननमावण और
सामान्य वस्थवत की बहाली सवम्मवलत हैं।
आपदा जोवखम प्रबंधन गवतविवधयों के अंतगवत तीन प्रमुख चरण हैं:
1.7.1. आपदा से पहले (आपदा-पू िव )
इसमें संभावित संकट के कारण होने िाली जान ि माल की क्षवतयों को कम करने के वलए की जाने
िाली गवतविवधयााँ सवम्मवलत हैं। उदाहरण के वलए- जागरूकता अवभयान चलाना, ितवमान
कमजोर ढांचों को मजबूत बनाना, घरे लू ि सामुदावयक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएाँ तैयार
करना आक्रद। इस चरण के तहत उठाये गये जोवखम न्यूनीकरण उपायों को शमन तथा तैयारी
गवतविवधयां कहा जाता है।
8 www.visionias.in ©Vision IAS
1.7.2. आपदा के दौरान (आपदा का घरटत होना)
इसमें पीवड़तों की आिश्यकताओं की पूर्नत एिं रसद सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी तथा उनके
कष्टों को कम करने संबंधी पहलों को सवम्मवलत क्रकया जाता है। इस चरण के तहत सवम्मवलत
गवतविवधयों को आपातकालीन अनुक्रक्रया गवतविवधयां कहा जाता है।
1.7.3. आपदा के बाद (आपदा पश्चात् )
इसमें क्रकसी आपदा के घरटत होने के तुरंत पश्चात, प्रभावित समुदायों की शीघ्र पुनबवहाली तथा
पुनिावस के उद्देश्य से आपदा की अनुक्रक्रया में की गई पहलें सवम्मवलत होती हैं। इन्हें अनुक्रक्रया ि
पुनबवहाली गवतविवधयां कहा जाता है।
9 www.visionias.in ©Vision IAS
अध्याय-2
2. भारत में आपदा प्रबं ध न
(Disaster Management in India)
2.1. पृ ष्ठ भू वम (Background)
भारत में आपदा प्रबंधन एक गवतविवध-आधाररत प्रवतक्रक्रयाशील व्यिस्था से एक अग्रसक्रक्रय
संस्थागत संरचना तथा एक राहत-आधाररत दृवष्टकोण से एक ‘जोवखम न्यूनीकरण हेतु बहु-
आयामी अग्रसक्रक्रय दृवष्टकोण’ के रूप में विकवसत हुआ है।
स्ितंत्रता से पूिव के दौर में यह नीवत राहत-उन्मुख थी तथा आपदाओं के दौरान उत्पन्न आपात
वस्थवतयों के वलए राहत विभाग स्थावपत क्रकए गए थे। इनकी गवतविवधयों में राहत कोड तैयार
करना तथा काम के बदले अनाज कायवक्रम आरम्भ करना सवम्मवलत थे। स्ितंत्रता के पश्चात,
आपदाओं के प्रबंधन का उत्तरदावयत्ि के न्द्रीय राहत आयुक्त के अधीन कायवरत प्रत्येक राज्य के
राहत आयुक्तों में वनवहत कर क्रदया गया। इन राहत आयुक्तों की भूवमका प्रभावित क्षेत्रों में राहत
सामग्री एिं मुआिजे के प्रत्यायोजन तक सीवमत रही।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को ‘अंतरावष्ट्रीय प्राकृ वतक आपदा न्यूनीकरण दशक‘
(International Decade for Natural Disaster Reduction: IDNDR) के रूप में घोवषत
क्रकया गया। इस घोषणा के पश्चात् 1990 के दशक में कृ वष मंत्रालय के तहत एक आपदा प्रबंधन
इकाई की स्थापना के साथ एक स्थायी एिं संस्थागत व्यिस्था आरम्भ की गई। लातूर भूकंप
(1993), माल्पा भूस्खलन (1994), उड़ीसा के चक्रिात (1999) एिं भुज के भूकंप (2001) जैसी
कई आपदाओं के बाद कृ वष मंत्रालय के सवचि श्री जे. सी. पंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय
सवमवत गरठत की गई। इसके पररणामस्िरूप, आपदा प्रबंधन प्रभाग को 2002 में गृह मंत्रालय के
अधीन स्थानांतररत कर क्रदया गया तथा भारत में आपदा प्रबंधन हेतु एक पदानुक्रवमत संरचना
विकवसत की गई।
10िीं पंचिषीय योजना दस्तािेज में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय जारी
क्रकया गया। बाद में 12िें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन के वलए वित्तीय व्यिस्था की समीक्षा
करने के वलए भी अवधदेवशत क्रकया गया।
आपदा प्रबंधन दृवष्टकोण में आमूल पररितवन (Paradigm Shift in Disaster
Management)- भारत सरकार द्वारा 23 क्रदसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005
अवधवनयवमत क्रकया गया। आपदा प्रबंधन के प्रवत एक समग्र एिं एकीकृ त दृवष्टकोण के पालन हेतु
इस अवधवनयम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन
प्रावधकरण (SDMA) एिं वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (DDMA) की स्थापना की
पररकल्पना की गई। इस अवधवनयम के पररणामस्िरूप आमूल पररितवन दजव क्रकया गया तथा इस
पररितवन के तहत पूिव की राहत-कें क्रद्रत अनुक्रक्रया के स्थान पर जीिन, आजीविका एिं संपवत्त की
हावन कम करने हेतु एक अग्रसक्रक्रय वनिारण, शमन एिं तैयारी-आधाररत दृवष्टकोण को अंगीकृ त
क्रकया गया।
2.2. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न अवधवनयम, 2005
(National Disaster Management Act, 2005)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 राष्ट्र, राज्य, वजला एिं स्थानीय स्तरों पर संस्थागत,
कानूनी, वित्तीय एिं समन्िय तंत्र स्थावपत करता है। यह अवधवनयम राष्ट्रीय स्तर पर NDMA,
राज्य स्तर पर SDMA एिं वजला स्तर पर DDMA की स्थापना का प्रािधान करता है।
10 www.visionias.in ©Vision IAS
आपदा प्रबंधन हेतु प्राथवमक उत्तरदावयत्ि संबंवधत राज्य सरकार का होता है। कें द्र, राज्य एिं
वजला स्तर पर स्थावपत संस्थागत तंत्र, राज्यों को प्रभािी रूप से आपदाओं का प्रबंधन करने में
सक्षम बनाते हैं।
2.2.1. राष्ट्रीय स्तर पर सं स्थागत ढााँ चा
(Institutional Framework at National Level)
आपदा प्रबंधन प्रभाग (Disaster Management Division), गृह मंत्रालयैः आपदा प्रबंधन का
समग्र समन्िय गृह मंत्रालय (MHA) का दावयत्ि है। प्राकृ वतक आपदाओं एिं मानि-जवनत
आपदाओं (सूखे ि महामारी के अवतररक्त) हेतु अनुक्रक्रया, राहत ि तैयारी का उत्तरदावयत्ि आपदा
प्रबंधन प्रभाग का है। प्रभािी आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन
प्रभाग, कें द्र सरकार की ओर से आपदा प्रभावित राज्य सरकारों, संबि मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (National Disaster Management Authority: NDMA),
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force: NDRF), राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management: NIDM) एिं अविशमन
सेिा वनदेशालय, होम गार्डसव ि नागररक सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों के साथ समन्िय करता है।
राष्ट्रीय कायवकारी सवमवत (National Executive Committee: NEC): यह आपदा प्रबंधन के
वलए समन्ियकारी ि वनगरानी वनकाय के रूप में कायव करता है। इसकी अध्यक्षता कें द्रीय गृह
सवचि द्वारा की जाती है तथा कृ वष, परमाणु ऊजाव, रक्षा, पेयजल आपूर्नत, पयाविरण ि िन, वित्त
(व्यय), स्िास््य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान ि प्रौद्योवगकी, अंतररक्ष, दूरसंचार, शहरी
विकास ि जल संसाधनों पर वनयंत्रण िाले मंत्रालयों एिं विभागों के सवचि स्तर के अवधकारी
इसके सदस्य होते हैं। चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी का एकीकृ त रक्षा स्टाफ प्रमुख (Chief of
Integrated Defence Staff) इसका पदेन सदस्य होता है। क्रकसी भी भीषण आपदा की वस्थवत
या आपदा की ऐसी वस्थवत में जहां कें द्रीय सहायता की आिश्यकता हो, आपदा प्रबंधन अनुक्रक्रया
का समन्िय NEC करती है। NEC, कें द्र सरकार के संबंवधत मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों
एिं राज्य अवधकाररयों को क्रकसी विवशष्ट भीषण आपदा की संभावित वस्थवत या आपदा के
दौरान, राज्य की आिश्यकताओं के अनुसार, उनके द्वारा क्रकए जाने िाले उपायों के बारे में वनदेश
दे सकती है।
11 www.visionias.in ©Vision IAS
प्रश्नैः 50 से कम शब्दों में वनम्नवलवखत पर रटप्पणी करें :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण की राष्ट्रीय कायवकारी सवमवत की संरचना और कायव (UPSC, 2011)
सुरक्षा मामलों पर मंवत्रमंडलीय सवमवत (Cabinet Committee on Security: CCS) और
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन सवमवत (National Crisis Management Committee: NCMC): ये
आपदा प्रबंधन से सम्बंवधत उच्चस्तरीय वनणवयन प्रक्रक्रया में सवम्मवलत होने िाली महत्िपूणव
सवमवतयों में शावमल हैं। प्राकृ वतक आपदाओं के प्रबंधन हेतु गरठत मंवत्रमंडलीय सवमवत 2014 में
समाप्त क कर दी गई थी।
o सुरक्षा मामलों पर मंवत्रमंडलीय सवमवत (CCS) : CCS देश की सुरक्षा, कानून एिं
व्यिस्था, आंतररक सुरक्षा, विदेशी मामलों से संबंवधत आंतररक या बाह्य सुरक्षा वनवहताथव
िाले नीवतगत मामलों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने िाले आर्नथक एिं राजनीवतक
मामलों से संबवं धत मुद्दों से सरोकार रखती है। CCS को गंभीर सुरक्षा वनवहताथों िाली
आपदा से संबंवधत वनणवयन प्रक्रक्रया में सवम्मवलत क्रकया जाता है।
o राष्ट्रीय संकट प्रबंधन सवमवत (National Crisis Management Committee: NCMC):
NCMC गंभीर या राष्ट्रीय जरटलताओं िाले बड़े संकटों से संबंवधत मामलों पर कायविाही
करती है। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों और/या खुक्रफया एजेंवसयों की अत्यवधक भागीदारी की
आिश्यकता होती है। ऐसी घटनाओं में आतंकिाद (जिाबी कायविाही), कानून और व्यिस्था
से संबंवधत मामले, शृंखलाबि बम विस्फोट, हाईजैककग, हिाई दुघवटना, CBRN हवथयार
व्यिस्था, खान दुघवटनाएं, बंदरगाह ि पत्तन संबंधी आपात वस्थवत, िनावि, तेल-क्षेत्र में आग
और तेल ररसाि (oil spills) सवम्मवलत हैं।
राष्ट्रीय आपदा जोवखम न्यूनीकरण मंच (National Platform for Disaster Risk
Reduction: NPDRR) : भारत सरकार ने कें द्र एिं राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र
में विवभन्न वहतों का प्रवतवनवधत्ि करने िाले लोगों सवहत अन्य वहतधारकों की सक्रक्रय भागीदारी
के साथ वनणवयन की एक सहभागी प्रक्रक्रया विकवसत करने की आिश्यकता को स्िीकार क्रकया।
तदनुसार, एक बहु-वहतधारक एिं बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय आपदा जोवखम न्यूनीकरण मंच (NPDRR)
का गठन क्रकया गया। NPDRR की अध्यक्षता के न्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय के
तहत आपदा प्रबंधन का प्रभारी राज्य मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। गृह मंत्रालय में आपदा
प्रबंधन प्रभाग का प्रभारी विशेष सवचि/अवतररक्त सवचि आपदा जोवखम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच
(NPDRR) का संयोजक होता है।
यह वनम्नवलवखत कायव करता है:
o आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुई प्रगवत की सामवयक समीक्षा करना।
o कें द्र एिं राज्य सरकारों ि अन्य संबंवधत एजेंवसयों द्वारा आपदा प्रबंधन नीवत को कायाववन्ित
करने के वलए अपनाए जाने िाले तरीकों का आकलन तथा इस मामले में उवचत परामशव
प्रदान करना।
o आपदा जोवखम न्यूनीकरण प्रणाली के विकास के वलए कें द्र एिं राज्य सरकारों/ संघ शावसत
प्रदेशों, स्थानीय सरकारों तथा वसविल सोसाइटी संगठनों के मध्य समन्िय के संबंध में
परामशव प्रदान करना।
o कें द्र सरकार या क्रकसी राज्य सरकार/ संघ शावसत प्रदेश द्वारा उठाए गए, या स्ियं ही, आपदा
प्रबंधन से संबंवधत क्रकसी भी प्रश्न पर परामशव प्रदान करना।
o आपदा प्रबंधन नीवत की समीक्षा करना।
12 www.visionias.in ©Vision IAS
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (National Disaster Management Authority:
NDMA): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA), भारत में आपदा प्रबंधन के वलए सिोच्च
वनकाय है। NDMA आपदा प्रबंधन संबंधी नीवतयााँ, योजनाएाँ एिं क्रदशावनदेश तैयार करने हेतु
उत्तरदायी है। NDMA के क्रदशावनदेश कें द्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों की उनकी संबंवधत
आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में सहायता करते हैं। NDMA सभी प्रकार की आपदाओं
(प्राकृ वतक या मानि-जवनत) से संबंवधत मामलों में कायविाही करने हेतु अवधदेवशत है:
o यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं एिं के न्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की योजनाओं को मंजर
ू ी
प्रदान करता है।
o राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के सामान्य अधीक्षण, वनदेशन एिं वनयंत्रण का
उत्तरदावयत्ि NDMA में वनवहत हैं तथा ये कायव NDMA द्वारा संपन्न क्रकए जाते
हैं।
o राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management:
NIDM) NDMA द्वारा वनधावररत व्यापक नीवतयों एिं क्रदशा-वनदेशों के फ्रेमिकव के तहत कायव
करता है।
o क्रकसी भीषण आपदा की आशंका की वस्थवत में या आपदा के दौरान बचाि ि राहत कायों के
वलए आिश्यक सामग्री की आपातकालीन िरीद हेतु NDMA को विवभन्न विभागों या
प्रावधकाररयों को अवधकृ त करने की शवक्त है।
o NDMA, क्रकसी भीषण आपदा की आशंका की वस्थवत या आपदा से वनपटने हेतु, आपदाओं
की रोकथाम या शमन के वलए, या तैयारी ि क्षमता वनमावण हेतु, आिश्यकतानुसार अन्य
उपायों को भी अपना सकता है।
o यह शमन एिं तैयारी सम्बन्धी उपायों हेतु वित्तीय प्रािधान तथा अनुप्रयोग का वनरीक्षण
करता है।
ऐसी घटनाएं वजनमें सुरक्षा बलों और/या खुक्रफया एजेंवसयों की अत्यवधक भागीदारी की
आिश्यकता होती है, जैसे आतंकिाद (जिाबी कायविाही), कानून और व्यिस्था से संबंवधत
मामले, शृंखलाबि बम विस्फोट, हाईजैककग, हिाई दुघवटना, CBRN (रासायवनक, जैविक,
रे वडयोलॉवजकल और नावभकीय) िेपन वसस्टम; तथा खान दुघटव नाओं, बंदरगाह ि पत्तन
संबंधी आपात वस्थवत, िनावि, तेल-क्षेत्र की आग (oilfield fires) एिं तेल ररसाि (oil
spills) जैसी अन्य घटनाएं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन सवमवत द्वारा वनयंवत्रत की जाती हैं।
13 www.visionias.in ©Vision IAS
NDMA की परामशवदात्री सवमवत: NDMA के तहत 15-सदस्यीय परामशवदात्री सवमवत में आपदा
प्रबंधन के विवभन्न क्षेत्रों तथा संबि विषयों के विशेषज्ञ, शैक्षवणक समुदाय, सरकारी, गैर-सरकारी
संगठनों (NGOs) तथा वसविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रवतवनवध सवम्मवलत होते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management: NIDM):
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानि संसाधन विकास, क्षमता वनमावण,
प्रवशक्षण, अनुसंधान, दस्तािे़ीकरण और नीवतयों के समथवन हेतु उत्तरदायी एक नोडल एजेंसी
है।
o NIDM ने कें द्रीय, राज्य ि स्थानीय सरकारों के विवभन्न मंत्रालयों एिं विभागों के साथ; भारत
एिं विदेश में शैक्षवणक, अनुसध
ं ान और तकनीकी संगठनों के साथ; तथा अन्य वद्वपक्षीय एिं
बहुपक्षीय अंतरावष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सामररक समझौते क्रकए हैं।
o यह राज्यों एिं संघ शावसत प्रदेशों के प्रशासवनक प्रवशक्षण संस्थानों (ATIs) में आपदा प्रबंधन
कें द्रों (DMCs) के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
o ितवमान में यह लगभग 30 ऐसे कें द्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। इनमें से 6 कें द्रों को जोवखम
प्रबंधन के विवशष्ट क्षेत्रों, जैस-े बाढ़, भूकंप, चक्रिात, सूखा, भूस्खलन और औद्योवगक आपदाओं
आक्रद के सन्दभव में उत्कृ ष्टता के न्द्रों (Centres of Excellence) के रूप में विकवसत क्रकया जा
रहा है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force:NDRF): NDRF एक
विशेषज्ञ अनुक्रक्रया बल है वजसे क्रकसी भीषण आपदा की आशंका की वस्थवत में या आपदा के दौरान
तैनात क्रकया जा सकता है। इस बल के सामान्य अधीक्षण, वनदेशन एिं वनयंत्रण का उत्तरदावयत्ि
NDMA में वनवहत है। NDRF के महावनदेशक को इस बल की कमान एिं अधीक्षण का अवधकार
प्राप्त क है। ितवमान में, NDRF में 12 बटावलयन सवम्मवलत हैं- BSF और CRPF से प्रत्येक में से
तीन तथा CISF, ITBP एिं SSB से प्रत्येक में से दो। प्रत्येक बटावलयन में 45 कार्नमकों
(personnel) िाले 18 आत्मवनभवर विशेषज्ञ अन्िेषण एिं बचाि दल विद्यमान हैं, वजनमें
इं जीवनयर, तकनीवशयन, इलेवक्रवशयन, डॉग स्वॉर्डस और वचक्रकत्सक/परावचक्रकत्सक सवम्मवलत
हैं। ितवमान में, प्रत्येक बटावलयन में 1149 कार्नमक हैं। राज्यों में इस बल की “अग्रसक्रक्रय
उपलब्धता” और भीषण आपदा की आशंका की वस्थवतयों में इसके “पूि-व संस्थापन” से देश में
आपदाओं के कारण होने िाली क्षवत के न्यूनीकरण में अत्यवधक सहायता वमली है।
o NDRF के वलए क्रकसी बड़ी आपदा से वनपटने की पहली परीक्षा की घड़ी 2008 में कोसी नदी में
आई बाढ़ थी। NDRF द्वारा अत्यवधक मुस्तैदी के साथ पांच बाढ़ प्रभावित वजलों में प्रवशवक्षत बाढ़
बचाि दल भेजकर इस वस्थवत को युि स्तर पर संभाला गया था। पररणामस्िरूप, प्रारं वभक चरण
के दौरान ही एक लाख से अवधक बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाया जा सका। वबहार के तत्कालीन
मुख्यमंत्री द्वारा NDRF की त्िररत एिं समयानुकूल कायविाही की सराहना की गयी थी।
o 2015 में नेपाल में आए भूकंप (7.8 तीव्रता) के समय घटनास्थल पर सिवप्रथम पहुाँच कर आपदा
प्रबंधन के गोल्डन ऑिसव में महत्िपूणव भूवमका वनभाते हुए भारत का NDRF सुर्नखयों में बना
रहा। बचाि कायव के दौरान NDRF कर्नमयों ने कु ल 16 पीवड़तों में से 11 को जीवित बाहर
वनकाला।
o NDRF ने CBRN (रासायवनक, जैविक, रे वडयोलॉवजकल और नावभकीय) चुनौवतयों का सामना
करने में अत्यवधक विशेषज्ञता प्राप्त क कर ली है। अप्रैल और मई 2010 के दौरान, क्रदल्ली वस्थत
14 www.visionias.in ©Vision IAS
मायापुरी में कोबाल्ट-60 रे वडयोएवक्टि सामग्री का पता लगाना, NDRF की CBRN क्षमता को
प्रदर्नशत करने िाला एक उल्लेखनीय कायव था।
2.2.2. राज्य स्तर पर सं स्थागत ढााँ चा
(Institutional Framework at State Level)
आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य का आपदा प्रबंधन हेतु स्ियं
का संस्थागत ढांचा होगा तथा प्रत्येक राज्य अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें गे। आपदा
प्रबंधन अवधवनयम यह अवधदेवशत करता है क्रक प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य विकास योजनाओं के
अंतगवत आपदाओं की रोकथाम या शमन के उपायों के एकीकरण करने, वित्त आिंटन करने और
पूिव चेतािनी प्रणावलयों की स्थापना करने हेतु आिश्यक कदम उठाएगी।
विवशष्ट वस्थवतयों और जरूरतों के आधार पर, राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के विवभन्न पहलुओं में
कें द्र सरकार तथा कें द्रीय एजेंवसयों की भी सहायता करे गी।
आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005, राज्य आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (SDMA) की स्थापना का
भी प्रािधान करता है। संबंवधत राज्य का मुख्यमंत्री SDMA का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रत्येक संघ
शावसत प्रदेश में उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में समान प्रणाली कायव करती है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (State Disaster Management Authority :SDMA):
आपदा प्रबंधन अवधवनयम, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य
आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (SDMA) की स्थापना क्रकये जाने का प्रािधान करता है। संघ शावसत
प्रदेशों के मामले में, उप-राज्यपाल या प्रशासक, उस प्रावधकरण के अध्यक्ष होते हैं। संघ शावसत
प्रदेश क्रदल्ली में उप-राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, इस राज्य प्रावधकरण के क्रमशैः अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष होते हैं। SDMA के उत्तरदावयत्िों में वनम्नवलवखत सवम्मवलत हैं:
o यह राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंवधत नीवतयााँ एिं योजनाएाँ तैयार करता है।
o NDMA द्वारा वनधावररत क्रदशा-वनदेशों के अनुसार यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना को
स्िीकृ वत प्रदान करता है।
o यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना के कायावन्ियन का समन्िय करता है तथा शमन एिं तैयारी
संबंधी उपायों हेतु वित्तीय प्रािधानों की अनुशस
ं ा करता है।
o रोकथाम, तैयारी एिं शमन संबध
ं ी उपायों के समेकन को सुवनवश्चत करने हेतु यह राज्य के
विवभन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करता है।
राज्य कायवकारी सवमवत (State Executive Committee: SEC): राज्य सरकार, मुख्य सवचि
की अध्यक्षता में एक राज्य कायवकारी सवमवत (SEC) का गठन करती है। इसके गठन का उद्देश्य
SDMA की उसके कायों के वनष्टपादन में सहायता करना है। SEC आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय
नीवत, राष्ट्रीय योजना एिं राज्य योजनाओं के कायावन्ियन का समन्िय तथा वनरीक्षण करती है।
यह NDMA को आपदा प्रबंधन के विवभन्न पहलुओं से संबंवधत सूचना भी प्रदान करती है।
2.2.3. वजला स्तर पर सं स्थागत ढााँ चा
(Institutional Framework at District Level)
वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (District Disaster Management Authority: DDMA)
वजला स्तर पर, वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (DDMA), आपदा प्रबंधन संबंधी प्रयासों एिं
वनयोजनों के समग्र समन्िय के वलए उत्तरदायी होता है। DDMA की अध्यक्षता वजला
कलेक्टर/वजला मवजस्रेट द्वारा की जाती है।
15 www.visionias.in ©Vision IAS
o आपदा प्रबंधन अवधवनयम के प्रािधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक
वजले हेतु एक वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरण की स्थापना करती है।
o वजला कलेक्टर द्वारा सह-अध्यक्ष के रूप में स्थानीय प्रावधकरण के वनिाववचत प्रवतवनवध के
साथ DDMA की अध्यक्षता की जाती है।
o राज्य सरकार, वजले के अपर कलेक्टर/अपर वजला मवजस्रेट के बराबर या ऊाँचे ओहदे िाले
एक अवधकारी को वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरण के मुख्य कायवकारी अवधकारी के रूप में
वनयुक्त करती है।
o DDMA वजले के वलए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करता है और इसके कायावन्ियन का
वनरीक्षण करता है।
o इसके द्वारा NDMA तथा SDMA द्वारा वनधावररत क्रदशा-वनदेशों का सभी वजला स्तरीय
कायावलयों द्वारा अनुपालन भी सुवनवश्चत क्रकया जाता है।
स्थानीय प्रावधकरण : पंचायती राज संस्थाएाँ (PRIs), नगरपावलकाएं, वजला एिं छािनी बोडव
और नगर वनयोजन प्रावधकरण, नागररक सेिाओं का वनयंत्रण एिं प्रबंधन करते हैं तथा साथ ही
प्रभावित क्षेत्रों में आपदाओं के प्रबंधन तथा राहत, पुनिावस एिं पुनर्ननमावण गवतविवधयों के
कायावन्ियन हेतु अपने कमवचाररयों के क्षमता वनमावण को सुवनवश्चत करते हैं। ये अपनी आपदा
प्रबंधन योजनाओं को राष्ट्रीय तथा राज्य के क्रदशा-वनदेशों के अनुसार तैयार करते हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन प्रावधकरणों एिं वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरणों का सुदढृ ीकरण
गृह मंत्रालय ने सभी SDMAs एिं चयवनत DDMAs की प्रभािकाररता में सुधार लाने तथा उन्हें
समर्नपत आपदा प्रबंधन पेशेिरों की उपलब्धता सुवनवश्चत कर कायावत्मक रूप से सक्रक्रय बनाने हेतु
एक योजना को अनुमोक्रदत क्रकया है। यह योजना NDMA की योजना कायावन्ियन इकाई (SIU)
द्वारा कायाववन्ित की जा रही है।
2.2.4. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न अवधवनयम, 2005 के तहत वित्तीय व्यिस्थाएाँ
(Financial Arrangements under NDM Act, 2005)
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रक्रया वनवध (National Disaster Response Fund: NDRF)
यह क्रकसी भीषण आपदा की आशंका से उत्पन्न वस्थवत के कारण क्रकए गए आपदा अनुक्रक्रया, राहत
एिं पुनिावस संबंवधत व्यय की पूर्नत करने हेतु के न्द्र सरकार द्वारा प्रबंवधत वनवध है। क्रकसी आपदा
की वस्थवत में यक्रद राहत अवभयानों के वलए आिश्यक धनरावश, राज्य आपदा अनुक्रक्रया वनवध के
खाते में उपलब्ध रावश से अवधक है, तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रक्रया वनवध से अवतररक्त कें द्रीय
सहायता प्रदान की जाती है। 11िें वित्त आयोग द्वारा आरं भ की गई राष्ट्रीय आपदा आकवस्मकता
वनवध (National Calamity Contingency Fund: NCCF) का विलय भी राष्ट्रीय आपदा
अनुक्रक्रया वनवध में कर क्रदया गया है।
राज्य आपदा अनुक्रक्रया वनवध (State Disaster Response Fund: SDRF)
राज्य आपदा अनुक्रक्रया वनवध (SDRF) का उपयोग के िल आपदा पीवड़तों को तत्काल राहत
प्रदान करने में हुए व्यय की पूर्नत करने के वलए क्रकया जाता है। स्थानीय संदभव में, ऐसी राज्य
विवशष्ट आपदाएं जो आपदाओं की वनर्ददष्ट सूची में सवम्मवलत नहीं होती हैं, िे भी राज्य आपदा
अनुक्रक्रया वनवध से सहायता प्राप्त क करने के योग्य होती हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रक्रया वनवध एिं राज्य
आपदा अनुक्रक्रया वनवध में आनुग्रवहक राहत, खोज और बचाि अवभयानों, राहत उपायों,
हेलीकॉप्टर द्वारा आिश्यक सामग्री की आपूर्नत, पेयजल की आपात आपूर्नत, मलबे के प्रबंधन सवहत
प्रभावित क्षेत्र को साफ करने, कृ वष, पशुपालन, मत्स्य-पालन, हस्तवशल्प, कारीगरों, क्षवतग्रस्त
अिसंरचना (तात्कावलक प्रकृ वत की) की मरम्मत/पुनैःस्थापन और क्षमता विकास (तत्काल प्रकृ वत)
हेतु प्रािधान क्रकया गया है।
16 www.visionias.in ©Vision IAS
राष्ट्रीय आपदा शमन वनवध (National Disaster Mitigation Fund: NDMF)
राष्ट्रीय आपदा शमन वनवध (NDMF) का गठन नहीं क्रकया गया है। सरकार के अनुसार ितवमान में
विवभन्न पररयोजनाओं में शमन संबध ं ी उपायों के वित्त पोषण हेतु पयावप्त क योजनाएं विद्यमान हैं
तथा पृथक राष्ट्रीय आपदा शमन वनवध का वनमावण करने की आिश्यकता महसूस नहीं की गई है।
राष्ट्रीय आपदा शमन वनवध के वनमावण का उद्देश्य अनन्य रूप से शमन के उद्देश्य हेतु संपन्न की जाने
िाली पररयोजनाओं हेतु वित्त की उपलब्धता सुवनवश्चत करना है। इस उद्देश्य की पूर्नत ितवमान कें द्र
प्रायोवजत योजनाओं तथा कें द्रीय क्षेत्रक योजनाओं, यथा- प्रधानमंत्री कृ वष ससचाई योजना, राष्ट्रीय
सतत कृ वष वमशन, नमावम गंग-े राष्ट्रीय गंगा योजना, नदी बेवसन प्रबंधन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण
योजना एिं जल संसाधन प्रबंधन आक्रद द्वारा की जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रक्रया ररजिव (National Disaster Response Reserve: NDRR)
13िें वित्त आयोग ने आपदा पश्चात् राहत सामग्री/ उपकरण की तत्काल आिश्यकता की पूर्नत
करने हेतु 250 करोड़ रुपए की रावश के साथ NDRR के गठन की अनुशस
ं ा की। NDRR के गठन
का उद्देश्य ऐसी आपदाओं के पीवड़तों के कष्टों को कम करना है, वजनकी तत्काल सहायता करने में
राज्य असमथव होते हैं।
आपदा प्रबंधन हेतु वनवध जुटाने पर 14िााँ वित्त आयोग (14th Finance Commission on
Fund Mobilisation for DM)
आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 के तहत की गई पररकल्पना के अनुरूप वित्त आयोग द्वारा
आपदा प्रबंधन वनवधयों के वित्तपोषण संबंधी व्यिस्थाओं की समीक्षा क्रकये जाने की आिश्यकता
है।
17 www.visionias.in ©Vision IAS
14िें वित्त आयोग की अनुशस
ं ाएं इस प्रकार हैं:
o इसने अनुशस
ं ा की है क्रक राज्य आपदा राहत वनवध (State Disaster Relief Fund:
SDRF) के अंतगवत उपलब्ध वनवधयों के 10% तक के भाग का उपयोग राज्य द्वारा ऐसी
घटनाओं के वलए क्रकया जा सकता है वजन्हें राज्य स्थानीय संदभव में ‘आपदाएं’ मानते हों तथा
जो गृह मंत्रालय की अवधसूवचत आपदाओं की सूची में सवम्मवलत न हों।
o चूाँक्रक NDRF का वित्तपोषण अभी तक पूणत
व या चयवनत िस्तुओं पर उपकर का अवधरोपण
करके क्रकया जाता रहा है, अतैः इसने अनुशंसा की है क्रक सभी उपकरों और उद्ग्रहणों के िस्तु
एिं सेिा कर के अंतगवत समाविष्ट होने के पश्चात् कें द्र सरकार को आपदा वनवध के वित्तपोषण
हेतु सुवनवश्चत स्रोत वनधावररत करना चावहए।
o 14िें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन हेतु सभी राज्यों को 55000 करोड़ रुपए आिंरटत करने
की अनुशंसा की है।
2.2.5. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न अवधवनयम, 2005 की कवमयााँ
(Drawbacks of the National Disaster Management Act, 2005)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 का कायावन्ियन अत्यंत मंद एिं वनवष्टक्रय रहा है। राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन योजना को 2006 से 2013 तक सात िषव के विलम्ब पश्चात अंवतम रूप प्रदान क्रकया
गया। योजना को अंतत: 2016 में जारी क्रकया गया। इस अवधवनयम में गैर सरकारी संगठनों
(NGOs), वनिाववचत स्थानीय जनप्रवतवनवधयों, स्थानीय समुदायों एिं नागररक समूहों की भूवमका को
गौण माना गया है। इस आधार पर इस अवधवनयम की आलोचना की जाती है। इस पर एक
पदानुक्रमिादी, नौकरशाही आधाररत तथा आदेश एिं वनयंत्रण िाले ’टॉप डाउन’ दृवष्टकोण (जो कें द्र,
राज्य एिं वजला प्रावधकरणों को व्यापक शवक्तयां प्रदान करता है) को पोवषत करने का आरोप भी
लगता रहा है ।
भारत के वनयंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General: CAG) द्वारा देश
में आपदा प्रबंधन तंत्र की परफॉरमेंस ऑवडट ररपोटव 2013 में जारी की गई थी। CAG की ररपेाटव में
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA) की कायवप्रणाली में कई अन्य कवमयों को उजागर क्रकया
गया है।
इसमें कहा गया है क्रक NDMA द्वारा वजम्मेदारी ली गयी प्रमुख पररयोजनाओं में से कोई भी पूरी
नहीं की गई। पररयोजनाओं को या तो बीच में छोड़ क्रदया गया या आरं वभक वनम्नस्तरीय योजना
वनमावण के कारण उनकी पुनरव चना की गई।
CAG ररपोटव के अनुसार, NDMA आपदा शमन के उद्देश्य हेतु वनवधयों के प्रािधान की अनुशंसा
तथा ऋण पुनभुवगतान में राहत की अनुशस
ं ा जैसे कई अन्य कायों का भी वनष्टपादन नहीं करता
रहा है।
इसने यह भी उजागर क्रकया क्रक NDMA में कई महत्िपूणव पद ररक्त हैं और रोजमराव के कायों के
वलए परामशवदाताओं की सहायता ली जाती है।
लोक लेखा सवमवत ने क्रदसंबर 2015 में 'भारत में आपदा तैयारी' विषय पर अपनी ररपोटव प्रस्तुत की।
इसमें वनम्नवलवखत अिलोकन क्रकए गए हैं:
इस अवधवनयम के अनुसार तीन महीने में कम से कम एक बार राष्ट्रीय कायवकारी सवमवत की बैठक
का आयोजन करना आिश्यक है। हालांक्रक, यह पाया गया क्रक यहााँ तक क्रक जब 2007 में पवश्चम
बंगाल में बाढ़ एिं राजस्थान में 2008 में भगदड़ जैसी आपदाएाँ घरटत हुईं तो भी सवमवत की
बैठक कभी-कभार ही हुई।
18 www.visionias.in ©Vision IAS
कें द्र, राज्य और वजलों में आपदा तैयारी ि पुनैःस्थापन हेतु प्रयुक्त की जा सकने िाली शमन
वनवधयों का गठन नहीं क्रकया गया।
आपदा प्रबंधन के वलए संचार नेटिकव की सुदढृ ीकरण हेतु आरम्भ की गई विवभन्न पररयोजनाएं या
तो वनयोजन की अिस्था में थी या विवलम्बत थी।
CAG की ररपोटव के सारांश के अनुसार 2012 एिं 2017 के मध्य 219 टेलीमेरी स्टेशनों (बाढ़
पूिावनुमान उपकरणों) की स्थापना करने के लक्ष्य के विरुि अगस्त 2016 तक के िल 56 स्टेशन
स्थावपत क्रकये गए थे और मौजूदा टेलीमेरी स्टेशनों में से 59% क्रक्रयाशील नहीं थे।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) में 27% पद ररक्त थे। NDRF के प्रवशक्षण संस्थान, राष्ट्रीय
आपदा मोचन संस्थान की स्थापना नहीं की गई थी, जबक्रक 2006 में इसे अनुमोक्रदत कर क्रदया
गया था।
2.3. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न नीवत, 2009
(National Policy on Disaster Management, 2009)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण द्वारा िषव 2009 में 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीवत (NDMP)'
जारी गई। इसे “रोकथाम, शमन, तैयारी और अनुक्रक्रया की संस्कृ वत के माध्यम से समग्र,
अग्रसक्रक्रय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योवगकी आधाररत रणनीवत विकवसत कर सुरवक्षत और
आपदा प्रत्यास्थ भारत के वनमावण” के वि़न के तहत तैयार क्रकया गया है।
आपदा प्रबंधन बहु-विषयक गवतविवध है वजसे सभी वहतधारकों के मध्य परस्पर सहक्रक्रया के साथ
सम्पन्न करने की आिश्यकता होती है। NDMP विवभन्न स्तरों पर रणनीवतक साझेदारी के
वनमावण पर बल देते हुए प्रबंधन हेतु एकीकृ त दृवष्टकोण का प्रािधान करती है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीवत, 2009 के उद्देश्य
ज्ञान, निाचार और वशक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और प्रत्यास्थता की
संस्कृ वत को बढ़ािा देना।
प्रौद्योवगकी, पारं पररक ज्ञान और पयाविरणीय संधारणीयता के आधार पर शमन संबंधी उपायों को
प्रोत्सावहत करना।
आपदा प्रबंधन को विकासात्मक योजना वनमावण प्रक्रक्रया में सवम्मवलत करना।
सक्षमकारी विवनयामकीय पररिेश और अनुपालन व्यिस्था का वनमावण करने के वलए संस्थागत
और तकनीकी-कानूनी ढााँचों की स्थापना करना।
आपदा जोवखमों की पहचान, आकलन और वनगरानी के वलए कु शल तंत्र सुवनवश्चत करना।
सूचना प्रौद्योवगकी की सहायता से अनुक्रक्रयाशील एिं अचूक सम्प्रेषण (fail-safe
communication) द्वारा समर्नथत समकालीन पूिावनुमान और पूिव चेतािनी प्रणाली का विकास
करना।
समाज के सुभेद्य िगों की जरूरतों के प्रवत देखभाल के दृवष्टकोण के साथ कु शल अनुक्रक्रया और
राहत सुवनवश्चत करना।
सुरवक्षत जीिन सुवनवश्चत करने हेतु पुनर्ननमावण गवतविवधयों को आपदा प्रत्यास्थ संरचनाओं का
वनमावण करने का एक अिसर मानकर सम्पन्न करना।
आपदा प्रबंधन के वलए मीवडया के साथ उपयोगी और अग्रसक्रक्रय भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान
करना।
19 www.visionias.in ©Vision IAS
यह सभी के वलए सक्षमकारी पररिेश की स्थापना करती है और क्रदव्यांगजनों, मवहलाओं, बच्चों
और अन्य िंवचत समूहों सवहत समाज के सभी िगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास
करती है।
इसका उद्देश्य समुदाय, समुदाय आधाररत संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs), स्थानीय
वनकायों और वसविल सोसाइटी को सहभागी बना कर आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में
पारदर्नशता और जिाबदेही सुवनवश्चत करना है।
2.4. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न योजना, 2016
(The National Disaster Management Plan, 2016)
भारत सरकार ने पहली बार 2016 में अपनी प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इस
योजना का वि़न “प्रशासन के सभी स्तरों एिं समुदायों के मध्य आपदाओं से वनपटने की क्षमता
को अवधकतम कर, भारत को आपदा प्रत्यास्थ बनाना, आपदा जोवखम न्यूनीकरण उपलवब्ध प्राप्त
करना तथा जीिन, आजीविकाओं और आर्नथक, शारीररक, सामावजक, सांस्कृ वतक एिं
पयाविरणीय पररसम्पवत्तयों की हावन को न्यूनतम करना है। "
इसे व्यापक रूप से आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव , सतत विकास लक्ष्य 2015-
2030 एिं COP-21 में जलिायु पररितवन पर पेररस समझौते में वनधावररत लक्ष्यों और
प्राथवमकताओं के अनुसार सूत्रबि क्रकया गया है। जहााँ सेंडाई फ्रेमिकव 2015 के बाद के विकास
एजेंडे के अंतगवत अंगीकृ त क्रकया गया प्रथम अंतरावष्ट्रीय समझौता है, िहीं सतत विकास लक्ष्य भी
आपदा जोवखम न्यूनीकरण के महत्ि को सतत विकास के अवभन्न घटक के रूप में मान्यता प्रदान
करते हैं। पेररस समझौता िैविक जलिायु पररितवन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती
बारं बारता पर तत्काल विचार करने की आिश्यकता पर ध्यान आकर्नषत करता है।
2.4.1. योजना के प्रमु ख वबन्दु
(Major highlights of the Plan)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शावमल दृवष्टकोण के तहत, प्रत्येक संकट के वलए आपदा जोवखम
न्यूनीकरण के फ्रेमिकव में सेंडाई फ्रेमिकव में घोवषत चार प्राथवमकताओं को शावमल क्रकया गया है।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण के वलए पांच कायवक्षेत्र वनम्न हैं:
o जोवखम को समझना
o एजेंवसयों के मध्य समन्िय
o आपदा जोवखम न्यूनीकरण (DRR) में वनिेश– संरचनात्मक उपाय
o आपदा जोवखम न्यूनीकरण में वनिेश– गैर-संरचनात्मक उपाय
o क्षमता विकास
यह आपदा प्रबंधन के सभी चरणों अथावत् रोकथाम, शमन, अनुक्रक्रया और सामान्य वस्थवत की
बहाली को किर करती है और मानि जवनत आपदाओं जैसे रासायवनक, नावभकीय आक्रद को किर
करती है।
यह आपदाओं से वनपटने हेतु लघु, मध्यम और दीघाविवध (क्रमशैः 5, 10, और 15 िषव) योजनाओं
की पररकल्पना करती है।
20 www.visionias.in ©Vision IAS
सुस्पष्ट भूवमका के साथ एकीकृ त दृवष्टकोण
o यह सभी सरकारी एजेंवसयों एिं विभागों के मध्य क्षैवतज और ऊध्िावधर एकीकरण का
प्रािधान करती है तथा साथ ही एक मैररक्स प्रारूप में पंचायत और शहरी स्थानीय वनकाय
स्तर तक सरकार के सभी स्तरों की भूवमकाएं और उत्तरदावयत्ि वनधावररत करती है।
o मंत्रालयों को विवशष्ट आपदाओं हेतु भूवमका सौंपी जाती है; जैसे चक्रिातों से संबंवधत
उत्तरदावयत्ि पृ्िी विज्ञान मंत्रालय को सौंपा गया है।
o इस योजना का दृवष्टकोण क्षेत्रीय है, जो न के िल आपदा प्रबंधन के वलए अवपतु विकास
योजना के वनमावण में भी लाभदायक होगा।
o इसे इस प्रकार तैयार क्रकया गया है क्रक इसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में मापनीय रूप से
कायाववन्ित क्रकया जा सकता है।
प्रमुख गवतविवधयााँ
o यह आपदा के प्रवत अनुक्रक्रया करने िाली एजेंवसयों हेतु चेकवलस्ट के रूप में उपयोग क्रकए
जाने के वलए पूिव चेतािनी, सूचना प्रसार, वचक्रकत्सा देखभाल, ईंधन, पररिहन, खोज और
बचाि, फाँ से हुए लोगों को बाहर वनकालना (evacuation) आक्रद प्रमुख गवतविवधयों की
पहचान करती है।
o यह सामान्य वस्थवत की बहाली हेतु सामान्यीकृ त ढांचा प्रदान करती है तथा वस्थवत का
आकलन करने और बेहतर पुनर्ननमावण हेतु लचीलापन भी प्रदान करती है।
सूचना एिं मीवडया विवनयमन
o समुदायों को आपदाओं से वनपटने हेतु तैयार करने के वलए यह सूचना, वशक्षा और सम्प्रेषण
कायवकलापों की आिश्यकता पर अत्यवधक बल देती है।
o यह आपदाओं की किरे ज के वलए नैवतक क्रदशा-वनदेशों एिं स्ि-वनयमन का वनदेश देती है।
o यह योजना, मीवडया से आपदा प्रभावित लोगों की गररमा और वनजता का सम्मान करने की
अपेक्षा करती है।
o साथ ही, अफिाहों और दहशत के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इस योजना ने अवधकाररयों
को वनयवमत रूप से मीवडया िीकफग (आपदा की गंभीरता के आधार पर) का कायवक्रम तय
करने एिं सरकार की ओर से मीवडया से बातचीत करने हेतु एक नोडल अवधकारी को नावमत
करने का वनदेश भी क्रदया है।
यह प्रवशक्षण, क्षमता वनमावण और सिवश्रेष्ठ अंतरावष्ट्रीय प्रणावलयों को समाविष्टट करने पर ध्यान
के वन्द्रत करती है।
2.4.2. राष्टरीय आपदा प्रबं ध न योजना का महत्ि
(Significance of the NDMP)
यह सरकारी एजेंवसयों को आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के वलए रूपरे खा और क्रदशा-वनदेश
प्रदान करती है।
यक्रद उत्तरदावयत्ि सम्बन्धी रूपरे खा (responsibility framework) में क्रकसी भी प्रकार की ऐसी
अस्पष्टता है वजसे समाप्त न क्रकया जा सके , तो यह योजना उस अस्पष्टता को न्यूनतम करने का
प्रयास करती है। इस प्रकार यह वनर्ददष्टट करती है क्रक आपदा प्रबंधन के विवभन्न चरणों में कौन
क्रकस कायव के वलए उत्तरदायी है।
इस योजना की पररकल्पना इस प्रकार की गई है क्रक देश के क्रकसी भी भाग में आपातवस्थवत की
अनुक्रक्रया में सक्रक्रय होने हेतु यह सदैि तैयार बनी रहे।
इसे इस प्रकार तैयार क्रकया गया है क्रक आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में आिश्यकतानुसार लचीले
एिं मापनीय तरीके से कायाववन्ित क्रकया जा सकता है।
21 www.visionias.in ©Vision IAS
2.4.3. राष्ट्रीय आपदा प्रबं ध न योजना, 2016 की कवमयााँ
(Shortcomings of National Disaster Management Plan, 2016)
NDMP, 2016 में एक बेहतर एिं सशक्त कायव योजना का वनमावण करने िाले कई महत्िपूणव तत्िों का
अभाि है।
कवमयााँ
यह योजना स्पष्ट एिं व्यािहाररक रोडमैप बनाने में असफल रही है। इसमें कें द्र एिं राज्य सरकारों
द्वारा आपदा जोवखम शमन, तैयारी, अनुक्रक्रया, सामान्य वस्थवत की बहाली, पुनैःवनमावण और
शासन हेतु अपनाई जाने िाली कायव प्रणावलयों की पहचान करने का तरीका अत्यंत सामान्य है।
इन कायव प्रणावलयों के वनष्टपादन के वलए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है। अस्पष्ट रूप से
के िल यह बताया गया है क्रक उन्हें लघु, औसत, मध्य तथा दीघवकावलक आधार पर वनष्टपाक्रदत
क्रकया जाना चावहए।
योजना में इन प्रणावलयों के संचालन हेतु िांवछत वनवध की आिश्यकता को व्यक्त नहीं क्रकया गया
है, न ही इससे ऐसा कोई संकेत प्राप्त क होता है क्रक इस उद्देश्य हेतु वनवध क्रकस प्रकार संग्रवहत की
जाए।
इसके अवतररक्त योजना की वनगरानी तथा मूल्यांकन हेतु कोई फ्रेमिकव प्रदान नहीं क्रकया गया है।
इस योजना को आपदा जोवखम न्यूनीकरण एिं सतत विकास लक्ष्यों की प्रावप्त क हेतु सेंडाई फ्रेमिकव
के साथ संरेवखत क्रकया गया है; क्रकन्तु सेंडाई फ्रेमिकव या SDGs के समान इस योजना के तहत
कोई लक्ष्य वनधावररत नहीं क्रकया गया है। साथ ही इसमें यह भी नहीं बताया गया है क्रक सेंडाई
लक्ष्यों (Sendai goals) को क्रकस प्रकार प्राप्त क क्रकया जाए।
अतैः, राष्ट्रीय योजना के साथ-साथ आपदा प्रत्यास्थता हेतु स्पष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों, समय सीमाओं तथा
इसके कायावन्ियन में संसाधनों के उपयोग हेतु एक राष्ट्रीय कायवयोजना का प्रािधान क्रकया जाना
चावहए।
2.5. भारत में आपदा प्रबं ध न चक्र
(Disaster Management Cycle in India)
2.5.1. जोवखम न्यू नीकरण एिं प्रत्यास्थता में िृ वि करना
(Reducing Risk and Enhancing Resilience)
संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण कायावलय (United Nations Office for Disaster Risk
Reduction: UNISDR) द्वारा स्िीकृ त शब्दािली में, आपदा जोवखम न्यूनीकरण संबंधी अिधारणा
और कायवप्रणाली में आपदा के कारण संबंधी कारकों के विश्लेषण एिं प्रबंधन संबंधी सुवनयोवजत प्रयास
सवम्मवलत क्रकये गये हैं। इनमें जोवखम की प्रकृ वत की जानकारी, व्यवक्तयों तथा पररसंपवत्त की बेहतर
सुरक्षा, भूवम तथा पयाविरण का बुविमतापूणव प्रबंधन तथा प्रवतकू ल प्रभािों हेतु बेहतर तैयारी
सवम्मवलत है। आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 के अनुसार शमन से तात्पयव ऐसे उपायों से है वजनका
लक्ष्य क्रकसी आपदा या आसन्न आपदा वस्थवत के जोवखम, संघात तथा प्रभाि का न्यूनीकरण करना है।
दी गयी सारणी में आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु प्रधानमंत्री के 10-सूत्री एजेंडे का उल्लेख क्रकया गया
है।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु 10-सूत्री एजेंडा
विकास संबंधी सभी क्षेत्रकों में आपदा जोवखम आपदा सम्बन्धी अध्ययन हेतु
प्रबंधन के वसिांत को अवनिायव रूप से आत्मसात वििविद्यालयों के एक नेटिकव का विकास
करना। करना।
22 www.visionias.in ©Vision IAS
सािवभौवमक जोवखम सुरक्षा प्रदान करने की क्रदशा सोशल मीवडया और मोबाइल टेक्नोलॉजी
में कायव करना। द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अिसरों का
लाभ उठाना।
आपदा जोवखम प्रबंधन में मवहलाओं की अवधक स्थानीय क्षमता तथा पहलों को प्रोत्साहन
भागीदारी और उनकी नेतृत्िकारी भूवमका को देना।
प्रोत्साहन देना।
िैविक रूप से जोवखम मानवचत्रण में वनिेश। यह सुवनवश्चत करना क्रक क्रकसी आपदा से
सीखने का अिसर व्यथव न जाए।
आपदा जोवखम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता के आपदाओं के प्रवत अंतरावष्ट्रीय अनुक्रक्रया में
संिधवन हेतु प्रौद्योवगकी का लाभ उठाना। बेहतर सामंजस्य लाना।
राष्ट्रीय नीवत में आपदा जोवखम न्यूनीकरण तथा शमन हेतु एक बहु-आयामी दृवष्टकोण का सुझाि क्रदया
गया है, वजसमें वनम्नवलवखत त्य सवम्मवलत हैं:
सभी विकासात्मक पररयोजनाओं में जोवखम न्यूनीकरण संबंधी उपायों को सवम्मवलत करना।
कें द्र तथा राज्य सरकारों के सवम्मवलत प्रयासों के माध्यम से वनधावररत उच्च प्राथवमकता प्राप्त क क्षेत्रों
में शमन पररयोजनाओं को प्रारं भ करना।
राज्य स्तरीय शमन पररयोजनाओं को प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करना।
आपदा तथा उसका सामना करने सम्बन्धी प्रणावलयों के संबंध में स्थानीय ज्ञान को महत्ि देना।
विरासत अिसंरचनाओं की सुरक्षा को उवचत महत्ि प्रदान करना।
सेंडाई फ्रेमिकव के वनदेशक वसिांतों के अनुसार, आपदा जोवखम न्यूनीकरण के वलए विवभन्न सरकारी
प्रभागों तथा विवभन्न एजेंवसयों द्वारा उत्तरदावयत्िों को साझा करने की आिश्यकता होती है। आपदा
जोवखम न्यूनीकरण की प्रभािशीलता सभी क्षेत्रकों के मध्य, क्षेत्रकों के भीतर तथा सभी स्तरों पर
सम्बंवधत वहतधारकों के समन्िय तंत्रों पर वनभवर करती है। प्रत्येक संकट के वलए, सेंडाई फ्रेमिकव में
घोवषत चार प्राथवमकताओं को आपदा जोवखम न्यूनीकरण के फ्रेमिकव में शावमल क्रकया गया है। आपदा
जोवखम न्यूनीकरण के वलए पांच कायवक्षत्र
े वनम्नवलवखत हैं:
जोवखम को समझना: इसमें जोवखम की समझ विकवसत करने पर बल क्रदया जाता है तथा यह
सेंडाई फ्रेमिकव के तहत प्रथम प्राथवमकता है। इसमें a) प्रेक्षण नेटिकव , शोध, पुिावनम
ु ान, b) जोनों
में िगीकरण/मानवचत्रण, c) वनगरानी तथा चेतािनी प्रणावलयााँ, d) संकट जोवखम तथा सुभेद्यता
मूल्यांकन (Hazard Risk and Vulnerability Assessment: HRVA), तथा e) चेतािवनयााँ,
आंकड़े तथा सूचना का विस्तार सवम्मवलत होते हैं। चेतािवनयााँ ़ारी करने तथा सूचना प्रसाररत
करने हेतु पयावप्त क वसस्टम का होना जोवखमों की समझ में सुधार का एक अवभन्न वहस्सा है।
एजेंवसयों के मध्य समन्िय: एजेंवसयों के मध्य समन्िय आपदा जोवखम शासन के सुदढ़ृ ीकरण हेतु
मुख्य अियि है। प्रमुख क्षेत्र, वजनमें एजेंवसयों के मध्य शीषव स्तरीय समन्िय में सुधार की
आिश्यकता है, िे वनम्नवलवखत हैं: a) समग्र आपदा शासन b) अनुक्रक्रया c) चेतािवनयााँ, सूचना
और आंकड़े उपलब्ध कराना, तथा d) गैर-संरचनात्मक उपाय।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण में वनिेश– संरचनात्मक उपाय: आपदा जोवखम न्यूनीकरण तथा
प्रत्यास्थता बढ़ाने हेतु प्रमुख कायव-क्षेत्रों में से एक आिश्यक संरचनात्मक उपायों को आरं भ करना
है। इनमें आपदाओं से वनपटने में प्रयासरत समुदायों की सहायता हेतु आिश्यक विवभन्न भौवतक
अिसंरचनाएं तथा सुविधाएं सवम्मवलत हैं।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण में वनिेश– गैर-संरचनात्मक उपाय: यथोवचत कानूनों, व्यिस्थाओं तथा
तकनीकी-क़ानूनी व्यिस्था का समुच्चय, आपदा जोवखम को प्रबंवधत करने के वलए आपदा जोवखम
शासन के सुदढ़ृ ीकरण हेतु महत्िपूणव घटक है। इन गैर-संरचनात्मक उपायों में क़ानून, प्रवतमान,
23 www.visionias.in ©Vision IAS
वनयम, मागवदशवक वसिांत तथा तकनीकी-क़ानूनी व्यिस्था (उदाहरण के वलए, संवहताओं का
वनमावण) इत्याक्रद सवम्मवलत होते हैं। ये उपाय आपदा जोवखम न्यूनीकरण एिं आपदा प्रत्यास्थता
को विकासात्मक गवतविवधयों की मुख्य धारा में समावहत करने में प्रावधकाररयों की सहायता
करते हैं।
क्षमता वनमावण: क्षमता वनमावण में प्रवशक्षण कायवक्रम, पाठ्यक्रम का विकास, व्यापक पैमाने पर
जागरुकता का प्रसार करने संबध
ं ी प्रयास, वनयवमत माक विल्स तथा आपदा अनुक्रक्रया अभ्यासों
का संचालन सवम्मवलत होता है।
आपदा जोवखम शमन हेतु संकटों के अनुरूप समुवचत उत्तरदावयत्ि मैररक्स (Responsibility
Matrices) विकवसत क्रकए गए हैं तथा सम्बंवधत वहतधारकों की पहचान की गयी है।
10 संकट-बहुल वजलों में आपदा जोवखम का सतत न्यूनीकरण
सिाववधक सुभेद्य राज्यों के सिाववधक संकट-ग्रस्त वजलों के क्षमता वनमावण के वलए भारत सरकार ने पांच
चयवनत राज्यों (उत्तराखंड, असम, वबहार, वहमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर) में से प्रत्येक के दो
वजलों में आपदा जोवखम के सतत न्यूनीकरण हेतु एक पररयोजना आरं भ की है।
2.5.2.आपदा तै यारी तथा अनु क्रक्रया
(Disaster Preparedness and Response)
अनुक्रक्रया संबंधी उपाय उपयुक्त प्रावधकाररयों द्वारा पूिव चेतािनी वमलते ही या क्रकसी घटना के
तत्काल पश्चात् अमल में लाये जाते हैं। यह आपदा प्रबंधन के विविध चरणों में सिाववधक स्पष्ट
चरण होता है। अनुक्रक्रया में न के िल उन गवतविवधयों को सवम्मवलत क्रकया जाता है जो
तात्कावलक जरूरतों, यथा खोज और बचाि, प्राथवमक उपचार तथा अस्थायी आश्रयस्थलों की
उपलब्धता की पूर्नत करें बवल्क प्रयासों के समन्िय और समथवन हेतु आिश्यक विवभन्न प्रणावलयों
की त्िररत लामबंदी भी इसके अंतगवत आती है।
जैसा क्रक UNISDR द्वारा पररभावषत है, तैयारी के अंतगवत सरकार द्वारा विकवसत ज्ञान तथा
क्षमता; पेशेिर अनुक्रक्रया और उस घटना से उबरने में सहायता करने िाले संगठन, समुदाय तथा
व्यवक्त; संभावित, आसन्न या ितवमान संकटपूणव घटनाएं या वस्थवतयों का पूिावनुमान करने, उनके
प्रवत अनुक्रक्रया करने तथा उनसे उबर पाने की क्षमता इत्याक्रद सवम्मवलत होते हैं। तैयारी के आधार
पर यह स्पष्ट होते ही क्रक कोई विनाशकारी घटना आसन्न है, अनुक्रक्रया संबंधी प्रक्रक्रया आरम्भ हो
जाती है तथा यह तब तक चलती रहती है जब तक क्रक आपदा समावप्त क की घोषणा न कर दी जाए।
कोई भी एकल एजेंसी या विभाग क्रकसी भी स्तर की आपदा वस्थवत से अके ले नहीं वनपट सकता।
अनुक्रक्रया के कायवक्षत्र
े में विवशष्ट कायव, भूवमकाएं तथा उत्तरदावयत्ि सवम्मवलत होते हैं तथा
अनुक्रक्रया को आपदा प्रबंधन का सिाववधक महत्िपूणव तथा समय-संिेदनशील (time-sensitive)
पहलू माना जाता है।
अनुक्रक्रया प्रणाली की संस्थागत व्यिस्थाओं में वनम्नवलवखत तत्ि सवम्मवलत होते हैं:
राष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रक्रया के समन्िय तथा सभी आिश्यक संसाधनों की लामबंदी हेतु आपदा
विवशष्ट उत्तरदावयत्िों िाला नोडल के न्द्रीय मंत्रालय।
पूि-व चेतािनी प्रणावलयों तथा चेतािवनयों के वलए आपदा-विवशष्ट उत्तरदावयत्िों िाली के न्द्रीय
एजेंवसयां।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)।
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)।
राष्ट्रीय पूि-व चेतािनी प्रणाली
भारत सरकार ने विवभन्न प्राकृ वतक आपदाओं की वनगरानी के वलए विवशष्ट एजेंवसयों को प्रावधकृ त
क्रकया है। पयावप्त क पूि-व चेतािनी प्रणावलयााँ स्थावपत की गयी हैं तथा क्रकसी भी आसन्न संकट के संबंध
में चेतािवनयों के प्रसारण की व्यिस्था की गयी है। ये एजेंवसयां मानि संसाधन विकास मंत्रालय
24 www.visionias.in ©Vision IAS
को अपने इनपुट सौंपती हैं, वजसके पश्चात विवभन्न संचार चैनलों के माध्यम से आपदा की सूचना
और चेतािवनयााँ प्रसाररत की जाती हैं।
सारणी : प्राकृ वतक संकट-विवशष्ट पूिव चेतािनी जारी करने हेतु प्रावधकृ त के न्द्रीय एजेंसी
संकट एजेंसी
1 वहमस्खलन वहम एिं वहमस्खलन अध्ययन प्रवतष्ठान (Snow and Avalanche Study
Establishment: SASE)
2 चक्रिात भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department: IMD)
3 सूखा कृ वष एिं क्रकसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers'
Welfare: MoAFW)
4 भूकंप भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department: IMD)
5 महामारी स्िास््य एिं पररिार कल्याण मंत्रालय (MInistry of Health and Family
Welfare: MoHFW)
6 बाढ़ के न्द्रीय जल आयोग (Central Water Commission: CWC)
7 भूस्खलन भारतीय भूिैज्ञावनक सिेक्षण (Geological Survey of India: GSI)
8 सुनामी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेिा के न्द्र (Indian National Center for
Ocean Information Services: INCOIS)
के न्द्रीय एजेंवसयों/ विभागों की भूवमका
नेशनल इमरजेंसी ऑपरे शन सेंटर (NEOC) इस चरण के दौरान समन्िय तथा संचार के कें द्र के
रूप में कायव करे गा तथा इनपुट को अपडेट करने हेतु विवभन्न चेतािनी एजेंवसयों के साथ सतत
संपकव बनाए रखेगा। यह स्टेट इमरजेंसी ऑपरे शन सेंटर (SEOC) तथा वडवस्रक्ट इमरजेंसी
ऑपरे शन सेंटर (DEOC) को आपदा की सूचना प्रदान करे गा। मानि संसाधन विकास मंत्रालय
का आपदा प्रबंधन विभाग प्रावधकृ त पूिव-चेतािनी एजेंवसयों, विवभन्न नोडल मंत्रालयों एिं राज्य
सरकारों के साथ संपकव तथा समन्िय स्थावपत करे गा।
राष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रक्रया समन्िय
राष्ट्रीय स्तर पर, कें द्र सरकार के द्वारा आपदा-विवशष्ट अनुक्रक्रयाओं के समन्िय हेतु मुख्य
उत्तरदावयत्ि कु छ विवशष्ट मंत्रालयों को सौंपे गए हैं। क्रकसी आपदा की आशंका की वस्थवत में या
आपदा के दौरान अनुक्रक्रया का समन्िय NEC द्वारा क्रकया जाता है।
सारणी : राष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रक्रयाओं के समन्िय हेतु के न्द्रीय मंत्रालय
आपदा नोडल मंत्रालय /विभाग/एजेंसी
1 जैविक आपदाएं स्िास््य एिं पररिार कल्याण मंत्रालय (MInistry of
25 www.visionias.in ©Vision IAS
Health and Family Welfare: MoHFW)
2 रासायवनक आपदाएं और पयाविरण, िन एिं जलिायु पररितवन मंत्रालय (Ministry
औद्योवगक दुघवटनाएं
of Environment, Forest & Climate Change:
MoEFCC)
3 नागररक विमानन दुघवटनाएं नागररक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation:
MoCA)
4 चक्रिात, टोरनेडो और सुनामी गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA)
5 खानों में आपदाएं कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय (Ministry of Coal:
MoC, Ministry of Mines: MoM)
6 सूखा, ओलािृवष्ट, शीत लहर और कृ वष एिं क्रकसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of
पाला, कीट आक्रमण Agriculture and Farmers' Welfare: MoAFW)
7 भूकंप गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA)
8 बाढ़ गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA)
9 िनावि पयाविरण, िन एिं जलिायु पररितवन मंत्रालय (Ministry
of Environment, Forest & Climate Change:
MoEFCC)
10 भूस्खलन और वहमस्खलन गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA)
11 नावभकीय और रे वडयोलॉवजकल परमाणु ऊजाव विभाग, गृह मंत्रालय (Department of
(विक्रकरण संबंधी) आपात
Atomic Energy: DAE, MHA)
12 तेल ररसाि (ऑयल वस्पल्स) रक्षा मंत्रालय/इं वडयन कोस्ट गाडव (Ministry of Defence:
MoD/ Indian Coast Guard: ICG)
13 रे ल दुघवटनाएं रे ल मंत्रालय (Ministry of Railways: MoR)
14 सड़क दुघवटनाएं सड़क पररिहन और राजमागव मंत्रालय (Ministry of
Road Transport and Highways: MoRTH)
15 शहरी बाढ़ आिासन और शहरी कायव मंत्रालय ( Ministry of
Housing and Urban Affairs: MoHUA)
राहत उपाय
यह आिश्यक है क्रक आपदा प्रभावित क्षेत्र में यथाशीघ्र प्रथम अनुक्रक्रयाकतावओं (First
Responders) और राहत सामग्री की उपलब्धता सुवनवश्चत की जाए। प्रायैः ऐसा पाया गया है
26 www.visionias.in ©Vision IAS
क्रक आपदा की अिवस्थवत, प्रकृ वत तथा अपयावप्त क तैयाररयों के कारण उत्पन्न बाधाओं से राहत कायव
में अत्यवधक विलम्ब हो जाता है। एक-दूसरे के कायव-क्षेत्र के अवतव्यापन से बचने हेतु क्रकसी स्पष्ट
योजना के अभाि में तथा राहत के विवभन्न पहलुओं यथा आश्रय स्थलों, िस्त्रों, खाद्य-पदाथों या
औषवधयों की प्राथवमकता तय क्रकए वबना ही, एक-दूसरे से स्ितंत्र रूप से कायव कर रहे विवभन्न
संगठनों द्वारा क्रकये गए राहत कायव प्रायैः खवडडत तथा अवनयवमत होते हैं।
राहत के वलए न्यूनतम मानदंड के संबध
ं में NDMA द्वारा जारी क्रदशा-वनदेश
NDMA द्वारा राहत हेतु जारी न्यूनतम मानदंड संबंधी क्रदशा-वनदेशों में वनम्नवलवखत सवम्मवलत हैं:
राज्य तथा वजला प्रशासन को विद्यालयों, आंगनिाड़ी के न्द्रों जैसे ऐसे स्थानों की पहचान पहले से
कर लेनी चावहए वजनका उपयोग आपदा के दौरान राहत वशविर के रूप में क्रकया जा सके ।
टेंट/शौचालय/मूत्रालय आक्रद के प्रािधानों हेतु आपूर्नतकतावओं के साथ पूिव में ही समझौता ज्ञापन
(MoU) हस्ताक्षररत क्रकया जा सकता है।
सुभेद्य िगों यथा मवहलाओं, बच्चों, िृि व्यवक्तयों तथा विकलांगों के वलए विवशष्ट देखभाल की
व्यिस्था की जानी चावहए। वबजली की व्यिस्था के साथ प्रवत व्यवक्त 3.5 िगव मीटर क्षेत्र अिश्य
उपलब्ध कराया जाना चावहए।
पुरुषों तथा वस्त्रयों के वलए प्रवत क्रदन 2,400 क्रकलो कै लोरी युक्त भोजन की उपलब्धता सुवनवश्चत
की जानी चावहए। प्रवत व्यवक्त कम से कम 3 लीटर पेयजल आपूर्नत की व्यिस्था की जानी चावहए।
व्यवक्तगत स्ि्छता हेतु पयावप्त क जल की व्यिस्था सुवनवश्चत करने के साथ ही प्रत्येक कै म्प में
स्ि्छता स्तर को अिश्य बनाए रखा जाना चावहए। शौचालयों से वनकली नावलयों की क्रदशा
क्रकसी सतही जल स्रोत की ओर नहीं होनी चावहए।
27 www.visionias.in ©Vision IAS
सभी वशविरों में मोबाइल मेवडकल टीमों का वनयवमत दौरा होना चावहए तथा गभविती मवहलाओं
के वलए सुरवक्षत प्रसि की व्यिस्था की जानी चावहए।
वजला प्रशासन द्वारा विधिाओं को उनके पवत का मृत्यु प्रमाण-पत्र आपदा के पंद्रह क्रदनों के भीतर
वनगवत क्रकया जाना चावहए तथा 45 क्रदनों के भीतर आिश्यक वित्तीय सहायता की व्यिस्था की
जानी चावहए।
राहत वशविर अस्थायी होने चावहए तथा उस क्षेत्र में वस्थवत सामान्य होते ही उन्हें बंद कर क्रदया
जाना चावहए।
अविशमन तथा आपातकालीन सेिाएं (Fire and Emergency Services: FES)
क्रकसी भी आपदा के पश्चात के गोल्डन ऑिर में FES प्रथम अनुक्रक्रयाकतावओं (responders) में
से एक होती हैं तथा जान-माल की रक्षा में इनकी महत्िपूणव भूवमका होती है। FES की मुख्य
भूवमका आग की घटनाओं के दौरान अनुक्रक्रया करना होता है। अविशमन के अवतररक्त, FES अन्य
आपात वस्थवतयों यथा इमारत के ढहने, सड़क दुघवटनाओं, मानि तथा पशुओं के बचाि तथा अन्य
कई आपातकालीन वस्थवतयों में भी सहायता करती है।
ितवमान में राज्य, संघ शावसत प्रदेश तथा ULBs, FES का प्रबंधन करती हैं। यद्यवप उपकरणों के
स्तर, प्रकार तथा कमवचाररयों के प्रवशक्षण की बात की जाए तो इस हेतु कोई तय मानक उपलब्ध
नहीं हैं। राज्यों द्वारा की गई पहलों तथा FES के वलए उपलब्ध कराए गए धन की मात्रा के
अनुसार, प्रत्येक राज्य का अपना पृथक मानदडड है।
2.5.3. आपदा जोवखम शासन
(Disaster Risk Governance)
21िीं सदी के प्रथम दशक के मध्य से, शासन को सामान्यत: आपदा जोवखम न्यूनीकरण के आधार
के रूप में स्िीकार क्रकया गया। आपदा जोवखम शासन िह पिवत है वजसके अंतगवत सािवजवनक
प्रावधकरण, वसविल सेिक, मीवडया, वनजी क्षेत्र और वसविल सोसाइटी (नागररक समाज) आपदा
संबंधी जोवखमों के प्रबंधन एिं न्यूनीकरण हेतु विवभन्न स्तरों पर सहयोग करते हैं।
इसके वलए आपदाओं की रोकथाम और तैयारी हेतु उपलब्ध क्षमता और संसाधनों का पयावप्त क स्तर
सुवनवश्चत करने की आिश्यकता होती है। यह नागररकों के वलए ऐसे संस्थानों और प्रक्रक्रयाओं को
भी लागू करता वजनके पररणामस्िरूप उनके मध्य मतभेदों में मध्यस्थता की जा सके और िे अपने
वहतों को व्यक्त कर सकें तथा अपने कानूनी अवधकारों ि दावयत्िों का प्रयोग कर सकें ।
सेंडाई फ्रेमिकव के अनुसार आपदा जोवखम शासन, विवभन्न स्तरों पर आपदा जोवखम के प्रभािी
एिं कु शल प्रबंधन हेतु अवत महत्िपूणव है। सेंडाई फ्रेमिकव , आपदा जोवखम शासन के सुदढृ ीकरण
हेतु वनम्नवलवखत त्यों पर बल देता है:
o सभी क्षेत्रकों के मध्य तथा क्षेत्रकों के भीतर, आपदा जोवखम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना
और समेक्रकत करना। इसे सािवजवनक और वनजी, दोनों क्षेत्रकों का मागवदशवन करना चावहए तथा
भूवमकाओं और उत्तरदावयत्ि की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चावहए। आपदा जोवखम
पारदर्नशता में िृवि करने िाली प्रणावलयों एिं पहलों को प्रोत्सावहत क्रकया जाना चावहए।
o आर्नथक, सामावजक, स्िास््य और पयाविरणीय प्रत्यास्थता के सुदढृ ीकरण हेतु विवभन्न स्तरों
(स्थानीय से राष्ट्रीय) और समय-सीमाओं में आपदा जोवखम न्यूनीकरण रणनीवतयों और योजनाओं
का अंगीकरण और कायावन्ियन करना।
o विवभन्न स्तरों पर पहचाने गये जोवखमों से वनपटने हेतु आपदा जोवखम प्रबंधन क्षमता का आकलन
करना।
28 www.visionias.in ©Vision IAS
o सुरक्षा में िृवि करने िाले प्रािधानों के साथ उच्च स्तरीय अनुपालन सुवनवश्चत करने हेतु आिश्यक
तंत्र और प्रोत्साहनों को बढ़ािा देना।
o विवभन्न DM योजनाओं की प्रगवत की आिवधक समीक्षा एिं मूल्यांकन करना; DRR योजनाओं
पर संसद सदस्यों एिं संबंवधत अवधकाररयों सवहत संस्थागत िाद-वििाद को प्रोत्सावहत करना;
तथा वशकायत वनिारण तंत्रों की स्थापना करना।
o आपदा जोवखम प्रबंधन के तहत समुदाय के प्रवतवनवधयों को स्पष्ट भूवमकाएं और कायव सौंपना।
o राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर प्रासंवगक वहतधारकों से वमलकर बने सरकारी समन्िय मंचों की
स्थापना एिं सुदढृ ीकरण करना, जैसे क्रक राष्ट्रीय आपदा जोवखम न्यूनीकरण मंच और स्थानीय
आपदा जोवखम न्यूनीकरण मंच।
o प्रासंवगक कानूनों के वनमावण या संशोधन तथा बजट आिंटन के माध्यम से सांसदों और अन्य
वनिाववचत प्रवतवनवधयों के साथ आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु कायव करना।
o गुणित्ता मानकों के विकास को प्रोत्सावहत करना, जैसे आपदा जोवखम प्रबंधन हेतु प्रमाणपत्र और
पुरस्कार।
2.5.4. सामान्य वस्थवत की बहाली एिं बे ह तर पु न र्ननमाव ण
(Recovery and Build Back Better: BBB)
िैविक रूप से आपदा पश्चात् पुनस्थावपना और पुनिावस के प्रवत दृवष्टकोण अब बेहतर पुनर्ननमावण की
ओर संकेंक्रद्रत हो गया है। समुदायों को आपदा प्रत्यास्थ बनाने हेतु, सामान्य वस्थवत की बहाली, पुनिावस
और पुनर्ननमावण चरण को ‘बेहतर पुनर्ननमावण’ तथा आपदा जोवखम न्यूनीकरण को विकास उपायों में
सवम्मवलत करने के एक अिसर के रूप में देखा जाता है। भारत में पुनर्ननमावण एिं सामान्य वस्थवत की
बहाली के प्रवत दृवष्टकोण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीवत 2009 द्वारा वनदेवशत होता है। इस नीवत के
अनुसार:
पुनर्ननमावण की प्रक्रक्रया व्यापक होनी चावहए। आपदा प्रत्यास्थ विशेषताओं का संयोजन 'BBB’ के
वलए मागवदशवक वसिांत होगा।
पुनर्ननमावण योजना और मकानों की वड़ाइसनग िस्तुतैः सरकार, प्रभावित समुदाय, गैर-सरकारी
संगठनों और कॉपोरे ट क्षेत्रकों को सवम्मवलत करने िाली सहभावगतापूणव प्रक्रक्रया होनी चावहए।
यद्यवप िरीयता मकान मावलक द्वारा वनमावण करिाने संबंधी विकल्प को दी जाएगी, तथावप गैर-
सरकारी संगठनों और कॉपोरे ट क्षेत्रकों की भागीदारी को प्रोत्सावहत क्रकया जाएगा।
आिश्यक सेिाएं, सामावजक अिसंरचना और मध्यिती आश्रय स्थलों/राहत वशविरों की यथाशीघ्र
स्थापना की जाएगी।
अत्यवधक आपदा प्रिण क्षेत्रों में पुनर्ननमावण की योजना सामान्य वस्थवत के दौरान तैयार की जानी
चावहए। इस योजना में विवभन्न वहतधारकों के परामशव से स्थापत्य संबंधी (architectural) तथा
संरचनात्मक (structural) वडजाइनों को भी सवम्मवलत क्रकया जा सकता है।
पुनबवहाली प्रक्रक्रया (Recovery Process)
UNISDR (2009) के अनुसार, पुनबवहाली अथिा सामान्य वस्थवत की बहाली से तात्पयव पुनस्थावपना
और आपदा प्रभावित समुदायों को प्राप्त क सुविधाओं, आजीविका और रहन-सहन की वस्थवतयों में सुधार
से है। इसमें आपदा जोवखम कारकों को कम करने के प्रयास सवम्मवलत हैं।
पुनबवहाली के वनम्नवलवखत तीन चरणों के अंतगवत समुवचत नीवतयों एिं कायवक्रमों का वनमावण तथा
कायावन्ियन क्रकया जाता है:
(a) प्रारं वभक (b) मध्यािवधक, और (c) दीघाविवधक।
29 www.visionias.in ©Vision IAS
पुनबवहाली के चरण
पुनबवहाली समयािवध संवक्षप्त क वििरण
चरण
प्रारं वभक 3-18 माह कायों के बदले नकदी; बा़ार,िावणज्य तथा व्यापार का
पुनैः आरम्भ होना, सामावजक सेिाओं की पुनस्थावपना;
माध्यवमक तथा अस्थायी आश्रय-स्थलों का वनमावण
मध्यािवधक 5 िषव तक (प्रारं वभक पररसंपवत्तयों और आजीविकाओं के वलए पुनबवहाली
पुनबवहाली के साथ-साथ) योजनाएाँ; आिासों, अिसंरचना, सािवजावनक भिनों और
सांस्कृ वतक विरासत भिनों हेतु पुनर्ननमावण योजनाएाँ
दीघाविवधक 10 िषव के भीतर विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ कायावन्ियन क्रकया
जाता है; अिसंरचना सुदढ़ृ ीकरण; पयाविरणीय, नगरीय एिं
क्षेत्रीय वनयोजन
पुनबवहाली के दौरान उठाये जाने िाले कदम
पुनबवहाली प्रक्रक्रया के दौरान उठाये जाने िाले प्रमुख कदम वनम्नानुसार हैं:
आपदा पश्चात् की जरूरतों का आकलन: इसमें सरकार के नेतृत्ि में एिं लोकोपकारी अनुक्रक्रया
एजेंवसयों की सहायता से क्षवत का वििसनीय आकलन सवम्मवलत है। सभी क्षेत्रों में हुई क्षवत,
आर्नथक हावन और जरूरतों के वलए गुणात्मक और मात्रात्मक बेसलाइन मूल्यांकन क्रकया जाना
चावहए।
BBB हेतु एक विजन विकवसत करना: विशेषज्ञों, नागररक समाज और प्रमुख वहतधारकों के साथ
व्यापक विचार-विमशव क्रकया जाना चावहए तथा सहमवत बनाई जानी चावहए।
विकास लक्ष्यों के साथ BBB की सम्बिता सुवनवश्चत करना: सरकार के व्यापक दीघवकावलक
विकास लक्ष्यों के साथ ररकिरी वि़न के संरेखण हेतु शीषव स्तर पर चचाव-पररचचाव की जानी
चावहए।
ररकिरी वि़न में प्रत्यास्थता का संयोजन: इसमें आपदा प्रवतरोधी भौवतक पुनबवहाली पर
परामशव, लैंवगक और समानता के मुद्दों को संबोवधत करना, सुभेद्यता न्यूनीकरण आक्रद सवम्मवलत
हैं।
सभी क्षेत्रकों में पुनबवहाली को संतवु लत करना: सािवजवनक और वनजी क्षेत्र के कायवक्रमों में संतुलन
होना चावहए। प्रभावित जनसंख्या के प्रवत संिेदनशीलता प्रदर्नशत करते हुए अिसंरचना
पुनर्ननमावण को प्राथवमकता प्रदान की जानी चावहए।
पुनबवहाली हेतु क्षेत्रकों को प्राथवमकता प्रदान करना: आिास, जल और स्ि्छता, शासन,
पररिहन, विद्युत, संचार, अिसंरचना, पयाविरण, आजीविका, पयवटन, सामावजक सुरक्षा, स्िास््य
और वशक्षा जैसे विवभन्न क्षेत्रकों का सापेवक्षक महत्ि वनधावररत क्रकया जाना चावहए।
पुनर्ननमावण (Reconstruction)
दीघवकावलक पुनबवहाली प्रयास को आपदा क्षेत्र (क्षेत्रों) की सामावजक-आर्नथक व्यिहायवता को
पुनर्निकवसत और पुनस्थाववपत करने पर कें क्रद्रत होना चावहए। पुनर्ननमावण चरण को सरकारों (राज्य और
कें द्र) और अन्य एजेंवसयों द्वारा समय और संसाधनों की पयावप्त क प्रवतबिता की आिश्यकता होती है। इन
पुनर्ननमावण प्रयासों में सवम्मवलत हैं:
आपदा द्वारा क्षवतग्रस्त सािवजवनक अिसंरचनाओं और सामावजक सेिाओं का पुनर्ननमावण, वजसे
दीघाविवध में पूरा क्रकया जा सकता है।
क्षवतग्रस्त हो चुके आिासों को प्रवतस्थावपत करने हेतु पयावप्त क आिासों की पुनस्थावपना।
आपदा के कारण नष्ट रोजगारों/आजीविका की पुनस्थावपना।
आपदा क्षेत्रों के आर्नथक आधार की पुनस्थावपना।
30 www.visionias.in ©Vision IAS
पुनिावस (Rehabilitation)
पुनिावस को प्रभावित जनसंख्या की सहायता के उद्देश्य से अिसंरचना और सेिाओं के संस्थागत सुधार
और उन्नवत की रणनीवत के रूप में पररभावषत क्रकया जाता है। सामान्यत:, पुनिावस पैकेज में क्षवतग्रस्त
भौवतक और मनोिैज्ञावनक अिसंरचना के संपूणव पुनर्ननमावण के साथ ही साथ् प्रभावित क्षेत्र के लोगों का
आर्नथक और सामावजक पुनिावस भी सवम्मवलत है। पुनिावस का िगीकरण वनम्नवलवखत रूप में क्रकया
गया है:
भौवतक पुनिावस (Physical Rehabilitation)
यह पुनिावस का अवत महत्िपूणव पहलू है। इसके अंतगवत वनम्नवलवखत उपाय सवम्मवलत हैं:
o भिनों, रे लमागों, सड़कों, संचार नेटिकव , जलापूर्नत, विद्युत आक्रद जैसी भौवतक अिसरं चना
का पुनर्ननमावण।
o जल-विभाजक प्रबंधन, नहर द्वारा ससचाई, सामावजक िावनकी, फसल वस्थरीकरण, िैकवल्पक
शस्यन प्रौद्योवगक्रकयां, रोजगार सृजन, रोजगार जनक और पयाविरण संरक्षण से संबंवधत
अल्पकावलक और दीघवकावलक रणनीवतयां।
o कृ वष, वशल्पकारी कायव और पशुपालन की पुनबवहाली।
o सवब्सडी के वलए पयावप्त क प्रािधान, भूवम उपयोग योजना का अनुपालन, बाढ़ के मैदानों को
विवभन्न ़ोनो में िगीकृ त करना, गैर-क्षवतग्रस्त मकानों की रे रोक्रफटटग या सुदढृ ीकरण और
मॉडल घरों का वनमावण करना।
स्थानान्तरण भौवतक पुनिावस प्रक्रक्रया का अत्यवधक संिद े नशील भाग है और यह सुवनवश्चत क्रकया
जाना चावहए क्रक पुनिावस नीवत आिश्यकता आधाररत कारकों से संचावलत हो न क्रक असम्बि
कारकों से। पुनिावस प्रयासों में वनम्नवलवखत पर विचार क्रकया जाना चावहए:
o जहााँ तक संभि हो, वद्वतीयक विस्थापन से बचना चावहए।
o प्रभावित समुदायों की सहमवत प्राप्त क करनी चावहये।
o भूवम अवधग्रहण प्रक्रक्रया स्पष्ट रूप से पररभावषत की जानी चावहए।
o आगे बढ़ने से पहले शहरी/ग्रामीण भूवम-उपयोग योजना पर विचार क्रकया जाना चावहए।
o वस्थवत के अनुरूप स्थानांतरण पैकेज प्रदान क्रकया जाना चावहए।
o जहां तक संभि हो, सुवनवश्चत क्रकया जाना चावहए क्रक पुनिावस स्थल विस्थावपतों की
आजीविका के स्रोतों के वनकट हो।
प्रश्न: बड़ी पररयोजनाओं के वनयोजन के समय मानि बवस्तयों का पुनिावस एक महत्िपूणव पाररवस्थवतक
संघात (environmental impact) है, वजस पर सदैि वििाद होता है। विकास की बड़ी पररयोजनाओं
के प्रस्ताि के समय इस संघात को कम करने के वलए सुझाए गए उपायों पर चचाव कीवजए। (UPSC,
2016)
सामावजक पुनिावस (Social Rehabilitation)
सामावजक पुनिावस भी आपदा पुनिावस का एक महत्िपूणव भाग है। आपदाओं के प्रभाि से बचने के
वलए कारीगरों, बुजुगों, अनाथों, अके ली मवहलाओं और छोटे बच्चों जैसे सुभेद्य समूहों के वलए
विशेष सामावजक सहायता की आिश्यकता होती है। पुनिावस योजना में ऐसे घटक को शावमल
क्रकया जाना चावहए जो इस त्य की उपेक्षा न करें क्रक पीवड़तों को पूरी तरह से अपररवचत
सामावजक पररिेश में पुन: समाजीकरण और समायोजन की संपण ू व प्रक्रक्रया से गुजरना पड़ता है।
अतैः, इस प्रकार के पुनिावस में विवभन्न गवतविवधयां सवम्मवलत हैं जैसे क्रक:
o शैवक्षक गवतविवधयों का पुनरुत्थान: क्रकसी बड़ी आपदा में शैवक्षक सुविधाओं को अत्यवधक
क्षवत पहुंच सकती है वजससे बच्चों पर काफी दबाि पड़ सकता है। इसवलए, बच्चों को ऐसी
वस्थवत से उबरने एिं सामना करने हेतु सक्षम बनाने में वनम्नवलवखत चरण सहायक होंगे:
वशक्षकों और बच्चों को वनयवमत परामशव (काउं ससलग) देना।
31 www.visionias.in ©Vision IAS
बच्चों को स्कू लों में वनयवमत रूप से उपवस्थत रहने हेतु प्रोत्सावहत करना।
ब्चे को लेखन सामग्री और अभ्यास-पुवस्तकाएं उपलब्ध कराना।
स्कू ल में सामान्य वस्थवत की बहाली से संबंवधत सभी गवतविवधयों में बच्चों की भागीदारी
सुवनवश्चत करना।
अनुकूल दृवष्टकोण विकवसत करने का प्रयास करना वजससे क्रक छात्र स्ि-विकास में
सकारात्मक भूवमका वनभा सकें ।
ग्राम स्तर पर वशक्षा सवमवतयों की स्थापना करना।
वशक्षा गवतविवधयों से संबंवधत प्रकायों के सुचारु संचालन हेतु स्थानीय समूहों की
पहचान करना।
o बुजग
ु ों, मवहलाओं और बच्चों का पुनिावस: क्रकसी बड़ी आपदा के पश्चात् बुजुगव, मवहलाएं और
बच्चे सिाववधक सुभेद्य होते हैं। अतैः वनम्नवलवखत उपायों से उनके पुनिावस में सहायता वमलेगी:
बुजुगों, मवहलाओं और बच्चों के पुनिावस हेतु सुपररवचत पररिेशों की पहचान करना।
वनरावश्रतों, विधिाओं और अनाथ बच्चों को उनके विस्तृत पररिार से जोड़ने का प्रयास
करना, यक्रद यह संभि नहीं है तो पालक पररिारों (foster families) की पहचान
करना।
मवहलाओं और बच्चों का मानवसक स्िास््य बेहतर करने हेतु वनयवमत परामशव
(काउं ससलग) की व्यिस्था करना।
मवहलाओं को आर्नथक रूप से आत्मवनभवर बनाने के वलए विवभन्न प्रवशक्षण कायवक्रम
आरं भ करना।
मवहलाओं और बच्चों के वलए दीघाविवधक पुनिावस पैकेज में स्िास््य, पोषण और
स्ि्छता पर ध्यान देना।
आंगनिाड़ी के न्द्रों (डे के यर सेंटर) और िृिाश्रमों को यथाशीघ्र सक्रक्रय/पुनैःसक्रक्रय करना।
प्रत्येक गांि में कम से कम एक बहु-उद्देश्यीय सामुदावयक कें द्र स्थावपत करना।
ब्लॉक स्तर पर आिासीय बावलका गृहों का वनमावण करने का प्रयास करना।
अनाथों और बच्चों के कौशल उन्नयन हेतु व्यािसावयक प्रवशक्षण वशविरों की स्थापना
करना।
स्ियं सहायता समूहों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
आर्नथक पुनिावस (Economic Rehabilitation)
आजीविका पुनस्थावपना तथा व्यापार एिं िावणज्य की वनरं तरता सुवनवश्चत करना आर्नथक पुनिावस
के प्रमुख घटक हैं। आपदा के कारण आिश्यक पररसंपवत्तयों के विनाश या क्षवत से आजीविका के
अिसर गंभीर रूप से बावधत होते हैं; इसके पररणामस्िरुप लोग सामान्य आय सृवजत करने िाली
गवतविवधयों में संलि नहीं हो पाते हैं; िे हतोत्सावहत एिं मानिीय सहायता पर आवश्रत हो जाते
हैं। आर्नथक वस्थवत की पुनबवहाली वनम्नवलवखत वबन्दुओं पर आधाररत होनी चावहए:
o ितवमान आजीविका रणनीवतयों के विश्लेषण और व्यिसायों की संधारणीयता पर।
o ितवमान और भविष्टय के जोवखमों के व्यापक विश्लेषण पर।
o प्रभावित पररिारों की सुभेद्यता पर।
o कौशल और ज्ञान सवहत बाह्य प्रभािों और संस्थानों तक संपकव (सलके ज) सुवनवश्चत करने पर।
o कायवशील बाजारों तक पहुंच पर।
मनोिैज्ञावनक पुनिावस (Psychological Rehabilitation)
आपदा पुनिावस का एक अन्य महत्िपूणव आयाम मनोिैज्ञावनक पुनिावस है। पीवड़तों के मनोविज्ञान
को समझना अत्यंत संिेदनशील मुद्दा है। इनके साथ बहुत ही सािधानी एिं सहानुभूवतपूिक व
व्यिहार क्रकया जाना चावहए। पीवड़तों द्वारा संबंवधयों और वमत्रों को खोने के मनोिैज्ञावनक
आघात और आपदा की घटना के सदमे का घाि भरने में लंबा समय लग सकता है। यह समय
प्राय: आपदा प्रबंधन वहतधारकों द्वारा अनुमावनत अिवध से अवधक होता है। इस प्रकार, तनाि
प्रबंधन हेतु परामशव (काउं ससलग) प्रदान करना आपदा पुनिावस योजना का एक सतत भाग होना
चावहए। वनम्नवलवखत वबन्दुओं पर अवधक ध्यान देने का प्रयास करना चावहए:
o मनो-वचक्रकत्सीय स्िास््य कायवक्रम।
o व्यािसावयक मनोवचक्रकत्सा (Occupational therapy)।
32 www.visionias.in ©Vision IAS
o वडिीकफग और रॉमा के यर (Debriefing and trauma care)।
o आपदा प्रभावित लोगों की परं परा, मूल्यों, मानदंडों, वििासों और प्रथाओं पर।
2.5.5. क्षमता विकास
(Capacity Development: CD)
क्षमता विकास में संस्थानों, तंत्रों और सभी स्तरों पर सभी वहतधारकों की क्षमताओं को सशक्त बनाना
सवम्मवलत है। आपदा जोवखम प्रबंधन के क्षेत्र में, सेंडाई फ्रेमिकव विवभन्न स्तरों पर पहचाने गए
जोवखमों से वनपटने के वलए संस्थानों, सरकारों और समुदायों की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासवनक
क्षमताओं को बढ़ाने की आिश्यकता पर बल देता है।
क्षमता विकास में सवम्मवलत संस्थाएं
राष्टरीय आपदा प्रबंधन संस्थान का एक प्रमुख उत्तरदावयत्ि अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ
साझेदारी कर क्षमता विकास करना है। विवभन्न राज्यों में ऐसे कई प्रवतवष्ठत संस्थान हैं जो आपदा
प्रबंधन हेतु प्रवशक्षण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, सभी प्रशासवनक प्रवशक्षण संस्थानों, पुवलस
अकादवमयों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, CAPF के पांच प्रवशक्षण
कें द्र (BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB) और NDRF अकादमी, नागपुर आपदा प्रबंधन
संबंधी कौशल विकवसत करने में सिाववधक महत्िपूणव भूवमका वनभाएंगे। क्षेत्रीय और स्थानीय
आिश्यकताओं के अनुसार ितवमान संस्थानों की क्षमता का उन्नयन क्रकए जाने तथा और अवधक
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की भी आिश्यकता है।
o राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर
नागपुर वस्थत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) अकादमी, आपदा प्रबंधन में NDRF और
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) बटावलयनों, नागररक सुरक्षा स्ियंसेिकों और SAARC
देशों के आपदा अनुक्रक्रया कमवचाररयों को उच्च स्तरीय प्रवशक्षण प्रदान करने िाला प्रमुख
संस्थान है। राष्ट्रीय नागररक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर का NDRF अकादमी में विलय
कर क्रदया जाएगा। यह अकादमी NDRF, SDRF के कमवचाररयों और अन्य वहतधारकों को
क्षवतग्रस्त संरचना संबंधी खोज और बचाि (Collapsed Structure Search &
Rescue: CSSR), मेवडकल फस्टव ररस्पॉन्डर (MFR), बाढ़ से बचाि, डीप डाइसिग,
भूस्खलन, पहाड़ों में फं से लोगों का बचाि और रासायवनक, जैविक, रे वडयोलॉवजकल और
नावभकीय (CBRN) आपात संबंधी विषयों में प्रवशक्षकों के प्रवशक्षण (ToT) और मास्टर
रेनर (MoT) हेतु पाठ्यक्रम संचावलत करे गी।
स्थानीय वनकायों का क्षमता विकास
स्थानीय नेतृत्ि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में महत्िपूणव भूवमका वनभा सकता है। पंचायतों और
शहरी स्थानीय वनकायों के वनिाववचत नेताओं और अवधकाररयों को विवभन्न प्रकार के संकटों से
वनपटने, आपदा तैयारी में योगदान करने, उपलब्ध चेतािवनयों का उवचत उपयोग करने, खोज,
बचाि, राहत, वचक्रकत्सा सहायता जैसे कायों को आयोवजत करने और क्षवतपूर्नत का आकलन करने
के वलए प्रवशवक्षत क्रकया जाना चावहए। उन्हें आपदा पश्चात् समुवचत पुनिावस की जरूरतों की ठोस
समझ भी होनी चावहए। स्थानीय वनकायों की वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता का
विकास क्रकया जाना चावहए। राज्य स्तरीय प्रवशक्षण संस्थानों (ATI, SIDM और अन्य) द्वारा
ग्रामीण और शहरी स्थानीय वनकायों के क्षमता विकास हेतु आिश्यकता-आधाररत प्रवशक्षण
कायवक्रम (need-based training programs) विकवसत क्रकए जाएंगे।
33 www.visionias.in ©Vision IAS
समुदायों को प्रवशक्षण (Training Communities)
चूाँक्रक समुदाय, आपदा के प्रथम अनुक्रक्रयाकताव होते हैं, अतैः उनकी क्षमता का संिधवन क्रकया जाना
चावहए। समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाना क्षमता विकास प्रक्रक्रया का एक महत्िपूणव वहस्सा है।
सेंडाई फ्रेमिकव , आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर नागररक समाज, समुदायों और स्ियंसेिकों के ज्ञान
में िृवि करने की आिश्यकता का उल्लेख करता है। जागरूकता, संिेदीकरण, अनुकूलन तथा
समुदायों एिं समुदाय के नेतृत्िकतावओं के कौशल विकास को वनवश्चत रूप से क्षमता वनमावण में
सवम्मवलत क्रकया जाना चावहए।
प्रश्नैः विपदा पूिव (pre-disaster) प्रबंधन के वलए संिद
े नशीलता (vulnerability) ि जोवखम वनधावरण
(risk assessment) क्रकतना महत्िपूणव है? प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में क्रकन
मुख्य वबन्दुओं पर ध्यान देंग?
े (UPSC, 2013)
34 www.visionias.in ©Vision IAS
अध्याय-3
3. भारत में प्राकृ वतक सं क ट
(Natural Hazards in India)
3.1. भारत: सु भे द्य ता पररदृ श्य
(India: Vulnerability Profile)
भारत विि के दस सिाववधक आपदा प्रिण देशों में से एक है। यह अपनी विवशष्ट भू-जलिायिीय
तथा सामावजक-आर्नथक पररवस्थवतयों के कारण बहुत सी प्राकृ वतक एिं मानि-वनर्नमत आपदाओं
के प्रवत सुभेद्य है। भारत के 36 राज्यों ि कें द्र शावसत प्रदेशों में से 27 आपदा प्रिण हैं।
देश के पांच अलग-अलग क्षेत्रों अथावत् वहमालयी क्षेत्र, जलोढ़ मैदानों, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पहाड़ी
भागों और तटीय क्षेत्र की अपनी विवशष्ट समस्याएं हैं। एक ओर जहां वहमालयी क्षेत्र में भूकंप तथा
भूस्खलन जैसी आपदाओं की प्रिणता है िहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र लगभग प्रवत िषव बाढ़ से
प्रभावित होता है। देश का मरुस्थलीय भाग सूखे और अकाल से प्रभावित होता है जबक्रक तटीय
क्षेत्रों में चक्रिातों तथा तूफानों की अवधक सम्भािना होती
है।
o 58.6 प्रवतशत भूभाग, मध्यम से अत्यवधक उच्च तीव्रता िाले भूकंपों के प्रवत प्रिण है।
o इसके भूवम-क्षेत्र का 40 वमवलयन हेक्टेयर (12%) से अवधक क्षेत्र, बाढ़ों तथा नक्रदयों द्वारा
अपरदन के प्रवत प्रिणता रखता है।
o 7,516 क्रक.मी. लंबे समुद्र तट में से लगभग 5,700 क्रक.मी. चक्रिात तथा सुनामी के प्रवत
प्रिण हैं।
o इसके कृ वष योग्य क्षेत्र का 68 % भाग सूखे के प्रवत सुभद्य
े है।
o इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा वहमस्खलन का जोविम रहता है।
o रासायवनक, जैविक, रे वडयोलॉवजकल और नावभकीय (CBRN) आपदाओं/आपात-वस्थवतयों
के प्रवत सुभेद्यता भी विद्यमान है।
35 www.visionias.in ©Vision IAS
सुभद्य
े समूहों के अंतगवत िृि, मवहलाएं, बच्चे (विशेषकर वनरावश्रत मवहलाएं और अनाथ बच्चे) तथा
क्रदव्यांग व्यवक्त अपेक्षाकृ त उच्च जोवखमों के प्रवत अनािररत होते हैं।
प्राकृ वतक कारकों के अवतररक्त मानि-प्रेररत गवतविवधयां, जैस-े बढ़ता जनसांवख्यकीय दबाि,
वबगड़ती पयाविरणीय पररवस्थवतयां, िनोन्मूलन, अिैज्ञावनक विकास, दोषपूणव कृ वष ि चराई
पिवतयां, अवनयोवजत शहरीकरण, नक्रदयों पर बड़े-बड़े बांधों का वनमावण आक्रद भी देश में
आपदाओं के प्रभाि तथा आिृवत्त में िृवि के वलए उत्तरदायी हैं। भिन वनमावण सामग्री एिं
प्रौद्योवगकी संिधवन पररषद (Building Material and Technology Promotion Council:
BMTPC) ने भारत का सुभेद्यता एटलस प्रकावशत क्रकया है।
आपदाओं के कारण आर्नथक हावन
विि बैंक के अनुसार, आपदाओं के कारण GDP के 2% की आर्नथक हावन होती है।
3.2. प्राकृ वतक आपदाएं
(Natural Disasters)
3.2.1. भू कं प (Earthquake)
भूकंप क्या है?
भूकंप भू-पटल या भूपपवटी का
आकवस्मक कं पन है। भूकंप का प्रभाि
आकवस्मक होता है और इसका
पहले से कोई संकेत भी प्राप्त क नहीं
होता है, वजससे इसकी भविष्टयिाणी
करना असंभि हो जाता है।
भूकंप के कारण
भूकंप, मैंटल के ऊपर गवतशील
प्लेटों की सीमाओं पर हुए संचलनों
के कारण आता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे के संपकव में आती हैं, तो पपवटी पर दबाि बढ़ता है। इन
दबािों को प्लेटों की सीमाओं पर होने िाले संचलन के प्रकार के अनुसार िगीकृ त क्रकया जाता है:
o प्लेटों के विपरीत क्रदशा में गवत के कारण उत्पन्न सखचाि (अपसारी सीमा पर),
o प्लेटों की एक-दूसरे की ओर गवत के कारण उत्पन्न दबाि (अवभसारी सीमा पर) और
o प्लेटों के बीच एक-दूसरे के सापेक्ष क्षैवतज गवत से उत्पन्न घषवण (संरक्षी सीमा पर)
36 www.visionias.in ©Vision IAS
प्लेट की सीमाओं पर दबाि के िे क्षेत्र, जो वखसकने या विखंवडत होने के कारण संवचत ऊजाव मुक्त
करते हैं, ‘भ्रंश (faults)’ कहलाते हैं। ऐसे में भ्रंश पर एक दरार उत्पन्न होती है और चट्टान अपने
स्ियं के प्रत्यास्थ दबािों के अधीन तब तक गवत करती रहती है जब तक दबाि मुक्त नहीं हो
जाता। भ्रंश दरारों के कारण उत्पन्न होने िाले कम्पनों को भूकंपीय तरं गें (seismic waves) कहा
जाता है।
भूकंप को दो विवशष्टतया वभन्न पैमानों का प्रयोग करके मापा जा सकता है। ये भूकंप के पररमाण
(ररक्टर स्के ल द्वारा) तथा तीव्रता (मके ली स्के ल द्वारा) की जानकारी देते हैं। हालांक्रक, कु छ
िैज्ञावनक भूकंपों की भविष्टयिाणी करने की क्षमता का दािा करते हैं तथावप ऐसी आकवस्मक
घटनाओं की सही ि सटीक भविष्टयिाणी अभी भी संभि नहीं हैं।
भारत में भूकंप का जोवखम
विगत 15 िषों की अिवध में छह बड़े भूकंपों ने भारत के विवभन्न वहस्सों को प्रभावित क्रकया है।
भूकंप के जोवखम में िृवि का कारण विकास गवतविवधयों में आयी तेजी है। यह तेजी शहरीकरण,
आर्नथक विकास तथा भारत की अथवव्यिस्था के िैिीकरण द्वारा प्रेररत है। भारत में बहुत अवधक
आबादी िाले शहर हैं और इन शहरों में हुए वनमावण भूकंप-रोधी नहीं हैं। विवनयामक तंत्र कमजोर
हैं, ऐसे में इनमें से क्रकसी भी शहर में आने िाला भूकंप एक बड़ी आपदा में पररिर्नतत हो जाएगा।
भारत में भूकंपों का वितरण स्िरूप
भारत प्रमुख रूप से ‘अल्पाइन-वहमालयी बेल्ट (Alpine - Himalayan Belt)’ पर वस्थत है। यह
बेल्ट िह रे खा है वजसके साथ इं वडयन प्लेट यूरेवशयन प्लेट से वमलती है। एक अवभसरण प्लेट होने
के कारण भारतीय प्लेट 5 से.मी प्रवत िषव की दर से यूरेवशयन प्लेट के नीचे अितवलत हो रही है।
यह संचलन अत्यवधक तनाि उत्पन्न करता है वजससे चट्टानों में ऊजाव संवचत होती रहती है और
यह समय-समय पर भूकंप के रूप में वनमुवक्त होती है।
37 www.visionias.in ©Vision IAS
भूकंप की संभावित अवधकतम तीव्रता के अनुसार, भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों (seismic
zones) में विभावजत क्रकया गया है। इनमें से ़ोन V सबसे अवधक सक्रक्रय है। इसमें संपण
ू व
पूिोत्तर भारत, वबहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड, वहमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात
तथा अंडमान ि वनकोबार द्वीप समूह सवम्मवलत हैं। संपूणव वहमालयी क्षेत्र को ररक्टर स्के ल पर
8.0 से अवधक पररमाण के उच्च तीव्रता िाले भूकंपों के प्रवत सुभेद्य माना जाता है। भारत का
अवधकांश क्षेत्र ़ोन III और ़ोन II में आता है।
भूकंप के पररणाम
प्राथवमक क्षवत: मानि बवस्तयों, भिनों, संरचनाओं ि अिसंरचनाओं, विशेष रूप से पुलों, फ्लाई-
ओिरों, रे ल की पटररयों, पानी की टंक्रकयों, पाइपलाइनों और विद्युत उत्पादन इकाइयों आक्रद को
क्षवत पहुाँचती है। भूकंप के पश्चिती झटके (Aftershocks) पहले से ही कमजोर हो चुकी
संरचनाओं को बहुत अवधक क्षवत पहुंचा सकते हैं।
भूकंप जोनों के अंतगवत भौगोवलक क्षेत्र
भूकंप जोन भौगोवलक क्षेत्र का प्रवतशत
II 41.40
III 30.40
IV 17.30 58.6%
V 10.90
वद्वतीयक प्रभािों में आग, बांध की विफलता तथा भूस्खलन (जो जल वनकायों के मागों को अिरुि
कर सकते हैं, वजससे बाढ़ आ सकती है), सुनामी, रासायवनक ररसाि, संचार सुविधाओं का बावधत
होना, मानि जीिन की क्षवत आक्रद शावमल हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सािवजवनक स्िास््य प्रणाली,
पररिहन सुविधाओं एिं जल-आपूर्नत व्यिस्था को भी भारी क्षवत पहुाँचती है।
भूकंप के तृतीयक प्रभािों में पोस्ट-रॉमेरटक तनाि विकार, दीघवकावलक मनोिैज्ञावनक समस्याएं,
आजीविका की हावन, स्थानांतरण संबंधी मुद्दों के कारण सामावजक पूंजी की क्षवत आक्रद सवम्मवलत
हैं।
भूकंप के संकट का शमन
चूंक्रक भूकंप अवधकांश पररिहन ि संचार संपकों को भी ध्िस्त कर देता है इसवलए पीवड़तों को
समय पर राहत प्रदान करना करठन हो जाता है। भूकंप को रोक पाना संभि नहीं है; इसवलए
आपदा के उपचारात्मक उपायों के स्थान पर इससे वनपटने की तैयारी तथा शमन के उपायों पर
बल देना ही सिवश्रष्ठ े विकल्प बचता है।
सुभेद्य क्षेत्रों में वनयवमत वनगरानी तथा जनता में सूचना के तीव्र प्रसार हेतु भूकंप वनगरानी कें द्र
(भूकंप-विज्ञान कें द्र) स्थावपत क्रकये जाने चावहए। ितवमान में, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान कें द्र
(National Centre for Seismology: NCS) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो
संपूणव देश और इसके आस-पास की भूकंपीय गवतविवधयों की वनगरानी हेतु उत्तरदायी है।
38 www.visionias.in ©Vision IAS
प्रवतकू ल प्रभािों को कम करने के वलए लोगों के बीच सुभेद्यता जोवखम की जानकारी का प्रसार
करने के साथ-साथ देश की सुभद्ये ता का मानवचत्रण भी क्रकया जाना चावहए।
वनयोजन: भारतीय मानक ब्यूरो (The Bureau of Indian Standards) ने भूकंप-रोधी
सुरवक्षत भिनों के वनमावण हेतु वनमावण संवहता तथा क्रदशा-वनदेश जारी क्रकए हैं। वनधावररत उप-
कानूनों के अनुसार भिन वनमावण से पूिव नगरपावलका द्वारा भिन वनमावण योजना की जांच की
जानी चावहए।
महत्िपूणव भिनों जैसे अस्पतालों, स्कू लों और फायर स्टेशनों को रे रोक्रफटटग तकनीकों द्वारा बेहतर
बनाये जाने की आिश्यकता
है।
सामुदावयक तैयारी एिं
भूकंप के कारणों तथा
विशेषताओं के साथ-साथ
तैयारी संबंधी उपायों पर
सािवजवनक वशक्षा महत्िपूणव
है। इसे समुदाय के वलए
जागरूकता एिं प्रवशक्षण
कायवक्रमों के माध्यम से एिं
स्कू लों, मॉलों, अस्पतालों
आक्रद द्वारा आपदा प्रबंधन
योजना तैयार करके क्रकया
जा सकता है। साथ ही, इस
उद्देश्य के वलए मोक विल्स
और वपछले भूकंपों से वमली
सीख पर दस्तािेज तैयार कर उन्हें व्यापक रूप से प्रसाररत करने का सहारा भी वलया जा सकता
है।
योजनाबि वनमावण: वनमावण से पूिव मृदा के प्रकार का विश्लेषण क्रकया जाना चावहए। नरम वमट्टी
पर संरचनाओं के वनमावण से बचा जाना चावहए। नक्रदयों के क्रकनारे जलोढ़ मृदा पर वनर्नमत भिनों
में भी नरम मृदा पर बनी
संरचनाओं जैसी समस्याएं
आ सकती हैं, अतैः ऐसे
स्थानों पर भी वनमावण से
बचना चावहए।
स्िदेशी विवधयों के उपयोग
को प्रोत्सावहत करना -
स्िदेशी भूकंप-रोधी घर जैसे
गुजरात के क्छ क्षेत्र में
भोंगा, जम्मू और कश्मीर
की धज्जी दीिारी की
इमारतें, वहमाचल प्रदेश के
ईंटों से भरे गये लकड़ी के
ढांचों िाले वनमावण (brick-
nogged wood frame constructions) और असम में बांस से बने एकरा (ekra) वनमावण
आक्रद आधुवनक रीन्फोस्डव सीमेंट कं क्रीट (RCC) के भिनों द्वारा तेजी से प्रवतस्थावपत क्रकये जा रहे
हैं। साथ ही इन RCC भिनों का वनमावण प्रायैः भूकंप-रोधी उपायों को समाविष्ट क्रकए वबना और
भिन वनमावण संवहता तथा उप-वनयमों का अनुपालन क्रकये वबना ही क्रकया जा रहा है। अतैः ऐसे में
यह आिश्यक हो जाता है क्रक उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्िदेशी तकनीकी ज्ञान का उपयोग
39 www.visionias.in ©Vision IAS
क्रकया जाए और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए भूकंप-रोधी भिनों का
वनमावण क्रकया जाए।
त्िररत और प्रभािी अनुक्रक्रया: अनुभिों से पता चलता है क्रक विशेषीकृ त बचाि एिं राहत दल के
हस्तक्षेप से पूिव ही समुदायों द्वारा 80% से अवधक खोज तथा बचाि कायव कर वलया जाता है। इस
प्रकार समुदाय के सदस्यों को आधारभूत प्रवशक्षण देना आिश्यक है क्योंक्रक क्रकसी भी आपदा के
पश्चात् प्रथम अनुक्रक्रयाकताव सदैि समुदाय ही होता है।
प्रारं वभक भूकंप चेतािनी और सुरक्षा प्रणाली: चेन्नई वस्थत स्रक्चरल इंजीवनयटरग ररसचव सेंटर
(CSIR-SERC), िैज्ञावनक तथा औद्योवगक अनुसंधान पररषद (CSIR) के अधीन एक अग्रणी
एिं उन्नत भूकंपीय परीक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसने जमवनी द्वारा विकवसत “भूकंप
पूि-व चेतािनी और सुरक्षा प्रणाली (Early Earthquake Warning and Security System)”
का परीक्षण पूणव कर वलया है और इसे हाल ही में भारत में पहली बार लांच क्रकया गया।
भारतीय प्रौद्योवगकी संस्थान (IIT) रुड़की द्वारा उत्तर भारत (उत्तराखंड) के वलए, भूकंप पूिव
चेतािनी (EEW) प्रणाली पर एक प्रायोवगक पररयोजना कायाववन्ित की जा रही है। इसे पृ्िी
विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा वित्त पोवषत क्रकया गया है।
बीमा और जोवखम अंतरण उपाय: इन्हें बीमा कं पवनयों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग के साथ
विकवसत क्रकया जाना चावहए।
राष्ट्रीय भूकंप जोवखम शमन पररयोजना (National Earthquake Risk Mitigation Project)
राष्ट्रीय भूकंप जोवखम शमन (प्रारं वभक चरण) को 2013 में एक के न्द्र-प्रायोवजत योजना के रूप में
मंजरू ी दी गई थी। इस पररयोजना को NDMA द्वारा देश के भूकंप ़ोन IV एिं V में वस्थत राज्यों
की सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्िय से कायाववन्ित क्रकया जाना है। इसका उद्देश्य मुख्य
वहतधारकों में मॉडल भिन वनमावण उपवनयमों एिं भूकंप-रोधी वनमावण ि योजना मानकों को
अपनाने की आिश्यकता पर जागरूकता बढ़ाना है।
40 www.visionias.in ©Vision IAS
राष्ट्रीय भिन वनमावण संवहता (National Building Code)
भारत की राष्ट्रीय भिन वनमावण संवहता (National Building Code of India-NBC) भिन
वनमावण गवतविवधयों को विवनयवमत करने के वलए भिनों की विवभन्न सामवग्रयों, योजना,
वडजाइन एिं वनमावण प्रक्रक्रयाओं के संबंध में क्रदशा-वनदेश प्रदान करता है। यह संरचनात्मक
पयावप्त कता, आग के खतरों एिं स्िास््य सम्बन्धी पहलुओं के संबंध में जनता की सुरक्षा को ध्यान में
रखते हुए भिनों के वनमावण के वलए विवभन्न प्रािधानों का वनधावरण करता है।
निंबर 2010 में पूिी क्रदल्ली में लक्ष्मी नगर के लवलता पाकव में एक भिन ढह गया था वजसमें 71
लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस सन्दभव में यह त्य सामने आया क्रक क्षेत्रीय वबल्डर अवतररक्त
क्रकराये के लालच में भिनों में अवतररक्त मंवजल जोड़कर तथा सड़क का अवतक्रमण कर भिन
कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। सेिावनिृत्त न्यायाधीश लोके िर प्रसाद की अगुिाई िाले एक
जांच आयोग ने पाया क्रक पूिव क्रदल्ली में अवधकतर भिन घरटया वनमावण सामग्री का उपयोग क्रकए
जाने के कारण असुरवक्षत थे। हाल ही में, जुलाई 2017 में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में ही एक और चार-
मंवजला भिन ढह गया। ये राष्ट्रीय भिन संवहता के कम़ोर प्रितवन की ओर इशारा करते हैं।
भारत में भूकंप शमन संबध
ं ी ितवमान गंभीर चुनौवतयां
भूकंप-रोधी भिन संवहता एिं शहर वनयोजन उप-कानूनों का अपयावप्त क प्रितवन;
शहरी एिं ग्रामीण क्षेत्रों में वनमावण कायों में भूकंप-रोधी विशेषताओं की अनुपवस्थवत;
पेशि
े रों में भूकंप-रोधी वनमावण प्रणावलयों संबंधी औपचाररक प्रवशक्षण का अभाि;
विवभन्न वहतधारक समूहों के बीच पयावप्त क तैयारी का अभाि एिं खराब अनुक्रक्रया क्षमता;
भूकंप जोवखम के विषय में विवभन्न वहतधारकों के बीच जागरूकता का अभाि;
अवभयंताओं एिं राजवमवस्त्रयों के वलए लाइसेंससग व्यिस्था की अनुपवस्थवत।
प्रश्नैः भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की आिृवत्त बढ़ती हुई प्रतीत होती है। क्रफर भी, इनके प्रभाि के
न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी (तत्परता) में महत्त्िपूणव कवमयााँ हैं। विवभन्न पहलुओं की चचाव कीवजए।
(UPSC, 2015)
भूकंप प्रबंधन पर NDMA क्रदशा-वनदेश
NDMA द्वारा जारी क्रदशा-वनदेश भारत में भूकंप प्रबंधन की प्रभािशीलता में सुधार के वलए भूकंपीय
सुरक्षा के छह स्तंभों पर आधाररत हैं:
i. नई संरचनाओं का भूकंप-रोधी वनमावण: सभी कें द्रीय मंत्रालय एिं विभाग तथा राज्य सरकारें
अपने प्रशासवनक क्षेत्र में आने िाली इमारतों और अत्यािश्यक ि व्यािसावयक रूप से
महत्िपूणव अन्य संरचनाओं जैसे क्रक पुल, फ्लाईओिर, बंदरगाह, पत्तन आक्रद के वलए भूकंप से
सुरवक्षत वडजाइन एिं वनमावण हेतु प्रासंवगक मानकों के कायावन्ियन को सुविधाजनक बनाएाँगे।
ii. चयनात्मक भूकंपीय सुदढ़ृ ीकरण एिं ितवमान प्राथवमक रूप से महत्िपूणव संरचनाओं तथा
अत्यािश्यक संरचनाओं की रे रोक्रफटटग: सभी कें द्रीय मंत्रालयों एिं राज्य सरकारों द्वारा
प्राथवमक रूप से महत्िपूणव संरचनाओं के भूकंपीय सुदढ़ृ ीकरण हेतु शहरी स्थानीय वनकायों
(ULBs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के माध्यम से कायवक्रम तैयार करना आिश्यक
है। इन संरचनाओं में राज भिन, विधानसभा, न्यायालय जैसी राष्ट्रीय महत्ि की इमारतें,
अकादवमक संस्थानों जैसे महत्िपूणव भिन, जलाशय ि बांध जैसी सािवजवनक सुविधाओं िाली
संरचनाएं तथा पांच या अवधक मंवजल िाली बहुमंवजला इमारतें शावमल हैं। इन संरचनाओं की
पहचान करने की वजम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है।
iii. विवनयमन एिं प्रितवन: राज्य सरकारें भिन वनमावण संवहता एिं अन्य सुरक्षा संवहताओं के
कायावन्ियन हेतु ऐसे तंत्र स्थावपत करने हेतु उत्तरदायी हैं वजससे यह सुवनवश्चत हो सके क्रक
वबल्डर, िास्तुविद् (आर्दकटेक्ट्जस), अवभयंता ि सरकारी विभागों जैसे सभी वहतधारक वडजाइन
तथा वनमावण सम्बन्धी समस्त गवतविवधयों में भूकंप सुरक्षा वनयमों का पालन कर रहे हैं। गृह
41 www.visionias.in ©Vision IAS
मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ समूह का गठन क्रकया था। इस समूह ने शहरी ि ग्रामीण
वनयोजन अवधवनयमों, भूवम उपयोग ि जोनों में िगीकरण (zoning) हेतु विवनयमों, विकास
वनयंत्रण विवनयमों (DCRs) तथा भिन वनमावण उप-वनयमों में संशोधन की संस्तुवत की थी,
ताक्रक इन्हें तकनीकी रूप से सुदढ़ृ और विि स्तर पर स्िीकृ त मानदंडों के अनुरूप बनाया जा
सके ।
iv. जागरूकता एिं तैयारी: NDMA ने स्िीकार क्रकया है क्रक भूकंप संबंधी तैयारी ि इसके शमन
हेतु सभी वहतधारकों को जागरूक बनाना सबसे अवधक चुनौतीपूणव कायों में से एक है। यह
भूकंप सुरक्षा पर पुवस्तकाओं (हैंडबुक्स), मकान मावलकों के वलए भूकंपीय सुरक्षा वनयमािवलयों
(मैनअ
ु ल्स), संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा पर एक वनयमािली तथा आम जनता के वलए
िीवडयो क्रफल्में तैयार करने की संस्तुवत करता है। यह स्थलीय क्षेत्रों के सुभेद्यता मानवचत्र तैयार
करने तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) एिं स्ियंसि
े ी समूहों के उवचत वनयोजन की
आिश्यकता को भी रे खांक्रकत करता है।
v. क्षमता विकास (वशक्षा, प्रवशक्षण, अनुसध
ं ान एिं विकास, क्षमता वनमावण ि दस्तािे़ीकरण):
क्षमता विकास के वलए लवक्षत समूहों में वनिाववचत प्रवतवनवध, सरकारी अवधकारी, दृश्य ि सप्रट
मीवडया के पेशेिर, शहरी वनयोजनकताव, अवभयंता, आर्दकटेक्ट एिं वबल्डसव, NGOs, समुदाय
आधाररत संगठन (CBOs), सामावजक कायवकताव, समाज-िैज्ञावनक, स्कू ल वशक्षक एिं स्कू ली
बच्चे सवम्मवलत हैं।
vi. आपातकालीन अनुक्रक्रया: अनुक्रक्रया सम्बन्धी सभी गवतविवधयां स्थानीय प्रशासन द्वारा
समवन्ित घटना कमान प्रणाली (Incident Command System) के माध्यम से सम्पाक्रदत की
जाती हैं। इस प्रणाली में समुदाय, कॉपोरे ट क्षेत्र एिं विशेष टीमों की भागीदारी होती है।
3.2.2. सु नामी (Tsunami)
सुनामी क्या है?
सुनामी एक जापानी शब्द है वजसमें ‘tsu’ का अथव बंदरगाह और ‘nami’ का अथव लहर है, अतैः
इसका सामान्य अथव बंदरगाह लहर है। सुनामी बेहद लंबी तरं गदैध्यव एिं आितवकाल िाली दीघव
लहरों की एक श्रृंखला है, जो प्रायैः तट के पास या समुद्र में क्रकसी गवतविवध या क्रकसी
अन्तैःसागरीय विक्षोभ से उत्पन्न होती है।
सुनामी कै से उत्पन्न होती है?
सुनामी सागरीय अधस्तल के स्तर में एक बड़े, आिेगपूणव विस्थापन द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूकंप,
सागरीय अधस्तल के ऊध्िावधर संचलन से सुनामी उत्पन्न करते हैं। सुनामी, भूस्खलन के मलबे के
जल में वगरने या जल की सतह के नीचे भूस्खलन होने, ज्िालामुखीय गवतविवध तथा उल्कासपड के
टकराने के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं। गंगा एिं ससधु नक्रदयों द्वारा विशाल तलछट वनक्षेप के
कारण बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में भूस्खलन से सुनावमयों के उत्पन्न होने की सम्भािना
बन सकती है।
42 www.visionias.in ©Vision IAS
भारत में सुनामी का जोवखम
अतीत में, सहद महासागर एिं भूमध्य सागर में कु छ विनाशकारी सुनावमयााँ उत्पन्न हो चुकी हैं।
सहद महासागर की सिाववधक प्रमुख सुनामी अगस्त 1883 में क्राकाटोआ द्वीप के ज्िालामुखी के
उग्र विस्फोट से उत्पन्न हुई थी। यद्यवप सहद महासागर क्षेत्र में सुनामी लहरें कभी-कभी ही उत्पन्न
होती हैं, क्रफर भी वपछले 300 िषों में इस क्षेत्र में 13 सुनावमयााँ दजव की गई हैं। इनमें से 3
अंडमान-वनकोबार क्षेत्र में घरटत हुई हैं। 26 क्रदसंबर, 2004 को सहद महासागर में उठने िाली
सुनामी भारत में तबाही मचाने िाली सबसे विनाशकारी सुनावमयों में से एक थी।
भारत में सुनामी का वितरण प्रवतरूप
भारत की पूिव एिं पवश्चम, दोनों तटरे खाएाँ सुनामी लहरों के प्रवत सुभेद्य हैं। भारत की तटरे खा के
लगभग 2200 क्रकलोमीटर से अवधक भाग में घनी आबादी है। भारतीय तटीय क्षेत्रों के सुनामी
द्वारा प्रभावित होने के वलए 6.5 से अवधक पररमाण के सुनामीकारक भूकंप का होना आिश्यक है।
तटीय क्षेत्रों में िास्तविक सुनामी का खतरा उसकी बैथीमीरी (bathymetry) अथावत् तट के
वनकट जल की गहराई एिं तटीय स्थलाकृ वत पर वनभवर करता है।
भारत में सुनावमयों का इवतहास
वतवथ अिवस्थवत ि कारण प्रभाि
1524 दाभोल के वनकट, महाराष्ट्र पयावप्त क आंकड़े उपलब्ध नहीं
02 अप्रैल अराकान तट, म्यांमार पयावप्त क आंकड़े उपलब्ध नहीं
1762
16 जून क्छ का रण, गुजरात पयावप्त क आंकड़े उपलब्ध नहीं
1819
31 ग्रेट वनकोबार द्वीप पयावप्त क आंकड़े उपलब्ध नहीं
अक्टू बर
1847
31 कार वनकोबार द्वीप पर ररक्टर पैमाने पर 7.9 भारत का सम्पूणव पूिी तट तथा अंडमान
क्रदसंबर की तीव्रता का भूकंप और वनकोबार द्वीप समूह; चेन्नई में 1
1881 मीटर की ऊाँचाई िाली सुनामी लहरें द़व
की गयी थीं।
26 अगस्त इं डोनेवशया में क्राकाटोआ ज्िालामुखी का भारत का पूिी तट प्रभावित हुआ था;
विस्फोट
1883 चेन्नई में 2 मीटर की ऊाँचाई िाली सुनामी
लहरें द़व की गयी थीं।
26 जून अंडमान द्वीप समूह पर ररक्टर पैमाने पर 8.1 भारत का पूिी तट प्रभावित हुआ था क्रकन्तु
की तीव्रता का भूकंप सुनामी लहरों की ऊाँचाई के आंकड़े
1941
उपलब्ध नहीं हैं।
27 निंबर कराची से दवक्षण में लगभग 100 क्रकमी की भारत के पवश्चमी तट के उत्तरी भाग से
लेकर कारिार (कनावटक) तक प्रभावित
43 www.visionias.in ©Vision IAS
1945 दूरी पर ररक्टर पैमाने पर 8.5 की तीव्रता का हुआ था; कांडला में 12 मीटर ऊाँची
भूकंप सुनामी आयी थी।
26 बांदा आचेह, इं डोनेवशया; तवमलनाडु , के रल, भारत का पूिी तट प्रभावित हुआ था।
क्रदसंबर आंध्र प्रदेश, अंडमान और वनकोबार द्वीप लगभग 10 मीटर ऊाँची सुनामी लहरों से
2004 समूह, भारत; श्रीलंका; थाईलैंड; मलेवशया; 10,000 से अवधक लोगों की मृत्यु हो गयी
थी।
के न्या; तंजावनया
सुनामी आपदा के पररणाम
सुनामी के प्रभाि, विनाश एिं क्षवत, मौतों, बीमाररयों, चोटों, करोड़ों डॉलर की वित्तीय हावन से लेकर
क्षेत्र के वनिावसयों के वलए दीघाविवध तक चलने िाली मनोिैज्ञावनक समस्याएं तक हो सकते हैं।
सुनामी के प्रभाि वनम्नवलवखत कारकों पर वनभवर करते हैं:
सुनामी उत्पन्न करने िाली भूकंपीय घटना के अवभलक्षणों पर;
उत्पवत्त सबदु से दूरी ि सुनामी के आकार (पररमाण) पर; तथा
बैथीमीरी विन्यास (महासागरों में जल की गहराई) पर।
भारतीय तट पर क्रदसम्बर, 2004 में सहद महासागर में आयी सुनामी ने इस बात को रे खांक्रकत क्रकया
क्रक सिाववधक क्षवत तट के वनकटिती वनचले क्षेत्रों में हुई एिं अवधक मौतें घनी आबादी िाले क्षेत्रों में
देखी गईं। मैंग्रोि, जंगल, रे त के रटब्बों एिं तटीय चट्टानों ने सुनामी के प्रभाि को कम करने में उत्कृ ष्ट
प्राकृ वतक अिरोधों का कायव क्रकया तथा उन क्षेत्रों में भारी क्षवत हुई जहां रे त के रटब्बों का अत्यवधक
खनन क्रकया जा चुका था।
सुनामी पूिावनम
ु य
े ता (Tsunami Predictability)
चूंक्रक िैज्ञावनक भूकंप का सटीक पूिावनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसवलए िे सुनामी के उत्पन्न होने की
भी सटीक भविष्टयिाणी नहीं कर सकते हैं। सुनामी चेतािनी के दो वभन्न प्रकार हैं:
i. अंतरावष्ट्रीय सुनामी चेतािनी प्रणावलयां तथा
ii. क्षेत्रीय चेतािनी प्रणावलयां।
भारत में सुनामी चेतािनी की ितवमान वस्थवत
‘भारतीय सुनामी पूिव चेतािनी कें द्र (Indian Tsunami Early Warning Centre: ITEWC)’
भारत के साथ-साथ सहद महासागरीय राष्ट्रों को सुनामी संबंवधत परामशव देने के वलए सभी
आिश्यक अिसंरचनाओं तथा क्षमताओं से लैस है। ITEWC भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना
सेिा कें द्र (Indian National Centre for Ocean Information Services: INCOIS),
हैदराबाद में अिवस्थत है तथा INCOIS इसका संचालन भी करता है। सुनामी की पूिव चेतािनी
के वलए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के तीन स्टेशनों- पोटवब्लेयर, वमवनकॉय ि वशलांग
के ररयल-टाइम सतत भूकंपीय तरं ग डेटा (real-time continuous seismic waveform
data) को IMD के भूकंप-विज्ञान कें द्र द्वारा िैविक समुदाय के साथ साझा भी क्रकया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र शैवक्षक, िैज्ञावनक एिं सांस्कृ वतक संगठन (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) के अंतसवरकारी समुद्र-विज्ञान आयोग
(Intergovernmental Oceanographic Commission: IOC) द्वारा ITEWC को संपूणव
सहद महासागरीय क्षेत्र के वलए क्षेत्रीय सुनामी सेिा प्रदाताओं में से एक के रूप में वनर्ददष्ट क्रकया
गया है। यह भारतीय तटीय क्षेत्रों/द्वीपों को समग्र रूप से सेिाएं प्रदान करने के अवतररक्त सहद
महासागर के क्रकनारे वस्थत सभी देशों (24 देशों) को सुनामी चेतािवनयााँ तथा संबंवधत सेिाएं
प्रदान कर रहा है।
44 www.visionias.in ©Vision IAS
यह कें द्र, सहद महासागर के साथ-साथ विि भर के महासागरों में आये सुनामीकारक भूकंपों का
उनके घरटत होने के 10 वमनट के भीतर पता लगाने में सक्षम है तथा ईमेल, फै क्स, SMS, िैविक
दूरसंचार प्रणाली (Global Telecommunication System: GTS) ि िेबसाइट के माध्यम से
संबंवधत प्रावधकाररयों के वलए 20 वमनट के भीतर सलाहकारी सूचना (advisories) का प्रसार
कर सकता है।
ITEWC में, वहन्द ि प्रशांत महासागरों के आस-पास के भूकंपीय स्टेशनों, समुद्र स्तर वनगरानी
कें द्रों (sea level gauge stations) तथा सुनामी उत्प्लिों (tsunami buoys) का राष्ट्रीय एिं
अंतरावष्ट्रीय प्रेक्षण नेटिकव सवम्मवलत है। इसके द्वारा लगभग 400 सीस्मोमीटसव से ररयलटाइम
आाँकड़े प्राप्त क क्रकये जाते हैं और उनकी ऑटोमेटेड प्रॉसेससग के द्वारा पृ्िी पर कहीं भी आए 4.0 ि
उससे अवधक पररमाण िाले भूकंप का पता लगाया जाता है। जैसे ही भूकंप का पता चलता है,
चेतािनी कें द्र भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर भूकंप की अिवस्थवत, उसके पररमाण, उसके उद्गम
की गहराई तथा घटना के अन्य लक्षणों का िणवन करने िाला प्रथम बुलेरटन प्रसाररत करता है।
प्रथम बुलेरटन जारी करने के पश्चात्, भूकंपीय आकं ड़ों का और अवधक विश्लेषण क्रकया जाता है
ताक्रक भूकंप के मापदंडों (पररमाण, गहराई तथा अिवस्थवत) की पररशुिता में सुधार क्रकया जा
सके । यथासंभि कम समय में विशाल भूकंपों की पहचान करने तथा उनके लक्षणों को वनधावररत
करने के वलए भूकंपीय आकं ड़ों की प्रोसेससग को इष्टतम बनाया जाता है।
सुनावमयों के प्रबंधन पर NDMA क्रदशा-वनदेश
सुनामी जोवखम आकलन और सुभद्य
े ता विश्लेषण: NDMA, तटीय भूवम उपयोग मानवचत्रों एिं
तटीय बैथीमीरी के आधार पर सुनामी संकटों की सुभेद्यता के आकलन तथा जोवखम मानवचत्रण
की अनुशस
ं ा करता है। इसने सुनामी तरं गों के आगमन तथा ऊपर उठने िाली लहरों की ऊाँचाई का
अनुमान लगाने के वलए विवभन्न मॉडल विकवसत करने का सुझाि भी क्रदया है। भारतीय नौसै वनक
जल सिेक्षण विभाग (Indian Naval Hydrographic Department: INHD) भारत सरकार
के मुख्य जल सिेक्षक के अधीन कायव करता है। यह जलप्लािन मानवचत्रों (inundation maps)
को वचवत्रत करने के वलए अवधकृ त एजेंवसयों को वनयवमत रूप से बैथीमीरी सूचनाएं प्रदान करता
है।
45 www.visionias.in ©Vision IAS
सुनामी संबध
ं ी तैयारी: IMD द्वारा 17-स्टेशनों िाले ररयल टाइम सीवस्मक मॉवनटटरग नेटिकव
(RTSMN) की स्थापना क्रकये जाने की पररकल्पना की गयी है। खुले महासागर में सुनामी तरं गों
के प्रसार का पता लगाने के वलए बॉटम प्रेशर ररकार्डसव (BPRs) का उपयोग क्रकया जाता है। एक
प्रमुख सचता का विषय यह है क्रक समुद्र में वबना वनगरानी िाले महासागरीय प्रेक्षण प्लेटफामों को
भारी क्षवत पहुाँच रही है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योवगकी संस्थान (National Institute of
Ocean Technology: NIOT) सतही उत्प्लिों के संरक्षण के वलए राष्ट्रीय डेटा उत्प्लि कायवक्रम
(National Data Buoy Programme) कायाववन्ित कर रहा है। सुनामी बुलेरटन तथा चेतािनी
प्रणावलयां, तैयारी का एक महत्िपूणव भाग हैं। बचाि मागों की सूचना के वलए तटीय क्षेत्रों में
“सुनामी बचाि-मागव (Tsunami Escape)” की क्रदशा के साइनबोडव लगाए जाने चावहए। दृश्य
एिं रे वडयो मीवडया भी सचेत करने तथा चेतािनी देने में एक महत्िपूणव भूवमका वनभाते हैं। साथ
ही साथ जन जागरूकता अवभयान भी प्रायैः अवधक आयोवजत क्रकये जाने चावहए।
संरचनात्मक शमन उपाय: विवभन्न अनुशंवसत संरचनात्मक उपाय वनम्नवलवखत हैं:
o चक्रिात आश्रय-स्थलों (cyclone shelters), जलमि रे त के अिरोधों/तटबंधों, समुद्री खर-
पतिारों िाले रे त के टीलों का वनमावण तथा तटरे खा पर मैंग्रोि ि तटीय िनों का रोपण।
o संकट के समय आिश्यक प्रवशक्षण एिं आपातकालीन संचार सुविधा प्रदान करने के वलए तट
रे खाओं के क्रकनारे स्थानीय सूचना कें द्रों (ग्रामीण/शहरी) के एक नेटिकव का विकास (उदाहरण
के वलए पांवडचेरी में एम.एस. स्िामीनाथन फाउं डेशन द्वारा विकवसत कें द्र)।
o विशेषज्ञों के परामशव के साथ स्थान विवशष्ट समुद्री दीिारों तथा प्रिाल वभवत्तयों का वनमावण।
o सुनामी की तीव्रता को कम करने हेतु तट पर तरं गरोधों का विकास।
46 www.visionias.in ©Vision IAS
o “बायो-शील्ड” यानी जैि-किच का विकास। यह तटरे खा के साथ-साथ भूवम की एक संकीणव
पट्टी होती है। इसे तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन संरवक्षत क्षेत्र (coastal zone disaster
management sanctuary) के रूप में विकवसत क्रकया जा सकता है, वजसमें सघन
िृक्षारोपण क्रकया गया हो और उसमें सािवजवनक जागरूकता, जानकारी के प्रसार ि प्रदशवन
के वलए सािवजवनक स्थान भी हों।
o सुनामी आश्रय-स्थलों की पहचान करने के साथ-साथ सुभेद्य संरचनाओं की पहचान करना
तथा सुनामी/चक्रिात प्रवतरोध के वलए ऐसे सभी भिनों की उपयुक्त रे रोक्रफटटग करना।
तकनीकी-कानूनी व्यिस्था का विवनयमन और प्रितवन: इसके वलए वनम्नवलवखत उपाय क्रकए जा
सकते हैं:
o तटीय क्षेत्र विवनयमों का कठोर कायावन्ियन (औसत समुद्र तल से 10 मीटर से कम ऊंचाई
िाले क्षेत्रों में उच्च ज्िार रे खा के 500 मीटर के भीतर)
o सुनामी-सुरवक्षत ़ोनों के िगीकरण, वनयोजन, वड़ाइन तथा वनमावण कायव-प्रणावलयों के
अनुपालन को सुवनवश्चत करने के वलए तथा भूवम के इष्टतम उपयोग को प्रोत्सावहत करने हेतु
MHA द्वारा विकवसत, आदशव तकनीकी-कानूनी फ्रेमिकव को अपनाना।
आपातकालीन सुनामी अनुक्रक्रया: चूंक्रक क्रकसी भी आपदा में समुदाय प्रथम अनुक्रक्रयाकताव होता है,
इसवलए विवभन्न माध्यमों द्वारा पूरे तटीय क्षेत्र में जन जागरूकता अवभयान की एक श्रृंखला आरं भ
की जा सकती है। SHGs, NGOs ि CBOs को खोज तथा बचाि अवभयानों में सवम्मवलत
क्रकया जा सकता है। जलमि क्षेत्रों, िृक्षों पर ि विवभन्न ध्िस्त संरचनाओं में फं से हुए लोगों की
खोज तथा बचाि के वलए सुनामी के तुरंत पश्चात् िायु से फु लायी जा सकने िाली मोटरचावलत
नौकाओं, हेलीकॉप्टरों तथा खोज ि बचाि उपकरणों की आिश्यकता होती है। भारतीय नौसैवनक
जल सिेक्षण विभाग, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने िाली आपदाओं के दौरान महत्िपूणव भूवमका
वनभाता है। 26 क्रदसंबर, 2004 की सहद महासागरीय सुनामी के दौरान, सात सिेक्षण जहाजों को
वचक्रकत्सा सहायता प्रदान करने के साथ-साथ संचार के समुद्री मागों को खोलने के वलए भी तैनात
क्रकया गया था। उन्हें इस क्षेत्र के तत्काल पुन: मानवचत्रण करने तथा निीनतम बैथीमीरी
जानकारी प्राप्त क करने के कायव पर लगाया गया था।
प्रबंधन योजनाओं का कायावन्ियन सुवनवश्चत करना:
o सुनामी तथा चक्रिात की आपदाओं का सामना करने हेतु स्थानीय लोगों तथा प्रशासन में
आिश्यक अत्याधुवनक स्तर की प्रभािी क्षमताओं का विकास करना।
o फं से हुए लोगों को बाहर वनकालने तथा सुनामी पश्चात् प्रबंधन गवतविवधयों के संबंध में
मछु आरों, तट-रक्षकों (coast guards), मत्स्यपालन विभाग के अवधकाररयों, बंदरगाह
प्रावधकाररयों तथा वजले के स्थानीय अवधकाररयों आक्रद के बीच जागरूकता उत्पन्न करना
तथा उन्हें प्रवशक्षण प्रदान करना। आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रभािकाररता के परीक्षण हेतु
वनयवमत अभ्यास क्रकए जाने चावहए।
ितवमान चुनौवतयां
भारत में सुनामी जोवखम प्रबंधन के संबंध में सचता के महत्िपूणव क्षेत्र वनम्नवलवखत हैं:
बेहतर जोवखम मूल्यांकन के वलए पूिव काल में हुई सुनामी घटनाओं की बेहतर समझ के वलए सरल
रूप से उपलब्ध सुनामी दस्तािेजों तथा पुरा-सुनामी (paleo-tsunami) अध्ययनों की कमी;
तटों के वनकटिती सागरीय क्षेत्रों की हाई-रे ़लूशन बैथीमीरी तथा स्थलाकृ वतक आकं ड़ों का
अभाि जलप्लािन (inundation) मॉडलों के विकास को सीवमत करता है;
सुनामी जोवखमों तथा सुभेद्यता पर समुदाय में अपयावप्त क जागरूकता।
तटीय क्षेत्रों में आपदा संबंधी तैयारी, शमन एिं आपातकालीन अनुक्रक्रयाओं को सुदढ़ृ बनाने में
लोगों की भागीदारी की कमी।
सुनामी जोवखम प्रबंधन के वलए पारं पररक ज्ञान के दस्तािेजीकरण की कमी।
47 www.visionias.in ©Vision IAS
कृ वत्रम अिरोधों की तुलना में िृक्षारोपण, सुनामी शमन का एक लागत-प्रभािी और दीघवकावलक
उपाय है। सहद महासागर के कु छ स्थान जहााँ 2004 में सुनामी आयी थी, लगभग अक्षत रहे
क्योंक्रक िहां के नाररयल तथा मैंग्रोि के िृक्षों ने सुनामी की अवधकांश ऊजाव को अिशोवषत कर
वलया था। इसी प्रकार, तवमलनाडु क्षेत्र में नालुिेदपावथ गांि में िषव 2002 में तटरे खा के साथ-
साथ लगाए गए 80,244 िृक्षों के िन के कारण न्यूनतम क्षवत तथा कम लोगों की मृत्यु हुई थी।
3.2.3. ज्िालामु खी (Volcano)
ज्िालामुखी क्या है?
ज्िालामुखी पृ्िी की पपवटी में
एक वछद्र होता है वजससे पृ्िी
की सतह के नीचे वस्थत मैग्मा
चैम्बर से गमव लािा, गैसें,
चट्टानें, ज्िालामुखीय राख और
भाप बाहर वनकलते हैं। ऐसे
ज्िालामुवखयों को वजनमें
वनयवमत रूप से विस्फोट होता
रहता है, सक्रक्रय ज्िालामुखी
कहा जाता है। सुप्त या
वनवष्टक्रय ज्िालामुखी िे होते हैं
वजनमें अतीत में तो विस्फोट
हुआ था क्रकन्तु ितवमान में िे
शांत हैं। वजन ज्िालामुवखयों में बेहद लम्बे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, उन्हें विलुप्त क ज्िालामुखी
कहा जाता है।
भारत के ज्िालामुवखयों की सूची
क्रमांक ज्िालामुखी का नाम राज्य
1. बैरन द्वीप (सक्रक्रय) अंडमान द्वीप समूह
2. नारकोंडम (विलुप्त क) अंडमान द्वीप समूह
3. बारातांग (विलुप्त क) अंडमान द्वीप समूह
4. दक्कन रैप (विलुप्त क) महाराष्ट्र
5. वधनोधर पहाड़ी (विलुप्त क) गुजरात
6. धोसी पहाड़ी (विलुप्त क) हररयाणा
ज्िालामुखी विस्फोट के कारण
ज्िालामुखी विस्फोट मुख्य रूप से कं पन गवतविवधयों या दुबल
व ता िाले क्षेत्रों में होते हैं, उदाहरण
के वलए, जहां पृ्िी की महाद्वीपीय प्लेटें एक-दूसरे से दूर हटती हैं या टकराती हैं। यह िहां भी
घरटत होता है जहां पृ्िी की परत वनरं तर वपघल रही होती है।
48 www.visionias.in ©Vision IAS
भारत में ज्िालामुखी जोवखम
भारत का एकमात्र सक्रक्रय ज्िालामुखी अंडमान और वनकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप ज्िालामुखी
है। इसने 150 से अवधक िषों तक वनवष्टक्रय रहने के बाद िषव 1991 में गवतविवध प्रदर्नशत करनी
प्रारम्भ की थी। जनिरी 2017 में इसने एक बार क्रफर से राख उगलना आरं भ कर क्रदया है। यह
ज्िालामुखीय द्वीप वनजवन है तथा इस द्वीप का उत्तरी वहस्सा बंजर और िनस्पवत रवहत है।
3.2.4. बाढ़ (Flood)
बाढ़ क्या है?
बाढ़, क्रकसी नदी के मागव के आस-पास या समुद्र के तटिती क्षेत्रों में उच्च जल स्तर की वस्थवत है
वजसके कारण भूवम जलप्लावित हो जाती है। भारत बाढ़ के प्रवत अत्यवधक सुभेद्य है। राष्ट्रीय बाढ़
आयोग (RBA) के आकलन के अनुसार, 329 वमवलयन हेक्टेयर के कु ल भौगोवलक क्षेत्रफल में से
40 वमवलयन हेक्टेयर से अवधक क्षेत्र बाढ़ प्रिण क्षेत्र है।
आकवस्मक बाढ़ (Flash Flood) क्या है?
अपेक्षाकृ त कम पररमाण क्रकन्तु तीव्र गवत से प्रिावहत जल के तेज चढ़ाि और उतार को आकवस्मक
बाढ़ कहते हैं। इस प्रकार की बाढ़ अपनी आकवस्मकता के कारण भारी नुकसान पहुाँचाती है।
आकवस्मक बाढ़ पहाड़ी और ढलान िाली भूवम में आती है जहां भारी िषाव और तवड़त झंझा या
बादल का फटना सामान्य रूप से घरटत होते रहते हैं।
पूिी तटीय क्षेत्रों में दबाि और चक्रिाती तूफानों से भी आकवस्मक बाढ़ आ सकती है।
नदी के ऊपरी प्रिाह पर वस्थत जलाशयों से अचानक पानी छोड़ने तथा बांधों और नक्रदयों के
क्रकनारों पर तटबंधों में दरार पड़ने से भी ऐसी बाढ़ आ जाती है।
डॉप्लर रडारों का प्रयोग करके ऐसी बाढ़ों का पूिावनम ु ान लगाया जाता है और आकवस्मक बाढ़
चेतािनी जारी की जाती है।
बाढ़ के कारण
भारी िषाव के पश्चात् ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से नीचे आए उच्च प्रिाह को अपने क्रकनारों के भीतर सीवमत
रखने की नक्रदयों की अपयावप्त क क्षमता से बाढ़ आती है।
अंधाधुंध िनोन्मूलन, अिैज्ञावनक कृ वष पिवतयां, प्राकृ वतक जल वनकासी चैनलों का अिरुि होना तथा
बाढ़ के मैदानों और नदी प्रिाह के मागव में जनसंख्या का बसाि आक्रद कु छ ऐसे मानिीय क्रक्रयाकलाप हैं
जो बाढ़ की तीव्रता, पररमाण और गंभीरता बढ़ाने में महत्िपूणव भूवमका वनभाते हैं। बाढ़ के कु छ कारण
वनम्नानुसार हैं:
प्राकृ वतक कारण (Natural causes)
o भारी िषाव: नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी िषाव से जल नदी के क्रकनारों के ऊपर से प्रिावहत
होने लगता है, इससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है।
o अिसाद का वनक्षेपण: अिसादन के कारण नदी तल उथला हो जाता है। ऐसी नदी की जल
िहन क्षमता कम हो जाती है। फलस्िरूप, भारी िषाव जल नदी के क्रकनारों के ऊपर से
प्रिावहत होने लगता है।
o चक्रिात: चक्रिात जवनत असामान्य ऊंचाई िाली समुद्री तरं गे आस-पास के तटीय क्षेत्र को
जलमि कर देती हैं। अक्टू बर 1994 में उड़ीसा चक्रिात से गंभीर बाढ़ आ गयी थी तथा
जान-माल की अभूतपूिव क्षवत हुई थी।
o नदी के मागव में पररितवन: विसपव (Meanders), नदी-तल और क्रकनारों के अपरदन तथा
भूस्खलन के कारण प्रिाह में बाधा से भी नदी का मागव बदल जाता है तथा बाढ़ आ जाती है।
o सुनामी: सुनामी के आने पर विशाल तटीय भू-भागों में ऊाँची समुद्री लहरों के कारण बाढ़ आ
जाती है।
o झीलों का अभाि: झीलें अवतररक्त जल संगृहीत कर सकती हैं और जल का प्रिाह वनयंवत्रत
कर सकती हैं। झीलें छोटी हो जाने पर प्रिाह वनयंवत्रत करने की उनकी क्षमता कम हो जाती
है और इसवलए बाढ़ आती है।
49 www.visionias.in ©Vision IAS
वहम का वपघलना और वहमनद का वपघलना धीमी गवत से चलने िाली प्रक्रक्रयाएं हैं और सामान्यत: इनसे
बड़ी बाढ़ नहीं आती है। लेक्रकन कभी-कभी वहमनदों में बड़ी मात्रा में ठहरा हुआ जल उपवस्थत होता है जो
वहमखंड वपघलने के साथ अचानक बह सकता है। इससे ग्लेवशयल लेक आउटबस्टव फ्लड (GLOF) की
वस्थवत उत्पन्न हो सकती है।
मानिजवनत कारण (Anthropogenic causes)
o िनोन्मूलन: िनस्पवत भूवम में जल के अन्तैःस्रिण (percolation) की सुविधा प्रदान करती
है। िनोन्मूलन के पररणामस्िरूप, भूवम बाधा मुक्त हो जाती है और जल तीव्र गवत से
प्रिावहत होकर नक्रदयों में जाता है और बाढ़ आती है।
o जल वनकास प्रणाली में हस्तक्षेप: पुलों, सड़कों, रे ल की पटररयों, नहरों आक्रद के िराब ढंग से
वनयोवजत वनमावण से जलवनकास प्रणाली में आने िाला व्यिधान जल-प्रिाह को बावधत
करता है और फलस्िरूप बाढ़ आती है।
o अंतरावष्ट्रीय आयाम: चीन, नेपाल और भूटान से वनकलने िाली नक्रदयां उत्तर प्रदेश, वबहार,
पवश्चम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में भारी बाढ़ लाती हैं। बाढ़ प्रबंधन के वलए
पड़ोसी देशों अथावत् चीन, नेपाल और भूटान के साथ सहयोग आिश्यक है।
o जनसंख्या का दबाि: विशाल जनसंखया
् के कारण लकड़ी, भूवम, भोजन इत्याक्रद सामवग्रयों
की अवधक आिश्यकता होती है। इससे अवतचारण, भूवम-अवतक्रमण, खेत की क्षमता से
अवधक कृ वष और मृदा अपरदन में िृवि होती है। इनके कारण बाढ़ आने का खतरा भी बढ़
जाता है।
o वनम्नस्तरीय जल और सीिरे ज प्रबंधन: शहरी क्षेत्रों में पुरानी जल वनकासी और सीिरे ज
प्रणावलयों की पूरी जांच-पड़ताल करके उनकी सम्पूणव मरम्मत नहीं की गई है। प्रत्येक िषव
िषाव ऋतु के दौरान, जल वनकासी और सीिर प्रणावलयााँ ध्िस्त हो जाती हैं वजससे शहरों में
बाढ़ आ जाती है।
भारत की बाढ़ के संकट के प्रवत सुभद्य
े ता
बाढ़ देश के लगभग सभी नदी बेवसनों में आती है। भारत में लगभग 12 प्रवतशत (40 वमवलयन
हेक्टेयर) भूवम बाढ़ प्रिण है। हमारे देश में 1200 वम.मी. िार्नषक िषाव होती है, वजसमें से 85
प्रवतशत 3-4 महीनों अथावत् जून से वसतंबर के दौरान संकेंक्रद्रत होती है। तीव्र और आिवधक िषाव
के चलते देश की अवधकांश नक्रदयों में भारी मात्रा में जल आ जाता है, जो उनकी िहन करने की
क्षमता से काफी अवधक होता है। इससे इस क्षेत्र में मामूली से लेकर गंभीर बाढ़ की वस्थवतयां
उत्पन्न हो जाती हैं।
भारत में बाढ़ क्षेत्रों का वितरण प्रवतरूप
िह्मपुत्र नदी क्षेत्र
इस क्षेत्र में िह्मपुत्र और बराक तथा उनकी सहायक नक्रदयां प्रिावहत होती हैं। यह क्षेत्र असम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वम़ोरम, मवणपुर, वत्रपुरा, नागालैंड, वसक्रक्कम और पवश्चम बंगाल के
उत्तरी भाग में फै ला है।
o मानसून के दौरान इन नक्रदयों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी िषाव होती है।
o ये नक्रदयां अपरदन के प्रवत अवतसंिद े नशील भंगरु पहावड़यों से वनकलती हैं वजससे इनके
प्रिाह में भारी मात्रा में गाद वनस्सरण होता है।
o यह क्षेत्र गंभीर और बार-बार आने िाले भूकम्पों का क्षेत्र है। इससे अनेक भूस्खलन होते हैं
वजनसे नदी तंत्र अस्त-व्यस्त हो जाती है।
o बादलों का फटना और उसके पश्चात् आने िाली आकवस्मक बाढ़ तथा भारी मृदा अपरदन भी
इस क्षेत्र की आम पररघटनाएाँ हैं।
50 www.visionias.in ©Vision IAS
गंगा नदी क्षेत्र: गंगा नदी की अनेक सहायक नक्रदयां है। इनमें यमुना, सोन, घाघरा, राप्त की, गंडक,
बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, अधिारा समूह की नक्रदयां, कोसी और महानंदा प्रमुख हैं।
इनका प्रिाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वबहार, पंजाब, पवश्चम बंगाल के दवक्षणी और
कें द्रीय भागों, हररयाणा के कु छ भागों, वहमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्रदल्ली में
विस्तृत है।
o बाढ़ की समस्या मुख्य रूप से गंगा नदी के उत्तरी क्रकनारे के क्षेत्रों तक ही सीवमत है क्योंक्रक
अवधकांश क्षवत गंगा की उत्तरी सहायक नक्रदयों के कारण होती है।
o सामान्यत:, पवश्चम से पूिव और दवक्षण से उत्तर की ओर बाढ़ की समस्या में िृवि होती है।
o हाल के िषों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बाढ़ की कु छ घटनाएं हुई हैं।
o बवस्तयों हेतु और विवभन्न विकास संबंधी गवतविवधयों के वलए नक्रदयों के बाढ़ मैदानों का बड़े
पैमाने पर अवतक्रमण इस क्षेत्र में बाढ़ आने का एक मुख्य कारण है।
उत्तर-पवश्चम नदी क्षेत्र: इस क्षेत्र की मुख्य नक्रदयां ससधु, सतलज, व्यास, रािी, वचनाब और झेलम
हैं। इनका प्रिाह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, पंजाब और वहमाचल प्रदेश, हररयाणा और राजस्थान के कु छ
भागों में विस्तृत है। गंगा और िह्मपुत्र नदी क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या
अपेक्षाकृ त कम है।
o अपयावप्त क भूपष्टृ ठीय जल वनकासी एक बड़ी समस्या है। इससे विशाल क्षेत्र में पानी ठहर जाता
है और िह जलप्लावित हो जाता है।
o ससचाई के वलए जल के अंधाधुध ं उपयोग तथा वनचले और गहरे क्षेत्रों के विकास ने जल
वनकास को बावधत क्रकया है एिं जल-जमाि की समस्या उत्पन्न की है।
o ये नक्रदयां बार-बार अपना मागव बदलती हैं और अपने पीछे रे तीले मलबे का विशाल क्षेत्र
छोड़ जाती हैं।
51 www.visionias.in ©Vision IAS
मध्य और दक्कन भारत
इस क्षेत्र की महत्िपूणव नक्रदयां नमवदा, तापी, महानदी, गोदािरी, कृ ष्टणा और कािेरी हैं। इन
नक्रदयों का मागव अवधकांशत: सुवनवश्चत और स्थायी है। इनमें इनके प्राकृ वतक क्रकनारों के भीतर,
डेल्टा क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में, बाढ़ के जल को प्रिावहत करने के वलए पयावप्त क क्षमता मौजूद
है। इस क्षेत्र में उड़ीसा की कु छ नक्रदयााँ, नामतैः महानदी, िाह्मणी, बैतरणी और सुिणवरेखा प्रवत
िषव बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं, इन्हें छोड़कर इस क्षेत्र में बाढ़ की कोई गंभीर समस्या नहीं है। मानसूनी
दबाि और चक्रिाती तूफानों के चलते पूिी तट के राज्यों का डेल्टाई और तटीय क्षेत्र समय-समय
पर बाढ़ और जल वनकासी की समस्याओं का सामना करता है।
बाढ़ के पररणाम
कृ वष भूवम और मानि बस्ती के बार-बार जलमि होने के राष्ट्रीय अथवव्यिस्था और समाज के वलए
गंभीर पररणाम होते हैं।
बाढ़ से मूल्यिान फसलें नष्ट हो जाती हैं और साथ ही सड़कों, पटररयों, पुलों जैसी भौवतक
अिसंरचनाओं तथा मानि बवस्तयों को भी नुकसान पहुंचता है।
बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। साथ ही साथ ही कई लोग और पशु बाढ़ के साथ बह भी
जाते हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाईरटस और अन्य दूवषत जलजवनत बीमाररयों का
प्रसार हो सकता है।
दूसरी ओर बाढ़ के कु छ लाभ भी हैं। प्रत्येक िषव बाढ़ खेतों में उपजाऊ वमट्टी लाकर जमा करती है
जो फसलों के वलए बहुत लाभदायक होती है।
बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के क्रदशा-वनदेश
भारत में अभी तक प्रारं भ क्रकए गए बाढ़ संरक्षण कायवक्रमों का जोर मुख्य रूप से संरचनात्मक उपायों
पर रहा है।
बाढ़ रोकथाम, तैयारी और शमन
संरचनात्मक उपाय (Structural Measures)
o जलाशय, बांध, अन्य जल भंडार: नक्रदयों के मागव में जलाशयों का वनमावण करके बाढ़ के समय
अवतररक्त जल को भंडाररत क्रकया जा सकता है। हालांक्रक, अभी तक अपनाए गए इस प्रकार
के उपाय सफल नहीं रहे हैं। उदाहरणस्िरुप, दामोदर नदी की बाढ़ को वनयंवत्रत करने के
वलए बनाए गए बांध बाढ़ वनयंवत्रत नहीं कर सके ।
o तटबंध/बाढ़ सुरक्षा बांध/बाढ़ सुरक्षा दीिारें : बाढ़ से सुरक्षा करने िाले तटबंधों का वनमावण
करके , बाढ़ के जल को नदीतट से बाहर बहने और आस-पास के इलाकों में फै लने से रोका जा
सकता है। उदाहरणस्िरुप, क्रदल्ली के वनकट यमुना पर तटबंध का वनमावण बाढ़ वनयंवत्रत
करने में सफल रहा है।
o जल वनकासी में सुधार: सामान्यत: सड़कों, नहरों, रे ल पटररयों आक्रद के वनमावण से जल
वनकासी प्रणाली अिरूि हो जाती है। यक्रद जल वनकासी प्रणाली के मूल रूप को पुनस्थाव वपत
कर क्रदया जाए तो बाढ़ को रोका जा सकता है।
o नदी जलमागव में सुधार/गाद वनकालना/तलकषवण: नदी जलमागव की जल िहन क्षमता में
सुधार करके बाढ़ के जल के प्रिाह के ितवमान उच्च स्तर को कम क्रकया जा सकता है। इसका
उद्देश्य नदी की िहन क्षमता बढ़ाने के वलए प्रिाह के क्षेत्र या प्रिाह के िेग (या दोनों) को
बढ़ाना होता है। स्थानीय स्तर पर समस्या से वनपटने के उपाय के रूप में मुहाने/संगम या
स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों में चयनात्मक गाद वनकासी / तलकषवण उपायों को अपनाया जा
सकता है।
o बाढ़ के जल को मोड़ना: बाढ़ मैदान के भीतर या कु छ वस्थवतयों में इससे बाहर प्राकृ वतक या
कृ वत्रम रूप से वनर्नमत जल िावहकाओं में बाढ़ के पूरे जल या जल के कु छ भाग को मोड़ना,
नदी में जल स्तर को कम करने का एक उपयोगी माध्यम है।
52 www.visionias.in ©Vision IAS
श्रीनगर शहर के चारों ओर बाढ़ जल वनकासी चैनल और क्रदल्ली में ‘सप्लीमेंरी िेन’ शहरीकृ त
क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के वलए अवतररक्त जल को मोड़ने के उदाहरण हैं।
o जलग्रहण क्षेत्र उपचार/ िनीकरण: िाटरशेड प्रबंधन उपाय जैसे क्रक िनस्पवत आिरण विकवसत
करना अथावत् िनीकरण और चेक डैम, अिरोध बेवसन इत्याक्रद जैसे संरचनात्मक कायों के साथ
मृदा आिरण का संरक्षण, बाढ़ की प्रचंडता को कम करने और अपिाह की आकवस्मकता को
वनयंवत्रत करने हेतु प्रभािी उपाय के रूप में कायव करते हैं।
गैर-संरचनात्मक उपाय (Non-Structural Measures)
o बाढ़ के मैदान का जोनों में िगीकरण: यह बाढ़ से अवधकतम लाभ प्रावप्त क हेतु बाढ़ के कारण होने
िाली क्षवत को सीवमत करने के वलए बाढ़ के मैदानों में भूवम के उपयोग को वनयंवत्रत करने हेतु
क्रकया जाता है।
o फ्लड प्रूकफग: यह संकट के शमन में सहायता करता है और बाढ़ प्रिण क्षेत्रों में जनसंख्या को
तत्काल राहत प्रदान करता है। यह संरचनात्मक पररितवन और आपातकालीन कायविाही का
संयोजन है क्रकन्तु इसमें लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर वनकालना सवम्मवलत नहीं है। इसमें
लोगों और मिेवशयों के वलए बाढ़ आश्रय के वलए ऊंची समतल भूवम प्रदान करना; सािवजवनक
उपयोवगता संस्थापनाओं, विशेष रूप से पीने के पानी के हैंडपंपों और बोरिेल का प्लेटफॉमव बाढ़
के स्तर से ऊपर उठाना तथा दो-मंवजला इमारतों का वनमावण प्रोत्सावहत करना सवम्मवलत है,
वजसमें ऊपरी मंवजल का उपयोग बाढ़ के दौरान आश्रय-स्थल के वलए क्रकया जा सकता है।
o बाढ़ प्रबंधन योजनाएं: सभी सरकारी विभागों और एजेंवसयों को अपनी स्ियं की बाढ़ प्रबंधन
योजनाएं तैयार करनी चावहए।
o बेवसन या िाटरशेड पैमाने पर जल संसाधनों के एकीकृ त प्रबंधन के उद्देश्य से एकीकृ त जल
संसाधन प्रबंधन।
भारत में बाढ़ का पूिावनम
ु ान और चेतािनी
बाढ़ पूिावनम
ु ान के वलए जल प्रिाह और िषाव के ररयल-टाइम आंकड़े आधारभूत आिश्यकताएं हैं।
अवधकांश जल-मौसमविज्ञान संबध ं ी आंकड़े कें द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय के न्द्रों द्वारा प्रेवक्षत और
एकत्र क्रकए जाते हैं; IMD दैवनक िषाव संबंधी आंकड़े प्रदान करता है।
आपदा वमत्र योजना
NDMA ने भारत के 25 राज्यों के 30 सिाववधक बाढ़ प्रिण वजलों में आपदा अनुक्रक्रया में समुदाय के
स्ियंसेिकों के प्रवशक्षण पर कें क्रद्रत एक कें द्र प्रायोवजत योजना को स्िीकृ वत दी है। इसका उद्देश्य
समुदाय के स्ियंसेिकों को ऐसे कौशलों में प्रवशवक्षत करना है वजनकी उन्हें बाढ़, आकवस्मक बाढ़
और शहरी बाढ़ जैसी आपातकालीन वस्थवतयों में आधारभूत राहत और बचाि कायों के दौरान
आिश्यकता होगी। इन कौशलों के माध्यम से िे आपातकालीन सेिाओं के तत्काल उपलब्ध न हो
पाने की वस्थवत में अपने समुदाय की तात्कावलक आिश्यकताओं की पूर्नत हेतु उवचत अनुक्रक्रया करने
में समथव हो सकें गे।
53 www.visionias.in ©Vision IAS
प्रश्न: भारत में बाढ़ इतनी आिती विशेषता क्यों है? बाढ़ वनयंत्रण के वलए सरकार द्वारा उठाए गए
कदमों की वििेचना कीवजए। (85/II6c/20)
3.2.5. शहरी बाढ़ (Urban Floods)
शहरी बाढ़ क्या है?
भारत में शहरी बवस्तयों (7933 कस्बों) के अधीन क्षेत्रफल 2001 में 77370.50 िगव क्रक.मी. से
बढ़कर 2011 में 102220.16 िगव क्रक.मी. हो गया। यह शहरी उपयोग के अधीन लाए गए
24850.00 िगव क्रक.मी. अवतररक्त भूवम क्षेत्र को प्रदर्नशत करता है। नक्रदयों और जलमागों के
क्रकनारे अवनयोवजत विकास और फै लते आिासों के अवतक्रमण ने जलधाराओं के प्राकृ वतक प्रिाह में
हस्तक्षेप क्रकया है। इसके पररणामस्िरूप शहरीकरण के अनुपात में रन-ऑफ में िृवि हुई है, वजससे
शहरी बाढ़ की वस्थवतयां उत्पन्न हुई हैं।
शहरी बाढ़ के पररणामस्िरूप होने िाली क्षवतयााँ
प्रत्यक्ष क्षवतयााँ: बाढ़ के जल के प्रत्यक्ष संपकव में आने से इमारतों, अिसंरचनाओं तथा मानि एिं पशु
जीिन को होने िाली क्षवतयााँ।
अप्रत्यक्ष क्षवतयााँ: ऐसी क्षवतयााँ जो बाढ़ की घटना का पररणाम हों क्रकन्तु उसके प्रत्यक्ष संपकव का
प्रभाि न हों, उदाहरण के वलए, यातायात में व्यिधान, व्यिसाय की ऐसी क्षवत वजसकी भरपाई न
हो सके , पाररिाररक आय की क्षवत आक्रद।
क्षवतयों के दोनों िगों में दो स्पष्ट उपिगव हैं:
o मूतव क्षवतयााँ: ऐसी िस्तुओं की क्षवत वजनका कोई मौक्रद्रक (प्रवतस्थापनीय) मूल्य हो। उदाहरण के
वलए, इमारतें, अिसंरचना आक्रद।
o अमूतव क्षवतयााँ: ऐसी ची़ों की क्षवत वजनका क्रय-विक्रय न क्रकया जा सकता हो। उदाहरण के
वलए, जीिन की क्षवत और चोट, विरासत की िस्तुए,ाँ स्मृवत-वचह्न आक्रद।
शहरी बाढ़ के कारण
शहरों और कस्बों में बाढ़ निीन पररघटना है। ऐसा एक छोटी सी समयािवध में भारी िषाव की
बढ़ती घटनाओं, जलमागों के अंधाधुंध अवतक्रमण, नावलयों की अपयावप्त क क्षमता और जल वनकास
अिसंरचना के रखरखाि की कमी के कारण हो रहा है। शहरों के बीच िषाव में विस्तृत विविधता है
और, यहां तक क्रक एक शहर के भीतर भी, िषाव में व्यापक स्थावनक और कावलक वभन्नता क्रदखती
है; उदाहरण के वलए, मुंबई में, 26 जुलाई 2005 को, कोलाबा में के िल 72 वम.मी. िषाव दजव की
गई थी, जबक्रक सांताक्रूज, जो 22 क्रक.मी. दूर है, में 24 घंटे में 944 वम.मी. िषाव दजव की गई थी।
भारत में शहरी बाढ़ का जोवखम
शहरी बाढ़, ग्रामीण बाढ़ से काफी वभन्न होती है क्योंक्रक शहरीकरण के पररणामस्िरूप जलग्रहण
क्षेत्रों में शहरी अिसंरचना का विकास हो जाता है, इससे बाढ़ की प्रचंडता 1.8 से 8 गुना और
बाढ़ की मात्रा 6 गुना तक बढ़ जाती है। ये क्षेत्र महत्िपूणव अिसंरचना के साथ आर्नथक
गवतविवधयों के घनी आबादी िाले कें द्र हैं। इन अिसंरचनाओं को 24x7 सुरवक्षत क्रकए जाने की
आिश्यकता होती है। चेन्नई की बाढ़ (क्रदसंबर 2015), कश्मीर की बाढ़ (2014), सूरत की बाढ़
(2006) और मुंबई की बाढ़ (2005 और 2017) आक्रद घटनाएाँ हमारे शहरों की सुभेद्यता को
प्रदर्नशत करती हैं।
शहरी बाढ़ के प्रभाि और शहरी बाढ़ के वलए शमन रणनीवतयां
शहरी बाढ़ का िावणवज्यक, औद्योवगक, व्यापाररक, आिासीय और संस्थागत स्थानों पर स्थानीय
प्रभाि पड़ता है। जल आपूर्नत, सीिरे ज, विद्युत आपूर्नत और संचार में व्यिधान सामान्य बात है।
54 www.visionias.in ©Vision IAS
िावणवज्यक, औद्योवगक और व्यापाररक गवतविवधयों का बंद होना और संपवत्त और पररसंपवत्त की
क्षवत प्राय: देखी जाती है। यातायात (सड़क, रे ल और िायु) में प्राय: व्यिधान आता है। अनवधकृ त
क्षेत्रों में नई स्लम बवस्तयां अवस्तत्ि में आती हैं।
शहरी बाढ़ का खतरा रोकने के वलए, प्रत्येक शहर की बाढ़ शमन योजना (बाढ़ का मैदान, नदी
बेवसन, भूपृष्टठीय जल आक्रद) को समग्र भूवम उपयोग नीवत और शहर के मास्टर प्लान के साथ
बेहतर तरीके से एकीकृ त होना चावहए।
शहरी बाढ़ के प्रवत प्रभािी और कु शल अनुक्रक्रया के वलए आपदा प्रबंधन के वनम्नवलवखत तीन चरण
हैं:
o मानसून पूिव चरण (तैयारी): इसमें आपातकालीन आिश्यकताओं का आकलन, वहतधारकों (विशेष
रूप से समुदायों) का प्रवशक्षण और वसमुलेशन अभ्यासों के माध्यम से इन रणनीवतयों से पररचय,
नावलयों और सड़कों के रख-रखाि के वलए टीमों की पहचान और जल-जमाि/जलप्लािन की
रोकथाम के वलए अभ्यास आयोवजत करना सवम्मवलत हैं।
o मानसून के दौरान का चरण (पूिव चेतािनी और प्रभािी अनुक्रक्रया): इसमें वनिारक उपाय करने के
वलए विवभन्न एजेंवसयों को, िषाव की तीव्रता के आधार पर समय पर, गुणात्मक और मात्रात्मक
चेतािवनयां जारी करना सवम्मवलत है। अनुक्रक्रया चरण मुख्य रूप से आपातकालीन राहत कायों
पर ध्यान के वन्द्रत करता है: इसमें जान बचाना, प्राथवमक वचक्रकत्सा उपलब्ध कराना, संचार और
पररिहन प्रणावलयों की क्षवत को कम करना और उन्हें पुनस्थाववपत करना, आपदा से प्रभावित
लोगों की मूलभूत आिश्यकताओं (भोजन, जल और आश्रय) को पूरा करना तथा मानवसक
स्िास््य ि आध्यावत्मक समथवन के साथ-साथ सांत्िनापूणव देखभाल प्रदान करना सवम्मवलत हैं।
o मानसून पश्चात् चरण: पुनस्थावपन और पुनिावस चरण में आपदा स्थल और क्षवतग्रस्त सामवग्रयों को
सुदढ़ृ और प्रयोज्य वस्थवत में पुनस्थाववपत करने के वलए कायवक्रम का वनधावरण सवम्मवलत है।
शहरीकरण से िषाव में िृवि होती है: 1921 में, िैज्ञावनकों ने पाया क्रक बड़े शहरों के ऊपर तवड़तझंझा का
वनमावण होता है, जबक्रक ग्रामीण इलाकों के ऊपर ऐसे क्रकसी तवडतझंझा का वनमावण नहीं होता। इसे
शहरी ऊष्टमा द्वीप प्रभाि से बहुत अ्छी तरह समझा जा सकता है- बढ़ती गमी बादल वनमावण को प्रेररत
करती है और पिनें शहर द्वारा प्रेररत संिहन के साथ अंतरक्रक्रया करके िषाव करती हैं।
शहरी बाढ़ पर NDMA के क्रदशा-वनदेशों पर संवक्षप्त क सबदु
पूिव चेतािनी प्रणाली और संचार: राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान नेटिकव और डॉप्लर मौसम रडार 3
से 6 घंटे पूिव सूचना प्रदान कर सकते हैं। बाढ़ चेतािनी जारी क्रकए जाने के बाद, इसे जनता तक
प्रभािी ढंग से संचाररत क्रकया जाना चावहए।
55 www.visionias.in ©Vision IAS
शहरी जलवनकास की वडजाइन और प्रबंधन: द्रुत शहरीकरण के पररणामस्िरूप फु टपाथों, सड़कों
और वनर्नमत क्षेत्रों के रूप में अप्रिेश्य सतहों में िृवि हुई है। इससे वनस्यंदन (ररसाि) और प्राकृ वतक
भंडारण में कमी आई है।
o जलवनकास प्रणाली: पंसपग, भडडारण इत्याक्रद के समस्त वििरण के साथ जल आपूर्नत
प्रणावलयों, विशेष रूप से लघु जल वनकासी प्रणावलयों, की उवचत सूची रखी जानी चावहए।
o वडजाइन के आधार के रूप में जलग्रहण: चूंक्रक अपिाह प्रक्रक्रयाएं राज्य और शहर की
प्रशासवनक सीमाओं से स्ितंत्र होती हैं, अत: जल अपिाह विभाजक की रूपरे खा िाटरशेड
मानवचत्रण पर आधाररत होनी चावहए।
o समो्च रे खा संबवं धत आाँकड़े: िाटरशेड/जलग्रहण की सीमाओं और प्रिाह की क्रदशा के
वनधावरण के वलए सटीक समोच्च रे खाओं का वनधावरण आिश्यक है।
o वडजाइन फ्लो: पयावप्त क आकार वनधावरण और मात्रा वनयंत्रण सुविधाओं के वलए चरम प्रिाह
दर का आकलन।
o ठोस अपवशष्ट को हटाना: अवधकांश कस्बों और शहरों में सड़क के क्रकनारे खुली नावलयां हैं
वजनमें लोगों द्वारा अपवशष्ट का अनवधकृ त वनपटान कर क्रदया जाता है। ठोस अपवशष्ट के
कारण नावलयों में जल का प्रिाह बावधत होता है और सामान्यत: उनकी प्रिाह क्षमता कम
हो जाती है।
o िेन इनलेट कनेवक्टविटी: यह देखा जाता है क्रक सड़क क्रकनारे की नावलयों में सड़क से पानी
वनकालने के वलए मुहाने (इनलेट) या तो सही ढंग से संरेवखत नहीं हैं या अवस्तत्ि में ही नहीं
हैं। इससे सड़कों पर जल भराि की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
o िषाव बगीचे (Rain Gardens): पारगम्य वमट्टी को पलिार की पतली परत से ढक कर िषाव
बगीचे का वनमावण क्रकया जाता है। अपिावहत जल को इस सुविधा में एकवत्रत कर
पौधों/पलिार/मृदा पयाविरण के माध्यम से वनस्यंक्रदत होने क्रदया जाता है।
सुभद्य
े ता विश्लेषण और जोवखम आकलन: जोवखम िाले क्षेत्रों की पहचान, कायव के अनुसार
संरचनाओं का िगीकरण और संकट जोवखम के आधार पर ़ोनों के िगीकरण (Hazard Risk
Zoning) का उपयोग कर प्रत्येक संरचना और कायव के वलए जोवखम का अनुमान।
शहरी बाढ़ प्रकोष्टठ: शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) के अंतगवत एक पृथक शहरी बाढ़ प्रकोष्टठ
गरठत क्रकया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन गवतविवधयों का
समन्िय करे गा। शहरी स्थानीय वनकाय (ULBs) स्थानीय स्तर पर शहरी बाढ़ के प्रबंधन के वलए
उत्तरदायी होंगे।
अनुक्रक्रया: आपातकालीन संचालन कें द्र, घटना अनुक्रक्रया प्रणाली, बाढ़ आश्रय-स्थल, खोज और
बचाि अवभयान तथा आपातकालीन लॉवजवस्टक्स ‘बाढ़ अनुक्रक्रया तंत्र’ के कु छ महत्िपूणव कायवक्षेत्र
हैं।
स्ि्छता: पयावप्त क स्ि्छता और विसंक्रमण (disinfection) के अभाि में मलेररया, डेंगू और हैजा
जैसे रोग फै ल सकते हैं।
क्षमता विकास, जागरूकता सृजन और दस्तािे़ीकरण: स्थानीय सरकार और समुदाय दोनों को
सवम्मवलत करते हुए सहभागी शहरी बाढ़ वनयोजन और प्रबंधन।
ितवमान चुनौवतयां
शहरी बाढ़ के व्यापक जोवखम आकलन को कम महत्ि क्रदया जाना। इस आकलन में बाढ़ शमन
उपायों की योजना वनमावण और उन्हें कायाववन्ित करने से पहले शहरी बाढ़ के जोवखमों की समझ,
विश्लेषण और मूल्यांकन सवम्मवलत हैं।
विवभन्न शहरों में वभन्न-वभन्न कारकों और जोवखमों के मानवचत्रण के प्रवत अज्ञानता और इन्हें
विकास योजना में सवम्मवलत नहीं करना।
जन जागरूकता और आपदा प्रबंधकों को पेशेिर प्रवशक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनुभि साझा
करने के वलए विवभन्न संस्थानों के बीच असंतोषजनक समन्िय।
सूचना साझाकरण का अभाि,
एकीकृ त वनिेश वनणवयों का अभाि, और
वहतधारकों के साथ परामशव की कमी।
56 www.visionias.in ©Vision IAS
प्रश्न: कई िषों से उच्च तीव्रता की िषाव के कारण शहरों में बाढ़ की बारं बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में
बाढ़ के कारणों पर चचाव करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोवखम कम करने की तैयाररयों
की क्रक्रयाविवध पर प्रकाश डावलए। (UPSC, 2016)
3.2.6. भू स्खलन
(Landslides)
भूस्खलन क्या है?
चट्टान के टु कड़ों, मलबे या वमट्टी के ढेरों का ढलान के सहारे वखसककर नीचे वगरना भूस्खलन
कहलाता है। भूस्खलन “बृहत् क्षरण” का एक प्रकार है, वजसमें मृदा तथा चट्टान समूह गुरुत्ि के
प्रत्यक्ष प्रभाि के तहत वखसककर ढाल से नीचे वगरता है।
भूस्खलन प्राकृ वतक संकटों में से एक है जो देश के कम से कम 15 प्रवतशत भू-भाग को प्रभावित
करता है। वहमालय पिवत श्रृंखला का वनमावण इं वडयन और यूरेवशयाई प्लेट की टक्कर से हुआ है।
इं वडयन प्लेट की यूरेवशयाई प्लेट की क्रदशा में उत्तर की ओर गवत (5 से.मी./िषव की दर से) चट्टानों
पर वनरं तर दबाि बनाती है और उन्हें भुरभुरा, कमजोर और भूस्खलन तथा भूकम्प के वलए प्रिण
बना देती है।
भारत के भूस्खलन सुभद्य
े ता क्षेत्र
भूस्खलन की बारं बारता और इस घटना को प्रभावित करने िाले अन्य वनयंत्रण कारकों, जैस-े
भूविज्ञान, भू-आकृ वतक कारक, ढाल, भूवम उपयोग, िनस्पवत आिरण और मानि क्रक्रयाकलापों
आक्रद के आधार पर भारत को विवभन्न सुभद्य
े ता क्षेत्रों (़ोनों) में विभावजत क्रकया गया है, वजन्हें
नीचे दी गई तावलका में दशावया गया है:
अत्यवधक उच्च अत्यवधक अवस्थर, वहमालय और अंडमान एिं वनकोबार में सापेवक्षक रूप से
सुभेद्यता क्षेत्र युिा पिवतीय श्रृंखलाएं।
पवश्चमी घाट और नीलवगरर में खड़ी ढाल युक्त अवधक िषाव िाले क्षेत्र, उत्तर-
पूिी क्षेत्र,
भूकंप प्रभािी क्षेत्र
57 www.visionias.in ©Vision IAS
अत्यवधक मानि क्रक्रयाकलापों िाले क्षेत्र, विशेषकर सड़कों, बांध आक्रद के
वनमावण से संबंवधत।
उ्च सुभेद्यता उ्च सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यवधक उच्च सुभेद्यता क्षेत्रों से वमलती-जुलती
क्षेत्र पररवस्थवतयााँ हैं।
इन दोनों में अंतर मात्र भूस्खलन को वनयंवत्रत करने िाले कारकों के संयोजन,
गहनता और बारं बारता का है।
वहमालय क्षेत्र के सभी राज्य और उत्तर-पूिी राज्य (असम के मैदानों को
छोड़कर) इस क्षेत्र में सवम्मवलत हैं।
मध्यम से वनम्न िृवष्ट िाले क्षेत्र जैसे क्रक -
वनम्न सुभेद्यता o लद्दाख और वहमाचल प्रदेश में स्पीवत के पार वहमालयी क्षेत्र,
क्षेत्र o अरािली में विषम लेक्रकन वस्थर उच्चािच एिं वनम्न िषवण िाले क्षेत्र,
o पवश्चमी और पूिी घाट के िृवष्ट छाया क्षेत्र एिं
o दक्कन पठार
झारखडड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कनावटक,
तवमलनाडु , गोिा और के रल में खनन और भूवम धाँसने के कारण भूस्खलन एक
सामान्य घटना है।
अन्य क्षेत्र जहां तक भूस्खलन का प्रश्न है, भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हररयाणा,
उत्तर प्रदेश, वबहार, पवश्चम बंगाल (दार्नजसलग वजले को छोड़कर), असम (काबी
आंगलोंग वजले को छोड़कर) और दवक्षणी राज्यों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन से सुरवक्षत
हैं।
58 www.visionias.in ©Vision IAS
भूस्खलन के कारण
भारी िषाव: भारी िषाव भूस्खलनों का मुख्य कारण है।
वनिवनीकरण: वनिवनीकरण भूस्खलनों का एक अन्य प्रमुख कारण है। िृक्ष, झावड़यााँ और घास वमट्टी
के कणों को बााँध कर रखते हैं। िृक्षों को काटने से पिवतीय ढलान अपने सुरक्षात्मक आिरण को खो
देते हैं। िषाव जल इस प्रकार के ढलानों पर वनबावध गवत से प्रिावहत होता है।
भूकंप और ज्िालामुखी विस्फोट: भूकंप वहमालयी क्षेत्रों का एक सामान्य लक्षण है। कं पन पहाड़ों
और चट्टानों को अवस्थर कर देते हैं
और चट्टानें नीचे की ओर लुढ़कती हैं।
ज्िालामुखी विस्फोट भी पिवतीय
क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण हो सकते
हैं।
सड़कों का वनमावण: पिवतीय क्षेत्रों में
विकास गवतविवध के वलए सड़कों का
वनमावण क्रकया जाता है। सड़क के
वनमावण की प्रक्रक्रया के दौरान, बड़ी
मात्रा में चट्टानों और मलबे को
हटाया जाना होता है। यह प्रक्रक्रया
शैल संरचना को विस्थावपत कर देती
है और ढलानों की प्रिणता को
पररिर्नतत कर देती है। इस प्रकार
पिवतीय क्षेत्रों में सड़कों का वनमावण
भूस्खलन का कारण हो सकता है।
स्थानांतरी कृ वष: भारत के उत्तर-पूिी भाग में, स्थानांतरी कृ वष की प्रथा के कारण भूस्खलनों की
संख्या और बारं बारता में िृवि हुई है।
मकान और अन्य भिनों का वनमावण: वनरं तर बढ़ती जनसंख्या को आश्रय प्रदान करने एिं पयवटन
को अवधकावधक बढ़ािा देने के वलए अवधक से अवधक घर एिं होटल बनाए जा रहे हैं। वनमावण
प्रक्रक्रयाओं में भारी मात्रा में मलबा उत्पन होता है। अत्यवधक मलबा भूस्खलन का कारण बनता है।
भूस्खलन संकट के पररणाम
भूस्खलन आपदाओं के समाज पर अल्पकावलक और दीघवकावलक, दोनों प्रकार के प्रभाि पड़ते हैं। इससे
आर्नथक और सामावजक जीिन तथा पयाविरण में असंतुलन उत्पन्न होता है।
अल्पकावलक प्रभाि:
o प्राकृ वतक सौंदयव को
नुकसान
o सड़क मागव में अिरोध,
रे ल पटररयों का टू टना
o चट्टानें वगरने के कारण
जल िावहकाओं (चैनलों)
का बावधत होना
o भूस्खलनों के कारण नदी
मागों के पररितवन से
बाढ़ आ सकती है
o जान-माल की क्षवत
दीघवकावलक प्रभाि:
o भूदश्ृ य में पररितवन जो
स्थायी हो सकते हैं,
o कृ वषयोग्य भूवम की
हावन
o अपरदन ि मृदा क्षवत के रूप में पयाविरणीय प्रभाि,
o जनसंख्या विस्थापन एिं आबाक्रदयों और प्रवतष्ठानों का स्थान पररितवन
o जल के स्रोतों का सूखना
59 www.visionias.in ©Vision IAS
भूस्खलन संकट शमन
संकट िाले क्षेत्रों की पहचान एिं चयवनत स्थलों पर वनगरानी और पूिव चेतािनी प्रणाली स्थावपत
करने के अवतररक्त विवशष्टट ढालों को वस्थर एिं प्रबंवधत क्रकया जाना चावहए।
भूस्खलन से वनपटने के वलए क्षेत्र-विवशष्ट उपाय अपनाना सदैि उपयुक्त रहता है।
भूस्खलन के वलए सामान्य रूप से प्रिण क्षेत्रों के वनधावरण हेतु संकट का मानवचत्रण (Hazard
mapping) क्रकया जाना चावहए।
अिैज्ञावनक वनमावण और सड़क एिं बांध बनाने जैसे अन्य विकास कायों पर प्रवतबंध, कृ वष को
घारटयों एिं मध्यम ढाल िाले क्षेत्रों तक सीवमत करना एिं उच्च सुभेद्यता िाले क्षेत्रों में बड़ी
बवस्तयों के विकास पर वनयंत्रण जैसे उपायों को लागू क्रकया जाना चावहए।
जल प्रिाह को कम करने के वलए बड़े पैमाने पर िनीकरण कायवक्रमों एिं बांधों के वनमावण को
बढ़ािा देना चावहए।
उत्तर-पूिी पहाड़ी राज्यों में झूम या स्थानांतरी कृ वष को प्रवतस्थावपत कर सीढ़ीनुमा कृ वष को
बढ़ािा क्रदया जाना चावहए।
भूवम को क्रफसलने से रोकने के वलए पिवतीय ढालों पर धारक वभवत्तयााँ (Retaining walls)
बनायी जा सकती हैं।
सुभेद्य ढलानों एिं मौजूदा खतरनाक भूस्खलनों का उपचार करना।
भूस्खलन प्रिण क्षेत्रों में अिैज्ञावनक विकास गवतविवधयों को प्रवतबंवधत करना।
खुदाई, वनमावण और ग्रेसडग के वलए संवहताएं (कोड) तैयार करना।
ितवमान विकास का संरक्षण।
भूस्खलन बीमा एिं नुकसान की क्षवतपूर्नत हेतु उवचत व्यिस्था का वनधावरण करना।
ितवमान चुनौवतयााँ
विवभन्न स्तरों, अथावत् राष्ट्रीय, राज्य, वजला, नगरपावलका/पंचायत स्तरों पर आपदा प्रबंधन
योजनाओं के विकास में भूस्खलन सम्बन्धी सचताओं को एकीकृ त करना।
भूस्खलन के अलग-अलग उपचारण की कायवप्रणाली के स्थान पर वनयंत्रण उपायों के सवम्मवलत
एिं समग्र कायाांियन की ओर कदम बढ़ाना।
उवचत ढाल संरक्षण, वनयोवजत शहरीकरण, विवनयवमत भूवम उपयोग और पयाविरण अनुकूल
भूवम प्रबंधन पिवतयााँ अपनाने के वलए तकनीकी-कानूनी व्यिस्था।
पयाविरण को सोद्देश्य क्षवत पहुाँचाने एिं अस्िस्थ वनमावण प्रथाओं के विरुि शून्य सवहष्टणत
ु ा।
नए वनमावण को प्रशावसत करने िाले कानून एिं समस्याग्रस्त ढलानों और भूस्खलन प्रिण क्षेत्रों में
ितवमान भूवम उपयोग को पररिर्नतत करना।
बहु-संस्थागत और बहु-अनुशासनात्मक टीमों के प्रबंधन में निाचार।
आपदा ज्ञान नेटिकव की स्थापना एिं राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के प्रसार के वलए तंत्र, अंतरावष्ट्रीय
संपकों के वलए तंत्र, सहयोग और संयुक्त पहलें।
3.2.7. बादल फटना (Cloudburst)
बादल फटना क्या है?
कु छ क्रकलोमीटर के दायरे के भीतर अचानक मूसलाधार िषाव का होना बादल फटना कहलाता है।
यह आमतौर पर कु छ वमनट से अवधक समय तक नहीं होता है लेक्रकन पूरे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त करने
में सक्षम होता है। बादल फटने से होने िाली िषाव आमतौर पर 100 वमलीमीटर प्रवत घंटे से
अवधक होती है।
बादल फटने की पररघटना क्रकस प्रकार वनर्नमत होती है?
जल की सूक्ष्म बूाँदों (droplets) से पूररत मानसूनी बादल मैदानी भागों के ऊपर से होकर गवत
करते हैं। उष्टण िायु धाराएाँ इन बादलों को ऊपर की ओर धक्का देती रहती हैं और उन्हें िषाव नहीं
करने देतीं।
वनरं तर पहले से अवधक जल की बूाँदें एकवत्रत होती जाती हैं और पिवत या पहाड़ी के ऊपरी भाग
की ओर गवत करने के साथ बादल का आकार बड़ा होता जाता है। बादल शीघ्र ही गवत करना बन्द
कर देते हैं क्योंक्रक पिवतों के ऊपरी भागों में पिन प्रिाह नाममात्र ही होता है।
60 www.visionias.in ©Vision IAS
बादलों में जल की बूद
ाँ ों को धारण करने िाली उष्टण िायु ठं डी हो जाती है। पररणामस्िरूप बादल
गीले कागज के थैले की तरह फट जाता है और मूसलाधार िषाव होती है।
भारत में बादल फटने का जोवखम
बादल फटने की विवशष्ट पररभाषा के अनुसार, यक्रद लगभग 10 क्रक.मी. X 10 क्रक.मी. क्षेत्र में प्रवत
घंटे 10 सेमी या उससे
अवधक की िषाव दजव की
जाती है तो इसे बादल फटने
की घटना के रूप में िगीकृ त
क्रकया जाता है। इसका अथव
यह है क्रक आधे घंटे में 5
सेमी की िषाव को भी बादल
फटने के रूप में िगीकृ त
क्रकया जाएगा। सामान्यतैः
भारत, एक िषव में लगभग
116 सेमी िषाव प्राप्त करता है अथावत् देश में प्रत्येक क्षेत्र को औसत रूप से, के िल इतनी िषाव की
मात्रा प्राप्त करने की अपेक्षा करनी चावहए। इसवलए बादल का फटना मात्र एक घंटे में उस क्षेत्र
की िार्नषक िषाव के 10-12 प्रवतशत के वलए वजम्मेदार होगा।
भूमंडलीय तापन के कारण वपछले कु छ दशकों में चरम िषवण की घटनाओं में वनरं तर िृवि हुई है;
यह माना जा रहा है क्रक संभित: बादल फटने की घटनाओं में भी िृवि हो रही होगी।
बादल फटने की कु छ बड़ी घटनाएाँ
2 अगस्त, 2010 लेह, लद्दाख मात्र 1 घंटे में 25 सेमी िषाव
29 वसतम्बर, 2010 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मात्र 1 घंटे में 14.4 सेमी िषाव
4 अक्टू बर, 2010 पाषाण, पुणे मात्र 1.5 घंटे में 18.2 सेमी िषाव
26 जुलाई, 2005 मुम्बई 10 घंटे में 144.8 सेमी िषाव
बादल फटने की घटना का वितरण प्रवतरूप
बादल फटने की घटना मैदानी भागों में भी होती है, लेक्रकन पिवतीय क्षेत्रों में इसके घरटत होने की
संभािना अवधक होती है क्योंक्रक इसका संबंध क्षेत्र की स्थलाकृ वत से होता है। उदाहरण के वलए,
खड़ी ढाल िाली पहावड़यााँ इन मेघों के वनमावण हेतु अनुकूल होती हैं। बादलों का फटना के िल उसी
वस्थवत में ध्यान आकर्नषत करता है जब उसके पररणामस्िरूप जीिन और संपवत्त का बड़े पैमाने
पर विनाश हुआ हो, जो क्रक मुख्यतैः पिवतीय क्षेत्रों में होता है।
बादल फटने के पररणाम
आकवस्मक बाढ़ / भूस्खलन;
मकान का ढहना, सम्पवत्त का नुकसान ;
यातायात का अस्त-व्यस्त होना; एिं
बड़े पैमाने पर मानि जीिन की क्षवत।
बादल फटने के विषय में पूिावनम
ु य
े ता
छोटे पैमाने पर घरटत होने के कारण बादल फटने की घटना के पूिावनुमान हेतु कोई संतोषजनक
तकनीक नहीं है। बादल फटने के विषय में लगभग 6 घंटे पहले, या कभी-कभी 12-14 घंटे पहले,
61 www.visionias.in ©Vision IAS
पता लगाने में समथव होने के वलए रडारों के अत्यवधक उच्च क्षमता िाले नेटिकव की आिश्यकता
होती है। यह अत्यवधक महंगा होगा। भारी िषाव होने की संभािनाओं िाले क्षेत्रों की पहचान के िल
सीवमत पैमाने पर की जा सकती है। हालााँक्रक, बादल फटने की घटनाओं के अनुकूल क्षेत्रों एिं
मौसम की वस्थवतयों की पहचान करके अवधकांश क्षवत को टाला जा सकता है।
नोट: बादल फटने के संकट का शमन; इससे सम्बंवधत चुनौवतयााँ; इस आपदा के पूि,व उसके दौरान और
पश्चात् क्या करें और क्या न करें आक्रद से संबंवधत सािधावनयों एिं उपायों के साथ-साथ ही
आकवस्मक/शहरी बाढ़ एिं भूस्खलन के उपाय भी चलते रहते हैं।
प्रश्न: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (एन. डी. एम. ए.) के सुझािों के संदभव में, उत्तराखंड के अनेकों
स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के वलए अपनाए जाने िाले
उपायों पर चचाव कीवजए। (UPSC, 2016)
3.2.8. चक्रिात (Cyclone)
चक्रिात क्या है?
सामान्य रूप में चक्रिात वनम्न दाब के कें द्र होते हैं वजनके चारों तरफ संकेंद्रीय समिायुदाब रे खाएं
विस्तृत होती हैं तथा कें द्र से बाहर की ओर िायुदाब बढ़ता जाता है, पररणामस्िरूप पररवध से कें द्र
की ओर हिाएं चलने लगती हैं। वजनकी क्रदशा उत्तरी गोलाधव में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा
दवक्षणी गोलाधव में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। चक्रिातों का आकार प्रायैः गोलाकार,
अंडाकार या V अक्षर के समान होता है। जलिायु तथा मौसम में चक्रिात का पयावप्त क महत्ि होता
है, क्योंक्रक इनके द्वारा क्रकसी भी स्थान जहां पर यह पहुंचते हैं, िहााँ की िषाव तथा तापमान
प्रभावित होती है। चक्रिातों को िायुमड
ं लीय विक्षोभ भी कहा जाता है।
अिवस्थवत के आधार पर चक्रिातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं:
(i) शीतोष्टण करटबंधीय चक्रिात (Temperate cyclones)
(ii) उष्टणकरटबंधीय
चक्रिात (Tropical
cyclones)
शीतोष्टण करटबंधीय
चक्रिात
मध्य अक्षांशों में
वनर्नमत िायु
विक्षोभ के कें द्र में
वनम्न दाब तथा
बाहर की ओर
उच्च दाब होता है।
इस चक्रिात में
समदाब रे खाएं V
आकार की होती
हैं। इनका वनमावण दो विपरीत स्िभाि िाली ठं डी तथा उष्टणाद्रव िायुरावश के वमलने के कारण
होता है तथा इनका क्षेत्र 35 वडग्री से 65 वडग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलािव में पाया जाता है,
जहां पर पछु आ पिनों के प्रभाि में यह पवश्चम से पूिव क्रदशा में गवत करते हैं। भारत में इस
चक्रिात का प्रभाि शीत ऋतु में पवश्चमी विक्षोभ के रूप में दृवष्टगोचर होता है। यह चक्रिात
भारत के उत्तर पवश्चमी क्षेत्रों में रबी की फसल के वलए लाभदायी है। यह चक्रिात भारत के वलए
लाभकारी है इसीवलए इसका आपदा के रूप में अध्ययन नहीं करते हैं।
उष्टणकरटबंधीय चक्रिात
उष्टणकरटबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रिात को उष्टणकरटबंधीय चक्रिात कहते हैं। यह वनम्न िायुदाब
िाले अवभसरणीय पररसंचरण तंत्र होते हैं, वजनका औसत व्यास 640 क्रकलोमीटर तक होता है।
िायु संचरण की क्रदशा उत्तरी गोलाधव में घड़ी की सुइयों के प्रवतकू ल तथा दवक्षणी गोलाधव में
62 www.visionias.in ©Vision IAS
अनुकूल क्रदशा में होती है। उष्टणकरटबंधीय चक्रिात अत्यवधक शवक्तशाली, विनाशकारी, खतरनाक
तथा घातक िायुमंडलीय तूफान होते हैं। भारत के पूिी तटीय प्रदेशों में उष्टणकरटबंधीय चक्रिात
से प्रवतिषव भारी आपदा आती है। भारत के पूिी तटीय प्रदेशों में इसे चक्रिात के नाम से जाना
जाता है। अतैः हम इस अध्याय में चक्रिात का विस्तृत अध्ययन करें गे। जो वनम्नवलवखत है:
उष्टण करटबंधीय चक्रिात का वनमावण
अनुकूल पररवस्थवतयााँ: उष्टणकरटबंधीय चक्रिात िायुमंडलीय और महासागरीय घटनाएं होती हैं।
इसकी उत्पवत्त से सम्बंवधत कु छ वचवन्हत अनुकूल पररवस्थवतयााँ वनम्नवलवखत हैं:
उष्टण करटबन्धीय चक्रिातों की उत्पवत महासागर के ऊपर होती है। इसकी उत्पवत्त विषुित रे खा
के दोनों ओर 5o-30o अक्षांशों तक दोनों गोलािों में होती है।
समुद्री सतह गमव (26o–27o सेंटीग्रेड से अवधक तापमान) होनी चावहए एिं इस तापन का विस्तार
सतह के नीचे 60 मीटर की गहराई तक होना चावहए। साथ ही इस सतह के ऊपर वस्थत विशाल
िायु में प्रचुर मात्रा में जल िाष्टप (िाष्टपीकरण द्वारा) होनी चावहए।
िायुमंडल में लगभग 5,000 मीटर की ऊाँचाई तक उच्च सापेवक्षक आद्रवता विद्यमान हो,
ऊपर उठती आद्रव िायु के संघनन के कारण अवतविशाल ऊध्िावधर कपासी मेघ के वनमावण को
प्रोत्सावहत करने िाली िायुमंडलीय अवस्थरता विद्यमान हो,
िायुमंडल के वनम्न और उच्च स्तरों के बीच ऊध्िावधर पिन अपरूपण (कतवन) कम या क्षीण होना
चावहए जो मेघों से उत्पन्न एिं वनमुक्
व त ताप को क्षेत्र से वनकलने नहीं देता है (ऊध्िावधर पिन
अपरूपण, िायुमंडल के वनम्न और उच्च स्तरों के बीच पिन के पररितवन की दर होती है।),
चक्रिात भंिर (cyclonic vorticity) (िायु के घूणन
व की दर) की उपवस्थवत होनी चावहए जो िायु
की चक्रिातीय गवत को प्रारम्भ करता है और इसे बनाए रखने में सहयोग करता है।
चक्रिातों को विि के विवभन्न भागों में वभन्न-वभन्न नामों से जाना जाता है:
अंतरावष्ट्रीय वतवथरे खा के पवश्चम में उत्तरी-पवश्चमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टाइफ़ू न;
उत्तरी अटलांरटक महासागर, अंतरावष्ट्रीय वतवथ रे खा के पूिव में उत्तरी-पूिी प्रशांत महासागर और
दवक्षणी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में हररके न;
दवक्षणी-पवश्चमी प्रशांत महासागर और दवक्षणी-पूिी वहन्द महासागर के क्षेत्रों में उष्टणकरटबंधीय
चक्रिात ;
उत्तरी वहन्द महासागर क्षेत्र में भीषण चक्रिाती तूफ़ान;
दवक्षणी-पवश्चमी वहन्द महासागरीय क्षेत्र में उष्टणकरटबंधीय चक्रिात;
ऑस्रेवलया में विली-विली ; एिं
दवक्षणी अमेररका में टोरनेडो ।
चक्रिात में, वनम्न दाब कें द्र के चारों ओर - उत्तरी गोलािव में िामाितव क्रदशा में एिं दवक्षणी गोलािव में
दवक्षणाितव क्रदशा में - प्रबल पिनें प्रिावहत होती हैं, हालांक्रक कें द्र (वजसे चक्रिात की आंख कहते हैं) में
पिन बहुत कम होती है और आम तौर पर यह क्षेत्र मेघ और िषाव रवहत होता है। कें द्र से लगभग 20 से
30 क्रक.मी. की दूरी पर पिनें तेजी से अपना अवधकतम िेग प्राप्त कर लेती हैं (प्राय: 150 क्रक.मी./घन्टे
से अवधक) और इसके आगे क्रवमक रूप से इनका िेग कम होता जाता है और लगभग 300 से 500
क्रक.मी. की दूरी पर सामान्य हो जाता है। चक्रिातों का व्यास 100 से 1000 क्रक.मी. तक होता है
लेक्रकन इनका प्रभाि महासागरों एिं साथ ही तट के क्रकनारे कई हजार क्रकलोमीटर के क्षेत्र में अवधक
होता है। इसकी ऊजाव का स्रोत चक्रिात की आाँख के 100 क्रकलोमीटर वत्रज्या में वस्थत होता है, जहााँ
आाँख के व्यास से परे एक संकीणव क्षेत्र में अत्यवधक प्रबल पिनें उत्पन्न हो सकती हैं, वजनकी गवत कभी-
कभी 250 क्रक.मी. प्रवत घंटे से अवधक होती है।
63 www.visionias.in ©Vision IAS
भारत में चक्रिात के जोवखम
भारत की तटरे खा 7,516 क्रकलोमीटर लम्बी है, वजसमें से 5,422 क्रकलोमीटर मुख्यभूवम के
क्रकनारे हैं तथा 2094 क्रकलोमीटर द्वीपीय क्षेत्र के अंतगवत हैं वजसमें से 132 क्रकलोमीटर लक्षद्वीप
में, तथा 1,962 क्रकलोमीटर अंडमान तथा वनकोबार द्वीप समूह में है। यद्यवप उत्तरी वहन्द
महासागर बेवसन (भारतीय तट समेत) में विि के के िल 7 प्रवतशत चक्रिात आते हैं, लेक्रकन
तुलनात्मक रूप से इनका प्रभाि गंभीर तथा विनाशकारी होता है। ऐसा विशेषतैः तब होता है जब
ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी की सीमा पर वस्थत तटों से टकराते हैं। औसतन, प्रवतिषव पांच से छैः
उष्टणकरटबंधीय चक्रिात वनर्नमत होते हैं वजनमें से दो या तीन विनाशकारी हो सकते हैं। बंगाल की
खाड़ी में अरब सागर की तुलना में कहीं अवधक तूफ़ान आते हैं तथा यह अनुपात लगभग 4:1 का
है।
उष्टणकरटबंधीय चक्रिात मई-जून तथा अक्टू बर-निम्बर के महीने में आते हैं। उत्तरी वहन्द
महासागर में अत्यवधक तीव्रता एिं आिृवत्त िाले चक्रिात बाई-मोडल (bi-modal) प्रकृ वत के होते
हैं। उनकी प्राथवमक उच्च आिृवत्त निम्बर में तथा वद्वतीयक उच्च आिृवत्त मई में होती है। साथ में
प्रिावहत विनाशकारी पिनों, तूफ़ानी लहरों तथा भारी िषाव के कारण उत्तरी वहन्द महासागर
(बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर) में लैंडफॉल के समय आपदा की संभािना विशेष रूप से
अवधक होती है।
भारत के चक्रिात संभावित क्षेत्र
देश में 13 तटीय राज्य तथा कें द्र शावसत प्रदेश हैं वजनमें वस्थत 84 तटीय वजले उष्टणकरटबंधीय
चक्रिात से प्रभावित हैं। पूिी तट पर चार राज्य (तवमलनाडु , आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पवश्चम
बंगाल) तथा एक कें द्र शावसत प्रदेश (पुर्डडु चेरी) तथा पवश्चमी तट पर एक राज्य (गुजरात)
चक्रिात आपदा के प्रवत अत्यवधक सुभेद्य हैं।
64 www.visionias.in ©Vision IAS
चक्रिात संबध
ं ी संकट के पररणाम
तटीय प्रदेशों के आस-पास वनचले क्षेत्रों का जलमि होना;
भारी बाढ़, भूस्खलन;
तटों तथा तटबंधों का अपरदन;
िनस्पवत ि अिसंरचना का विनाश तथा मानि जीिन की क्षवत;
भूवम की उिवरता के साथ-साथ फसलों तथा खाद्य-आपूर्नत की क्षवत;
भूवम तथा पाइप द्वारा जल आपूर्नत का संदषू ण; एिं
संचार सलक में गंभीर व्यिधान ।
भारत में चक्रिात चेतािनी प्रणाली
चक्रिातीय वनम्न दाब एिं इसके विकास का पता इसके क्षवत करने के कु छ घंटे से लेकर कु छ क्रदन
पूिव तक लगाया जा सकता है। उपग्रह इन चक्रिातों के संचलन का पता लगा लेते हैं वजसके आधार
पर प्रभावित होने की संभािना िाले क्षेत्रों से लोगों को बाहर वनकाल वलया जाता है। इसके
लैंडफॉल की सटीकता की भविष्टयिाणी करठन होती है। लैंडफॉल संबंधी सटीक भविष्टयिाणी के
पश्चात संकटापन्न जनसंख्या को स्ियं के बचाि के वलए के िल कु छ घंटों का समय वमल पाता है।
भारत की चक्रिात चेतािनी प्रणाली विि की सबसे अ्छी चक्रिात चेतािनी प्रणावलयों में से
एक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) िायु की गवत ि क्रदशा का पता लगाने, उस पर नजर
रखने तथा चक्रिात की भविष्टयिाणी करने के वलए नोडल विभाग है। चक्रिात के संबंध में
जानकारी INSAT उपग्रह की सहायता से जुटाई जाती है। चक्रिात के विषय में चेतािनी कई
साधनों यथा उपग्रह आधाररत आपदा चेतािनी प्रणावलयों, रे वडयो, टेलीवि़न, टेलीफोन, फै क्स,
सािवजवनक उद्घोषणाओं तथा प्रेस बुलेरटन आक्रद के माध्यम से प्रसाररत की जाती है। इन
चेतािवनयों को आम जनता, मछु आरों के समुदायों (विशेषतैः जो समुद्र में मछली पकड़ने गए हों),
पत्तन प्रावधकाररयों, व्यािसावयक उड़ान सेिाओं तथा सरकारी तंत्र तक प्रसाररत क्रकया जाता है।
चक्रिात संकट का शमन
एक प्रभािी चक्रिात आपदा रोकथाम एिं शमन योजना के वलए वनम्नवलवखत की आिश्यकता होती है:
प्रभािी चक्रिात पुिावनम
ु ान तथा चेतािनी सेिाएं;
सरकारी एजेंवसयों, विशेषकर पत्तनों, मत्स्य-पालन, जहा़रानी जैसे समुद्र संबि क्षेत्रों तथा आम
लोगों तक चेतािवनयों का तीव्र प्रसार, तथा
सुभेद्य क्षेत्रों में चक्रिात आश्रय-स्थलों का वनमावण, लोगों को सुरवक्षत स्थानों पर भेजने के वलए
एक कु शल तंत्र तथा क्रकसी भी पररवस्थवत से वनपटने के वलए सभी स्तरों पर सामुदावयक
तैयाररयां।
चक्रिात आश्रय-स्थल (Cyclone Shelters)
चक्रिात के दौरान मानि जीिन की हावन को रोकने के सिाववधक सफल तरीकों में से एक चक्रिात
आश्रय-स्थल का वनमावण करना है। सघन जनसंख्या िाले तटीय क्षेत्रों में जहां बड़े स्तर पर लोगों को
प्रभावित क्षेत्र से बाहर वनकालना संभि नहीं होता, सािवजवनक भिनों का उपयोग चक्रिात आश्रय-
स्थलों के रूप में क्रकया जा सकता है। इन इमारतों को इस प्रकार अवभकवल्पत (वड़ाइन) क्रकया जा
सकता है क्रक उसमें अग्रभाग ररक्त हो तथा िायु की क्रदशा में कम से कम वछद्र हों। भिनों के
अपेक्षाकृ त छोटे वहस्से को तूफ़ान के सम्मुख रहना चावहए, ताक्रक िायु का प्रवतरोध कम से कम रहे।
तूफ़ान का प्रभाि कम करने हेतु अथव बमव (earth berm) संरचनाओं और भिनों के अग्रभाग में ग्रीन
बेल्ट का प्रयोग क्रकया जा सकता है।
उपयुवक्त वबन्दुओं पर विचार करते हुए संभावित जोवखम शमन संबध
ं ी उपाय वनम्नवलवखत हो सकते हैं:
तटीय क्षेत्रों में िृक्षारोपण: यह ग्रीन बेल्ट क्षवत को कम करता है क्योंक्रक िन आकवस्मक बाढ़ों तथा
शवक्तशाली पिनों के विरुि बफर जोन के रूप में कायव करते हैं। िनों के अभाि में चक्रिात वनबावध
रूप से भीतरी भागों को प्रभावित कर सकते हैं।
65 www.visionias.in ©Vision IAS
संकट का मानवचत्रण (Hazard mapping): िायु की गवत तथा क्रदशा संबंधी मौसमी आंकड़े, एक
विवशष्ट गवत पर चक्रिात के घरटत होने का पैटनव उपलब्ध कराते हैं। संकट का मानवचत्रण क्रकसी
भी क्रदए गए िषव में चक्रिात के प्रवत सुभेद्य क्षेत्रों का वििरण प्रदान करता है तथा चक्रिात की
प्रचंडता तथा उक्त क्षेत्र में विविध प्रकार की क्षवत की गंभीरता का अनुमान लगाता है।
भूवम उपयोग वनयंत्रण: इसे इस
प्रकार अवभकवल्पत क्रकया जा
सकता है क्रक महत्िपूणव
गवतविवधयााँ सुभेद्य क्षेत्रों में कम
से कम संचावलत हों। बाढ़ के
मैदानों में आबाद बवस्तयों की
अिवस्थवत सिाववधक जोवखम में
होती है। भूवम उपयोग
अवभकल्पना (वड़ाइन) में मुख्य
सुविधाओं के स्थान को
अवनिायव रूप से वचवन्हत क्रकया
जाना चावहए। भूवम उपयोग को
विवनयवमत करने के वलए नीवतयााँ उपलब्ध होनी चावहए तथा भिनों वनमावण संवहता का प्रितवन
क्रकया जाना चावहए।
योजनाबि संरचनाएं: पिन के दबाि को झेलने के वलए योजनाबि संरचनाएं वनर्नमत की जानी
चावहए। उपयुक्त स्थान का चयन भी अत्यंत महत्िपूणव है। तटीय क्षेत्रों में अवधकांश इमारतें वबना
क्रकसी योजनाबि वड़ाइन के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामवग्रयों से ही बनाई जाती हैं। वनमावण
संबंधी बेहतर पिवतयों को अपनाया जाना चावहए, जैसे:
o चक्रिातीय तूफ़ान तटीय क्षेत्रों को जलप्लावित कर देते हैं। इसवलए, भिन आक्रद संरचनाओं
को खंभों या टीलों के ऊपर बनाने की सलाह दी जाती है।
o पिन का प्रवतरोध कर पाने तथा बाढ़ से होने िाली क्षवत से बचने के वलए घरों को मजबूत
बनाया जाना चावहए। िस्तुओं को ऊपर उठाने िाले बल का प्रवतरोध कर पाने तथा िस्तुओं
के उड़ जाने से बचाने के वलए संरचना को जकड़ कर रखने िाले वहस्सों को अ्छी तरह बांधा
जाना चावहए। उदाहरण के वलए छतों को अवधक न लटकाया जाए तथा बाहर वनकले भागों
को अ्छी तरह से बांधा जाए।
o िृक्षों की एक पंवक्त सुरक्षा किच (shield) का काम कर सकती है। यह चक्रिात की ऊजाव को
कम करती है।
o भिनों को पिन तथा जल के सन्दभव में प्रवतरोधी होना चावहए।
o खाद्य आपूर्नतयों का भंडारण करने िाली इमारतों का िायु तथा जल से बचाि क्रकया जाना
चावहए।
o नदी तटबंधों की रक्षा की जानी चावहए।
o संचार लाइनें भूवमगत रूप से वबछाई जानी चावहए।
o सुभेद्य स्थलों पर सामुदावयक आश्रय के वलए म़बूत कक्षों का वनमावण क्रकया जाना चावहए।
बाढ़ प्रबंधन: भारी िषाव, ते़ पिनों तथा तूफान के कारण चक्रिात प्रभावित क्षेत्र बाढ़ का वशकार
हो जाते हैं। भूस्खलन की संभािनाएं भी रहती हैं। इसवलए बाढ़ शमनकारी उपायों को सवम्मवलत
क्रकया जा सकता है।
िानस्पवतक आ्छादन में सुधार करना: पौधों तथा िृक्षों की जड़ें वमट्टी को बांधे रखती हैं तथा
अपरदन को रोकती हैं और जल के बहाि को धीमा कर देती हैं, इससे बाढ़ की संभािना समाप्त क या
कम हो जाती है। पंवक्तयों में लगाए गए िृक्ष तीव्र पिनों के विरुि सुरक्षा किच का कायव करते हैं।
तटों पर िातरोधी िृक्षारोपण कर पिनों की विध्िंसक गवत को कम क्रकया जा सकता है। इससे
विनाशकारी प्रभाि में कमी आ जाती है।
66 www.visionias.in ©Vision IAS
राष्ट्रीय चक्रिात जोवखम शमन योजना (National Cyclone Risk Mitigation Project:
NCRMP)
भारत सरकार ने तटीय समुदायों (जो सामान्यतैः वनधवन तथा समाज के कम़ोर िगों से हैं) की
सुभेद्यता का समाधान करने के वलए जनिरी, 2011 में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के वलए
NCRMP चरण-I का आरम्भ क्रकया। NCRMP चरण–II को एक कें द्र प्रायोवजत योजना के रूप
गोिा, गुजरात, कनावटक, के रल, महाराष्ट्र तथा पवश्चम बंगाल राज्यों में लागू करने के वलए के न्द्रीय
मंवत्रमंडल द्वारा जुलाई, 2015 में स्िीकृ वत प्रदान की गयी थी।
इस पररयोजना का लक्ष्य चक्रिात के प्रवत सुभेद्यता को कम करना तथा लोगों एिं अिसंरचना को
आपदा प्रत्यास्थ बनाना था। इस पररयोजना के चार मुख्य घटक हैं:
o घटक A – अंवतम सबदु तक कनेवक्टविटी।
o घटक B – संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपाय।
o घटक C – चक्रिात संकट जोवखम शमन हेतु तकनीकी सहायता, क्षमता वनमावण तथा ज्ञान सृजन
o घटक D – पररयोजना प्रबंधन तथा कायावन्ियन सहायता।
इस पररयोजना का विस्तृत या व्यापक लाभ चक्रिात संबंधी पुिावनुमान, चक्रिात संबंधी जोवखम
का शमन तथा बहु-संकट जोवखम प्रबंधन में क्षमता वनमावण है। पररयोजना के अंतगवत वनर्नमत की
जाने िाली मुख्य अिसंरचनाओं में बहुउद्देशीय चक्रिात आश्रय-स्थल (आश्रय-सह-गोदाम सवहत),
बवस्तयों तक अवभगम सड़कें /पुल तथा समुद्री तटबंध आक्रद का वनमावण सवम्मवलत है।
ितवमान चुनौवतयां
राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर वनयोजन तथा समन्िय की कमी के कारण जारी की गयी
चेतािवनयों के संबंध में पयावप्त क कायविाही न कर पाने के साथ-साथ लोगों द्वारा इनके जोवखम को न
समझ पाना।
संचार संबंधी टर्नमनल-एंड उपकरणों तथा संचार सहायक उपकरण सहायता का अभाि।
आपदाओं के प्रवत प्रभािी प्रत्यास्थता के वनमावण हेतु आपदा प्रबंधन में आधारभूत स्तर की
भागीदारी का अभाि।
NDMA तथा गृह मंत्राल में ऐसे पूणत
व ैः स्िचावलत तथा आधुवनकतम संचालन कें द्र का अभाि
वजसमें रो़-मराव की गवतविवधयों तथा साथ ही आपदाओं के समय के वलए सभी टर्नमनल-एंड
सुविधाएं तथा संचार कनेवक्टविटी उपलब्ध हो।
देश में आपदा प्रबंधन के वलए विविध प्रकार के नेटिकों की स्थापना हेतु विवभन्न एजेंवसयों द्वारा
स्थावपत नेटिकों के एकीकरण की आिश्यकता।
चक्रिात के पश्चात संचार तथा रांसवमशन टॉिरों जैसी सुवनयोवजत रूप से अवभकवल्पत
संरचनाओं की विफलता।
3.2.9. सू खा (Drought)
सूखा क्या है?
सूखा ऐसी वस्थवत को कहा जाता है जब लम्बे समय तक कम िषाव, अत्यवधक िाष्टपीकरण और
जलाशयों तथा भूवमगत जल के अत्यवधक प्रयोग के कारण जल का कमी हो जाए। जल की
उपलब्धता में कमी से कृ वष, पेयजल आपूर्नत तथा उद्योग प्रभावित होते हैं। यह मंद गवत से आने
िाली आपदा होती है। यह आपदा कई महीनों या िषों में विकवसत होकर अत्यवधक विस्तृत क्षेत्र
को प्रभावित करती है।
सूखा एक जरटल पररघटना होती है। इसके अंतगवत वनम्नवलवखत तत्ि सवम्मवलत होते हैं:
o िषवण, िाष्टपीकरण, िाष्टपोत्सजवन;
o भूवमगत जल, मृदा आद्रवता, संचयन तथा सतही अपिाह;
o कृ वष कायव प्रणावलयााँ, विशेषत: उगाई जाने िाली फसलों के प्रकार; एिं
o सामावजक-आर्नथक कायव तथा पाररवस्थवतक वस्थवतयां।
67 www.visionias.in ©Vision IAS
सूखे के कारण
आपूर्नत तथा मांग (विशेष रूप से गैर-कृ वष उद्देश्यों की मांग) के बीच तालमेल की कमी को सूखे का
प्रमुख कारण ठहराया जा सकता है। जल की पयावप्त क उपलब्धता कृ वष कायों हेतु महत्िपूणव है, क्रकन्तु
यह अन्य चरों यथा तापमान, आद्रवता, सौर विक्रकरण तथा पिन प्रवतरूप से प्रभावित होती रहती
है।
सूखे के प्रकार
मौसम विज्ञान इस वस्थवत में लंबी अिवध तक अपयावप्त क िषाव होती है और साथ ही िषाव का
संबंधी सूखा सामवयक एिं स्थावनक वितरण भी असमान होता है।
औसत से 90 प्रवतशत से कम िषाव की वस्थवत को मौसम विज्ञान संबंधी सूखे
के रूप में िगीकृ त क्रकया जाता है।
कृ वष संबंधी मृदा में नमी की कमी इस वस्थवत का लक्षण है। मृदा में नमी फसल की रक्षा के
सूखा वलए आिश्यक होती है और नमी के अभाि में फसलें नष्ट हो जाती हैं।
यक्रद क्रकसी क्षेत्र के सकल फसल क्षेत्र की 30 प्रवतशत से अवधक भूवम ससचाई
के तहत आती हो तो उस क्षेत्र को सूखा-प्रिण िगव के तहत सवम्मवलत नहीं
माना जाता है।
चरम कृ वष सूखे के पररणामस्िरुप अकाल की वस्थवत उत्पन्न हो सकती है।
अकाल से आशय क्रकसी सीवमत क्षेत्र में दीघवकाल तक खाद्यान्न की कमी से है,
वजसके पररणामस्िरूप व्यापक स्तर पर रोग तथा भूखमरी की वस्थवत उत्पन्न
68 www.visionias.in ©Vision IAS
होती है। इसीवलए, कभी-कभी सहदी भाषा में सूखे के पयावयिाची के रूप में
अकाल तथा अनािृवष्ट शब्द का भी प्रयोग क्रकया जाता है।
यक्रद मौसम विज्ञान संबंधी सूखे के कारण क्रकसी क्षेत्र विशेष में 50 प्रवतशत से
अवधक फसल की हावन होती है तो सरकार उस क्षेत्र को सूखा प्रभावित
घोवषत कर देती है।
जल विज्ञान इस वस्थवत में विवभन्न जलभृत, झीलों, जलाशयों जैसे विवभन्न भंडारों तथा
संबंधी सूखा स्रोतों में जल की उपलब्धता िषाव द्वारा पुनस्थाववपत क्रकए जाने िाले स्तर से
भी नीचे चली जाती है।
पाररवस्थवतकी इस वस्थवत में जल की कमी से क्रकसी प्राकृ वतक पाररवस्थवतक तंत्र की
सूखा उत्पादकता में कमी हो जाती है तथा इस पाररवस्थवतक संकट के कारण
पाररवस्थवतक तंत्र को हावन पहुाँचती है।
IMD पांच प्रकार की सूखा वस्थवतयों को वचवह्नत करता है:
‘सूखा सप्त काह (Drought Week)’ जब साप्त कावहक िषाव की मात्रा सामान्य के आधे से भी कम हो।
‘कृ वष संबंधी सूखा (Agricultural Drought)’ जब मध्य जून से वसतंबर के दौरान वनरं तर चार
सूखे सप्त काहों की वस्थवत उत्पन्न हो जाए।
‘मौसमी सूखा (Seasonal Drought)’ जब मौसमी िषाव सामान्य से मानक विचलन की तुलना
में कम हो।
‘सूखा िषव (Drought Year)’ जब िार्नषक िषाव सामान्य से 20 प्रवतशत या अवधक कम हो।
‘गंभीर सूखा िषव (Severe Drought Year)’ जब िार्नषक िषाव सामान्य से 25 से 40 प्रवतशत
या और अवधक कम हो।
भारत में सूखा संबध
ं ी जोवखम
भारत में सूखे की अपनी विवशष्टता है, इसवलए इसके संबंध में कु छ आधारभूत त्यों को समझा जाना
आिश्यक है। जैसे:
भारत में औसत िषाव लगभग 1150 वममी होती है। क्रकसी भी अन्य देश का िार्नषक औसत इतना
उच्च नहीं है, यद्यवप इसमें िार्नषक रूप से पयावप्त क विविधता देखने को वमलती है।
69 www.visionias.in ©Vision IAS
िषाव का 80% से अवधक भाग दवक्षण-पवश्चम मानसून के दौरान 100 क्रदनों के भीतर प्राप्त क होता
है तथा उसका भौगोवलक वितरण असमान है।
21% क्षेत्र संपूणव िषव 700 वममी से कम िषाव प्राप्त क करता है वजससे यह क्षेत्र गंभीर सूखा प्रभावित
क्षेत्र हो जाता है।
िषाव की अपयावप्त कता के बािजूद भी देश के िृहद भाग में क्रकसान िषाव-आधाररत कृ वष हेतु बाध्य हैं।
साथ की साथ प्रवतकू ल भूवम-मानि अनुपात के कारण समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
भूवमगत-जल से की जाने िाली ससचाई अंततैः पाररवस्थवतकी को और विकृ त कर देती है क्योंक्रक
भूवमगत जल की वनकासी की दर, जल के पुनभवरण से अवधक होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अपयावप्त क
िषाव िाले िषों में सतही जल अत्यंत कम हो जाता है।
देश में प्रवत व्यवक्त जल की उपलब्धता धीरे -धीरे घटती जा रही है।
सम्पूणव िार्नषक उपलब्धता 1953 km3 की तुलना में सतही जल स्रोतों का 690 km3 तथा
भूवमगत जल स्रोतों का 396 km3 उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक 600 km3 की मात्रा
का उपयोग क्रकया जा चुका है।
जल संचय की पारं पररक प्रणावलयों का प्रयोग मुख्यत: नहीं क्रकया जाता है।
भारत में सूखा प्रिण क्षेत्रों का वितरण
सूखा तथा बाढ़ भारतीय जलिायु की अन्तसवम्बवन्धत विशेषताएं हैं। कु छ आकलनों के अनुसार,
देश के कु ल भौगोवलक क्षेत्र के 19 प्रवतशत तथा इसकी जनसंख्या के 12 प्रवतशत को प्रवतिषव सूखे
के कारण करठनाई का सामना करना पड़ता है। देश के लगभग 30 प्रवतशत क्षेत्र को सूखा प्रिण
घोवषत क्रकया गया है। विवभन्न क्षेत्रों में एक ही समय में सूखे तथा बाढ़ का प्रकोप एक सामान्य
घटना है। यह भी सामान्य-सी ही बात है क्रक एक ही क्षेत्र एक ऋतु में सूखे तथा अन्य ऋतु में बाढ़
का दंश झेलता है। ऐसा मानसून में स्थावनक तथा सामवयक अवनवश्चतता के कारण होता है।
70 www.visionias.in ©Vision IAS
हाल ही में, IMD ने खराब मानसून को दशावने के वलए ’सूखा (Drought)’ शब्द को हटा कर उसके
स्थान पर ‘न्यूनता (Deficient)’ शब्द के प्रयोग की घोषणा की है। IMD के पास सूखा घोवषत
करने का अवधदेश कभी नहीं रहा है तथा ऐसा करना राज्य सरकार का उत्तरदावयत्ि है क्योंक्रक
सूखे विविध प्रकार के होते हैं- जैसे जलविज्ञान संबंधी और कृ वष संबंधी आक्रद।
प्राप्त क िार्नषक िषाव सम्बन्धी अद्यतन नामािली
निीन शब्दािली पुरानी शब्दािली
सामान्य (Normal) सामान्य (Normal) प्राप्त क िषाव का दीघाविवधक औसत से
प्रवतशत विचलन ± 10% हो
सामान्य से कम (Below सामान्य से कम (Below प्राप्त क िषाव का दीघाविवधक औसत से
Normal) Normal) प्रवतशत विचलन < 10% हो
सामान्य से अवधक (Above सामान्य से अवधक (Above प्राप्त क िषाव का दीघाविवधक औसत से
Normal) Normal) प्रवतशत विचलन > 10% हो
न्यूनता िाला िषव सम्पूणव भारत में सूखे का िषव जब िषाव की कमी 10% से अवधक हो
(Deficient Year) (All India Drought Year) और देश के 20-40% भाग में सूखे की
दशाएाँ व्याप्त क हों
भारी न्यूनता िाला िषव सम्पूणव भारत में गंभीर सूखे का जब िषाव की कमी 10% से अवधक हो
(Large Deficient Year) िषव (All India Severe और देश के 40% से अवधक भाग में
Drought Year) सूखे की दशाएाँ व्याप्त क हों
सूखे की गंभीरता के आधार पर भारत को तीन क्षेत्रों में विभावजत क्रकया जा सकता है:
71 www.visionias.in ©Vision IAS
अत्यवधक सूखा राजस्थान के अवधकांश भाग, विशेषतैः अरािली की पहावड़यों के पवश्चम में
प्रभावित क्षेत्र
वस्थत क्षेत्र, अथावत् मरुस्थली तथा गुजरात का क्छ क्षेत्र इस िगव में आते हैं।
इसमें जैसलमेर तथा बाड़मेर वजले भी सवम्मवलत हैं जहााँ िषव में 90 वममी से
भी कम िषाव होती है।
अवधक सूखा पूिी राजस्थान के कु छ भाग, मध्य प्रदेश के अवधकांश वहस्से, महाराष्ट्र का पूिी
प्रभावित क्षेत्र
भाग, आंध्र प्रदेश का आतंररक भाग तथा कनावटक का पठार, आंतररक
तवमलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दवक्षणी वहस्सा तथा उड़ीसा का
आंतररक भाग।
मध्यम सूखा राजस्थान का उत्तरी भाग, हररयाणा, उत्तर प्रदेश के दवक्षणी वजले, गुजरात का
प्रभावित क्षेत्र
शेष भाग, कोंकण के अवतररक्त सम्पूणव महाराष्ट्र, झारखंड तथा तवमलनाडु में
कोयम्बटू र का पठार तथा आंतररक कनावटक।
सूखे के पूिव संकेतक
चूाँक्रक आपदा के रूप में सूखे की प्रकृ वत आरं भ में धीमी होती है, इसवलए इसके पूिव चेतािनी संकेतकों के
बारे में जानना आिश्यक होता है। ये वनम्न हैं:
दवक्षण-पवश्चम मानसून के आगमन में विलम्ब/ मानसून में वनम्न िषाव।
दवक्षण-पवश्चम मानसून ऋतु के दौरान दीघव अंतराल।
अपयावप्त क िषाव तथा विषम स्थावनक वितरण विशेषतैः जून तथा जुलाई के महीने में।
चारे के मूल्य में िृवि।
जल भंडारों के स्तर में िृवि की प्रिृवत्त का अभाि और/या जलधारा प्रिाह में कमी तथा भूवमगत
जल स्तर में वगरािट।
ग्रामीण पेयजल आपूर्नत स्रोतों का सूखना।
बुिाई की प्रक्रक्रया में विलम्ब की प्रिृवत।
ग्रामीण जनसंख्या का प्रिसन।
सामान्य िषों के आंकड़ों की तुलना में भूवमगत जल के स्तर में अत्यंत वगरािट।
मृदा में आद्रवता की कमी के संकेत।
टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्नत में िृवि।
संकट के रूप में सूखा का प्रभाि
समाज पर सूखे का प्रभाि उसकी सूखे का सामना करने की क्षमता तथा संबंवधत राष्ट्रीय अथवव्यिस्थाओं
की सामान्य दशा पर वनभवर करता है। सूखे के कु छ अवनिायव प्रभाि वनम्नवलवखत हैं:
आर्नथक:
o कृ वष तथा संबंवधत क्षेत्रों, विशेषतैः पशुपालन, डेयरी, कु क्कु ट पालन, बागिानी तथा मत्स्य-
पालन में उत्पादन में कमी।
o यह कृ वष आधाररत जनसंख्या की आजीविका तथा जीिन की गुणित्ता को प्रभावित करता है,
रो़गार के अिसरों में कमी से लोगों का मनोबल वगरने लगता है।
o कच्चे माल के वलए प्राथवमक क्षेत्र पर वनभवर सभी उद्योग-धंधे आपूर्नत में कमी तथा बढ़ती हुई
कीमतों के कारण प्रभावित होते हैं।
पयाविरणीय:
o भूवमगत जल एिं सतही जलाशयों, झीलों एिं तालाबों में वनम्न जल स्तर; तथा झरनों,
जलधाराओं, नक्रदयों में वनम्न प्रिाह, िना्छादन में कमी आक्रद।
o िन्य जीिों का प्रिास, मानि-जंतु संघषों में िृवि तथा जैि विविधता पर सामान्य दबाि।
o जलधारा प्रिाह में कमी तथा आद्रव भूवमयों का ह्रास लिणता के स्तर को प्रभावित कर सकते
हैं।
o भूवमगत जल स्तर में कमी की दर में िृवि तथा पुनभवरण में कमी से जलभृतों को क्षवत पहुाँच
सकती है तथा जल की गुणित्ता (लिण की सांद्रता, अम्लता, घुवलत ऑक्सीजन, गंदलापन)
प्रभावित हो सकती है वजससे मृदा की जैविक उत्पादकता को स्थायी क्षवत पहुाँच सकती है।
72 www.visionias.in ©Vision IAS
o उत्पादन न होने के कारण खाद्यान्न की कमी, अपयावप्त क िषाव, इसके पररणामस्िरूप जलाभाि
तथा इन तीनों में कमी के गंभीर विनाशकारी पररणाम हो सकते हैं।
सामावजक:
o सूखा प्रभावित क्षेत्रों से जनसंख्या का उत्प्रिास, विद्यालय छोड़ने िाले बच्चों की दर में िृवि
तथा ऋणग्रस्तता में िृवि।
o सिाववधक सुभेद्य िगों का भूवम और पशुधन से विलगाि, कु पोषण, भुखमरी तथा उनकी
सामावजक वस्थवत में वगरािट।
o जल की कमी के कारण लोग संदवू षत जल को पीने को बाध्य होते हैं पररणामस्िरूप जठरांत्र
शोथ (gastroenteritis), है़ा, हेपेटाईरटस इत्याक्रद जैसे विवभन्न जलजवनत रोगों के प्रसार
में िृवि होती है।
o कु छ मामलों में सूखे के कारण सामावजक तनाि में िृवि हो सकती है तथा सामावजक पूज
ाँ ी
का क्षय हो सकता है।
एक आपदा के रूप में सूखा क्रकस प्रकार अन्य आपदाओं से वभन्न है?
बाढ़, भूकंप तथा चक्रिातों के ठीक विपरीत, सूखे की कु छ स्पष्ट विशेषताएं होती हैं-
सूखे का आगमन मंद गवत से होता है वजससे पयावप्त क पूिव चेतािनी प्राप्त क हो जाती है।
यह व्यापक क्षेत्र में लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है।
इस आपदा की अिवध सिाववधक होती है, इसवलए राहत संबध
ं ी प्रयासों को दीघव अिवध तक
चलाए रखना पड़ता है।
यह सामान्यत: एक ग्रामीण घटना होती है, परन्तु अत्यंत गंभीर सूखे की वस्थवत में स्रोतों के सूखने
तथा उस क्षेत्र में जल-स्तर में तीव्र वगरािट आने से शहरी जल आपूर्नत व्यिस्था प्रभावित हो
सकती है।
इस आपदा के तहत यह संभािना रहती है क्रक सूखा प्रबंधन के प्रयासों के माध्यम से आद्रवता
संरक्षण तथा िानस्पवतक आ्छादन में िृवि कर लोगों की सुभेद्यता में कमी लायी जा सकती है।
अन्य आपदाओं में ऐसा नहीं होता है। अन्य शब्दों में, सूखा स्ियं को वजस प्रकार प्रबंवधत क्रकये जाने का
अिसर प्रदान करता है, िह अन्य आपदाओं में संभि नहीं है। ये सभी कारक सूखा प्रबंधन से संबंवधत
पृथक विचार-विमशव को आिश्यक बनाते हैं।
सूखा संकट का शमन
शमन उपायों का उद्देश्य मृदा अपरदन को कम करना, मृदा की नमी में िृवि करना, िषाव जल के सतही
अपिाह को सीवमत करना एिं जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। यह मृदा एिं जल संरक्षण के
उपायों तथा कृ वष प्रणावलयों की व्यापक रें ज को समाविष्टट करता है।
73 www.visionias.in ©Vision IAS
जल संचयन और संरक्षण: विशाल जलग्रहण क्षेत्रों से िषाव और जल अपिाह संग्रहण की प्रक्रक्रयाओं,
संरचनाओं तथा पारं पररक तरीकों का उपयोग करके या भूवमगत जल का कृ वत्रम पुनभवरण कर
मानि उपभोग हेतु जल की उपलब्धता सुवनवश्चत करना। यह बांध, टैंक, ऐनीकट (anicut) और
अंत:स्रिण टैंकों जैसी भूवमगत जल पुनभवरण तकनीकों को अपनाकर अिक्षवयत उच्च क्षमता िाले
जलिाही स्तरों को पुनभवरण करने में सहायता करता है; जल उपलब्धता में सुधार कर सकता है
और लगातार पड़ने िाले सूखे से वनपटने के वलए अवतररक्त जल उपलब्ध करता है।
सूखे की वनगरानी: इसके तहत िषाव की वस्थवत, जलाशयों, झीलों, नक्रदयों आक्रद में जल की
उपलब्धता का सतत अिलोकन एिं समाज के विवभन्न क्षेत्रकों में जल की ितवमान आिश्यकताओं
के साथ तुलना की जाती है।
सूखा प्रवतरोधी फसलों की बुआई: कपास, मूाँग, बाजरा, गेहाँ आक्रद सूखा प्रवतरोधी फसलों की
बुआई करके एक वनवश्चत सीमा तक सूखे के प्रभाि को कम क्रकया जा सकता है।
आजीविका योजना उन आजीविकाओं की पहचान करती है जो सूखे से सबसे कम प्रभावित होती
हैं। ऐसी कु छ आजीविकाओं में गैर-कृ वष क्षेत्रों में रोजगार के अिसरों में िृवि, सामुदावयक िनों से
गैर इमारती िन उपज का संग्रह, बकरी पालन, बढ़ईगीरी आक्रद सवम्मवलत हैं।
शुष्टक कृ वष की उपयुक्त विवधयााँ: कु छ ऐसी विवधयााँ हैं वजन्हें अपनाकर सूखे की तीव्रता को कम
क्रकया जा सकता है। इन विवधयों में सवम्मवलत हैं: मोटे अनाजों का उत्पादन, गहरी जुताई करके
मृदा में नमी का संरक्षण; छोटे बांधों के पीछे जल भंडारण, तालाबों और टैंकों में जल का
एकत्रीकरण एिं ससचाई के वलए सस्प्रक्लर का उपयोग।
सूखा योजना: सूखा योजना का मूल लक्ष्य वनगरानी, शमन और अनुक्रक्रया के उपायों में िृवि कर,
तैयारी और अनुक्रक्रया प्रयासों की प्रभाविता में सुधार करना है।
विप ससचाई एिं सस्प्रकलर विवधयों का उपयोग करके जल की कम मात्रा से अपेक्षाकृ त बड़े क्षेत्र
की ससचाई की जा सकती है।
जलभृत के रूप में भूजल क्षमता की पहचान, अवधशेष क्षेत्रों से जलाभाि िाले क्षेत्रों की ओर नदी
जल का स्थानांतरण तथा विशेष रूप से नक्रदयों को आपस में जोड़ने एिं जलाशय और बांध बनाने
हेतु योजना वनमावण।
मेघ बीजन (cloud seeding) का उपयोग करना। इस उद्देश्य से एरोसोल अवभलक्षणों का
आकलन करने, मेघ बीजन के वलए न्यूक्लाइड की उपयुक्तता एिं मेघ बीजन के िैकवल्पक प्रकारों
(भू-आधाररत या हिाई, गमव या ठं डे मेघ बीजन आक्रद) के सन्दभव में समुवचत परीक्षण क्रकया जा
सकता है। इन उपायों को विवनयवमत करने के वलए आिश्यक पररिेश के वनमावण हेतु राष्ट्रीय स्तर
और राज्य स्तर पर मेघ बीजन नीवत का वनमावण क्रकए जाने की आिश्यकता है।
सूखा संकट प्रबंधन योजना, 2015
राष्टरीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA) मैनुअल, कें द्र सरकार की सहायता से चार महत्िपूणव
उपाय वनधावररत करता है। राज्य सरकार को सूखे के समय वनम्नवलवखत उपायों को अपनाना चावहए:
MNREGA के माध्यम से सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना।
भोजन ि चारा उपलब्ध कराने के सािवजवनक वितरण तंत्र को सुदढ़ृ क्रकया जाना चावहए।
चेक डैम का वनमावण कर भूवमगत जल स्तर पुनभवरण अवभयान आरम्भ करना तथा पाइपलाइन
जल एिं अन्य ससचाई सुविधाएं प्रदान करना।
सरकार द्वारा क्रकसानों के ऋण या तो माफ या स्थवगत कर क्रदए जाने चावहए एिं फसल हावन की
क्षवतपूर्नत के वलए व्यिस्था की जानी चावहए।
सूखा प्रबंधन में ितवमान चुनौवतयां
सूखा प्रबंधन में वनम्नवलवखत तीन महत्िपूणव अियिों को समाविष्टट क्रकया जाता है:
o सूखे की तीव्रता का आकलन और वनगरानी;
o सूखे की घोषणा एिं सूखा प्रबंधन के वलए क्षेत्रों की प्राथवमकता; एिं
o सूखा प्रबंधन रणनीवतयों का विकास एिं कायावन्ियन।
74 www.visionias.in ©Vision IAS
प्रभािी अंवतम पररणाम सुवनवश्चत करने के वलए सूखा प्रबंधन के प्रत्येक के चरण में समग्र
दृवष्टकोण का अभाि है।
प्रत्येक राज्य में सूखे के प्रवत सुभद्य
े ता के आकलन हेतु मानक प्रक्रक्रयाओं का विकास तथा सुभेद्यता
मानवचत्रों का वनमावण करने की आिश्यकता है।
सूखे के विवभन्न चरणों को प्रबंवधत करने के वलए संकट प्रबंधन प्रावधकरण का अभाि।
लोगों और मीवडया तक सूखे के प्रासंवगक पहलुओं पर वििसनीय और सत्यावपत जानकारी के
प्रभािी प्रसार का अभाि।
िषाव, बोए गए फसल क्षेत्र, मृदा में आद्रवता संबधी डेटा, धारा के प्रिाह, भूवमगत जल, झील और
जलाशय के भंडारण पर सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के वलए अप्रभािी ‘वनगरानी
और पूिव चेतािनी प्रणाली।’
वजला कृ वष आकवस्मकता योजनाओं एिं संकट प्रबंधन योजना को लागू करने के वलए सूखे की
वस्थवत का यथासंभि शीघ्रतापूिक
व पता लगाने हेतु अधूरे मन से क्रकया गया प्रयास।
सामुदावयक सहभावगता का अभाि।
आिश्यक रूप से क्रकये जाने िाले कायव (Must-Do-Practices: MDPs): प्रारं वभक तैयारी
भूवम उपचार िषावजल संचयन उपयुक्त आिश्यकता उपयुक्त कृ वष चारा
और कु शल फसलें/ फसल आधाररत उपकरण व्यिस्था
उपयोग प्रवतरूप पोषक तत्ि
विविधता प्रबंधन
सम्पूणव िषावजल बीज फोवलअ कृ वष परररवक्षत
ढाल में संचयन बैंक र स्प्रे यंत्रीकर चारा
बुआई संरचनाएं बीज (foliar ण घरे लू/सा
मेड़ और कृ वष तालाब उपचार कृ वष मुदावयक
spray)
हल-रे खा पररसंचरण अंतर- उपकर चारा
के वलए
(ridge टैंक फसल ण कें द्र व्यिस्था
पोषक
सूक्ष्म ससचाई प्रणाली (कस्टम इत्याक्रद
and तत्ि
प्रणाली इत्याक्रद। हायटरग
furrow) जैविक
इत्याक्रद। सेंटर)
मेंड़ पुनचवक्र
श्रम
बााँधकर ण
साझा
खेत को तालाब
करने
क्यारी में की
िाला
बााँटना तलछट
मशीनी
चौड़ी हल- (टैंक
करण
रे खा वसल्ट)
इत्याक्रद
का
(broad
प्रयोग
bed इत्याक्रद
furrow)
उवत्थत
और
जलमि
क्यारी
(raised
and
sunken
bed)
इत्याक्रद
75 www.visionias.in ©Vision IAS
मंद गवत से आने िाली आपदाएाँ
आपदाओं को ‘मंद गवत से आने िाली’ आपदाओं एिं ‘तीव्र गवत से आने िाली’ आपदाओं के रूप में
भी िगीकृ त क्रकया जा सकता है। भूकंप, चक्रिात, बाढ़ तथा सुनामी को ‘तीव्र गवत से आने िाली’
आपदाओं की श्रेणी में सवम्मवलत क्रकया जाता है; जलिायु पररितवन (भूमंडलीय तापन),
मरूस्थलीरण, मृदा क्षरण और सूखा ‘मंद गवत से आने िाली’ आपदाओं के अंतगवत सवम्मवलत क्रकये
जाते हैं।
‘मंद गवत से आने िाली’ आपदाओं को 'धीमी आपात वस्थवतयों’ (Creeping Emergencies) के
रूप में भी जाना जाता है। 'प्रबंधन चक्र' में ‘रोकथाम' को अविभाज्य अंग के रूप में समाविष्ट कर,
भूमंडलीय तापन में िृवि एिं मरूस्थलीरण जैसी ‘मंद गवत से आने िाली’ आपदाओं को आपदा
तैयाररयों में पयावप्त क रूप से प्रवतसबवबत क्रकया जाना चावहए। िस्तुतैः ये पररघटनाएं पाररवस्थवतकी
तंत्रों के 'स्िास््य' को क्रवमक रूप से नष्ट करती हैं एिं समाज को प्रकृ वत की अवनयवमतताओं के
प्रवत अनािररत कर देती हैं। तीव्र गवत से आने िाली आपदाओं के विपरीत, उनके प्रभाि तत्काल
अनुभि नहीं होते हैं; परन्तु समय के साथ समाज अपने पररिेश से भरण–पोषण प्राप्त करने की
क्षमता खो देते हैं। विकास की नीवतयां एिं उन्हें कायाववन्ित क्रकए जाने की कायवपिवतयााँ ‘मंद गवत
से आने िाली’ आपदाओं के कु छ प्रमुख कारण हैं।
प्रश्न: 1987-88 के सूखे से भारत के कौन-से भाग मुख्यतैः प्रभावित हुए थे? इसके मुख्य पररणाम क्या
थे? (UPSC, 88/II/6b/20)
प्रश्न: भारत में सूखे के कारणों पर रटप्पणी वलवखए। (UPSC, 2005)
प्रश्न: सूखे को उसके स्थावनक विस्तार, कावलक अिवध, मंथर प्रारं भ और कमजोर िगों पर स्थायी प्रभािों
की दृवष्ट से आपदा के रूप में मान्यता दी गयी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA) के वसतंबर
2010 मागवदशी वसिांतों पर ध्यान के वन्द्रत करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित
दुष्टप्रभािों से वनपटने के वलए तैयारी की कायवविवधयों पर चचाव कीवजए। (UPSC, 2014)
3.2.10. हीट िे ि (Heat Wave)
हीट िेि क्या है?
हीट िेि असामान्य रूप से उच्च तापमान की अिवध है। इस अिवध में तापमान उत्तर-पवश्चमी तथा
देश के कु छ अन्य भागों में ग्रीष्टम ऋतु के दौरान रहने िाले सामान्य अवधकतम तापमान से अवधक
होता है। हीट िेि आमतौर पर माचव और जून के बीच प्रिावहत होती है और कु छ दुलभ व मामलों में
जुलाई तक भी बनी रहती है।
हीट िेि का वनमावण कै से होता है?
जब क्रकसी क्षेत्र के ऊपर दीघवकाल तक उ्च दाब बना रहता है और उसके कारण शुष्टक एिं गमव िायु
नीचे धरातल की ओर आती है, तब हीट िेि की पररघटना घरटत होती है। जैस-े जैसे िायु अितवलत
होती है, यह गमव होती जाती है और धरातल पर पहुाँचने तक अत्यवधक गमव हो जाती है।
यह गमव िायु धरातल को शीघ्रता से गमव कर देती है और इस प्रकार धरातल के तापमान के बढ़ते
जाने से हीट िेि की उत्पवत्त होती है। चूाँक्रक उच्च दाब क्षेत्रों के के न्द्र आमतौर पर मेघरवहत होते हैं,
इसवलए सीधे पड़ने िाले सूयव के प्रकाश से क्रदन के तापमान में और अवधक िृवि हो जाती है। वजससे
हीट िेि का वनमावण होता है।
76 www.visionias.in ©Vision IAS
हीट िेि के कारण
धरातल पर प्रिावहत होने िाली शुष्टक पिनों के साथ मरुस्थलों से प्रिावहत होने िाली गमव पिनें।
प्रवतचक्रिात के पररणामस्िरूप मेघों के वनमावण एिं तवड़तझंझा की गवतविवधयााँ नहीं होती हैं।
इस कारण से तापमान का संतुलन न हो पाना।
जलिायु पररितवन और भूमंडलीय तापन के कारण िैविक तापमान में िृवि।
दाब परट्टयों में पररितवन के कारण िायु धाराओं एिं मौसम प्रवतरूपों में पररितवन।
ओजोन परत का क्षरण।
जेट धाराएं।
हीट िेि के लक्षण
अत्यवधक गमी - क्षेत्र के औसत तापमान की तुलना में न्यूनतम 9 वडग्री सेवल्सयस उ्च तापमान।
आद्रवता – उच्च तापमान पर िायु में अत्यवधक नमी की उपवस्थवत अत्यंत असुविधाजनक हो सकती
है।
क्रकसी क्षेत्र में न्यूनतम पांच क्रदनों के वलए तेज गमी।
मृदा में नमी की कमी।
भारत में हीट िेि जोवखम
जलिायु पररितवन के कारण उच्च दैवनक शीषव तापमान एिं अवधकावधक लंबी, अवधक प्रचंड हीट
िेव्स िैविक रूप से वनरं तर घरटत होने िाली घटनाएं बनती जा रही हैं। हीट िेि की बढ़ती
घटनाओं की दृवष्ट से भारत भी जलिायु पररितवन के प्रभािों का अनुभि कर रहा है। हीट िेि िषव
दर िषव अवधकावधक तीव्र होती जा रही हैं और मानि स्िास््य पर विनाशकारी प्रभाि डालती हैं।
पररणामस्िरूप हीट िेि के कारण होने िाली मौतों की संख्या में िृवि होती जा रही है।
भारत में, अप्रैल से जून विवशष्ट हीट िेि की ऋतु है। जून दवक्षण-पवश्चम मानसून के आगमन का
महीना है इस महीने में प्रायद्वीपीय एिं मध्य भारत से ग्रीष्टमऋतु जैसी वस्थवतयााँ समाप्त होने
लगती हैं परन्तु उत्तर भारत में बनी रहती हैं। जनसंख्या घनत्ि, औद्योवगक गवतविवधयों से प्रदूषण
एिं इमारतों की उपवस्थवत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर अवधक गमव होते हैं।
असाधारण ग्रीष्टम तनाि एिं भारत में विद्यमान ग्रामीण जनसंख्या की अवधकता के कारण भारत
हीट िेि के प्रवत सुभेद्य है। हीट िेि देश के आंतररक क्षेत्रों में अपेक्षाकृ त अवधक प्रभािी होती हैं।
पहाड़ी क्षेत्र, पूिोत्तर भारत और तटीय क्षेत्र आम तौर पर हीट िेि अनुभि नहीं करते हैं। हीट िेि
हररयाणा, क्रदल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओवडशा, पवश्चम बंगाल, वबहार, झारखंड,
छत्तीसगढ़ और कनावटक के क्षेत्रों में प्रिावहत होती हैं।
77 www.visionias.in ©Vision IAS
हीट िेि के पररणाम
मानि स्िास््य पर प्रभाि
o उच्च तापमान में उच्च आद्रवता होने पर शरीर से पसीना आसानी से िाष्टपीकृ त नहीं हो पाता है।
पररणामस्िरुप शरीर ठं डा नहीं हो पाता है एिं शरीर का तापमान बढ़ता जाता है तथा
अंतत: व्यवक्त बीमार हो जाता है।
o हीट स्रोक, गमी के कारण थकान तथा गमी के कारण शरीर में ऐंठन।
o जल की कमी, मतली, चक्कर आना, वसर ददव।
o रासायवनक िायु द्वारा संचाररत रोग।
o व्यवक्त की मृत्यु होना। हीट िेि सिाववधक प्राणघातक प्राकृ वतक आपदाओं में से एक है।
प्रकृ वत पर प्रभाि
o हीट िेि, िायु और मृदा में आद्रवता में कमी कर सूखे की वस्थवत उत्पन्न कर सकती है। मृदा में
उपवस्थत नमी िाष्टपीकरण द्वारा तापमान में कमी करती है।
o कु छ प्रजावतयााँ विलुप्त क हो सकती हैं। कु छ नई ताप प्रवतरोधी प्रजावतयों का उिि हो सकता
है।
o कु छ जीिों की जीिन शैली और व्यिहार में रूपांतरण।
o हीट िेि के कारण खुले क्षेत्रों या िनों में आग लगने की घटनाएाँ प्राय: घरटत होने लगती हैं।
o महासागरों में प्रिाल विरं जन (ब्लीसचग) में िृवि हो सकती है।
o फसलों की भारी क्षवत के पररणामस्िरूप भोजन की कमी।
अिंसरचना और अथवव्यिस्था पर प्रभाि
o गमी, बढ़ती ऊजाव मांग के कारण उत्पन्न दबाि को सहन करने की अिसंरचना के साम्यव का
परीक्षण करती है। गमी के कारण विद्युत पारे षण लाइनों में फै लाि आ जाता है।
o पररिहन सेिाएं प्रभावित हो जाती हैं।
o श्रम क्षमता में कमी आती है।
भारत में हीट िेि के मानदंड
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट िेि के संबंध में वनम्नवलवखत मानदंड वनधावररत क्रकए हैं:
जब तक मैदानी क्षेत्रों में अवधकतम तापमान 40oC तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30oC तक न पहुाँच जाए, तब
तक हीट िेि पर विचार करने की आिश्यकता नहीं होती है।
क्रकसी स्थान का अवधकतम सामान्य तापमान 40oC से कम या उसके बराबर होने की वस्थवत में
o सामान्य तापमान से 5 से 6 वडग्री सेंटीग्रेड अवधक तापमान पर हीट िेि की वस्थवत होती है।
o सामान्य तापमान से 7 वडग्री सेंटीग्रेड अवधक तापमान पर प्रचंड हीट िेि की वस्थवत होती है।
क्रकसी स्थान का सामान्य अवधकतम तापमान 40oC से अवधक होने की वस्थवत में
o सामान्य तापमान से 4 से 5 वडग्री सेंटीग्रेड अवधक तापमान पर हीट िेि की वस्थवत होती है।
o सामान्य तापमान से 6 वडग्री सेंटीग्रेड अवधक तापमान पर प्रचंड हीट िेि की वस्थवत होती है।
िास्तविक अवधकतम तापमान 45oC या अवधक रहे तो हीट िेि की घोषणा की जानी चावहए।
ऐसी वस्थवत में सामान्य अवधकतम तापमान का सन्दभव नहीं वलया जाता है।
हीट िेि संबध
ं ी संकट का शमन
हीट िेि की रोकथाम एिं शमन के वलए 4 मानदंड महत्िपूणव हैं:
o हीट िेि का पूिावनम
ु ान तथा पूिव चेतािनी प्रणाली की व्यिस्था करना;
o हीट िेि संबंधी आपात वस्थवतयों से वनपटने के वलए स्िास््य देखभाल पेशेिरों का क्षमता
वनमावण;
o विवभन्न माध्यमों से समुदाय तक पहुाँच; और
o एजेंवसयों के मध्य सहयोग तथा उस क्षेत्र में वस्थत अन्य नागररक सामावजक संगठनों के साथ
साझेदारी।
शहरों में हीट िेि के प्रवत सुभेद्य उच्च जोवखमयुक्त क्षेत्रों की एक सूची तैयार करना, वजससे गमी से
बचाि के संबंध में अवधक कें क्रद्रत गवतविवधयों का संचालन क्रकया जा सके । उदाहरण हेतु ‘हीट
एक्शन प्लान’ (HAP) का अंगीकरण।
78 www.visionias.in ©Vision IAS
सड़क के क्रकनारों जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में िृक्षारोपण अवभयान आरम्भ करना तथा जून में
िृक्षारोपण पिव के दौरान ‘ग्रीन किर’ गवतविवध प्रारम्भ करना।
शहर के चारों ओर उच्च जोवखम िाले क्षेत्रों में शीतलन कें द्र जैसी सुविधाओं की स्थापना पर
विचार करना।
जन जागरूकता: मवहलाओं सवहत सुभेद्य समुदायों को सूचना प्रदान करने और सक्रक्रय रूप से
मुख्यधारा में सवम्मवलत करने हेतु सामुदावयक समूहों तथा मवहला आरोग्य सवमवत, सेल्फ-
एम्प्लॉयड विमेंस एसोवसएशन (SEWA), ASHA कायवकताव, आंगनिाड़ी जैसी लोगों को संगरठत
करने िाली संस्थाओं तथा नगर पररषद् के साथ वमलकर प्रवशक्षण कायवशालाएं आयोवजत करना
तथा लोगों तक पहुाँच बनाना। समुदायों तक पहुाँच में िृवि करने के वलए उच्च वशक्षा, गैर-
लाभकारी संगठनों जैसे अन्य क्षेत्रों तथा सामुदावयक नेताओं को इसमें समाविष्ट करना।
पयाविरण संरक्षण; सतत पयाविरण कायव-प्रणावलयों को अपनाना।
हीट िेि प्रबंधन में विद्यमान चुनौवतयां
उप-वजला स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के प्रयोग से क्रकये जाने िाले शोध का अभाि। इससे
अपेक्षाकृ त अवधक लवक्षत भौगोवलक हस्तक्षेप की साम्यव प्राप्त क करने के वलए शहरी तथा ग्रामीण
क्षेत्रों की पृथक सूवचयााँ प्राप्त क नहीं हो पातीं।
शहर के भीतर सुभेद्यता प्रवतरूप प्रदान करने हेतु शहरी िाडों के स्तर के आंकड़ों का सीवमत
विश्लेषण।
सािवजवनक सन्देश सम्प्रेषण (रे वडओ, TV), मोबाइल फोन आधाररत टेक्स्ट मैसज
े , स्िचावलत फोन
कॉल तथा चेतािवनयों जैसे उपलब्ध प्रािधानों का वनम्न सक्रक्रय उपयोग।
परम्परागत अनुकूलन प्रणावलयों, यथा घर के भीतर रहना, आरामदायक िस्त्र पहनना आक्रद से
संबंवधत जागरुकता में कमी।
79 www.visionias.in ©Vision IAS
सरल वड़ाइन संबंधी विशेषताओं यथा आ्छाक्रदत वखड़क्रकयााँ, भूवमगत जल-संचय टैंकों तथा
रोधक गृह-वनमावण सामवग्रयों आक्रद को लोकवप्रय बनाने का अधूरे मन से क्रकया गया प्रयास।
आिासीय पररसर तथा घर के अन्दर वस्थत प्रसाधन कक्षों के भीतर पेयजल व्यिस्था की
अनुपलब्धता।
3.2.11. शीत लहर (Cold Waves)
शीत लहर क्या है?
शीत लहर क्रकसी विस्तृत क्षेत्र में िायु के ठं डे होने या अत्यंत ठं डी िायु के प्रिेश द्वारा वचवन्हत एक
मौसमी पररघटना है। यह अत्यंत ठं डे मौसम िाली एक दीघवकालीन अिवध भी हो सकती है। इस
वस्थवत के दौरान उच्च अक्षांशीय पिनें (high winds) भी प्रिावहत हो सकती हैं वजससे िायु में
शीतलक प्रभाि (wind chills) अत्यवधक बढ़ जाता है। शीत लहर, ठं ड के मौसम से संबंवधत
महत्िपूणव घटनाओं यथा वहमझंझािात या बफीले तूफान से पहले या उनके साथ प्रिावहत हो
सकती हैं।
शीत लहर के कारण
भारत में शीत लहर का विस्तार अपेक्षाकृ त उच्च अक्षांशों से ठं डी िायु के आगमन के कारण होता
है। यह सामान्यतैः, अल नीनो, चक्रिातीय गवतविवधयों तथा जेट धाराओं (पवश्चमी विक्षोभ) से
संबि होती है।
पवश्चमी विक्षोभ, 20°N के उत्तर में ऊपरी क्षोभमंडलीय पछु आ पिनों के साथ पूिव की ओर अग्रसर
सुस्पष्ट गतव (troughs) के रूप में प्रकट होते हैं और प्रायैः वनचले क्षोभमंडल तक विस्ताररत होते
हैं। ये उत्तरी अक्षांश से ठं डी िायु को भारत की ओर ले आते हैं। उत्तरी अरब सागर के ऊपर वनम्न
दाब तंत्र के विकवसत होने के कारण भी शीत लहर के कु छ दृष्टांत सामने आए हैं। इन वस्थवतयों में,
वनम्न दाब तंत्र के उत्तर की ओर की पूिाव पिनें उच्च अक्षांशों से ठं डी पिनें अपने साथ लाती हैं।
भारत में शीत लहर संबध
ं ी खतरे
शीत ऋतु में निम्बर से फरिरी के मध्य चलने िाली शीत लहर उत्तर भारत के लोगों के वलए
िासी परे शानी का कारण बन जाती है। शीत लहरों के विस्तार के दौरान, न्यूनतम तापमान में 4o
सेंटीग्रेड से अवधक की वगरािट देखी जाती है। यह दौर सामान्यतैः 3 से 5 क्रदनों तक चलता है तथा
जनिरी में ऐसी वस्थवतयां सिाववधक देखने को वमलती हैं।
80 www.visionias.in ©Vision IAS
भारत में शीत लहर का वितरण प्रवतरूप
उत्तरी भारत
उत्तरी मैदानों में क्रदसंबर तथा जनिरी सिाववधक ठं डे महीने होते हैं। पंजाब तथा राजस्थान में
रावत्रकालीन तापमान के वहमांक के भी नीचे जाने की संभािना रहती है। उत्तर भारत में अत्यवधक
ठं ड के वनम्नवलवखत कारण हो सकते हैं:
o समुद्र के समकारी प्रभाि से बहुत दूर वस्थत होने के कारण पंजाब, हररयाणा तथा राजस्थान
जैसे राज्यों में महाद्वीपीय जलिायु पाई जाती है।
o वनकटिती वहमालय पिवतश्रेवणयों में होने िाली बफ़व बारी के कारण शीतलहर की वस्थवत
उत्पन्न हो जाती है; तथा
o फरिरी के आस-पास कै वस्पयन सागर तथा तुकवमेवनस्तान से आने िाली ठं डी पिनें भारत के
उत्तर-पवश्चमी भागों में तुषार तथा कोहरे के साथ-साथ शीतलहर के आगमन का कारण
बनती हैं।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र
भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पररभावषत शीत ऋतु नहीं होती है। समुद्री समकारी
प्रभाि तथा विषुितरे खा से वनकटता के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण प्रवतरूप में
कदावचत ही कोई मौसमी पररितवन आता है।
शीत लहर के प्रभाि
तुषार के साथ यह कृ वष, अिसंरचना तथा संपवत्त को नुकसान पहुाँचा सकती है।
भारी वहमपात तथा अत्यवधक ठं ड के कारण सम्पूणव क्षेत्र वनवष्टक्रय हो सकता है।
वहमआंवधयों के कारण बाढ़ आना, तूफान महोर्नम, राजमागव एिं सड़कें अिरुि होना, वबजली की
लाइनों का धराशायी होना तथा हाइपोथर्नमया।
आर्नथक तथा मानिीय क्षवत।
सिड वचल यह िास्तविक तापमान नहीं बवल्क खुली त्िचा पर पिन एिं ठं ड का अहसास
(Wind Chill) होता है। जैस-े जैसे पिन आगे बढ़ती है, अत्यंत तीव्रता से शरीर में ऊष्टमा की
कमी होती है तथा शरीर का तापमान कम होने लगता है। जीि-जंतु भी सिड
वचल से प्रभावित होते हैं; हालांक्रक गावड़यााँ, िनस्पवतयााँ एिं अन्य िस्तुएं
प्रभावित नहीं होती हैं।
81 www.visionias.in ©Vision IAS
शीतदंश शीतदंश से आशय अत्यवधक ठं ड के कारण शरीर के ऊतक को होने िाले
(frostbite) नुकसान से है। -20 वडग्री F पर सिड वचल के कारण मात्र 30 वमनट में
शीतदंश की वस्थवत उत्पन्न हो सकती है। शीतदंश के कारण संिेदनशून्यता
तथा नाक, कान, उं गवलयों, पैर की उं गवलयों आक्रद के अग्रभाग की त्िचा सफ़े द
या पीली पड़ जाती है। यक्रद क्रकसी व्यवक्त में ऐसे लक्षण क्रदखाई देते हैं तो उसे
तुरंत वचक्रकत्सीय सहायता प्रदान की जानी चावहए। वचक्रकत्सीय सहायता प्राप्त क
होने में विलम्ब की वस्थवत में व्यवक्त के प्रभावित अंगों को धीरे -धीरे पुनैः गमी
दी जानी चावहए। हालांक्रक यक्रद व्यवक्त में हाइपोथर्नमया के लक्षण भी देखे
जाते हैं तो इन अग्रभागों को गमव करने से पहले मुख्य शरीर को गमी प्रदान की
जानी चावहए।
हाइपोथर्नमया यह वस्थवत तब उत्पन्न होती है जब शरीर का तापमान 95 वडग्री फ़ारे नहाइट
(Hypothermia) से भी कम हो जाता है। इसमें मृत्यु भी हो सकती है। िे व्यवक्त जो जीवित रह
जाते हैं उन्हें स्थाई रूप से गुद,े अिाशय एिं यकृ त सम्बन्धी समस्या की
सम्भािना रहती है। चेतािनी सम्बन्धी संकेतकों में अवनयंवत्रत कं पकं पी,
याददाश्त जाना, आत्मविस्मृवत, विचारों में असंबिता, बोलने में करठनाई,
सुस्ती और अत्यवधक थकान सवम्मवलत हैं। ऐसे लक्षण क्रदखने पर व्यवक्त के
शरीर के तापमान की जांच की जानी चावहए तथा उसके 95 वडग्री
फ़ारे नहाइट से कम होने की वस्थवत में तत्काल वचकत्सीय देखभाल प्रदान की
जानी चावहए।
शीत लहर के संकट का शमन
शीत लहर/पाले की वस्थवत में, राज्य को इनके प्रभाि को कम करने हेतु संबंवधत राज्य कृ वष
वििविद्यालयों के परामशव से तथा वजला फसल आकवस्मकता योजनाओं में रे खांक्रकत वनयमों के
अनुसार स्थान विवशष्ट उपायों को कायाववन्ित करने की आिश्यकता होती है।
क्रकसानों को आिश्यकतानुसार वनम्न ससचाई, शाखाओं या कोंपलों के क्षवतग्रस्त क्रकनारों की छंटाई
करने, बगीचों में अिवशष्ट पदाथों को जला कर धुआं करने, मृत भागों की छंटाई कर फसलों को
पुनैः निजीिन प्रदान करने तथा पवत्तयों पर वछड़काि के माध्यम से उिवरक की अवतररक्त खुराकों
की आपूर्नत करने की आिश्यकता होती है।
सुभेद्य जनसंख्या को ठं ड से बचाने के वलए विद्यालयों तथा अन्य सािवजवनक इमारतों को आश्रय-
स्थलों में पररिर्नतत करने की संभािना से संबंवधत योजना तैयार करना।
बच्चों, िृि एिं बीमार व्यवक्तयों पर ठं ड से होने िाले प्रभािों के प्रवत जागरूक तथा अवभगम एिं
तैयारी संबंधी प्रयासों को बढ़ािा देना।
बाह्य दीिारों से लगी पाइपलाइनों पर ऊष्टमा रोधी परत चढ़ाना ताक्रक इनके भीतर का जल जमे
नहीं और जलापूर्नत के प्रभावित होने की संभािना कम हो सके ।
अपने घर के वलए शीत ऋतु हेतु एक क्रकट तैयार रखना। मानक आधारभूत घरे लू आपातकालीन
क्रकट के अवतररक्त ऐसे खाद्य-पदाथव रखना वजन्हें पकाने या क्रफ्रज में रखने की आिश्यकता न हो।
साथ ही जल, कं बल, सेंधा नमक तथा वबजली आपूर्नत व्यिस्था भंग होने की वस्थवत में अपने घर
को सुरवक्षत तरीके से गमव रखने की व्यिस्था की जानी चावहए।
समुदाय तथा स्थानीय शासन की पयावप्त क तैयारी शीत लहर के कारण होने िाली मौतों में कमी ला
सकती है।
82 www.visionias.in ©Vision IAS
शीत लहर संकट प्रबंधन के मागव में ितवमान बाधाएं:
चूाँक्रक शीत लहर/पाला एक स्थानीय आपदा है, अतैः इसके वलए राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं की
बजाय संबंवधत राज्य सरकारों द्वारा स्थान विवशष्ट शमनकारी योजनाएं तैयार क्रकये जाने की
आिश्यकता होती है।
स्थानीय स्तर पर SHGs तथा PRIs आक्रद की भागीदारी में कमी।
समयपूिव तैयारी का अभाि।
नोट: िषव 2016 में, शीत लहर तथा हीट िेि को पररभावषत करने िाले मानकों में पररितवन कर
राष्ट्रीय मौसम संस्थान IMD ने एक नयी वनयमािली को अंगीकृ त क्रकया है।
3.2.12. िनावि (Wild Fires)
िनावि क्या है?
िनावि सामान्यतैः विस्तृत खेतों, फसलों तथा भू-क्षेत्रों को जला देने िाली एक अवनयंवत्रत आग
होती है। ये आग कभी-कभी कई क्रदनों तथा सप्त काहों तक जारी रहती है। िनावि, सम्पूणव िन का
नाश कर सकती है तथा इसमें उपवस्थत क्रकसी भी जैविक तत्ि को विनष्ट कर सकती है।
83 www.visionias.in ©Vision IAS
िनावि के कारण
िनावि प्रसार को तीन मुख्य कारक यथा मौसम, स्थलाकृ वत तथा ईंधन प्रभावित करते हैं। िनावि
की उत्पवत्त प्राकृ वतक एिं मानि-जन्य कारणों से होती है।
o प्राकृ वतक कारण- यथा तवड़त, वजसके कारण िृक्षों में आग लग जाती है। हालांक्रक िषाव ऐसी
िनावियों को अवधक नुकसान होने से पहले ही बुझा देती है। उच्च िायुमंडलीय तापमान तथा
शुष्टकता (वनम्न आद्रवता) िनावि की शुरुआत के वलए सहायक पररवस्थवतयों का वनमावण करते हैं।
o मानि-जन्य कारण- अनािृत्त आग, वसगरे ट या बीड़ी, इलेवक्रक स्पाकव या प्रज्िलन के अन्य क्रकसी
स्रोत के ज्िलनशील पदाथव के संपकव में आने पर भी िनावि आरम्भ हो सकती है। भारत में िनावि
के 95% मामले मानि-जन्य होते हैं।
िनावि के प्रकार
िनावि दो प्रकार की होती है:
i. सतह िनावि (Surface Fire)- िनावि का आरम्भ सतह िनावि के रूप में हो सकता है। यह
भूवम पर वस्थत अिवशष्ट पदाथों (सूखी पवत्तयों, टहवनयों तथा सूखी घास इत्याक्रद) के सहारे िन
की सतह पर फै लती जाती है तथा सम्पूणव सतह को अपनी चपेट में ले लेती है।
ii. शीषव िनावि– एक अन्य प्रकार की िनावि शीषव िनावि होती है वजसमें िृक्षों और झावड़यां के शीषव
भाग जल जाते हैं। ये भाग सतह िनावि के पश्चात प्रायैः बच जाया करते हैं। क्रकसी शंकुधारी िन
में शीषव िनावि अत्यंत खतरनाक वसि हो सकती है क्योंक्रक जलते हुए लट्ठों से वनकली हुई रे व़न
भीषण रूप से उद्दीप्त क हो उठती है। पिवतीय ढलानों पर यक्रद आग पहाड़ी के नीचे से आरं भ होती है,
तो ढलान के चारों ओर की िायु गमव होकर ऊपर उठने के कारण यह तीव्र िेग से ऊपर की ओर
बढ़ती है। यक्रद आग पहाड़ी के शीषव या ऊपरी वहस्से पर आरम्भ हो तो इसके नीचे की ओर फै लने
की संभािना अत्यंत कम होती है।
िनावि के संकेतक
दृश्य आग तथा धूम्रस्तंभ (smoke column);
धुंए के कारण सूयव के ढक जाने से दृश्यता में कमी होना;
दहन की ध्िवन तथा िायु की गवत में िृवि; तथा
जलती हुई िनस्पवतयों की गंध।
भारत में िनावि का जोवखम
76.4 वमवलयन हेक्टेयर क्षेत्रफल के िनािरण के साथ भारत में उष्टणकरटबंधीय दवक्षणी क्षेत्र,
उत्तर-पवश्चमी मरुस्थल, वहमालय पिवतमाला एिं आद्रव पूिोत्तर क्षेत्र सवहत विवभन्न प्रकार के
जलिायु क्षेत्र सवम्मवलत हैं। िन देश भर में व्यापक रूप से फै ले हुए हैं। देश में पवश्चमी तट एिं
पूिोत्तर में उष्टणकरटबंधीय सदाबहार िनों से लेकर उत्तर में वहमालय क्षेत्र में विस्तृत अल्पाइन
िनों तक, वभन्न-वभन्न प्रकार की िनस्पवत पाई जाती है। इन दो चरम वस्थवतयों के मध्य, अिव
84 www.visionias.in ©Vision IAS
सदाबहार िन, पणवपाती िन, उपोष्टणकरटबंधीय चौड़ी पवत्तयों िाले पहाड़ी िन,
उपोष्टणकरटबंधीय शंकुधारी िन एिं उपोष्टणकरटबंधीय पिवतीय समशीतोष्टण िन विद्यमान हैं।
जनसंख्या के बढ़ते दबाि के साथ ही देश में िनािरण का सचताजनक रूप से ह्रास हो रहा है।
विवभन्न कारकों के साथ, िनावि भारत में िनों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। भारतीय िन
सिेक्षण की ररपोटव के अनुसार, देश के लगभग 50 प्रवतशत िन क्षेत्र अवि-प्रिण (कु छ राज्यों में 50
प्रवतशत से लेकर अन्य में 90 प्रवतशत तक) हैं। लगभग 6 प्रवतशत िनों में िनावि के कारण गंभीर
क्षवत होती है।
भारत में िनावि का वितरण प्रवतरूप
देश के विवभन्न क्षेत्रों में सामान्य एिं चरम िनावि के वभन्न-वभन्न मौसम होते हैं। ये प्रायैः जनिरी
से जून के मध्य होते हैं। उत्तरी एिं मध्य भारत के मैदानी इलाकों में आग लगने की अवधकांश
घटनाएं फरिरी से जून के मध्य होती हैं। उत्तरी भारत की पहावड़यों में िनावि िाले मौसम की
शुरुआत बाद में होती है तथा आग लगने की अवधकांश सूचनाएं अप्रैल से जून के मध्य प्राप्त क होती
हैं। देश के दवक्षणी भाग में आग का मौसम जनिरी से मई के बीच रहता है। वहमालयी क्षेत्र में मई
तथा जून के महीने में आग की घटनाएं सामान्य हैं।
भारत के िनों में आग के प्रवत सुभेद्यता वभन्न-वभन्न स्थानों पर िनस्पवत एिं जलिायु के प्रकार के
आधार पर वभन्न-वभन्न होती है। वहमालयी क्षेत्र में पाए जाने िाले शंकुधारी िन आग के प्रवत
अवतसंिेदनशील होते हैं। इस क्षेत्र में प्रत्येक िषव िनावि की एक या दो बड़ी घटनाएं होती ही
रहती हैं। देश के अन्य वहस्सों में प्रमुखता से पाए जाने िाले पणवपाती िन भी आग से क्षवतग्रस्त
होते हैं।
िनावि के प्रभाि
िनावि को वनयंवत्रत करने हेतु सरकार द्वारा भारी व्यय।
बाढ़, मलबे के प्रिाह एिं भूस्खलन की संभािना बढ़ जाती है।
धुएाँ एिं अन्य उत्सजवनों में प्रदूषक होते हैं, जो गंभीर स्िास््य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
भूवम की उत्पादकता में ह्रास, प्रजावतयों के पुनजवनन पर प्रभाि तथा िाटर शेड पर अत्यवधक
हावनकारक प्रभाि।
85 www.visionias.in ©Vision IAS
भूमडडलीय तापन, मृदा अपरदन, ईंधन, लकड़ी एिं चारे की कमी, जल को पहुाँचने िाली क्षवत।
अल्पकावलक प्रभािैः लकड़ी, चारा, िन्यजीि आिास, प्राकृ वतक पररदृश्य एिं िॉटरशेड
(watersheds) का विनाश।
दीघवकावलक प्रभािैः मनोरं जक क्षेत्रों तक सीवमत पहुंच; सामुदावयक अिसंरचना तथा सांस्कृ वतक
ि आर्नथक संसाधनों का विनाश।
िनावि के लाभ
िनावि कभी-कभी एक प्राकृ वतक प्रक्रक्रया होती है तथा पुष्टपण, शाखाओं के विस्तार एिं निोविद
पौधों को बढ़ािा देकर िनािरण की िृवि में सहायक होती है। सतह तक सीवमत रहने िाली आग
िनों के प्राकृ वतक पुनरुत्थान में सहायता कर सकती है। मृदा तापन के पररणामस्िरूप लाभकारी
सूक्ष्मजैविक गवतविवधयों में िृवि हो सकती है और विखंडन प्रक्रक्रया में तीव्रता आ सकती है, जो
िनस्पवतयों के वलए उपयोगी है।
इन िनों की पाररवस्थवतकी तथा जैि-भौगोवलक उत्पवत्त पर हाल में हुए अनुसंधान से संकेत
वमलता है क्रक िनावि की घटनाएाँ एिं प्रकाश की उपलब्धता पाररवस्थवतकी तंत्र को बनाए रखने
के महत्िपूणव कारक हैं।
इसके अवतररक्त, बार-बार कम तीव्रता िाली िनावियााँ संभितैः िन में आग के प्रसार के वलए
ईंधन की तरह कायव करने िाली कई आक्रामक प्रजावतयों के प्रसार को वनयंवत्रत करती हैं।
िनावि संकट का शमन
विरटश काल के दौरान, िन सीमा के साथ फै ले खरपतिार को हटाकर ग्रीष्टम ऋतु में आग की रोकथाम
की जाती थी। इसे फॉरे स्ट फायर लाइन (िनावि रे खा) कहा जाता था तथा इसे िन के एक भाग से
दूसरे भाग में आग को फै लने से रोकने के वलए प्रयोग क्रकया जाता था।
असंबि क्षेत्र में िनावि के जोवखम को कम करने हेतु वनम्नवलवखत विस्तृत रणनीवतयों की
आिश्यकता है :
o िनस्पवत प्रबंधन: फ्यूल िेक, वनधावररत दहन, यांवत्रक सफाई, झावड़यों के जैविक वनयंत्रण एिं
रासायवनक वनयंत्रण सवहत िनस्पवत प्रबंधन पिवतयों पर अनुसध
ं ान।
o संवहता एिं अध्यादेश: िन भूवम-शहरी अंतरापृष्ठ (wild land - urban interface) क्षेत्रों में
वस्थत संरचनाओं के आस-पास भिन संवहता तथा िनस्पवत सफाई आिश्यकताओं सवहत
िनावि से संबंवधत ितवमान संवहताओं की समीक्षा।
o लाल भृग
ं प्रबंधन- लाल भृंग (bark beetle) उन्मूलन या वनयंत्रण पिवतयों पर अनुसंधान।
o सािवजवनक वशक्षा- आग के जोवखम के न्यूनीकरण हेतु आिश्यक कदमों एिं उनके लाभ के
विषय में जनता को वशवक्षत करने हेतु रणनीवतयों का विस्तार।
o िनावि के बेहतर प्रबंधन हेतु आग का पता लगाने, उसके वनयंत्रण एिं आग पाररवस्थवतकी के
क्षेत्र में शोध।
यक्रद आग को उसके वलए ईंधन (शुष्टक िनस्पवत) की अनिरत आपूर्नत होती रहे तो उसका प्रसार
होता है। अतैः, िनावि को वनयंवत्रत करने का सबसे अ्छा उपाय इसे फै लने से रोकना है, जो िन
में छोटी िनस्पवत रवहत खाइयों को अविरोधक के रूप में विकवसत कर क्रकया जा सकता है।
न के िल अवि-शमन में बवल्क शुरुआत से ही िनावि की घटना पर नजर रखने ि चेतािनी जारी
करने में स्ियंसेिकों की भागीदारी।
वनरं तर फायर फाइटटग विल्स (fire fighting drills) का आयोजन करना।
जनता एिं सरकार तक सटीक सूचना के प्रसार हेतु मीवडया ि उपलब्ध प्रौद्योवगक्रकयों का उवचत
उपयोग।
िनावि जोवखम प्रबंधन में विद्यमान चुनौवतयां
देश में िनावि की घटनाओं में िृवि हो रही है तथा प्रत्येक िषव आग से प्रभावित क्षेत्रों में भी िृवि होती
जा रही है। समस्या के प्रवत विखंवडत दृवष्टकोण का अपनाया जाना इस विफलता का मुख्य कारण है।
देश में एक व्यिवस्थत िनावि प्रबंधन कायवक्रम को बनाए रखने हेतु आिश्यक राष्ट्रीय फोकस एिं
तकनीकी संसाधन दोनों का अभाि है।
प्रज्िलन स्रोतों, आग की प्रचंडता का प्रवतरूप, िनावि का मौसम एिं आग के विस्तार सवहत
िनावि की पूिव घटनाओं पर अपयावप्त क शोध।
86 www.visionias.in ©Vision IAS
जलीय पाररवस्थवतक तंत्रों तथा प्रजावतयों पर अवि पश्चात के अपिाह एिं अपरदन प्रभािों के
अध्ययन हेतु क्रकए गये आधे-अधूरे प्रयास।
नई तकनीक, सेंसर जाल (sensor webs) ि उपग्रह प्रौद्योवगकी के उपयोग से वनगरानी एिं पूिव
चेतािवनयां जारी करने हेतु संकीणव स्थावनक पहुाँच।
विशेष रूप से िन भूवम-शहरी अंतरापृष्ठ क्षेत्रों में मानि जीिन एिं संपवत्त पर प्रभाि के
न्यूनीकरण हेतु उपकरणों ि विवधयों को विकवसत करने की आिश्यकता।
ग्रामीण समुदायों से िन संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी के वलए आग्रह नहीं क्रकया जाता है,
परं तु संकट के समय उनसे सहयोग की अपेक्षा जाती है। उन्हें वस्थवत के बारे में जागरूक कर इस
प्रकार के मनोभाि एिं दृवष्टकोण को बदला जाना चावहए तथा उन्हें यह वसखाया जाना चावहए
क्रक ऐसी आपात वस्थवत के दौरान िे क्या कदम उठा सकते हैं।
देश के विवभन्न भागों में अनुषंगी कें द्रों के साथ एक राष्ट्रीय िनावि प्रबंधन संस्थान स्थावपत करने
की आिश्यकता है।
सामररक िनावि कें द्रों, मंत्रालयों के मध्य समन्िय, वित्त पोषण, मानि संसाधन विकास, अवि
अनुसंधान, अवि प्रबंधन तथा विस्तार कायवक्रमों जैसे महत्िपूणव िनावि प्रबंधन तत्िों का अभाि
है।
क्या क्रकया जाना चावहए
िनावि को पूणवरूपेण विनाशकारी प्रकृ वत के रूप में देखने के बजाय िन प्रबंधकों को कदावचत
अपने दृवष्टकोण का विस्तार करना चावहए। उन्हें आग को पुरुिारक एिं पुनजीिन प्रदान करने
िाली घटना के रूप में देखने िाली पाररवस्थवतकीय तथा स्थानीय ज्ञान प्रणावलयों से प्राप्त क
जानकाररयों के प्रवत और अवधक समािेशी होना चावहए।
3.3. मानि-जन्य आपदाएं (Man Made Disasters)
3.3.1. जै विक आपदा (Biological Disaster)
जैविक आपदा क्या है?
जैविक आपदाएं िस्तुतैः महामारी तथा एंथ्रक्
े स, स्मॉलपॉक्स इत्याक्रद जैसे जैविक एजेंटों का
उपयोग कर विषाक्त सूक्ष्मजीि/सूक्ष्मजीिों के द्रुत फै लाि या जैि आतंकिाद के कारण घरटत हो
सकती हैं। हाल के क्रदनों में यात्रा करना सुविधाजनक हो गया है। अवधकावधक लोग संपूणव विश्ि
की यात्रा कर रहे हैं वजसके पररणामस्िरूप संपूणव विश्ि में महामाररयों के प्रसार की संभािना बढ़
गयी है।
जैविक आपदाओं के प्रकार
जैविक आपदाएं वनम्नवलवखत प्रकार की हो सकती हैं:
87 www.visionias.in ©Vision IAS
महामारी (Epidemic)- महामारी एक ही समय में जनसंख्या या समुदाय के एक विशाल समूह
अथिा क्रकसी क्षेत्र को प्रभावित करती है। हैजा, प्लेग, जापानी इन्सेफेलाइरटस / एक्यूट
इन्सेफेलाइरटस ससिोम आक्रद इसके उदाहरण हैं; या,
विश्िव्यापी महामारी (Pandemic)- ये विश्ि में पहले से विद्यमान, उभरती या पुनैः उभरती
बीमाररयााँ एिं महामाररयााँ होती हैं। ये महामारी विशाल क्षेत्र, अथावत,् एक महाद्वीप या संपण
ू व
विि तक प्रसाररत हो जाती है; उदाहरण- इन्फ्लुएंजा H1N1 (स्िाइन फ्लू)।
महामाररयों के कारण
स्ि्छता के वनम्न स्तर के पररणामस्िरूप खाद्यान्न ि जल का संदवू षत होना।
आपदा पश्चात् मानि या पशु शिों का अपयावप्त क वनपटान।
बाढ़ और भूकंप के पश्चात् उत्पन्न पररवस्थवतयााँ।
वनम्न स्तरीय ठोस अपवशष्ट प्रबंधन, इससे प्लेग जैसी महामाररयााँ उत्पन्न हो सकती हैं।
ितवमान में प्लेग की घटना काफी असामान्य है, परन्तु यह अभी भी घरटत हो सकती है और व्यापक
स्तर पर मानि जीिन की क्षवत का कारण बन सकती है तथा सामान्य जीिन को अस्त-व्यस्त कर
सकती है; जैसा िषव 1994 में सूरत में हुआ था।
जैि-आतंकिाक्रदयों द्वारा प्रसार हेतु प्रयुक्त विवधयां
एरोसोल्स-जैविक एजेंटों को िायु में प्रसाररत कर क्रदया जाता है वजससे सूक्ष्म धुंध (fine mist)
का वनमावण होता है जो कई मीलों तक फै ल सकती है।
जंत-ु वपस्सू, चूह,े मवक्खयााँ, म्छर और पशुधन।
खाद्यान्न और जल संदष
ू ण - कु छ रोगजनक जीि एिं विषाक्त पदाथव खाद्य और जल आपूर्नतयों में
बने रह सकते हैं।
एक व्यवक्त से दूसरे व्यवक्त में (संक्रमण द्वारा)- छोटी चेचक, प्लेग और लस्सा विषाणु (Lassa
viruses)।
भारत में महामाररयों के प्रमुख स्रोत
भारत में महामाररयों के प्रमुख स्रोतों को व्यापक रूप से वनम्नानुसार िगीकृ त क्रकया जा सकता है:
जल जवनत रोग, जैस-े हैजा (एिं आंत्रशोथ के प्रकार), टाइफाइड, हेपेटाइरटस A, हेपेटाइरटस B
आक्रद; इन बीमाररयों के प्रसार से उत्पन्न प्रमुख महामाररयााँ अतीत में दजव की जाती रही हैं तथा
आज भी होती रहती हैं।
िेक्टर जवनत (प्राय: म्छर जवनत) महामाररयााँ, जैस-े डेंगू बुखार, वचकनगुवनया बुखार, जापानी
इन्सेफेलाइरटस, मलेररया, कालाजार आक्रद; ये महामाररयााँ प्राय: देश के वनवश्चत क्षेत्रों में घरटत
होती हैं;
एक व्यवक्त से दूसरे व्यवक्त में बीमाररयों का संचरण, जैस-े एर्डस एिं अन्य यौन रोग; एिं
इन्फ्लुएज
ं ा और खसरा जैसे िायु जवनत रोग जो फोमाइट (उपयोग क्रकए गए कपड़ों आक्रद) के
द्वारा भी संचररत हो सकते हैं।
इसके अवतररक्त, चीन में फै ले सीवियर एक्यूट रे वस्परे टरी ससिोम (SARS) तथा देश के कु छ वहस्सों में
हाल ही में घरटत एवियन फ्लू का प्रकोप आक्रद जैसे उभरते संक्रामक रोगों के कु छ प्रकारों के एक व्यवक्त
से दूसरे व्यवक्त में संचाररत होने की क्षमता होती है। डेंगू विषाणु के कारण भारत के कई महानगरों में
महामाररयााँ फै ली हैं और अन्य विवभन्न प्रकार की विषाणुजवनत बीमाररयों का प्रकोप भी आिती घटना
है।
जैविक आपदा हेतु सहयोगी प्रिृवत्तयां
जैविक एजेंटों की वनम्न लागत एिं व्यापक स्तर पर उपलब्धता।
कम मात्रा में अत्यवधक नुकसान पहुाँचाने की क्षमता।
88 www.visionias.in ©Vision IAS
जैि प्रौद्योवगकी के क्षेत्र में हुई प्रगवत ने उत्पादन को आसान बना क्रदया है।
प्रयुक्त एजेंट आमतौर पर मौजूदा बीमाररयों को उद्दीप्त क करने िाले प्राकृ वतक रोगजनक होते हैं।
अत्यवधक विनाशकारी क्षमता होती है।
घातक जैविक एजेंटों का उत्पादन आसानी से एिं कम लागत में क्रकया जा सकता है।
संक्रमण और बीमारी के लक्षण प्रकट होने के मध्य का समय-अंतराल रासायवनक अनािरण
(Chemical exposure) में लगे समय की तुलना में अवधक लंबा होता है।
जैविक आपदा के दुष्टपररणाम
इसके पररणामस्िरुप लघु अिवध में ही मृत्युदर में भारी िृवि हो सकती है वजससे जनसंख्या का
ह्रास हो सकता है तदनुसार आर्नथक गवतविवधयों में भी वगरािट हो सकती है।
इसके पररणामस्िरुप क्रकसी अथवव्यिस्था में संसाधनों की एक बड़ी मात्रा को विकास कायों के
स्थान पर आपदा से वनपटने में लगाना पड़ता है।
सामूवहक विनाश।
रोकथाम और शमन के उपाय
आम जनता को वशवक्षत क्रकया जाना चावहए तथा इससे संबंवधत खतरों और जोवखम से अिगत
कराया जाना चावहए।
के िल पका हुए भोजन तथा उबले हुए/क्लोरीन उपचाररत/छने हुए जल का उपयोग क्रकया जाना
चावहए।
कीटों और कृं तक वनयंत्रण उपायों को तत्काल आरं भ करना चावहए।
संक्रदग्ध और प्रमावणत मामलों में परीक्षण के पश्चात् उनको पृथक करना महत्िपूणव है।
89 www.visionias.in ©Vision IAS
उवचत प्रयोगशाला वनदान हेतु प्रयोगशालाओं का एक नेटिकव स्थावपत क्रकया जाना चावहए।
ितवमान रोग वनगरानी प्रणाली के साथ-साथ िेक्टर वनयंत्रण उपायों का अवधक सख्ती से पालन
क्रकया जाना चावहए।
संक्रदग्ध क्षेत्रों में सामूवहक टीकाकरण कायवक्रमों का अवधक सख्ती से पालन क्रकया जाना आिश्यक
है।
अनुपलब्ध टीकों के शोध पर अवधक ध्यान क्रदया जाना चावहए।
ितवमान चुनौवतयां
रोग के प्राकृ वतक एिं कृ वत्रम प्रकोपों (जैि आतंकिाद) से उत्पन्न महत्िपूणव चुनौवतयााँ वनम्नवलवखत हैं:
प्रारं वभक प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने िाली क्रक्रयाविवधयों के विकास का अभाि।
परीक्षण एिं वचक्रकत्सीय प्रत्युपायों को गवत प्रदान करने में अक्षमता।
अंतरावष्ट्रीय सहयोग का अभाि, जबक्रक महामाररयां राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती हैं।
आपदा पश्चात् उत्पन्न महामाररयों की रोकथाम हेतु एक उपयुक्त योजना का अभाि।
एकीकृ त रोग वनगरानी प्रणाली का विकास क्रकया जाना अभी भी शेष है।
मानक जोवखम और सुभेद्यता आकलन योजनाओं की अनुपवस्थवत।
जैविक आतंकिादी गवतविवधयों हेतु विवभन्न सुभेद्य स्थानों के वलए संकेतकों और फ़ील्ड-परीवक्षत
चरों का अभाि।
विशेषकर सीमा-पार प्रसार की संगणना (कं प्यूटटग) हेतु जोवखम-क्षेत्र वनधावरक मानवचत्रों की
उपलब्धता न होना।
विवभन्न िैविक आक्रमणों एिं भारतीय संदभव में संिर्नधत संभावित जोवखम के मध्य संपकों के
आकलन हेतु कोई व्यापक अध्ययन नहीं क्रकया गया है।
वहतधारकों के मध्य बहु-आयामी सूचना नेटिकव एिं विवभन्न जैविक एजेंटों से संबंवधत जानकारी
का अभाि है।
आपातकालीन कायवकतावओं की भूवमका के विस्तृत वििरण के साथ-साथ खुक्रफया जानकारी एकत्र
करने िाली एजेंवसयों का भी काफी अभाि है।
नमूनों के संग्रहण एिं प्रयोगशालाओं तक उनके उवचत प्रेषण हेतु क्षमता का अभाि।
घटना स्थल पर जैविक एजेंटों का शीघ्र पता लगाने एिं उनकी विशेषताओं के वनधावरण हेतु
अपयावप्त क सुविधाएाँ।
जैविक आपदा प्रबंधन के वलए आिश्यक कदम
विवधक ढांचा: महामारी रोग अवधवनयम को 1897 में अवधवनयवमत क्रकया गया था वजसे वनरस्त
क्रकए जाने की आिश्यकता है। यह अवधवनयम कें द्र को जैविक आपात वस्थवत में हस्तक्षेप करने की
कोई शवक्त प्रदान नहीं करता। इसे ऐसे अवधवनयम द्वारा प्रवतस्थावपत क्रकया जाना चावहए जो जैि
आतंकिादी हमलों एिं शत्रु द्वारा जैविक हवथयारों के उपयोग, सीमा-पार के मुद्दों तथा रोगों के
अंतरराष्ट्रीय प्रसार सवहत प्रचवलत एिं संभावित सािवजवनक स्िास््य आिश्यकताओं का ध्यान
रखें।
पररचालन ढांचा: राष्ट्रीय स्तर पर, जैविक आपदाओं पर कोई नीवत मौ़ूद नहीं है। स्िास््य एिं
पररिार कल्याण मंत्रालय की मौजूदा आपात योजना लगभग 10 िषव पुरानी है और इसमें व्यापक
संशोधन की आिश्यकता है। जन स्िास््य से संबंवधत सभी घटक, अथावत् सिोच्च संस्थाएं,
जानपक्रदक रोग विज्ञान (field epidemiology), पयविेक्षण, वशक्षण, प्रवशक्षण, अनुसंधान आक्रद
के सुदढ़ृ ीकरण की आिश्यकता है।
कमान, वनयंत्रण और समन्िय: 1994 में सूरत में प्लेग एिं 2006 में एवियन इं फ्लूएज
ं ा के प्रकोप
से सीखे गए सबकों में से एक यह है क्रक ऐसे के प्रकोप के प्रबंधन हेतु पशु स्िास््य, गृह विभाग,
90 www.visionias.in ©Vision IAS
संचार, मीवडया, इत्याक्रद जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ वनयवमत आधार पर समन्िय को सुदढृ करने की
आिश्यकता है।
मानि संसाधन में िृवि: वजला और उप-वजला स्तरों पर मेवडकल एिं पैरा-मेवडकल कर्नमयों की
कमी है। लोक स्िास््य विशेषज्ञों, महामारीविदों (एवपडेमोलोवजस्ट), वचक्रकत्सीय सूक्ष्मजीि
विज्ञानी (वक्लवनकल माइक्रोबायोलोवजस्ट) एिं विषाणुविज्ञावनयों (िाइरालवजस्ट) की भी
अत्यवधक कमी है। विगत िषों में इन प्रयोजनों के वलए वशक्षण/प्रवशक्षण संस्थानों की स्थापना की
क्रदशा में सीवमत प्रयास ही क्रकए गए हैं।
आधारभूत अिसंरचनागत ढांचा: शीघ्र वनदान के वलए बायोसेफ्टी लेबोरे टरी, उपस्िास््य कें द्रों के
नेटिकव , प्राथवमक स्िास््य के न्द्र एिं सामुदावयक स्िास््य कें द्र, महामारी को फै लने से रोकने के
वलए आिश्यक िैक्सीन और औषवधयों की पयावप्त क मात्रा युक्त औषधालयों के विस्तार की
आिश्यकता है।
3.3.2. औद्योवगक आपदाएाँ (Industrial Disasters)
औद्योवगक आपदाएं क्या हैं?
िस्तु और सेिाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन (अथावत् औद्योवगक स्तर पर उत्पादन) से लोगों एिं
जीिन-सहायता प्रणावलयों (लाइफ सपोटव वसस्टम) के वलए उत्पन्न होने िाले खतरे औद्योवगक
संकट हैं। जब ये खतरे मानि की सामना करने की क्षमताओं या पयाविरणीय प्रणावलयों की
अिशोषण क्षमताओं से अवधक हो जाते हैं तब औद्योवगक आपदाओं को जन्म देते हैं। वनष्टकषवण,
प्रसंस्करण, विवनमावण, पररिहन, भंडारण, उपयोग और वनपटान इत्याक्रद सवहत उत्पादन प्रक्रक्रया
के क्रकसी भी चरण पर औद्योवगक संकट उत्पन्न हो सकते हैं।
भारत की कु छ बड़ी औद्योवगक आपदाएाँ
भोपाल गैस त्रासदी, 1984
चासनाला खान दुघवटना, 1975
जयपुर ऑयल वडपो अविकांड, 2009
कोरबा में वचमनी का वगरना, 2009
मायापुरी रे वडयोलॉवजकल दुघवटना, 2010
बॉम्बे डॉक्स विस्फोट, 1944
ऊाँचाहार में NTPC के बॉयलर में विस्फोट, 2017
औद्योवगक आपदाओं के प्रकार
अप्रत्यावशत ररसाि (Accident release): खतरनाक रासायवनक ि अन्य पदाथों (जैसे रसायन,
रे वडयोधमी, आनुिवं शक पदाथव) के उत्पादन, पररिहन या हैंडसलग के दौरान ररसाि।
विस्फोट: आपदाओं को विस्फोट के रूप में के िल तभी िगीकृ त क्रकया जाएगा जब विस्फोट
िास्तविक आपदा हों। यक्रद विस्फोट क्रकसी अन्य आपदा का कारण है, तो उस घटना को पररणामी
आपदा के रूप में िगीकृ त क्रकया जाएगा।
रासायवनक विस्फोट: रासायवनक मूल की दहनशील सामग्री के विस्फोट के कारण भीषण विनाश।
परमाणु विस्फोट/विक्रकरण: वसविल उद्देश्यों से संचावलत नावभकीय संयंत्रों में अंतरावष्ट्रीय स्तर पर
स्थावपत सुरक्षा स्तरों से अवधक स्तर का अप्रत्यावशत ररसाि।
91 www.visionias.in ©Vision IAS
खदान विस्फोट: ऐसी दुघवटनाएं िायु के साथ प्राकृ वतक गैस या कोयले की धूल (coal dust) की
अवभक्रक्रया से घरटत होती हैं।
प्रदूषण: हावनकारक औद्योवगक, रासायवनक या जैविक अपवशष्ट द्वारा, मलबे या मानि वनर्नमत
उत्पादों द्वारा तथा प्राकृ वतक और पयाविरणीय संसाधनों के कु प्रबंधन द्वारा पयाविरण के एक या
एक से अवधक घटकों का वनम्नीकरण।
अम्ल िषाव: सल्फर और नाइरोजन के यौवगकों जैसे रासायवनक प्रदूषकों के पररणामस्िरूप
िायुमडडल में उत्पन्न अम्लीय यौवगकों की अत्यवधक सान्द्रता का िषाव के साथ बह जाना।
वनक्षेवपत होने पर ये मृदा एिं जल की अम्लीयता में िृवि करते हैं, वजससे कृ वष एिं पाररवस्थवतकी
को क्षवत होती है।
रासायवनक प्रदूषण: औद्योवगक क्षेत्रों के वनकट जल या िायु के अकस्मात प्रदूवषत होने से त्िचा की
स्थायी क्षवत के साथ शरीर के आंतररक भाग में विकार उत्पन्न होते हैं।
िायुमडडलीय प्रदूषण: प्राकृ वतक और कृ वत्रम ईंधनों के दहन, रसायनों और अन्य औद्योवगक
प्रक्रक्रयाओं एिं परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न गैसों, ठोस और विक्रकरणों की विशाल मात्रा द्वारा
िायुमंडल का संदष
ू ण।
भोपाल जैसी त्रासक्रदयााँ और भी घरटत
हो सकती हैं…
कें द्रीय प्रदूषण वनयंत्रण बोडव के द्वारा
खतरनाक प्रदूषकों से संदवू षत कु छ
स्थलों की पहचान की गई है।
1. इलूर-इडयार (Eloor-Edayar) 6. गंजाम पारा संदवू षत क्षेत्र, गंजाम, ओवडशा: विवभन्न
क्षेत्र, कोवच्च, के रल: इस क्षेत्र के स्थानों पर बंद हो चुके कॉवस्टक सोडा कारखानों का 50,000
नीचे 2,00,000 टन से अवधक टन से भी अवधक पारा अपवशष्ट मौजूद है।
मात्रा में अत्यवधक खतरनाक
92 www.visionias.in ©Vision IAS
रसायन, कीटनाशक अपवशष्ट दबे
हुए हैं।
2. रानीपेट क्रोवमयम संदवू षत क्षेत्र, 7. जूही-बबुरैया-राखी मंडी, कानपुर, उत्तर प्रदेश: सघन
तवमलनाडु : यहााँ लगभग 3 आबादी िाले अवधिासीय क्षेत्र के भीतर लगभग 2 हेक्टेयर
हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग क्षेत्र की मृदा हेक्सािैलेन्ट क्रोवमयम के लगभग 10,000 टन
2,20,000 टन क्रोवमयम अपवशष्ट से संदवू षत; प्रदूषणकतावओं के विषय में जानकारी नहीं।
का 2 से 4 मीटर ऊंचा ढेर लगा
हुआ है।
3. रतलाम औद्योवगक क्षेत्र, रतलाम, 8. रवनया, कानपूर देहात, उत्तर प्रदेश: वनजी भूवम के लगभग
मध्य प्रदेश: H-अम्ल बनाने िाले 200 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 45,000 टन हेक्सािैलेन्ट
फामाव उद्योग के अपिाह से क्रोवमयम अपवशष्ट का ढेर लगा हुआ है।
संदवू षत
4. क्रोवमयम संदवू षत क्षेत्र, सुद
ं रगढ़, 9. वनिा गााँि, पवश्चम बंगाल: 4440 टन क्रोवमयम का ढेर;
ओवडशा: 50,000 टन क्रोवमयम प्रदूषणकतावओं के विषय में जानकारी नहीं।
अपवशष्ट खुले में पड़ा हुआ है।
5. तालचेर क्रोवमयम संदवू षत क्षेत्र, 10. स्थायी काबववनक प्रदूषक (POP)-संदवू षत क्षेत्र, लखनऊ:
तालचेर, ओवडशा: बंद हो चुकी इं वडयन पेस्टीसाइड वलवमटेड ने 36,432 टन
क्रोम सॉल्ट वनमावण इकाई के हेक्साक्लोरोसाइडोहेक्सेन (HCH) अपवशष्ट उत्पन्न क्रकया है।
60,000 टन अपवशष्ट का खुले में
ढेर लगा हुआ है।
औद्योवगक आपदा के दुष्टपररणाम
मानि जीिन की क्षवत या चोट, कष्टट, पीड़ा, संपवत्त का नुकसान, सामावजक और आर्नथक अिरोध
एिं पयाविरणीय वनम्नीकरण।
भारत में औद्योवगक आपदा जोवखम
भारत, िषव 1984 में विश्ि की एक प्रमुख विनाशकारी रासायवनक (औद्योवगक) आपदा "भोपाल
गैस त्रासदी" का साक्षी रहा है। यह इवतहास में सबसे विनाशकारी रासायवनक दुघवटना थी, वजसमें
विषाक्त गैस वमथाइल आइसोसाइनेट (MIC) के दुघवटनािश ररसाि के कारण हजारों लोगों की
मृत्यु हो गयी थी।
भोपाल की त्रासदी द्वारा देश की सुभेद्यता सुस्पष्ट हो जाने के पश्चात् भी भारत वनरं तर विवभन्न
रासायवनक दुघवटनाओं का साक्षी रहा है। के िल वपछले दशक में ही, भारत में 130 महत्िपूणव
रासायवनक दुघवटनाएं दजव की गईं, वजनके कारण 259 लोगों की मृत्यु हुई और 563 लोग गंभीर
रूप से घायल हुए।
देश के सभी जोनों में लगभग 1861 प्रमुख दुघवटना संकट (Major Accident Hazard: MAH)
इकाइयााँ हैं जो 301 वजलों (25 राज्यों तथा 3 संघ शावसत प्रदेशों) में विस्तृत हैं। इसके अवतररक्त
विवभन्न प्रकार की खतरनाक सामवग्रयों से संबंवधत हजारों पंजीकृ त और खतरनाक कारखाने
(MAH मानदंड से नीचे) एिं असंगरठत क्षेत्र गंभीर और जरटल स्तर के आपदा जोवखम उत्पन्न कर
रहे हैं। तीव्र औद्योगीकरण के साथ, औद्योवगक आपदाओं से संबंवधत खतरे में भी िृवि हुई है।
93 www.visionias.in ©Vision IAS
औद्योवगक आपदा वनिारण और शमन रणनीवतयां (Industrial Disaster Prevention and
Mitigation Strategies)
वड़ाइन एिं पूिव रूपांतरण समीक्षा (Design and Pre-modification review): इसमें उवचत
विन्यास, सुविधाएाँ, सामग्री चयन सवम्मवलत है। अत्यवधक विषैले रसायनों को सुरवक्षत रसायनों
से प्रवतस्थावपत करने के प्रयास हेतु अनुसंधान क्रकए जाने चावहए। रसायनों का भंडारण कम क्रकया
जाना चावहए; स्टॉक में कमी से स्ित: ही दुघवटना घरटत होने पर कम क्षवत होगी।
रसायन जोवखम मूल्यांकन (Chemical Risk Assessment:): रसायनों का मूल्यांकन
अनुकूलता, प्रज्िलनशीलता, विषाक्तता, विस्फोट के खतरों और भंडारण के आधार पर क्रकया
जाता है।
प्रक्रक्रया सुरक्षा प्रबंधन (Process Safety Management): प्रमुख प्रक्रक्रया पररितवनों को लागू
करने से पूिव सेफ्टी विल्स एिं इंटरलॉक्स का समािेश, स्क्रसबग प्रणाली आक्रद सवहत प्रक्रक्रया में
शावमल उपकरणों की वििसनीयता का आकलन क्रकया जाना चावहए। प्रबंधन को औद्योवगक
संगठनों में सुरक्षा की संस्कृ वत विकवसत करने का प्रयास करना चावहए।
सुरक्षा ऑवडट: सुरक्षा पिवतयों एिं कायवप्रणावलयों, सुरक्षा तंत्रों एिं मशीनों के प्रदशवन का
अनुिती उपायों के साथ-साथ आिवधक मूल्यांकन क्रकया जाना चावहए।
आपातकालीन योजना: पररणामों तथा उपयुक्त सुविधाओं के साथ विवशष्ट रूप से वलवखत और
अभ्यास की गई आपातकालीन प्रक्रक्रयाओं के प्रभाि को इं वगत करने िाला व्यापक जोवखम
विश्लेषण क्रकया जाना चावहए। यह कायव समुदायों के साथ-साथ राष्ट्रीय या क्षेत्रीय वनगम
प्रावधकरणों द्वारा क्रकया जाना चावहए।
प्रवशक्षण: कमवचाररयों एिं सुरक्षात्मक सेिाओं का उवचत प्रवशक्षण क्रकया जाना चावहए।
खतरनाक िाहनों के वलए विशेष समय और अनुरक्षक (escorts)।
सड़क पर जन सहयोग: जनता को दुघवटनाओं से बचने के वलए पुवलस और क्रकसी भी टैंकर एिं
भारी िाहनों के साथ सहयोग करना चावहए। खतरनाक िाहनों हेतु यथासंभि लघुतम रोड टाइम
(road time) की अनुमवत प्रदान करनी चावहए।
जन जागरूकता: प्रत्येक व्यवक्त को संभावित आपदाओं के विषय में जागरूक होना चावहए एिं
सुरक्षात्मक और सुरक्षा उपायों की जानकारी होनी चावहए। घरे लू और कारों के रखरखाि से
संबंवधत खतरनाक उत्पादों की असाधारण देखभाल हेतु सािधानी बरती जानी चावहए।
खतरनाक सामवग्रयों का उवचत भंडारण: सभी रसायनों और खतरनाक सामवग्रयों का उवचत
तापमान पर भंडारण क्रकया जाना चावहए। इन्हें बच्चों और पशुओं से दूर बंद अलमाररयों में रखा
जाना चावहए। साथ ही, यक्रद प्रवतक्रक्रयाशील पदाथव संग्रवहत क्रकए जाते हैं तो उन्हें िाटरटाइट
कं टेनर में भंडाररत क्रकया जाना चावहए।
मौजूदा विवनयमों के अनुसार, खतरनाक अपवशष्टट का उवचत और सुरवक्षत वनपटान सुवनवश्चत
क्रकया जाए।
सुरवक्षत विकल्पों का उपयोग करना तथा सुरवक्षत, क्रकफायती और संधारणीय प्रौद्योवगक्रकयों एिं
प्रक्रक्रयाओं का अंगीकरण।
भू-उपयोग नीवत का सख्त कायावन्ियन होना चावहए। बफ़र ़ोन (या ‘नो मेन्स जोन’ के रूप में
संदर्नभत) के संबंध में एक कानून लाया जाना चावहए ताक्रक आिासीय/ स्लम बवस्तयों को उद्योगों
के वनकट स्थावपत न क्रकया जा सके । इन क्षेत्रों में पहले से अवधिावसत आिासीय कॉलोवनयों के
स्थानांतरण की आिश्यकता है।
अनुकरणीय सुरक्षा मानकों एिं सांविवधक अनुपालन सुवनवश्चत करने हेतु उद्योगों को उत्कृ ष्ट
प्रदशवन पुरस्कार प्रदान करने की योजना विकवसत एिं कायाववन्ित क्रकया जाना चावहए।
94 www.visionias.in ©Vision IAS
ितवमान चुनौवतयां
बड़ी संख्या में कानून के अवस्तत्ि में होने के बािजूद भी उनका प्रितवन िांवछत स्तर से बहुत कम
हुआ है।
औद्योवगक आपदाओं के मुद्दे पर सतत समाधान योजना वनमावण की क्रदशा में समझ और अनुसंधान
की कमी।
ऐसी आपदाओं हेतु मापदंडों, जागरूकता और तैयाररयों का पयावप्त पृथक्करण नहीं।
व्यािसावयक सुरक्षा एिं स्िास््य और वचक्रकत्सीय आपातकालीन प्रबंधन से संबंवधत राष्ट्रीय
विवनयमों की अनुपवस्थवत।
पेरोवलयम और पेरोवलयम उत्पाद सवहत ितवमान विवनयमों में िगीकरण और पररभाषाओं को
सुसगतं बनाना।
क्रायोजेवनक्स के भंडारण एिं पररिहन से संबंवधत विवनयमों का अभाि।
औद्योवगक रसायनों हेतु जोवखम मूल्यांकन आिश्यकताओं एिं िगीकरण, लेबसलग और पैकेसजग
से संबंवधत कानून का अभाि।
रासायवनक दुघवटना पीवड़तों को क्षवतपूर्नत प्रदान करने हेतु क़ानूनों की गैर-उपलब्धता।
रसायन प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सुसंगवतकरण एिं समािेशन।
उठाए जाने हेतु िांवछत कदम
रासायवनक आपदा से संबंवधत विवभन्न गवतविवधयों के कायावन्ियन की वस्थवत के वलए तकनीकी
रूप से सक्षम प्रावधकरणों की पहचान करने एिं ररपोर्टटग तंत्र के मानकीकरण की आिश्यकता है।
औद्योवगक आपदा को समझने की आिश्यकता पर अवधकावधक ध्यान के वन्द्रत क्रकए जाने की
जरुरत है। ये के िल सुरक्षा समस्याएं मात्र नहीं हैं वजनके समाधान की आिश्यकता है। बवल्क
इनका एक व्यापक महत्ि भी है, क्योंक्रक िे समाज, प्रौद्योवगकी और पयाविरण के मध्य सामंजस्य
के आकलन एिं उस सामंजस्य को अप्रत्यावशत घटनाओं द्वारा सशक्त या कमजोर क्रकए जाने की
कायवप्रणाली के विषय में सीखने का महत्िपूणव अिसर प्रदान करती हैं। इस प्रकार यह ऐसी सूचना
है जो गहन और दूरगामी सामावजक और पयाविरणीय पररितवनकारी युग के दौरान मानिता हेतु
अमूल्य होगी।
औद्योवगक आपदाओं के दो प्रकारों - "सामान्य" और "अप्रत्यावशत" के मध्य अब स्पष्ट विभेद
स्थावपत करने का समय आ गया है। सामान्य आपदाएाँ विशेषज्ञों द्वारा भली प्रकार समझी गयी
होती हैं एिं दीघवकाल से स्थावपत वसिांतों और प्रथाओं के उपयोग से प्रबन्धन के प्रवत संिद
े नशील
होती हैं। अप्रत्यावशत आपदाएं वनतांत ही वभन्न होती हैं तथा इनके प्रवत समझ भी कम होती है।
इनमें भोपाल और चेनोवबल एिं वमनामाता जैसी घटनाओं या उनके दुष्टपररणामों या दोनों जैसी
आपदाएं सवम्मवलत होती हैं- जो हमारे वपछले अनुभि के दायरे से बाहर होती हैं। यह शमन
रणनीवतयों एिं नीवतयों की बेहतर तैयारी में सहायक होगा।
3.3.3. नावभकीय सं क ट (Nuclear Hazards)
नावभकीय संकट क्या है?
यह क्रकसी पदाथव के परमाणु नावभक (atomic nuclei) से वनकलने िाले विक्रकरण से मानि
स्िास््य या पयाविरण को होने िाला जोवखम या खतरा है, या परमाणु नावभक के संलयन या
विखंडन अवभक्रक्रयाओं से उत्पन्न अवनयंवत्रत विस्फोट की संभािना है। इस पररघटना को
रे वडयोधर्नमता के रूप में जाना जाता है और रे वडयोधमी पदाथव से ऊजाव के उत्सजवन को
"रे वडयोधमी प्रदूषण” कहा जाता है।
नावभकीय संकट के स्रोत
प्राकृ वतक संसाधन: बाह्य अंतररक्ष से आने िाली िह्मांडीय क्रकरणें, भूपपवटी के रे वडयोधमी पदाथों
से होने िाले उत्सजवन।
95 www.visionias.in ©Vision IAS
मानि वनर्नमत स्रोत: परमाणु ऊजाव संयंत्र, एक्स-रे , परमाणु बम, परमाणु दुघवटनाएाँ, परमाणु
हवथयार, रे वडयोधमी अयस्कों का खनन और प्रसंस्करण।
नावभकीय आपात वस्थवतयााँ प्रचालन एजेंवसयों के वनयंत्रण के दायरे से बाहर के कारकों से भी उत्पन्न
हो सकती हैं; जैस-े मानिीय त्रुरट, प्रणाली की विफलता, तोड़फोड़, भूकंप, चक्रिात, बाढ़ आक्रद। ऐसी
विफलताओं की संभािना भले ही बहुत कम होती है, लेक्रकन ये ऑन-साइट या ऑफ़-साइट
आपातकालीन वस्थवत उत्पन्न कर सकती हैं। ये अस्पतालों, उद्योगों, कृ वष या अनुसंधान संस्थानों में
विक्रकरण स्रोतों के प्रयोग के दौरान उनमें क्रकसी प्रकार की क्षवत या उनकी दोषपूणव हैंडसलग के कारण
भी उत्पन्न हो सकती हैं।
भारत में नावभकीय संकट का जोवखम
अपनी विवशष्टट भू-जलिायविक पररवस्थवतयों के कारण भारत परं परागत रूप से प्राकृ वतक
आपदाओं के प्रवत सुभेद्य रहा है और ितवमान में विि के अन्य सभी देशों की तरह विवभन्न मानि-
जन्य आपदाओं के प्रवत भी सुभेद्य बन गया है।
भारत में नावभकीय ऊजाव विद्युत के प्रमुख स्रोतों में से एक है। भारत में एक समृि और लगभग
पूणव रूप से स्िदेशी नावभकीय ऊजाव कायवक्रम मौ़ूद है। वजसके तहत 2024 तक सतत सक्रक्रय
14.6 GWe एिं 2032 तक 63 GWe परमाणु क्षमता प्राप्त करने की संभािना है। इसका लक्ष्य
िषव 2050 तक नावभकीय ऊजाव से 25% विद्युत आपूर्नत करना है। क्रकसी नावभकीय संस्थापन में
संयंत्र स्तर पर नावभकीय और रे वडयोलॉवजकल आपात वस्थवत उत्पन्न हो सकती है। यह आपात
वस्थवत उस संयत्रं के आस-पास के क्षेत्र पर इसके प्रभाि की सीमा को देखते हुए संयंत्र/साइट या
ऑफ साइट आपात वस्थवत भी बन सकती है।
96 www.visionias.in ©Vision IAS
नावभकीय संकट के प्रभाि :
मृत्यु, अत्यवधक या स्थायी दुबवलता या कैं सर, आंखों में मोवतयासबद, बालों का झड़ना इत्याक्रद का
खतरा बढ़ जाना।
विक्रकरण रुग्णता: व्यवक्त के बीमार पड़ने का जोवखम इस त्य पर वनभवर करता है क्रक शरीर के
द्वारा क्रकतने विक्रकरण का अिशोषण क्रकया गया है। विक्रकरण रुग्णता प्राय: घातक होती है और
जठरांत्र पथ (gastrointestinal tract) की आंतररक परत से रक्तस्राि का कारण बन सकती है।
कृ वष उत्पादों, पशुओं और फसलों की क्षवत या विनाश;
पयाविरणीय संसाधनों का वनम्नीकरण;
सािवजवनक और वनजी संपवत्त की क्षवत या अिमूल्यन; तथा
भविष्टय की पीक्रढ़यों में उत्पररितवन द्वारा आनुिंवशक पररितवन।
नावभकीय संकट शमन रणनीवतयां
वचवन्हत विक्रकरण स्रोतों से व्यवक्तयों की सुरक्षा हेतु चार पिवतयां वनम्नवलवखत हैं:
o समय को सीवमत करना: व्यािसावयक पररवस्थवतयों में एक्सपोजर टाइम को सीवमत करके
ग्रहण क्रकये जाने िाली विक्रकरण की मात्रा कम की जा सकती है।
o दूरी: स्रोत से बढ़ती दूरी के साथ विक्रकरण की तीव्रता घटती है।
o परररक्षण (Shielding): सीसा, कं क्रीट या जल अिरोध गामा क्रकरणों जैसे उच्च स्तरीय भेदक
विक्रकरण से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीव्र रे वडयोधमी पदाथव जल के अन्दर
या मोटी कं क्रीट वनर्नमत या सीसे से आस्तररत कमरों में भडडाररत या संचावलत क्रकये जाते हैं।
o प्रसार का वनयंत्रण (Containment): अत्यवधक रे वडयोधमी पदाथों को भलीभांवत बंद करके
कायवस्थल और पयाविरण से बाहर रखा जाता है। परमाणु ररएक्टर कई अिरोध युक्त क्लोज्ड
वसस्टम के भीतर संचावलत क्रकए जाते हैं जो रे वडयोधमी पदाथों के प्रसार को वनयंवत्रत रखते
हैं।
संसाधनों के कु शल उपयोग हेतु आपात वस्थवतयों के प्रबंधन में लचीलेपन को प्रोत्साहन प्रदान
करना।
तत्काल कायविाही हेतु पूणवकावलक क्षमता का अनुरक्षण।
िांवछत सुरक्षा प्रदान करने के वलए अनुक्रक्रयाओं, योजनाओं, सुविधाओं और क्रकसी भी आिश्यक
अंतर-संगठनात्मक समन्िय को सुवनवश्चत करना पयावप्त क है।
97 www.visionias.in ©Vision IAS
नावभकीय दुघवटनाओं के वलए सुरक्षा उपाय एिं व्यािसावयक जोवखम के विरुि उवचत कदम और
उपाय क्रकए जाने चावहए।
भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम
नावभकीय प्रौद्योवगकी के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर बल क्रदए जाने के साथ ही परमाणु खतरों
के जोवखम में भी िृवि हुई है। सािवजवनक डोमेन में मानि-जन्य रे वडयोलॉवजकल आपात वस्थवत के
संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में परमाणु ऊजाव विभाग (DAE) की पहचान की गई है।
भारत में लोगों और पयाविरण की सुरक्षा सुवनवश्चत करने हेतु नावभकीय सुविधाओं में अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर अंगीकृ त क्रदशावनदेश को स्िीकृ वत प्रदान की गयी है।
क्रकसी भी परमाणु संकट से सािधान रहने हेतु संकट प्रबंधन प्रणाली भी विद्यमान है।
स्थानीय आपात वस्थवत पर वनयंत्रण हेतु सुविधा के भीतर अन्य आपातकालीन अनुक्रक्रया योजनाएं
तैयार की गयी हैं। सािवजवनक डोमेन में भी ऐसी आपात वस्थवत से वनपटने हेतु अनुक्रक्रया
योजनाओं को तैयार क्रकया गया है, वजसे "ऑफ साइट आपात वस्थवत" के रूप में जाना जाता है।
प्रत्येक स्थल या साइट के वलए अलग-अलग योजनाएं तैयार की गई हैं - जो स्थानीय वजला
प्रशासन के अवधकार क्षेत्र में हैं। यह संयंत्र के चारों ओर लगभग 16 क्रकमी वत्रज्या को किर करती
हैं या ऑफसाइट आपात वनयोजन जोन को किर करती हैं।
मोबाइल विक्रकरण जांच प्रणाली (Mobile Radiation Detection System: MRDS)
NDMA के द्वारा रे वडयोलॉवजकल आपात वस्थवत से वनपटने हेतु राष्ट्रीय स्तर की तैयाररयों पर एक
पायलट पररयोजना लांच की गयी है। इस पररयोजना के एक भाग के रूप में पुवलस ि NDRF
कर्नमयों को रे वडयोलॉवजकल आपात वस्थवत के प्रबंधन हेतु समथव बनाने की पहल की गयी है।
3.3.4. भीड़ प्रबं ध न (Crowd Management)
भीड़ प्रबंधन से आप क्या समझते है?
इसके अंतगवत सभी सािवजवनक सभाओं और समारोहों के आयोजन के सन्दभव में कानून प्रितवन ,
प्रबंधन, हस्तक्षेप और वनयंत्रण रणनीवतयों को सवम्मवलत क्रकया जाता है। यह आयोजन की िैध
गवतविवधयों को जारी रखने के उद्देश्य से समारोह पूि,व उसके दौरान और उसके पश्चात् प्रयुक्त
रणनीवतयों और कायवनीवतयों को भी विशेष रूप से संदर्नभत करता है, जबक्रक भीड़ वनयंत्रण से
तात्पयव समूह के व्यिहार पर प्रवतबंध या सीमा आरोवपत करना है।
भीड़ प्रबंधन की आिश्यकता
अवधक भीड़ समाज के एक बड़े वहस्से के वलए परे शानी और करठनाईयों का कारण बनती है
वजससे यातायात में गंभीर विलम्ब, भगदड़, लोगों के बीच झगड़े, दंग,े भूदश्ृ य में पररितवन वआद
98 www.visionias.in ©Vision IAS
जैसी वस्थवतयााँ उत्पन्न होती हैं और अंततैः ये वचक्रकत्सीय आपात और आपदाओं का कारण बन
जाती हैं। हाल के िषों में भारत ऐसी अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है वजससे बड़ी सं ख्या में लोग
हताहत हुए हैं।
भीड़ प्रबन्धन एिं भीड़ वनयंत्रण के मध्य अंतर
भीड़ प्रबन्धन
इसमें क्रकसी स्थान के उपयोग से पहले उसके संबंध में इस बात का मूल्यांकन सवम्मवलत है क्रक उसमें
क्रकतने लोगों को साँभालने की क्षमता है।
इसमें भीड़ के संभावित स्तर, प्रिेश और वनकास मागों की पयावप्त कता, रटकट कलेक्शन जैसी प्रिेश
संबंधी प्रक्रक्रयाएं और संभावित गवतविवधयों एिं समूह व्यिहार का मूल्यांकन सवम्मवलत है।
भीड़ वनयंत्रण
यह भीड़ प्रबन्धन योजना का एक भाग हो सकता है, या भीड़ द्वारा उत्पन्न क्रकसी समस्या की
प्रवतक्रक्रया स्िरूप की गयी आकवस्मक कायविाही भी हो सकता है।
इसमें चरम उपाय सवम्मवलत हो सकते हैं, जैसे क्रक बल प्रयोग, वगरफ़्तारी या शारीररक रूप से
क्रकसी प्रकार के नुकसान की धमकी।
इसके अंतगवत अिरोधों का प्रयोग करके लोगों के वलए उपलब्ध स्थान और उनकी सामूवहक
आिाजाही को वनयंवत्रत क्रकया जा सकता है।
अनुपयुक्त और खराब तरह से प्रबंवधत वनयंत्रण प्रक्रक्रया, भीड़ से होने िाली दुघवटनाओं को रोकने के
बजाए उनकी संभािनाओं को और बढ़ा देती है। उदाहरण के वलए, क्रकसी रॉक कं सटव में असभ्य
व्यवक्तयों के समूह पर पुवलस की प्रवतक्रक्रया दशवकों के समूह को ऐसे क्षेत्र में खदेड़ सकती है जहााँ कोई
वनकास मागव उपलब्ध न हो।
भीड़ आपदाओं के कारण और उत्प्रेरक
संरचनात्मक विध्िंस
o अिरोधों या अस्थाई संरचनाओं का का टू ट जाना;
o मागों में अिरोध;
o खराब सुरक्षा रे सलग;
o अपयावप्त प्रकावशत सीक्रढ़यााँ, संकीणव सीक्रढ़यााँ; एिं
o आपातकालीन वनकासों का अभाि।
अवि/विद्युत
o आग पकड़ने िाले लकड़ी के ढांचे;
o विद्युत आपूर्नत में विफलता; एिं
o शॉटव सर्दकट।
भीड़ वनयंत्रण
o भीड़ को पृथक करने हेतु उपयुक्त विभाजन व्यिस्था का अभाि;
o उवचत सािवजवनक संबोधन प्रणावलयों का अभाि;
o िाहनों की अवनयंवत्रत पार्ककग ि आिाजाही; एिं
o के िल एक प्रमुख वनकास मागव पर वनभवरता।
भीड़ व्यिहार
o प्रिेश द्वार या वनकास द्वारों की ओर असभ्य उतािलापन;
o क्रकसी िस्तु का वितरण क्रकए जाने के दौरान उतािलापन;
o अचानक सामूवहक वनकासी;
o रेनों के प्लेटफामों में अंवतम समय में बदलाि; एिं
o क्रकसी कायवक्रम की शुरुआत में विलंब के कारण क्रोवधत भीड़।
सुरक्षा
o भीड़ की CCTV वनगरानी का अभाि;
o सुरक्षा कमवचाररयों के पास िॉकी–टॉकी का अभाि;
99 www.visionias.in ©Vision IAS
o मेटल वडटेक्टर डोर फ्रेम्स की कमी; एिं
o भीड़ वनयंत्रण के विवनयमन हेतु सुरक्षा कर्नमयों का कम अनुभि ि प्रवशक्षण।
वहतधारकों के मध्य समन्िय का अभाि
o एजेंवसयों के मध्य समन्िय अंतराल;
o संप्रष
े ण में विलंब;
o खराब अिसंरचना; एिं
o कागजी योजनाएं एिं वित्त की कमी के कारण कोई कायावन्ियन नहीं।
भीड़ आपदा के वलए रोकथाम और शमन रणनीवतयााँ
भीड़ प्रबंधन, हस्तक्षेप और वनयंत्रण रणनीवतयों एिं नीवतगत आयामों में वनम्नवलवखत सवम्मवलत हो
सकते हैं:
भीड़ से संपकव स्थावपत करना, भीड़ के व्यिहार को समझना;
मौवखक स्िीकृ वत प्राप्त क करना;
क्षमता वनयोजन;
प्रथम संशोधन गवतविवधयों का समथवन और सुगमीकरण;
यातायात प्रबंधन और/या वनयंत्रण योजना विकवसत करना;
भीड़ वनयंत्रण रणनीवत (Crowd Control Strategy) और वततर-वबतर करने की विवधयों
(dispersal methods) का प्रयोग;
अत्यािश्यक सुविधाओं की सुरक्षा;
कानून व्यिस्था की उपवस्थवत को दशावना; एिं
सूचना का उवचत प्रसारण।
राष्टरीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA) क्रदशावनदेश
हाल ही में 2017 में NDMA के द्वारा 'त्योहारों के इस मौसम में जोवखम न्यूनीकरण’ हेतु भीड़ प्रबंधन
क्रदशावनदेश जारी क्रकए गए।
मुक्त आिागमन: पहला कदम पंडाल ि दशहरा मैदानों के चारों ओर के क्षेत्रों में यातायात को
विवनयवमत करना है।
o पैदल चलने िालों के वलए महत्िपूणव सबदुओं पर आयोजन स्थल तक पहुंचने एिं
आपातकालीन वनकास मागों तक पहुाँचने के वलए मागव मानवचत्र (route maps) प्रदर्नशत
क्रकया जाना चावहए।
o एक कतार में लोगों की आिाजाही सुवनवश्चत करने हेतु बैररके सडग करना बढ़ती भीड़ को
वनयंवत्रत करने हेतु महत्िपूणव है।
100 www.visionias.in ©Vision IAS
o पैदल मागव में अनवधकृ त पार्ककग एिं खाने-पीने की िस्तुओं के अस्थाई स्टालों पर भी ध्यान
क्रदए जाने की आिश्यकता है।
वनगरानी: छीनाझपटी (स्नैसचग) और अन्य छोटे अपराधों के जोवखम न्यूनीकरण हेतु गवतविवध की
वनगरानी के वलए CCTV कै मरे एिं पुवलस की उपवस्थवत भी आयोजनकतावओं की कायवसूची में
होनी चावहए।
भीड़-भाड़ िाले स्थानों में वचक्रकत्सीय आपात वस्थवत उत्पन्न हो सकती है। एम्बुलेंस और स्िास््य
देखभाल पेशेिरों को तैयार रखने (stand-by) से आकवस्मक पररवस्थवतयों में जीिन रक्षा की जा
सकती है।
प्रवतभावगयों के वलए:
o वनकास मागों से पररवचत होना, शांवत बनाए रखना एिं वनदेशों को पालन करना भगदड़
जैसी वस्थवतयों को रोकने में सहायक होगा।
o यक्रद भगदड़ हो जाती है तो अपने हाथों को एक बॉक्सर की तरह रखकर सीने को बचाएाँ और
भीड़ की क्रदशा में आगे बढ़ते रहें।
o ररक्त स्थान के वलए चौकन्ने रहें और कहीं भी भीड़ कम हो तो बल ल में चले जाएं। दीिारों,
बैररके ड या द्वारमागों जैसे मागाविरोधों से दूर रहें।
o अपने पैरों पर खड़े रहें और यक्रद वगर जाएाँ तो शीघ्रतापूिकव खड़े हो जाएं। यक्रद उठ नहीं पा
रहे हैं तो अपने वसर को अपने हाथों से ढक लें और गभवस्थ वशशु की भांवत अपने शरीर
वसकोड़ लें ताक्रक जोवखम क्षेत्र (exposure area) कम होने के कारण गंभीर रूप से घायल
होने की संभािना न्यूनतम हो जाए।
आग से संबवं धत: पंडालों में अवनयोवजत और अनवधकृ त वबजली के तार, खाने-पीने के स्टॉलों पर
LPG वससलडर एिं दशहरे में रािण दहन के वलए बनाए गए पुतलों में छु पे पटाखे आग लगने का
खतरा उत्पन्न करते हैं।
o आयोजकों को वबजली का अवधकृ त प्रयोग, अवि शामक एिं अन्य व्यिस्थाओं को सुवनवश्चत करना
चावहए तथा सुरक्षा क्रदशावनदेशों का अनुपालन करना चावहए। आस-पड़ोस में वस्थत अस्पतालों
की एक सूची आपात वस्थवत में काम आ सकती है।
101 www.visionias.in ©Vision IAS
102 www.visionias.in ©Vision IAS
अध्याय-4
4. अं त राव ष्ट्रीय सहयोग तथा ितव मान घटनाक्रम
(International Cooperation and Current Developments)
4.1. आपदा जोवखम न्यू नीकरण हे तु िै विक फ्रे मिकव
(Global Frameworks for Disaster Risk Reduction)
4.1.1. ह्योगो फ्रे मिकव फॉर एक्शन 2005-2015: राष्ट्रों तथा समु दायों की प्रत्यास्थता का
वनमाव ण
[Hyogo Framework for Action (HFA): Building the Resilience of Nations and
Communities 2005-2015]
भारत ह्योगो फ्रेमिकव फॉर एक्शन (HFA) का हस्ताक्षरकताव है। इस फ्रेमिकव को िैविक स्तर पर
आपदाओं से होने िाली जीिन की हावन तथा राष्ट्रों ि समुदायों की आर्नथक एिं पयाविरणीय
पररसंपवत्तयों की हावन को कम करने हेतु स्िीकृ त क्रकया गया था। इस फ्रेमिकव के अंतगवत
संधारणीय विकास नीवतयों, क्षमता वनमावण तथा तैयारी एिं सुभेद्यता न्यूनीकरण संबंधी
रणनीवतयों में आपदा जोवखम न्यूनीकरण (DRR) के एकीकरण हेतु तीन रणनीवतक लक्ष्य
(strategic goals) एिं पांच प्राथवमक कायविाही क्षेत्र (priority action areas) वनयत क्रकए
गए हैं।
HFA के तीन रणनीवतक लक्ष्य और उनके कायावन्ियन हेतु भारत द्वारा उठाए जाने िाले कदम:
(i) लक्ष्य 1 : “आपदा की रोकथाम, उसका शमन, संबवं धत तैयारी तथा सुभद्य
े ता में कमी लाने पर
विशेष बल देते हुए, सभी स्तरों पर संधारणीय विकास नीवतयों, वनयोजन तथा कायवक्रम वनमावण के
साथ आपदा जोवखम संबधी उपायों का अवधक प्रभािकारी समेकन”
o आपदा प्रबंधन अवधवनयम, 2005 के अवधवनयमन तथा आपदा प्रबंधन योजना, 2016 के
वनमावण के बाद, ितवमान में सरकार का ध्यान उनके अंतगवत क्रकये गए विवभन्न प्रािधानों के
कायावन्ियन पर है।
o सभी सरकारी कायवक्रम “कोई क्षवत न पहुंचाएं (do no harm)” के वसिांत को ध्यान में
रखते हुए वडजाइन क्रकये जा रहे हैं।
(ii) लक्ष्य 2: “सामुदावयक स्तर पर विशेष ध्यान देते हुए सभी स्तरों पर ऐसी संस्थाओं, कायवप्रणावलयों
और क्षमताओं का विकास तथा उन्हें सशक्त क्रकया जाना जो संकटों के प्रवत प्रत्यास्थता विकवसत करने
में व्यिवस्थत रूप से योगदान कर सकें ”
o राज्य आपदा प्रबंधन प्रावधकरणों (SDMA’s) तथा वजला आपदा प्रबंधन प्रावधकरणों
(DDMA’s) को सुदढ़ृ बनाने हेतु उपयुक्त रणनीवतयां स्िीकृ त की गयी हैं।
o संपूणव राष्ट्र के वलए एक व्यापक मानि संसाधन विकास कायवक्रम तैयार क्रकया जा रहा है।
o वसविल सोसाइटी के साथ विवभन्न साझेदाररयों को सशक्त बनाया जा रहा है।
(iii) लक्ष्य 3: "प्रभावित समुदायों के पुनर्ननमावण के वलए आपातकालीन तैयारी, अनुक्रक्रया तथा सामान्य
वस्थवत की बहाली संबध
ं ी कायवक्रमों की अवभकल्पना तथा उनके कायावन्ियन में जोवखम न्यूनीकरण
संबध
ं ी दृवष्टकोण का सुवनयोवजत समािेश।”
o "सरकार द्वारा आपदा पश्चात् पुनर्ननमावण तथा पुनबवहाली गवतविवधयों के वलए “बेहतर
पुनर्ननमावण (Build Back Better)” का वसिांत अमल में लाया जा रहा है।
103 www.visionias.in ©Vision IAS
ह्योगो फ्रेमिकव के अंतगवत पांच प्राथवमक कायविावहयां
i. यह सुवनवश्चत करना क्रक कायावन्ियन हेतु सशक्त संस्थागत आधार के साथ आपदा जोवखम
न्यूनीकरण एक राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्राथवमकता है।
ii. आपदा संबंधी जोवखमों की पहचान, मूल्यांकन तथा उनकी वनगरानी करना तथा पूिव चेतािनी
प्रणाली को उन्नत बनाना।
iii. ज्ञान, निाचार तथा वशक्षा का उपयोग कर सभी स्तरों पर सुरक्षा तथा प्रत्यास्थता की संस्कृ वत
विकवसत करना।
iv. आपदा से संबि सभी जोवखम कारकों को कम करना।
v. सभी स्तरों पर प्रभािी अनुक्रक्रया हेतु आपदा संबंधी तैयारी को सुदढ़ृ बनाना।
4.1.2. आपदा जोवखम न्यू नीकरण हे तु सें डाई फ्रे मिकव
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: SFDRR)
सेंडाई फ्रेमिकव एक 15 िषीय, स्िैव्छक, गैर-बाध्यकारी समझौता है जो इस बात को मान्यता
प्रदान करता है क्रक आपदा जोवखम न्यूनीकरण में प्राथवमक भूवमका राज्य की होती है क्रकन्तु इस
उत्तरदावयत्ि को स्थानीय शासन, वनजी क्षेत्रक समेत अन्य वहतधारकों के साथ साझा क्रकया जाना
चावहए।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव , 2015-2030 को सेंडाई (वमयागी, जापान) में
माचव, 2015 को आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर आयोवजत तृतीय संयुक्त राष्ट्र विि सम्मेलन में
अपनाया गया था। यह ‘ह्योगो फ्रेमिकव फॉर एक्शन (HFA) 2005-2015: राष्ट्रों तथा समुदायों
की प्रत्यास्थता का वनमावण’ का परिती दस्तािे़ है।
भारत व्यिवस्थत तथा संधारणीय प्रयासों के माध्यम से इस फ्रेमिकव के अंतगवत वनयत क्रकये गये 7
लक्ष्यों को प्राप्त क करने हेतु प्रवतबि है।
सेंडाई फ्रेमिकव के सात िैविक लक्ष्य
i. 2030 तक विि स्तर पर आपदाओं से होने िाली मौतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना और
2005-2015 की तुलना में 2020-2030 के बीच मृत्यु दर (प्रवत 100,000 जनसंख्या) के
िैविक औसत में कमी लाना;
ii. 2030 तक विि स्तर पर आपदाओं से प्रभावित होने िाले लोगों की संख्या में कमी करके
2005-2015 की तुलना में 2020-2030 के बीच प्रभावित लोगों की संख्या (प्रवत 100,000
जनसंख्या में) के िैविक औसत में कमी लाना;
iii. 2030 तक िैविक सकल घरे लू उत्पाद के संबंध में आपदाओं से होने िाली प्रत्यक्ष आर्नथक हावन
का न्यूनीकरण;
iv. महत्िपूणव अिसंरचनाओं को आपदाओं से होने िाली क्षवत तथा आधारभूत सेिाओं (वजसमें
स्िास््य तथा शैक्षवणक सुविधाएं शावमल हैं) में आने िाली बाधाओं को 2030 तक उल्लेखनीय
रूप से कम करना। इसके वलए अिसंरचनाओं तथा आधारभूत सेिाओं की प्रत्यास्थता का
विकास करना भी इसमें सवम्मवलत है।
v. 2020 तक राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपदा जोवखम न्यूनीकरण संबध
ं ी रणनीवतयों िाले राष्ट्रों की
संख्या में उल्लेखनीय िृवि करना;
vi. 2030 तक इस फ्रेमिकव के कायावन्ियन हेतु विकासशील राष्ट्रों द्वारा की जाने िाली राष्ट्रीय
पहलों को पयावप्त क तथा संधारणीय सहायता प्रदान करने के वलए अंतरावष्ट्रीय सहयोग में
उल्लेखनीय िृवि करना;
vii. 2030 तक बहु-संकट पूिव चेतािनी प्रणावलयों (multi-hazard early warning systems)
एिं आपदा जोवखम संबंधी सूचना और मूल्यांकनों की उपलब्धता तथा इन तक लोगों की पहुाँच
में उल्लेखनीय िृवि करना।
104 www.visionias.in ©Vision IAS
सेंडाई फ्रेमिकव के अंतगवत कायविाही हेतु चार प्राथवमकताएं
i. आपदा जोवखम को समझना: आपदा जोवखम प्रबंधन िस्तुतैः सुभेद्यता, क्षमता, लोगों तथा
पररसंपवत्तयों का जोवखम के प्रवत अनािरण, संकट के लक्षण तथा पयाविरण के सभी आयामों में
आपदा संबंधी जोवखमों की समझ पर आधाररत होना चावहए।
ii. आपदा जोवखम को प्रबंवधत करने हेतु आपदा जोवखम शासन का सुदढृ ीकरण: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय
तथा िैविक स्तरों पर रोकथाम, शमन, तैयारी, अनुक्रक्रया, सामान्य वस्थवत की बहाली तथा
पुनिावस के वलए आपदा जोवखम शासन अत्यंत महत्िपूणव है। यह सहयोग तथा साझेदारी को
बढ़ािा देता है।
iii. प्रत्यास्थता हेतु आपदा जोवखम न्यूनीकरण में वनिेश: संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक
उपायों के माध्यम से आपदा जोवखम के वनिारण तथा न्यूनीकरण में वनजी तथा सािवजवनक
वनिेश की आिश्यकता है। यह लोगों, समुदायों, राष्ट्रों तथा उनकी पररसंपवत्तयों और साथ ही
पयाविरण की आर्नथक, सामावजक, स्िास््य संबंधी तथा सांस्कृ वतक प्रत्यास्थता को बढ़ाने के
वलए अवनिायव है।
iv. प्रभािी अनुक्रक्रया हेतु आपदा संबध
ं ी तैयारी को उन्नत बनाना तथा सामान्य वस्थवत की बहाली,
पुनिावस तथा पुनर्ननमावण के सन्दभव में “बेहतर पुनर्ननमावण (build back better)”: विकास
संबंधी उपायों में आपदा जोवखम न्यूनीकरण को एकीकृ त करते हुए सामान्य वस्थवत की बहाली,
पुनिावस तथा पुनर्ननमावण चरण बेहतर पुनर्ननमावण करने हेतु एक महत्िपूणव अिसर होता है।
एवशया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा के प्रवत सामुदावयक प्रत्यास्थता को सक्षम बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय
समथवन को सुगम बनाने के अपने प्रयास के वलए भारत को आपदा जोवखम न्यूनीकरण के चैंवपयन
की उपावध प्रदान की गयी है। सेंडाई समझौते के पश्चात संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण
कायावलय (United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ने भारत
को प्रथम क्षेत्रीय चैंवपयन घोवषत क्रकया है।
सेंडाई फ्रेमिकव डेटा रे डीनेस ररव्यु (The Sendai Framework Data Readiness Review),
UNISDR 2017
आपदा क्षवत के कु छ विवशष्ट क्षेत्रों, अंतरावष्ट्रीय सहयोग के सभी क्षेत्रों तथा पूिव चेतािनी, जोवखम
संबंधी सूचना एिं आपदा जोवखम न्यूनीकरण रणनीवतयों के विवभन्न पहलुओं में आंकड़ों से
संबंवधत गंभीर अंतराल विद्यमान हैं। समीक्षा में इस बात की पुवष्ट की गयी है क्रक जब तक आंकड़ों
की उपलब्धता, गुणित्ता तथा पहुाँच के मध्य विद्यमान अंतराल का समाधान नहीं ढू ंढा जाता, तब
तक सेंडाई फ्रेमिकव के सभी लक्ष्यों तथा प्राथवमकताओं पर कायावन्ियन की सटीक, समयबि तथा
उच्च गुणित्तायुक्त ररपोर्टटग एिं वनगरानी करने की देशों की क्षमता गंभीर रूप से अप्रभािी रहेगी।
संधारणीय विकास हेतु आपदा-संबध
ं ी आंकड़ों के वलए एक िैविक साझेदारी से सरकारों,
अंतरावष्ट्रीय संस्थाओं, वनजी क्षेत्रक, वसविल सोसाइटी समूहों तथा सांवख्यकी एिं आाँकड़ों से
संबंवधत वनकायों को एक साथ लाया जा सके गा। इससे राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय स्तर पर आपदा
संबंधी जोवखम न्यूनीकरण से जुड़े प्रयासों के समथवन में ितवमान तथा भािी आंकड़ों को इष्टतम
बनाने तथा उनके पररचालन हेतु एक सहयोगात्मक, बहु-वहतधारक प्रयास संभि हो सके गा।
2030 एजेंडा फॉर सस्टेनब
े ल डेिलपमेंट: 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनब
े ल डेिलपमेंट में, 17
संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 10 में आपदा जोवखम से जुड़े विवशष्ट लक्ष्य वनवहत हैं।
इससे ‘2030 एजेंडा फॉर सस्टेनब
े ल डेिलपमेंट’ को अमल में लाने में आपदा जोवखम न्यूनीकरण
की भूवमका भली-भांवत स्थावपत होती है।
CoP 21 के दौरान पेररस समझौता: 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलिायु पररितवन फ्रेमिकव कन्िेंशन
(United Nations Framework Convention on Climate Change) के अंतगवत आयोवजत
21िीं कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पाटी़ (CoP) में अंगीकृ त पेररस समझौते में, सदस्य राष्ट्रों ने िैविक तापमान
में औसत िृवि पूि-व औद्योवगक स्तर से 2oC के नीचे रखने की प्रवतबिता दोहराई थी। साथ ही
105 www.visionias.in ©Vision IAS
सदस्य राष्ट्रों ने “जलिायु पररितवन के जोवखमों तथा प्रभािों को उल्लेखनीय रूप से कम करने” के
लक्ष्य के साथ, तापमान में होने िाली इस िृवि को 1.5oC तक सीवमत रखने हेतु प्रयास करने पर
भी सहमवत जताई थी।
4.2. अं त राव ष्ट्रीय एजें वसयों के साथ साझे दाररयां
(Partnerships with International Agencies)
4.2.1. सं यु क्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यू नीकरण कायाव ल य
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction)
संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण कायावलय (UNISDR), आपदा न्यूनीकरण संबंधी गवतविवधयों
में सवम्मवलत सभी वहतधारकों के बीच समन्िय हेतु एक कें द्र सबदु के रूप में कायव करता है। भारत
सरकार ने आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु निम्बर, 2016 में हुए सातिें मंवत्रस्तरीय सम्मेलन में 10
लाख अमेररकी डॉलर का अंशदान क्रकया तथा आपदा जोवखम न्यूनीकरण (DRR) के क्षेत्र में एवशया-
प्रशांत क्षेत्र में क्षमता वनमावण को बढ़ािा देने हेतु एक सहयोग िक्तव्य पर भी हस्ताक्षर क्रकए।
UNISDR ने अपने लक्ष्यों की प्रावप्त क हेतु वनम्नवलवखत तंत्रों/साधनों की स्थापना की है:
आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर विि सम्मेलन (The World Conference on Disaster Risk
Reduction: WCDRR)
यह संधारणीय विकास के पररप्रेक्ष्य में आपदा जोवखम न्यूनीकरण तथा जलिायु संबंधी जोवखम के
प्रबंधन को लवक्षत करने िाली संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला है। ये सम्मेलन सरकारी
अवधकाररयों तथा अन्य वहतधारकों को एक मंच पर लाते हैं ताक्रक िे आपदा तथा जलिायु संबध ं ी
जोवखमों का प्रबंधन करके विकास की संधारणीयता को सुदढ़ृ ता प्रदान करने के विषय पर विचार-
विमशव कर सकें । इन सम्मेलनों की मे़बानी जापान के द्वारा 1994 में योकोहामा में, 2005 में
कोबे में तथा 2015 में सेंडाई में की गई।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु िैविक मंच (Global Platform for Disaster Risk
Reduction: GPDRR)
यह आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर बल देने हेतु प्रमुख िैविक मंच के रूप में कायव करता है। यह
आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव (SFDRR) के कायावन्ियन में हुई प्रगवत का
मूल्यांकन करता है। इसकी बैठक िषव में दो बार होती है तथा भारतीय वशष्टमंडल ने इसमें 2017
में कानकु न (मेवक्सको) में भाग वलया। इस सम्मेलन के दौरान संग्र हालयों पर NDMA क्रदशा-
वनदेश भी ़ारी क्रकए गए।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु एवशयाई मंवत्रस्तरीय सम्मेलन (Asian Ministerial
Conference for Disaster Risk Reduction: AMCDRR)
AMCDRR की संकल्पना राष्ट्रों द्वारा आपदा जोवखम न्यूनीकरण की क्रदशा में की गई प्रगवत की
वनगरानी तथा उसे एवशया-प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय मंच पर साझा करने हेतु की गयी थी। यह
आपदा जोवखम प्रबंधन पर िैविक ढााँचे के अनुरूप, क्षेत्रीय स्तर पर योजना तथा नीवत वनमावण
के वलए 61 राष्ट्रों के आपदा प्रबंधन से संबंवधत मंवत्रयों को विचार-विमशव के वलए एक मंच प्रदान
करता है। इसकी बैठक दो िषव में एक बार होती है। दूसरे तथा सातिें AMCDRR की मे़बानी
भारत सरकार द्वारा क्रमशैः 2007 तथा 2016 में की गयी थी।
106 www.visionias.in ©Vision IAS
4.2.2. मानिीय मामलों के समन्िय हे तु सं यु क्त राष्ट्र कायाव ल य
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: UNOCHA)
मानिीय मामलों के समन्िय हेतु संयुक्त राष्ट्र कायावलय (UNOCHA) का गठन महासभा के द्वारा
क्रदसंबर 1991 में जरटल आपात पररवस्थवतयों तथा प्राकृ वतक आपदाओं के प्रवत संयक्त
ु राष्ट्र संगठनों की
अनुक्रक्रया को सशक्त करने हेतु क्रकया गया था। UNOCHA ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त क करने के वलए
वनम्नवलवखत तंत्रों/साधनों की स्थापना की है:
संयक्त
ु राष्ट्र आपदा मूल्यांकन तथा समन्िय (United Nations Disaster Assessment and
Coordination: UNDAC): यह आपदा प्रबंधन पेशि
े रों का एक सहायताथव दल होता है। इसके
सदस्यों का नामांकन तथा इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कायव सदस्य राष्ट्रों की
सरकारों, UNOCHA, UNDP तथा संयुक्त राष्ट्र की मानितािादी कायों को संचावलत करने
िाली एजेंवसयों जैसे क्रक WFP, UNICEF और WHO द्वारा क्रकया जाता है। भारत सरकार ने
2001 में UNDAC की सदस्यता ग्रहण की थी।
अंतरावष्ट्रीय खोज एिं बचाि सलाहकार समूह (International Search and Rescue
Advisory Group: INSARAG): यह संयुक्त राष्ट्र के अंतगवत 80 से अवधक देशों तथा आपदा
अनुक्रक्रया संगठनों का एक िैविक समूह है। यह समूह शहरी खोज तथा बचाि से जुड़े मुद्दों पर
कायव करता है। INSARAG के सदस्यों में भूकंप-प्रिण देश तथा उसके प्रवत अनुक्रक्रया करने िाले
देश ि संगठन, दोनों ही सवम्मवलत हैं। भारत से भेजे गए प्रवशक्षक INSARAG के द्वारा
आयोवजत छद्म अभ्यासों में भाग लेते हैं। भारत 2005-06 में INSARAG एवशया-प्रशांत क्षेत्रीय
समूह की अध्यक्षता का कायवभार संभाल चुका है।
4.2.3. आपदा न्यू नीकरण तथा सामान्य वस्थवत की बहाली हे तु िै विक सु विधा
(Global Facility for Disaster Reduction and Recovery: GFDRR)
आपदा न्यूनीकरण तथा सामान्य वस्थवत की बहाली हेतु िैविक सुविधा (GFDRR), विि बैंक
समूह के द्वारा प्रबंवधत एक िैविक साझेदारी कायवक्रम है। यह सभी विकासशील राष्ट्रों, विशेष रूप
से सिाववधक सुभेद्य प्राकृ वतक आपदा ‘हॉटस्पॉट’ के रूप में मान्यता प्राप्त क विकासशील राष्ट्रों, की
आपदा रोकथाम, आपातकालीन तैयारी, अनुक्रक्रया तथा सामान्य वस्थवत की बहाली से जुड़ी
क्षमता के संिधवन में सहायता करता है। यह वनम्नवलवखत उद्देश्यों के वलए भी विकासशील राष्ट्रों
की सहायता करता है:
o आपदा जोवखम प्रबंधन तथा जलिायु पररितवन के प्रवत अनुकूलन को विकास की रणनीवतयों तथा
वनिेश कायवक्रमों की मुख्य धारा में लाना, तथा
o क्रकसी आपदा के पश्चात प्रत्यास्थ पुनबवहाली तथा पुनर्ननमावण की गुणित्ता तथा समयबिता में
सुधार करना।
इसे ह्योगो फ्रेमिकव फॉर एक्शन (HFA) 2005-2015 के कायावन्ियन में सहायता के वलए
वसतम्बर, 2006 में प्रारम्भ क्रकया गया था। भारत 2013 में इसका सदस्य बना।
4.2.4. साकव आपदा प्रबं ध न कें द्र
(SAARC Disaster Management Centre: SDMC)
निम्बर, 2005 में ढाका में आयोवजत 13िें SAARC सम्मेलन में राष्ट्रीय आपदाओं के वलए
तैयारी तथा उनके शमन हेतु क्षेत्रीय सहयोग संबंधी मुद्दों पर विचार क्रकया गया। इसमें नई क्रदल्ली
में साकव आपदा प्रबंधन कें द्र (SDMC) की स्थापना हेतु भारत के प्रस्ताि को अनुमोदन प्रदान
क्रकया गया।
107 www.visionias.in ©Vision IAS
4.2.5. दवक्षण एवशया आपदा सं बं धी ज्ञान ने ट िकव
(South Asia Disaster Knowledge Network: SADKN)
SADKN िेब पोटवल इस क्षेत्र के वलए नेटिर्ककग तथा जानकारी साझा करने का एक मंच है। यह
विवभन्न एजेंवसयों को एक साथ लाता है तथा इस क्षेत्र हेतु आपदा आधाररत जानकारी का एक
व्यापक नेटिकव तैयार करता है ताक्रक आपदा जोवखम न्यूनीकरण के क्षेत्र में शोध, सूचना तथा
आंकड़े साझा क्रकये जा सकें । यह नेटिकों का एक नेटिकव है वजसमें एक क्षेत्रीय तथा आठ राष्ट्रीय
पोटवल हैं।
4.2.6. एवशयाई आपदा न्यू नीकरण कें द्र
(Asian Disaster Reduction Center: ADRC)
1997 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताि स्िीकार क्रकया गया था वजसका उद्देश्य 1990 के
दशक को अंतरावष्ट्रीय प्राकृ वतक आपदा न्यूनीकरण दशक घोवषत कर प्राकृ वतक आपदाओं से होने
िाली क्षवत को उल्लेखनीय रूप से कम करना था। आपदा न्यूनीकरण संबंधी सहयोग पर चचाव
करने के वलए 1994-1997 की अिवध में आयोवजत हुई राष्ट्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला के
पश्चात, 1995 में जापान के कोबे में एक मंवत्रस्तरीय सम्मेलन आयोवजत क्रकया गया था। इसमें
एवशया तथा अन्य क्षेत्रों के 28 राष्ट्रों ने भाग वलया था। इस सम्मेलन में कोबे घोषणा (Kobe
declaration) को स्िीकार क्रकया गया था वजसमें एक ऐसी प्रणाली वनर्नमत करने पर विचार
करने संबंधी एक समझौता सवम्मवलत था जो एवशया क्षेत्र के वलए आपदा न्यू नीकरण कें द्र के रूप
में कायव करे । इस प्रकार, एवशया आपदा न्यूनीकरण कें द्र (ADRC) की स्थापना जापान सरकार के
साथ भागीदार राष्ट्रों के द्वारा संपन्न एक समझौते के पश्चात कोबे में 1998 में हुई।
4.2.7. एवशयाई आपदा तै यारी कें द्र
(Asian Disaster Preparedness Center: ADPC)
एवशयाई आपदा तैयारी कें द्र (ADPC) की स्थापना 1986 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। यह
एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीवतक, स्िायत्त ि क्षेत्रीय संस्था है जो आपदा संबंधी तैयारी, आपदा
शमन, जागरूकता वनमावण, सूचना के आदान-प्रदान, सामुदावयक भागीदारी इत्याक्रद को बढ़ािा
देने के वलए एवशया-प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कें द्र के रूप में काम कर रही है। 2004 में, ADPC
एक अंतरावष्ट्रीय संस्था (अंतरसरकारी संगठन) बन गया।
4.2.8. आवसयान क्षे त्रीय मं च
(ASEAN Regional Forum: ARF)
आवसयान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना 1994 में हुई। भारत सवहत 25 देश इसके सदस्य हैं।
भारत 1996 में इसके सदस्य के रूप में सवम्मवलत हुआ था। यह एवशया में सुरक्षा िाताव का प्रमुख
मंच है तथा इस क्षेत्र के सुरक्षा के ताने-बाने को सशक्त बनाने िाले विवभन्न वद्वपक्षीय गठबंधनों एिं
िातावओं को सहयोग प्रदान करता है। ARF के गठन का आधार आवसयान से प्राप्त क यह अनुभि है
क्रक िाताव प्रक्रक्रया से राजनीवतक संबंधों में गुणित्तापूणव सुधार आ सकता है। यह सदस्यों को
तात्कावलक क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चचाव हेतु तथा क्षेत्र में सुरक्षा एिं शावन्त को बढ़ािा देने
के वलए सहयोगात्मक उपायों के विकास हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है।
सभी ASEAN सदस्य स्ितैः ही ARF के सदस्य भी हैं। भारत ARF की बैठकों तथा आपदा राहत
अभ्यासों में सक्रक्रय भागीदारी कर रहा है।
108 www.visionias.in ©Vision IAS
4.3. भारत की ने तृ त्िकारी पहलें
(India's Leadership Initiatives)
4.3.1. आपदा प्रत्यास्थ अिसं र चना पर प्रथम अं त राव ष्ट्रीय कायव शाला , 2018
(First International Workshop on Disaster Resilient Infrastructure, 2018)
माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोवखम न्यूनीकरण से संबंवधत 10 सूत्रीय एजेंडे के प्रथम सबदु के
अनुसरण में, UNISDR के सहयोग से NDMA ने नई क्रदल्ली में 15-16 जनिरी, 2018 को
आपदा प्रत्यास्थ अिसंरचना पर एक अंतरावष्ट्रीय कायवशाला (International Workshop on
Disaster Resilient Infrastructure: IWDRI) का आयोजन क्रकया। यह इस तरह की प्रथम
कायवशाला थी।
इस कायवशाला में जोवखम प्रत्यास्थ अिसंरचना की भूवमका पर बल क्रदया गया। इसमें प्रत्यास्थ
अिसंरचना संबंधी सिोत्तम िैविक प्रणावलयों की पहचान की गई। इसके साथ-साथ ितवमान
प्रणावलयों के समक्ष उपवस्थत मुख्य चुनौवतयों और अंतरालों तथा उनसे वनपटने के उपायों पर भी
विचार क्रकया गया। इसके अवतररक्त, आपदा प्रत्यास्थ अिसंरचना पर वहतधारकों के मध्य सहयोग
के संभावित क्षेत्रों पर भी विचार क्रकया गया।
4.3.2. वबम्सटे क राष्ट्रों के वलए प्रथम सं यु क्त आपदा प्रबं ध न अभ्यास, 2017
(BIMSTEC DMEx-2017)
[First Joint Disaster Management Exercise for BIMSTEC Countries (BIMSTEC
DMEx-2017)]
भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अक्टूबर 2017 में ‘बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और
आर्नथक सहयोग के वलए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) या वबम्सटेक’ देशों हेतु
प्रथम िार्नषक आपदा प्रबंधन अभ्यास (BIMSTEC DMEx-2017) की मे़बानी की। सभी सात
BIMSTEC देशों से आए लगभग 200 आपदा पेशेिरों ने पहली बार आपदा प्रबंधन से सम्बंवधत
विचार विमशव सत्रों तथा फील्ड अभ्यासों में वहस्सा वलया।
4.3.3. आपदा जोवखम न्यू नीकरण पर एवशयाई मं वत्रस्तरीय सम्मे ल न, 2016
(Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR), 2016)
AMCDRR की स्थापना िषव 2005 में की गयी थी। यह एक वद्विार्नषक सम्मेलन है। इसका
आयोजन विवभन्न एवशयाई राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण कायावलय
(UNISDR) के द्वारा संयुक्त रूप से क्रकया जाता है। निम्बर, 2016 में आयोवजत आपदा जोवखम
न्यूनीकरण हेतु एवशयाई मंवत्रस्तरीय सम्मेलन (AMCDRR) में ‘नई क्रदल्ली घोषणा-पत्र (New
Delhi Declaration)’ तथा ‘सेंडाई फ्रेमिकव के कायावन्ियन हेतु एवशयाई क्षेत्रीय योजना (Asian
Regional Plan for Implementation of the Sendai Framework)’ को स्िीकार करने
की घोषणा की गयी। यह आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव के अमल में आने के
पश्चात आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु प्रथम एवशयाई मंवत्रस्तरीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में
सुनामी के संबंध में जागरुकता के प्रसार के उद्देश्य से प्रथम विि सुनामी जागरुकता क्रदिस भी
मनाया गया।
AMCDRR 2016 की थीम “सामुदावयक प्रत्यास्थता के वलए जोवखम संिेदी विकास (Risk
Sensitive Development for Community Resilience)” रखी गई थी। सम्मेलन की
समावप्त क वनम्नवलवखत वनष्टकषव के साथ हुई:
109 www.visionias.in ©Vision IAS
o समुदायों, राष्ट्रों तथा एवशयाई क्षेत्रों की प्रत्यास्थता के सुदढृ ीकरण तथा आपदा जोवखम न्यूनीकरण
के प्रवत सरकार तथा अन्य वहतधारकों की प्रवतबिता की पुनैः पुवष्ट करते हुए नई क्रदल्ली घोषणा-
पत्र जारी क्रकया गया। इसमें आपदा जोवखम न्यूनीकरण के प्रवत जन-के वन्द्रत तथा समग्र समाज
आधाररत दृवष्टकोण के प्रवत प्रवतबिता दशावयी गयी।
o आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव के कायावन्ियन हेतु एवशयाई क्षेत्रीय योजना को
अंगीकृ त क्रकया गया। इसमें सेंडाई फ्रेमिकव पर 15 िषव की अिवध के वलए सहयोग संबंधी
दीघाविवधक रोडमैप पर सहमवत बनी तथा विवशष्ट ि व्यिहायव गवतविवधयों के साथ आपदा
जोवखम न्यूनीकरण संबंधी कायों को आगे बढ़ाने हेतु एक वद्व-िषीय कायव योजना भी तय की गयी।
4.3.4. UNISDR के साथ सहयोग (2016)
(Cooperation with UNISDR, 2016)
भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोवखम न्यूनीकरण कायावलय (UNISDR) के बीच
निम्बर, 2016 में एक सहयोग िक्तव्य पर हस्ताक्षर क्रकए गए। इस िक्तव्य में आपदा जोवखम
न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमिकव (SFDRR) के कायावन्ियन तथा उसकी प्रभािी वनगरानी हेतु
भारत तथा UNISDR के बीच सहयोग के वबन्दुओं तथा मागवदशवक वसिांतों को प्रस्तुत क्रकया गया
था।
भारत ने जोवखम प्रत्यास्थ विकास सुवनवश्चत करने हेतु एवशयाई देशों की क्षमता को सुदढ़ृ बनाने
के वलए UNISDR के साथ भागीदारी की है। यह गंभीर क्षेत्रीय चुनौवतयों से वनपटने हेतु अपने
ज्ञान तथा अनुभिों को भी साझा करे गा। इस सहयोग का उद्देश्य एवशयाई राष्ट्रों के प्रवशक्षण तथा
क्षमता वनमावण के माध्यम से सेंडाई फ्रेमिकव के प्रभािी कायावन्ियन तथा वनगरानी को सुवनवश्चत
करना है।
4.3.5. आपदा प्रबं ध न पर विक्स मं वत्रयों की बै ठ क, 2016
(Meeting of BRICS Ministers for Disaster Management, 2016)
आपदा प्रबंधन पर BRICS मंवत्रयों की बैठक राजस्थान के उदयपुर में अगस्त, 2016 में
आयोवजत की गयी थी। उदयपुर घोषणा में BRICS राष्ट्रों के बीच वनयवमत िाताव तथा सहयोग के
वलए आपदा जोवखम प्रबंधन पर एक संयक्त ु कायव बल की स्थापना पर सहमवत जताई गयी थी।
संयुक्त कायव बल द्वारा उन कारव िाइयों को आरम्भ क्रकये जाने की सम्भािना है वजन पर उदयपुर
सम्मेलन में BRICS राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षररत संयक्त
ु कायव योजना के कायावन्ियन के वलए रोडमैप
में सहमवत जतायी गयी है।
4.3.6. साकव दे शों के साथ प्रथम आपदा प्रबं ध न अभ्यास, 2015
(First Disaster Management Exercise with SAARC Countries, 2015)
भारत सरकार ने 2015 में प्रथम दवक्षण एवशयाई िार्नषक आपदा प्रबंधन अभ्यास (South
Asian Annual Disaster Management Exercise: SAADMex) का आयोजन क्रकया था।
सभी साकव सदस्य देशों ने भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster
Response Force: NDRF) द्वारा संचावलत प्रथम संयुक्त अभ्यास में भागीदारी की थी। इसमें
अंतरसरकारी समन्िय का परीक्षण करने तथा आपदा अनुक्रक्रया पर साकव सदस्य देशों के मध्य
क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से प्रयासों के समन्िय के वलए सह-क्रक्रयाशीलता
उत्पन्न करने पर फोकस क्रकया गया था। इसके पश्चात सिोत्तम कायव-प्रणावलयों की साझेदारी पर
साकव क्षेत्रीय कायवशाला (SAARC Regional Workshop on sharing best practices) का
आयोजन क्रकया गया था।
110 www.visionias.in ©Vision IAS
4.3.7. भारत-प्रशां त द्वीप समू ह सतत विकास सम्मे ल न
(India-Pacific Sustainable Development Conference)
भारत ने 25-26 मई, 2017 को क्रफजी के सुिा में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सतत विकास सम्मेलन
का आयोजन क्रकया। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ आपदा जोवखम न्यूनीकरण
गवतविवधयों में सहयोग के माध्यम से उनकी प्रत्यास्थता को सुदढ़ृ बनाना था।
4.3.8. अन्य सु वनयोवजत पहलें
(Other Planned Initiatives)
आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर जापान-भारत कायवशाला, 2018 (Japan-Indo Workshop
on Disaster Risk Reduction), 2018
आपदा जोवखम न्यूनीकरण पर जापान तथा भारत के मध्य समझौते के एक भाग के रूप में, 19-
20 माचव, 2018 को DRR पर एक कायवशाला का आयोजन क्रकया गया।
2019 में SCO सदस्य राष्ट्रों का संयक्त
ु शहरी भूकंप खोज तथा बचाि अभ्यास (Joint Urban
Earthquake Search and Rescue exercise of SCO member states in 2019)
भारत 2017 में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)
का सदस्य बना। भारत के अवतररक्त, SCO के सात अन्य सदस्य राष्ट्र (चीन, क़ािस्तान,
क्रकर्नग़स्तान, पाक्रकस्तान, रूस, तावजक्रकस्तान तथा उज़्बेक्रकस्तान) तथा चार पयविेक्षक राष्ट्र
(अफगावनस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोवलया) हैं।
अगस्त, 2017 में क्रकर्नग़स्तान में, SCO के सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के प्रमुखों की 9िीं बैठक का
आयोजन हुआ। इस दौरान भारत सरकार ने यह घोषणा की क्रक िह संयुक्त तैयारी को बेहतर
बनाने के वलए 2019 में SCO सदस्य राष्ट्रों के एक संयुक्त शहरी भूकंप खोज तथा बचाि अभ्यास
का आयोजन करे गी और साथ ही 2019 में ही SCO सदस्यों के आपदा रोकथाम से संबंवधत
विभागाध्यक्षों की अगली बैठक की मे़बानी भी करे गी।
4.4. विवभन्न राष्ट्रों के साथ वद्वपक्षीय समझौते
(Bilateral Agreements with Countries)
4.4.1. जापान
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु 2017 में भारत तथा जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन
(MoC) पर हस्ताक्षर क्रकये गये। इसके अनुसार दोनों पक्ष आपदा जोवखम न्यूनीकरण हेतु
जानकारी का आदान-प्रदान ि सहयोग करें गे। इसके साथ ही िे रोकथाम, अनुक्रक्रया एिं "बेहतर
पुनर्ननमावण" के वलए पुनबवहाली ि पुनर्ननमावण से संबंवधत नीवतयों के विषय में भी सहयोग और
जानकारी साझा करें गे। दोनों देश सुनामी जोवखम न्यूनीकरण हेतु सूचना, अनुभिों से वमली सीखों
एिं नीवतयों को साझा करने के वलए भी सहयोग करें गे। इसमें सुनामी जागरूकता, पूि-व चेतािनी
111 www.visionias.in ©Vision IAS
तथा तैयारी से जुड़ी जानकारी भी शावमल होगी। हाल ही में, माचव 2018 में भूकंप सुरक्षा पर
विशेष जोर देते हुए आपदा जोवखम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग के वलए ‘आपदा जोवखम
न्यूनीकरण पर प्रथम भारत-जापान कायवशाला’ का भी आयोजन क्रकया गया था।
4.4.2. शं घाई सहयोग सं ग ठन (SCO) दे श
(Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Countries)
SCO के सदस्य देशों के द्वारा आपदा राहत में परस्पर सहयोग के वलए एक समझौता क्रकया गया
है। यह समझौता आपदा अनुक्रक्रया में SCO देशों के मध्य परस्पर सहायता का आह्िान करता है।
4.4.3. जमव नी
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के वलए भारत तथा जमवनी के बीच एक संयुक्त घोषणा पर
अक्टू बर 2015 में हस्ताक्षर क्रकए गए थे। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचनाओं एिं
अन्य िैज्ञावनक/तकनीकी विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान करना है। इसका उद्देश्य नागररक सुरक्षा,
शहरी खोज ि बचाि, अविशमन सेिाओं तथा वचक्रकत्सा के क्षेत्र में प्रथम अनुक्रक्रयाकतावओं का
प्रवशक्षण एिं उनकी क्षमता वनमावण करना भी है।
4.4.4. इं डोने वशया
2013 में भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रावधकरण (NDMA) तथा इं डोनेवशया की आपदा
प्रबंधन की राष्ट्रीय एजेंसी के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग विकवसत करने के उद्देश्य से
एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर क्रकये गये थे। दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में
आपदा प्रबंधन, प्रवशक्षण तथा क्षमता वनमावण के क्षेत्र में जानकारी का आदान-प्रदान; आपदा
प्रबंधन के वलए विशेषज्ञों तथा मानि संसाधनों का आदान-प्रदान आक्रद सवम्मवलत हैं।
4.4.5. साकव दे श (SAARC Countries)
निंबर, 2011 में मालदीि के अद्दू वसटी (Addu City) में आयोवजत 17िें साकव वशखर सम्मेलन
में ‘प्राकृ वतक आपदाओं पर तीव्र अनुक्रक्रया हेतु साकव समझौते’ (SAARC Agreement on
Rapid Response to Natural Disasters) पर मंत्रालयी स्तर पर हस्ताक्षर क्रकए गए थे।
समझौते का उद्देश्य "आपदाओं पर तीव्र अनुक्रक्रया हेतु प्रभािी क्षेत्रीय तंत्र प्रदान कर आपदा से होने
िाली जीिन की हावन तथा सामावजक, आर्नथक ि पयाविरणीय पररसम्पवत्तयों की क्षवत में कमी
लाना, और समेक्रकत राष्ट्रीय प्रयासों तथा गहन क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आपदा आपातकालीन
वस्थवतयों में संयुक्त अनुक्रक्रया करना है।"
4.4.6. रूस
क्रदसंबर 2010 में नई क्रदल्ली में आयोवजत 11िें भारत-रूस िार्नषक वशखर सम्मेलन के दौरान
भारत सरकार तथा रूसी संघ की सरकार ने आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के वलए
समझौते पर हस्ताक्षर क्रकए थे। इसमें शावमल सहयोग के मुख्य क्षेत्र एिं प्रकार हैं: सूचना का
आदान-प्रदान, पूि-व चेतािनी, जोवखमों का मूल्यांकन, संयुक्त सम्मेलन, सेवमनार, कायवशालाएं,
विशेषज्ञों का प्रवशक्षण, तकनीकी सुविधाएं एिं उपकरण प्रदान करने में परस्पर सहायता आक्रद।
112 www.visionias.in ©Vision IAS
आपात वस्थवतयों के पररणामों की रोकथाम एिं उन्मूलन में सहयोग के वलए भारत-रूस संयक्त
ु
आयोग (the Indo-Russian Joint Commission for cooperation in Prevention and
Elimination of Consequences of Emergencies) की पहली बैठक 22 माचव, 2016 को
नई क्रदल्ली में आयोवजत की गई थी। इस बैठक के दौरान 2016-2017 के वलए आपात वस्थवतयों
की रोकथाम एिं उन्मूलन के क्षेत्र में सहयोग के वलए संयुक्त कायावन्ियन योजना पर हस्ताक्षर क्रकये
गये।
4.4.7. वस्िट्ज़रलैं ड
भारत एिं वस्िट्ज़रलैंड ने प्राकृ वतक आपदाओं से वनपटने के वलए रोकथाम तैयारी तथा आपदाओं
या प्रमुख आपात वस्थवतयों के दौरान सहायता के वलए सहयोग में िृवि हेतु एक समझौते पर
हस्ताक्षर क्रकये हैं।
113 www.visionias.in ©Vision IAS
अध्याय 5
5. विविध विषय
(Miscellaneous Topics)
5.1. आपदा बीमा
(Disaster Insurance)
राहत एिं पुनिावस पैकेज पर अत्यवधक वनभवरता एक ऐसी व्यिस्था वनर्नमत करती है जहां जोवखम
न्यूनीकरण के उपायों को अपनाने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। बीमा, आपदा-प्रिण क्षेत्रों में
संभावित रूप से महत्िपूणव शमन उपाय है क्योंक्रक यह अिसंरचना ि सजगता में गुणित्ता तथा
सुरक्षा ि रोकथाम की संस्कृ वत उत्पन्न करता है। आपदा बीमा प्रायैः ‘वजतना अवधक जोवखम,
उतना अवधक प्रीवमयम‘ के वसिांत के आधार पर काम करता है। इस प्रकार, यह सुभेद्य क्षेत्रों के
प्रवत जागरूकता उत्पन्न करता है तथा लोगों को अपेक्षाकृ त सुरवक्षत क्षेत्रों में बसने के वलए प्रेररत
करता है।
ग्रामीण विकास के वलए सूक्ष्म-ऋण की सफलता के बाद सूक्ष्म-बीमा, प्रत्यावशत जोवखम प्रबंधन के
एक उपकरण के रूप में उभरने लगा है। िास्ति में, सूक्ष्म-ऋण एिं सूक्ष्म-बीमा एक-दूसरे का
समथवन करते हैं। बीमा उपकरणों को नीवतगत उपायों तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से
आकषवक बनाया जाना चावहए।
5.2. समु दाय-आधाररत आपदा प्रबं ध न
(Community Based Disaster Management)
आपदा प्रबंधन के िल तभी प्रभािी हो सकता है जब इसमें समुदायों की भागीदारी हो। चूंक्रक एक
समुदाय परं परागत रूप से विकवसत ज्ञान तथा कौशल का भंडार होता है, इसवलए समुदाय को
आपदा प्रबंधन रणनीवत में एकीकृ त करने की आिश्यकता है। समुदाय अनुक्रक्रयाकतावओं की प्रथम
पंवक्त है, अतैः, आपदा के दौरान एक समवन्ित अनुक्रक्रया सुवनवश्चत करने के वलए समुदाय को
आपदा प्रबंधन के संबंध में वशवक्षत करना, कौशल प्रदान करना एिं विवशष्ट भूवमकाएाँ प्रदान करना
आिश्यक है। यह सब वनम्नवलवखत के माध्यम से प्राप्त क क्रकया जा सकता हैैः
o समुदाय के वलए स्थान विवशष्ट प्रवशक्षण कायवक्रमैः चूाँक्रक उन लोगों की संख्या काफी अवधक है
वजन्हें प्रवशक्षण प्रदान करना है, इसवलए प्रवशक्षण प्रदान करने के वलए कै स्के सडग दृवष्टकोण को
अपनाया जाना चावहए। अतैः, इस वजम्मेदारी को स्थानीय स्तर पर जैसे क्रक ग्राम पंचायतों को
सौंपा जा सकता है।
o आपदा प्रबंधन संबध ं ी वशक्षा को वशक्षण की औपचाररक तथा अनौपचाररक प्रणाली के तहत
एकीकृ त क्रकए जाने की आिश्यकता है।
o महत्िपूणव क्षेत्रों के नेतत्ृ िकतावओं तथा कर्नमयों को आपदा प्रबंधन प्रवशक्षण प्रदान क्रकया जाना
चावहए।
o समुदाय की तैयारी को उन्नत बनाने के वलए समस्त आपदा-पूिव वनयोजन को सवम्मवलत करते हुए,
जोवखम न्यूनीकरण हेतु एक उवचत सुरक्षा योजना का वनमावण क्रकया जाना चावहए।
o क्षवत मूल्यांकन एिं राहत पैकेज के वितरण की संपण
ू व प्रक्रक्रया को स्थानीय समुदाय के नेतृत्ि तथा
स्ियं सहायता समूहों (SHGs) की सक्रक्रय भागीदारी के द्वारा बहुत ही आसानी से संचावलत
क्रकया जा सकता है।
114 www.visionias.in ©Vision IAS
आपदा पीवड़तों के सामावजक-मनोिैज्ञावनक पुनिावस सवहत पुनबवहाली प्रक्रक्रया में भी समुदाय एक
महत्िपूणव भूवमका वनभाता है। वपछले कु छ समय के दौरान, यह अनुभि क्रकया गया है क्रक डू बने,
आग लगने आक्रद की वछटपुट घटनाओं के मामलों में भी समुदाय का क्षमता वनमावण बहुत उपयोगी
रहा है। आपदा शमन के विषय में जागरूकता वनमावण एिं आपदा प्रबंधन सवमवतयों की नजदीकी
वनगरानी में समय-समय पर आयोवजत छद्म अभ्यासों (mock drills) से, समुदाय क्रकसी भी
आपात वस्थवत में एक सुगरठत इकाई के रूप में कायव करने में सक्षम हो सके गा।
चेन्नई में हाल ही में बाढ़ के दौरान स्थानीय लोगों ने मागों का पता लगाने में सेना तथा अन्य बलों
की सहायता की थी, क्योंक्रक सड़कें पूरी भरी हुई थीं तथा सेना स्थानीय वनिावसयों की भांवत क्षेत्रों
से पररवचत नहीं थी।
5.3. आपदा प्रबन्धन में मीवडया की भू वमका
(Role of the Media in Disaster Management)
मीवडया की भूवमका बहुत ही महत्त्िपूणव है। उन्हें प्राय: सही जानकारी नहीं दी जाती है, वजसके
पररणामस्िरूप गलत जानकारी का प्रसार होता है और भय के माहौल में िृवि होती है।
आपदा-पूिव
o मीवडया, आपदा जोवखम के मुद्दों को प्राथवमकता देने के वलए सरकार को प्रभावित कर
सकता है। उदाहरण के वलए, यह क्रकसी विशेष क्षेत्र में आपदा तैयाररयों पर अत्यवधक और
अकु शल व्यय का पदावफाश कर सकता है।
o यह पूिव चेतािनी प्रणावलयों के वनमावण के संबंध में आपदा शमन विशेषज्ञों की सहायता कर
सकता है। देश भर में टी.िी., रे वडयो, के बल सेिाओं आक्रद के माध्यम से प्रसाररत आपात
अलटव अत्यवधक प्रभािी हो सकते हैं।
o समुदाय को आपदा के लक्षणों की पहचान करने और उन लक्षणों के क्रदखने पर तुरंत ररपोटव
करने के वलए वशवक्षत करने में मीवडया की महत्िपूणव भूवमका हो सकती है।
o यह लोगों को उनके खतरनाक कायों और क्रक्रयाकलापों के पररणामों के बारे में सचेत करके
जोवखम न्यूनीकरण में समुदाय के सहयोग को सुवनवश्चत कर सकता है।
आपदा के दौरान
आपदा के दौरान, लोगों का मनोबल बनाये रखना, उनमें आत्मवििास बनाये रखना और भय के
माहौल को फै लने से रोकना अत्यंत महत्िपूणव है। इन वस्थवतयों को सुवनवश्चत करने में मीवडया कई
प्रकार से सहायता कर सकता है:
o वनरं तर और त्यात्मक किरे ज, विशेष रूप से स्थानीय मीवडया द्वारा, अवधकाररयों और
स्िैव्छक संगठनों और स्ियं-सेिकों को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और राहत पहुाँचाने में
सहायक हो सकता है।
o प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित होने िाले लोगों को ‘क्या करना है’ और ‘क्या नहीं
करना है’ के विषय में सचेत करना, अफिाहों को वनष्टफल करना और भय के माहौल और भ्रम
के प्रसार को रोकना।
o अभािग्रस्त स्थलों की पहचान करना और उन पर ध्यान के वन्द्रत करना, बावधत मागों और
नष्ट हुई विद्युत लाईनों का वििरण प्रदान करना।
o जनता और सम्बवन्धत प्रावधकाररयों तक समय से जानकारी संप्रवे षत करना ताक्रक िे जान-
माल की क्षवत को कम करने के वलए आिश्यक कदम उठाने में समथव हो सकें ।
o यह बाहरी विि को इस बात की जानकारी देता है क्रक प्रभावित समुदाय क्रकन समस्याओं का
सामना कर रहा है।
115 www.visionias.in ©Vision IAS
आपदा पश्चात्
o महत्त्िपूणव संसाधनों के संग्रह और आिश्यक जनबल जुटाने हेतु लोगों से सहायता के वलए
आगे आने की अपील करना।
o प्रभावित लोगों को अपने वप्रयजनों से सम्पकव स्थावपत करने में सहायता करना।
o ऐसी वस्थवतयों का लाभ उठाने का प्रयास करने िाले असामावजक तत्िों पर नजर रखना।
o आपदाओं की घटनाओं पर विदेशी मीवडया में अवहतकारी, अवतरं वजत और नकारात्मक
ररपोर्टटग और प्रचार का सामना करने में योगदान देना।
5.3.1. मीवडया के नकारात्मक प्रभाि
(Negative Effects of Media)
मीवडया आपदा के कु छ तत्िों को अवतरं वजत कर सकता है और अनािश्यक भय का माहौल उत्पन्न
कर सकता है।
आपदा के दौरान और उसके पश्चात मानि व्यिहार का गलत वचत्रण एक बहुत ही नाटकीय और
रोमांचक वचत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो के िल आंवशक रूप से ही सत्य होता है।
प्रभािशाली राजनेता व्यवक्तगत और राजनैवतक लाभ के वलए मीवडया का उपयोग अपने वहतों के
अनुरूप कर सकते हैं।
भयानक विनाश की के िल कु छ छोटी घटनाओं को किर करके सनसनीखेज प्रयोजनों के वलए
उनकी पक्षपात पूणव प्रस्तुवत क्रकसी घटना की गलत ि भ्रामक ररपोर्टटग का कारण बनती है।
अत्यवधक चर्नचत कायवक्रमों को किर करने के वलए मीवडया प्रवतवनवधयों का एकवत्रत होना
प्रभावित क्षेत्र में जबदवस्त भीड़-भाड़ की वस्थवत उत्पन्न कर सकता है।
संिेदनशील कायविावहयों का सीधा प्रसारण सैन्य बलों की आतंक-रोधी रणनीवत को बावधत कर
सकता है, जैसा 26/11 के मुम्बई हमले में देखा गया था।
हमारे मीवडया द्वारा िास्तविक वस्थवत की त्िररत प्रस्तुवत और उनके द्वारा की गई गलतबयानी में
सुधार, विदेशों में वनर्नमत गलत धारणा को समाप्त क करने में सहायता करे गा, जो अन्यथा प्रशासन,
अथवव्यिस्था और देश की राजनीवत पर प्रवतकू ल प्रभाि डाल सकती है।
5.4. आपदा प्रबन्धन में सोशल मीवडया की भू वमका
(Role of Social Media in Disaster Management)
सोशल मीवडया पारम्पररक मीवडया से इस रूप में वभन्न है क्रक इसके माध्यम से िन-टू -िन (one-
to-one), िन-टू -मेनी (one-to-many) और मैनी-टू -मेनी (many-to-many) संचार संभि है।
यह ररयल-टाइम में या क्रकसी भी समय संचार संभि बनाता है। यह क्रकसी विवशष्ट वडिाइस तक
ही सीवमत नहीं है बवल्क कम्प्यूटर, टेबलेट और स्माटवफोन के माध्यम से भी हो सकता है जो
अपेक्षाकृ त गवतशील और कहीं भी ले जाने में सुविधाजनक हैं। यह प्रवतभावगयों को सोशल
मीवडया नेटिकव पर संचार सामग्री वनर्नमत करने और उन पर रटप्पणी करने का अिसर प्रदान
करता है।
आपदा के दौरान सामान्यतैः सभी पारं पररक संचार माध्यम कायव करना बंद कर देते हैं, जबक्रक
सोशल मीवडया या नेटिकव सेिाएं सक्रक्रय रहती हैं। विद्युत् आपूर्नत बावधत होने से टी.िी. स्टेशनों
और लैंडलाइनों के बंद होने पर तात्कावलक सूचना प्रसार करने की इनकी भूवमका नगडय हो जाती
है। आपातकालीन सेिा एजेंवसयां जनता को आपातकालीन चेतािवनयों के तत्काल और व्यापक
प्रसारण के वलए सोशल मीवडया और SMS का उपयोग कर रही हैं। सोशल मीवडया द्वारा
कायाववन्ित क्रकये जाने िाले महत्िपूणव कायव इस प्रकार हैं:
o आपदा संभावित क्षेत्रों में नागररकों को तैयार करना;
o प्रभावित क्षेत्रों और इ्छु क लोगों, दोनों के वलए ररयल-टाइम जानकारी प्रसाररत करना;
o प्रभावित क्षेत्रों से ररयल-टाइम डेटा प्राप्त क करना;
o तात्कावलक राहत प्रयासों को संगरठत और समवन्ित करना; और
o पुनबवहाली गवतविवधयों को इष्टतम बनाना।
116 www.visionias.in ©Vision IAS
विशाखापत्तनम में आए विनाशकारी हुदहुद चक्रिात के दौरान, PWD के अवधकाररयों ने एक
व्हाट्जसएप ग्रुप बनाया था, वजसने सूचनाएाँ साझा करने के वलए संचार के मुख्य साधन के रूप में
कायव क्रकया था। वजला स्तर पर कोई बैठक या चचाव नहीं की गयी थी क्योंक्रक व्हाट्जसएप ग्रुप ने
आिश्यक संसाधनों की पहचान और उन तक पहुाँचने में सहायता प्रदान कर दी थी।
ऑनलाइन सोशल नेटिर्ककग सेिाएं और फे सबुक, वट्जिटर, गूगल प्लस आक्रद सोशल मीवडया
प्लेटफॉमव, प्राकृ वतक आपदाओं के दौरान वप्रयजनों से सम्पकव स्थावपत करने में सहयोग कर कई
समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हालााँक्रक, आपातकालीन ऑनलाइन नेटिकव के
विकास के संबंध में प्रौद्योवगकीय विफलता, हैकर, स्टॉकर, िायरस के खतरे जैसी सचताओं को
संबोवधत क्रकया जाना आिश्यक है। इसके अवतररक्त अफिाहों का तेजी से प्रसार भय का माहौल
उत्पन्न कर सकता है। इसवलए, सोशल मीवडया, आपदा प्रबन्धन संचार के ितवमान दृवष्टकोणों से
अवधक प्रभािी नहीं हो सकता और न ही यह ितवमान संचार अिसंरचनाओं को प्रवतस्थावपत कर
सकता है, लेक्रकन यक्रद इसे रणनीवतक रूप से प्रबंवधत क्रकया जाए तो इसका उपयोग ितवमान
व्यिस्था को सुदढ़ृ बनाने के वलए क्रकया जा सकता है।
5.5. भिनों की रे रोक्रफटटग – समाधान इसके लचीले प न में है
(Retrofitting of Buildings- The Key is to Let it Swing)
भारतीय मानक संवहता, 2002 में भूकम्प रोधी वनमावण के वलए मानदंड वनधावररत क्रकये गये हैं।
इसमें भिन के वडजाइन का अध्ययन करना, और गैर-विनाशकारी रे वडयोलॉवजकल परीक्षणों द्वारा
इनकी वनमावण सामग्री का आकलन करना सवम्मवलत है। भूकम्प रोधी भिन बनाने के पीछे मुख्य
विचार इसे लचीला बनाना है, अथावत क्षैवतज कम्पन के वलए इसे कु छ लचीलापन प्रदान करना है।
यह भूकम्प के प्रभाि को वशवथल करने में सहायता करता है और भिन को इसकी ऊजाव को
अिशोवषत करने में सक्षम बनाता है।
भिनों को भूकम्प रोधी बनाने के वलए उनकी नींि को इस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है क्रक
भूकम्प के दौरान भिन का भार अके ले नींि उठा सके , और ऊपरी तल अवधक कम्पन का अनुभि
न करें । इसके वलए नींि और भिन की ऊपरी संरचना के बीच बेयटरग्स का उपयोग क्रकया जाता
है, ठीक उसी प्रकार जैसे पवहयों को बदलने के वलए जैक का उपयोग क्रकया जाता है। वनमावणाधीन
भिनों की नींि में रबड़ सामग्री (जैसे- उपयोग क्रकये जा चुके पुराने टायर) को भी सवम्मवलत
क्रकया जा सकता है। भिनों को भूकम्प रोधी बनाने के वलए वनमावणाधीन भिन की लागत में
लगभग 10% की िृवि होती है और रे रोक्रफटटग के मामले में अनुमावनत रूप से संरचना की कु ल
लागत का लगभग 15-20% व्यय होता है।
ग्रेनेडा में इिान नामक तूफ़ान के गुजरने के पश्चात (वसतम्बर 2004) के िल दो स्कू ल ही खड़े रहे
थे। दोनों स्कू लों की विि बैंक की पहल से रे रोक्रफटटग की गयी थी। इनमें से एक स्कू ल का उपयोग
घटना से विस्थावपत लोगों को आश्रय प्रदान करने के वलए क्रकया गया था।
भारत में, भिन सामग्री और प्रौद्योवगकी संिधवन पररषद (Building Materials &
Technology Promotion Council: BMTPC) ने अत्यािश्यक (लाइफ-लाइन) संरचनाओं की
रे रोक्रफटटग की पररयोजनाएं प्रारम्भ की हैं। पररषद ने क्रदल्ली में MCD स्कू ल भिनों और जम्मू-
कश्मीर में अन्य संरचनाओं की रे रोक्रफटटग की शुरुआत की है।
117 www.visionias.in ©Vision IAS
5.6. जलिायु पररितव न और आपदाएं
(Climate Change and Disasters)
ऐसे कई साक्ष्य हैं क्रक चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने िाली आर्नथक क्षवत में वपछले कु छ
दशकों में पयावप्त क िृवि हुई है। भारत जैसे देश के वलए, जहााँ 70% से अवधक जनसंख्या अपनी
आजीविका के वलए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृ वष पर वनभवर है, चरम मौसमी घटनाओं का
प्रभाि महत्त्िपूणव है।
लोग प्राय: उच्च पाररवस्थवतकीय सुभेद्यता और संसाधन उत्पादकता के अपेक्षाकृ त कम स्तर िाले
क्षेत्रों में रहते हैं और उनका उत्पादक प्राकृ वतक संसाधनों पर सीवमत और असुरवक्षत अवधकार
होता है।
िषवण प्रवतरूप में पररितवन और मानसून में क्रकसी भी प्रकार की अवधकता से बाढ़ आपदाओं और
भूवम वनम्नीकरण में िृवि होती है। भारत की जल आपूर्नत न के िल मानसूनी िषाव पर बवल्क
वहन्दुकुश और वहमालय के ग्लेवशयरों के वपघलने से प्राप्त क जल पर भी वनभवर है। बढ़ते तापमान के
कारण वहम-रे खा पीछे हटती है, इससे ग्रीष्टमकालीन मानसून ऋतु में बाढ़ के जोवखम में िृवि होती
है।
ओवडशा राज्य ने वपछले 100 िषों में से 49 िषों में बाढ़, 30 िषों में सूखा और 11 िषों में
चक्रिात का सामना क्रकया है। एक ही िषव के दौरान सूखे, बाढ़ और चक्रिात की घटना कोई
असामान्य बात नहीं है।
आपदा जोवखम न्यूनीकरण और जलिायु पररितवन शमन एिं अनुकूलन समान लक्ष्यों को साझा
करते हैं, दोनों का उद्देश्य समुदायों की सुभेद्यता को कम करना है और संधारणीय विकास को प्राप्त क
करना है। आपदा जोवखम न्यूनीकरण का बल भूकम्प, भूस्खलन इत्याक्रद भूगभीय संकटों के साथ-
साथ बाढ़, चक्रिात जैसी जल एिं जलिायु से जुड़ी आपदाओं के संबंध में रोकथाम, शमन, तैयारी
और सामान्य वस्थवत की बहाली से है। जलिायु पररितवन अनुकूलन मुख्य रूप से जल एिं जलिायु
से जुड़ी आपदाओं से संबंवधत है और इसका लक्ष्य दीघाविवध में जलिायु में क्रवमक पररितवनों के
प्रवत अनुकूलन के माध्यम से जलिायु पररितवन/पररितवनशीलता से उत्पन्न जोवखम के कारण व्याप्त क
सुभेद्यता को कम करना है।
5.7. वनधव न ता और आपदाएं
(Poverty and Disasters)
वनधवनता और प्राकृ वतक संकटों के प्रवत सुभेद्यता वनकटता से संबि हैं और पारस्पररक रूप से एक-
दूसरे में िृवि करते हैं। आपदाएं करठनाई और परे शानी का स्रोत होती हैं, ये कु छ समूहों को
अस्थायी रूप से वनधवनता की सीमा-रे खा के नीचे धके लने और साथ ही अवधक स्थायी,
दीघवकावलक वनधवनता में योगदान देने िाली भी होती हैं।
वनधवनता और आपदाओं के जोवखम जरटल ढंग से जुड़े हुए और पारस्पररक रूप से एक-दूसरे में
िृवि करने िाले होते हैं। आपदा की वस्थवत में समाज का वनधवन िगव सिाववधक बुरी तरह से
प्रभावित होता है। अपने अवस्तत्ि के वलए पयाविरणीय संसाधनों का दोहन करने की गरीबों की
मजबूरी के कारण, समाज का आपदाओं के प्रवत अनािरण और जोवखम बढ़ जाता है। साथ ही
वनधवनता गरीबों को प्राय: असुरवक्षत भूवम और असुरवक्षत आश्रयस्थलों के रूप में भौवतक रूप से
अवधक सुभेद्य स्थानों पर प्रिास करने और वनिास करने के वलए वििश करती है।
आपदाएं ितवमान में जारी वनधवनता न्यूनीकरण गवतविवधयों को भी बावधत कर सकती हैं और
इनसे संबंवधत वित्तीय संसाधनों को राहत और पुनिावस प्रयासों में उपयोग करने के वलए वििश
कर सकती हैं। वनधवन पररिारों द्वारा जोवखम-टालने के वलए स्िैव्छक रूप से चुने जाने िाले
संभावित आजीविका विकल्पों से उनकी वनधवनता और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के वलए, गरीब
पररिार अवधक पैदािार और अवधक लाभप्रद फसलों के संभावित लाभों को त्यागकर, उनके
स्थान पर उन फसलों को िरीयता दे सकते हैं जो अवधक संकट-प्रवतरोधी हों।
118 www.visionias.in ©Vision IAS
आिास की वनम्न गुणित्ता और प्राय: उनकी खतरनाक अिवस्थवत (उदाहरण के वलए, बाढ़ के
मैदानों, नदी के क्रकनारों या खड़ी ढलानों पर), आधारभूत सेिाओं तक पहुाँच का वनम्न स्तर
(विशेषकर ग्रामीण गरीबों और अनवधकृ त वनिावसयों के वलए); अवनवश्चत स्िावमत्ि अवधकार,
संसाधनों को संधारणीय ढंग से प्रबंवधत करने या संरचनात्मक शमन उपायों में वनिेश करने के
वलए कम होते जा रहे प्रोत्साहन; प्राय: अवधक सुभेद्य आजीविका; और वित्तीय संसाधनों तक
सीवमत पहुंच, आजीविका को विविधता देने और आपदा पश्चात् पुनबवहाली की गरीबों की क्षमता
को बावधत करते हैं।
जहां आजीविका के सीवमत अिसर स्थानीय पयाविरण के अत्यवधक दोहन के वलए बाध्य करते हैं,
िहां गरीब स्ियं भी अपना जोवखम बढ़ा सकते हैं। इस बीच, प्राकृ वतक संकटों की एक साथ पूरे
समुदाय को समान रूप से प्रभावित करने की प्रकृ वत (covariate nature) यह संकेत करती है क्रक
आपदा के पश्चात् औपचाररक और अनौपचाररक समुदाय-आधाररत सहायता प्रणावलयों के वलए
गुज
ं ाइश सीवमत है।
5.8. विविध NDMA क्रदशा-वनदे श
(Miscellaneous NDMA Guidelines)
5.8.1. सं ग्र हालय
(Museums)
भारतीय संग्रहालयों में संग्रहण (collections) और विषय-िस्तुओं की व्यापक रें ज और विविधता
दृवष्टगोचर होती है। संग्रहण एिं भिन संरचनाओं की क्षवत से आय और संबंवधत िस्तुओं से जुड़ी
सांस्कृ वतक मूल्यों की भी क्षवत होती है। संग्रहालयों में आपदा जोवखम प्रबंधन की कु छ विवशष्ट
चुनौवतयां नीचे सूचीबि की गई हैं:
o संग्रहालयों में पुरातावत्िक से लेकर काबववनक पदाथों तक विवशष्ट िस्तुओं की विविधता होती है,
ये िस्तुएं सुभेद्य होती हैं।
o आपदा पश्चात् सांस्कृ वतक धरोहर के पहलुओं को प्राथवमक महत्ि नहीं क्रदया जाता है क्योंक्रक
अिसंरचना और समुदायों के पुनिावस को प्राथवमकता दी जाती है।
o संग्रहालय में संग्रवहत िस्तुओं के वलए विशेष वनयोजन दृवष्टकोण की आिश्यकता होती है।
o संग्रहालय प्राय: ऐवतहावसक भिनों में होते हैं। ये भिन संरचनात्मक रूप से अवधक सुभेद्य होते हैं
और पहुंच की दृवष्ट से दुगम व क्षेत्रों में वस्थत होते हैं।
o सामान्यत:, संग्रहालय के कमवचारी आिश्यक साधनों से भली-भांवत सुसवज्जत नहीं होते हैं और
आपदा जोवखम न्यूनीकरण के आधारभूत उपायों से अनवभज्ञ होते हैं।
o अस्थायी भंडारण के वलए वनधावररत क्षेत्रों की कमी आपदा पश्चात् क्षवत में और अवधक िृवि करती
है।
o आपदा पश्चात् पुनबवहाली योजनाओं में प्राय: संग्रहालय सवम्मवलत नहीं होते हैं और इनके
पुनर्ननमावण के वलए धनरावश का आबंटन नहीं क्रकया जाता है।
संग्रहालयों को सािवजवनक, अिव-सािवजवनक, वनजी और सेिा क्षेत्रों में विभावजत क्रकया जाना
चावहए। मूल्य आकलन, प्रलेखन तथा िस्तुओं और संग्रह की प्राथवमकता का वनधावरण अिश्य
क्रकया जाना चावहए। िस्तुओं की प्रामावणकता और विवशष्टता को ध्यान में रखा जाना चावहए।
भिन के अंदर और बाहर, दोनों के वलए संकट और जोवखम की पहचान की जानी चावहए और
तदनुसार आपदा जोवखम न्यूनीकरण के वलए कदम उठाए जाने चावहए।
5.8.2. सां स्कृ वतक धरोहर स्थल और पररसर
(Cultural Heritage Sites and Precincts)
हाल ही में आपदा जोवखम न्यूनीकरण के समग्र ढांचे के भीतर सांस्कृ वतक धरोहर को प्रमुख पहलू के
रूप में मान्यता दी गई है। सामान्य जागरूकता का अभाि और विरासतों की प्राथवमकता के वनधावरण
119 www.visionias.in ©Vision IAS
में कमी इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौवतयों में से एक हैं। वनर्नमत सांस्कृ वतक धरोहर के वलए आपदा जोवखम
प्रबंधन के कु छ महत्िपूणव पहलू वनम्नवलवखत हैं:
वनर्नमत धरोहर की आयु, पररमाण और भौवतक वस्थवतयों में विविधता के कारण आपदा जोवखम
न्यूनीकरण के वलए क्रकसी एक मानकीकृ त दृवष्टकोण को लागू करना करठन है।
आपदाएं न के िल सांस्कृ वतक धरोहर स्थलों और पररसरों में रहने, भ्रमण करने या उनका प्रबंधन
करने िाले लोगों के जीिन के वलए बवल्क भौवतक ढांचे में सवन्नवहत धरोहर मूल्यों के वलए भी
जोवखम उत्पन्न करती हैं।
खराब प्रबंधन, उपेक्षा और जागरूकता की कमी वनर्नमत धरोहर के वलए आपदा जोवखम
न्यूनीकरण को और जरटल बनाते हैं क्योंक्रक प्राय: समय के साथ ऐसे भिनों की सं रचनात्मक
समग्रता के साथ समझौता हो जाता है।
ऐसे स्थलों के सन्दभव में, जोवखम कम करने िाले हस्तक्षेप कभी-कभी धरोहर मूल्य और
सौंदयावत्मक मूल्यों के वलए संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
वनर्नमत धरोहर शरणस्थल के रूप में कायव करने का अिसर प्रदान कर सकते हैं या परं परागत
तकनीक का उपयोग करके संरचनात्मक प्रत्यास्थता का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह
पहलू बड़े पैमाने पर जोवखम न्यूनीकरण रणनीवतयां विकवसत करने के वलए उपयोगी हो सकता
है।
भुज वसटी पैलस े की संस्मारक छतररयों (सेनोटैफ्स) को भूकंप के कारण भारी नुकसान पहुाँचा था।
इसी तरह, 2011 में, वसक्रक्कम में आए भूकंप से कई बौि मठ और मंक्रदर नष्ट हो गए थे। 2013 में
वनचले वहमालय में आकवस्मक बाढ़ और 2014 में कश्मीर की बाढ़ से बड़े पैमाने पर मंक्रदरों,
महलों, ऐवतहावसक उद्यानों एिं संग्रहालयों को नुकसान पहुाँचा था।
5.8.3 आपदाओं में मनो-सामावजक सहायता और मानवसक स्िास््य से िाएं
(Psycho-Social Support and Mental Health Services in Disasters)
आपदाओं के संदभव में मनो-सामावजक सहायता आपदा के पश्चात् उत्पन्न होने िाली विवभन्न
मनोिैज्ञावनक और मानवसक स्िास््य समस्याओं को संबोवधत करने के वलए लवक्षत व्यापक
हस्तक्षेपों को संदर्नभत करती है। इन हस्तक्षेपों से व्यवक्तयों, पररिारों और समूहों को अपनी
स्ितंत्रता, गररमा और सांस्कृ वतक अखंडता बनाए रखने के साथ-साथ मानि क्षमताओं का वनमावण
करने तथा सामावजक एकजुटता ि अिसंरचना की पुनस्थावपना करने में सहायता वमलती है। मनो-
सामावजक सहायता से िास्तविक और महसूस क्रकए जाने िाले तनाि के स्तर को कम करने तथा
आपदा प्रभावित समुदाय के बीच प्रवतकू ल मनोिैज्ञावनक और सामावजक पररणामों की रोकथाम में
सहायता वमलती है। अपराधबोध, भय, सदमा, दुैःख, अवत-सतकव ता, स्तब्धता, विचवलत करने
िाली यादें और वनराशा जैसी भािनात्मक प्रवतक्रक्रयाएं उन लोगों की सािवभौवमक प्रवतक्रक्रयाएाँ हैं
वजन्होंने अपनी समायोजन क्षमता से परे क्रकसी अप्रत्यावशत विनाशकारी घटना का सामना क्रकया
हो। लोगों द्वारा व्यक्त की जाने िाली ये भािनात्मक प्रवतक्रक्रयाएं असामान्य घटना के प्रवत सामान्य
प्रवतक्रक्रयाएं होती हैं। एक अनुमान के अनुसार आपदा के तुरंत बाद लगभग 90% जीवित बचे लोग
इन भािनात्मक प्रवतक्रक्रयाओं के दौर से गुजरते हैं। हालांक्रक, तनाि के प्रवत मनोिैज्ञावनक
प्रवतक्रक्रयाओं के पररणामस्िरूप व्यिहार, संबंधों और भौवतक या मानवसक-सामावजक वस्थवतयों में
पररितवन कारण समय बीतने के साथ यह घटकर 30% रह जाता है।
उड़ीसा के सुपर साइक्लोन, गुजरात के भूकंप, दंगों और सुनामी में भारतीय अनुभि ने दशावया है
क्रक बचाि, राहत, पुनिावस और पुनर्ननमावण अिवध के दौरान उवचत मनो-सामावजक हस्तक्षेप से
आपदा से सुरवक्षत बचे लोगों के कष्टों और अक्षमता में काफी कमी आती है। पररणामस्िरूप उनके
जीिन की गुणित्ता में समग्र सुधार होता है।
120 www.visionias.in ©Vision IAS
5.9 पशु ओं के वलए राष्ट्रीय आपदा योजना
(National Disaster Plan for Animals)
पशुओं के वलए आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य पशुओं की रक्षा करना और विवभन्न आपदाओं के
दौरान पशुधन संसाधनों की क्षवत की रोकथाम और शमन करना है। इसे तीन भागों में विभावजत
क्रकया गया है: a) आपदा पूिव तैयारी, b) आपदा के दौरान अनुक्रक्रया और c) आपदा पश्चात्
योजना।
आपदा पूिव तैयारी में पूिव चेतािनी के प्रसार, पशुधन की सुभेद्यता की पहचान, पशु टीकाकरण,
आहार और चारा आपूर्नत और आपदा प्रबंधन में विवभन्न वहतधारकों के क्षमता वनमावण आक्रद से
संबंवधत विस्तृत कायव योजना सवम्म्वलत है। आपदा के दौरान प्रभािी और तत्काल अनुक्रक्रया,
पशुधन का बचाि, आहार और चारा आपूर्नत, महामाररयों और बीमाररयों के विरूि उपाय और
स्ि्छता बनाए रखने आक्रद से संबंवधत रणनीवत/कायव योजना सवम्मवलत है। आपदा पश्चात् के
घटक में बीमार जानिरों का उपचार, बीमारी की वनगरानी, शिों का वनपटान तथा पशुधन
आबादी के पुराने स्तर को प्राप्त क करना सवम्मवलत है।
Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without prior permission of Vision IAS.
121 www.visionias.in ©Vision IAS
Courier service
Available
whatsapp NO
9310521834
DEEPAK PHOTOSTAT
& Consultant
Most appreciated SHOP by TOPPERS from last many years..
By a survey No.1 Shop in INDIA who deals with IAS,IES,
PCS,SSC,Bank Po, NET/JRF/All Competitive exams.
Study Materials for IAS,PCS,SSC BANK PO NET/JRF,
Old/New NCERT,IGNOU etc are available here .
741/4,Near AGGARWAL SWEET,DR.MUKHERJEE NAGAR,DELHI-110009
E-mail; deepakkumarnirala88@gmail.com
You might also like
- Modern History Vision HindiDocument396 pagesModern History Vision Hindijitendra mishraNo ratings yet
- World History Vision Hindi PDFDocument335 pagesWorld History Vision Hindi PDFEric DavidNo ratings yet
- Environment Geography and Disaster Management Hindi 1Document80 pagesEnvironment Geography and Disaster Management Hindi 1Aman TiwariNo ratings yet
- PT 365 Updation Material HindiDocument114 pagesPT 365 Updation Material HindiBibek BoxiNo ratings yet
- आजादी के बाद Printed Notes by VISION IASDocument83 pagesआजादी के बाद Printed Notes by VISION IASAbhay JainNo ratings yet
- VisionIAS Hindi Magazine March 2024 March 2024Document187 pagesVisionIAS Hindi Magazine March 2024 March 2024pushpendraNo ratings yet
- VisionIAS PT 365 December 2024 International RelationsDocument124 pagesVisionIAS PT 365 December 2024 International Relationssainiraj01041990No ratings yet
- VisionIAS PT 365 December 2024 EconomyDocument134 pagesVisionIAS PT 365 December 2024 Economysainiraj01041990No ratings yet
- Economy Hindi - PDF 1631962026 PDFDocument116 pagesEconomy Hindi - PDF 1631962026 PDFNarender KhedarNo ratings yet
- 6 आजादी के बाद का भारत VISION 2021 24907 unlocked 231126 221341Document84 pages6 आजादी के बाद का भारत VISION 2021 24907 unlocked 231126 221341Vandana GautamNo ratings yet
- Monthly Current Affairs - February 2024Document177 pagesMonthly Current Affairs - February 2024monishamonisha224yNo ratings yet
- Environment Note ShankerDocument139 pagesEnvironment Note ShankerBasudev MuduliNo ratings yet
- VisionIAS Hindi Magazine January 2024 January 2024Document180 pagesVisionIAS Hindi Magazine January 2024 January 2024putinmodi3No ratings yet
- VisionIAS PT 365 December 2024 Science and TechnologyDocument135 pagesVisionIAS PT 365 December 2024 Science and TechnologyAshish AGRAWALNo ratings yet
- World History Vision HindiDocument335 pagesWorld History Vision HindiNeelessh PatilNo ratings yet
- Vision World History Hindi P2Document122 pagesVision World History Hindi P2foreclosureindiaNo ratings yet
- VisionIAS Hindi Magazine September 2023 September 2023Document160 pagesVisionIAS Hindi Magazine September 2023 September 2023ADITYA AWASTHINo ratings yet
- VisionIAS Hindi Magazine October 2023 October 2023Document153 pagesVisionIAS Hindi Magazine October 2023 October 2023Ruhi GuptaNo ratings yet
- VisionIAS Hindi Magazine October 2023 October 2023Document153 pagesVisionIAS Hindi Magazine October 2023 October 2023Gourav PanchalNo ratings yet
- Indian Polity and Governance Part 1Document248 pagesIndian Polity and Governance Part 1bettingrkNo ratings yet
- Social Justice Vision HindiDocument143 pagesSocial Justice Vision Hindisaurabh bhardwajNo ratings yet
- Culture HindiDocument50 pagesCulture Hindisumit_srimalNo ratings yet
- UPSCDocument396 pagesUPSCdev100% (1)
- 5 6102862804916634461Document143 pages5 6102862804916634461Abhi RajNo ratings yet
- Vision Polity Part-1 @upsc - SarthiDocument169 pagesVision Polity Part-1 @upsc - SarthiTuhin PalNo ratings yet
- VisionIAS PT 365 December 2024 Social IssuesDocument71 pagesVisionIAS PT 365 December 2024 Social Issuessainiraj01041990No ratings yet
- C3d8b-Current Affairs April 2022 HDocument137 pagesC3d8b-Current Affairs April 2022 Hchirag chauhanNo ratings yet
- सरकारी योजनाऐं vision IASDocument136 pagesसरकारी योजनाऐं vision IASalishaNo ratings yet
- पोर्टफोलियो कक्षा10 PDFDocument9 pagesपोर्टफोलियो कक्षा10 PDFKiya kroge Name jankarNo ratings yet
- 9f36b June 2020Document122 pages9f36b June 2020Reman SinhaNo ratings yet
- Social-Issues Hindi 2022Document59 pagesSocial-Issues Hindi 2022Golu GautamNo ratings yet
- Class 1 Dec WSDocument2 pagesClass 1 Dec WSpratap2838No ratings yet
- शासनDocument141 pagesशासनVipin Pal Singh ChaudharyNo ratings yet
- Government-Schemes Comprehensive (Sscstudy - Com)Document171 pagesGovernment-Schemes Comprehensive (Sscstudy - Com)Tejaswini ReddyNo ratings yet
- VisionIAS PT 365 December 2024 CultureDocument85 pagesVisionIAS PT 365 December 2024 Culturesainiraj01041990100% (1)
- Day 4 Functional Goal Planning Part 2Document3 pagesDay 4 Functional Goal Planning Part 2AvantikaNo ratings yet
- लिंग कार्य पत्रिका -5Document1 pageलिंग कार्य पत्रिका -5Arun UdayabhanuNo ratings yet
- Document ViewerDocument9 pagesDocument ViewerSimran RoyNo ratings yet
- 036f8 May 2019 PDFDocument98 pages036f8 May 2019 PDFvaibhav singh Thakur100% (1)
- 8d341 World History Part 1Document117 pages8d341 World History Part 1manojkaamdevNo ratings yet
- 1712149524Document12 pages1712149524pawan70236No ratings yet
- 788e8 December 2019 PDFDocument114 pages788e8 December 2019 PDFAlpesh PrajapatiNo ratings yet
- प्रेस विज्ञप्ति बीमा मंथन जनवरी 24 - Press Release Bima Manthan Jan 24Document2 pagesप्रेस विज्ञप्ति बीमा मंथन जनवरी 24 - Press Release Bima Manthan Jan 24PriyankaKakruNo ratings yet
- PT 2 - Revision WorksheetDocument5 pagesPT 2 - Revision Worksheetpvr2k1No ratings yet
- January 2020Document120 pagesJanuary 2020Rahull DandotiyaNo ratings yet
- 5e802-Current-Affairs July 2022 Hindi 2022Document156 pages5e802-Current-Affairs July 2022 Hindi 2022RAHUL HEERADASNo ratings yet
- 22 भारतीयत अर्थव्यवस्था PART 3 24947 unlockedDocument200 pages22 भारतीयत अर्थव्यवस्था PART 3 24947 unlockedashish singhNo ratings yet
- Grade 5 Hindi WorksheetDocument3 pagesGrade 5 Hindi WorksheetNoddy 111No ratings yet
- MP MSMED Policy 2021 Booklet Hindi NewDocument48 pagesMP MSMED Policy 2021 Booklet Hindi NewconnectwithchiragvNo ratings yet
- Paper-5 Hindi (5.3.2024)Document24 pagesPaper-5 Hindi (5.3.2024)suryakant jarariyaNo ratings yet
- E3356 July 2023Document159 pagesE3356 July 2023PrashantNo ratings yet
- Vision World History Hindi P2Document122 pagesVision World History Hindi P2RabinNo ratings yet
- Jan HindiDocument173 pagesJan HindiAditya PayasiNo ratings yet
- mid-CLASS V-HINDI-221009105504Document2 pagesmid-CLASS V-HINDI-221009105504ANIL PNo ratings yet
- Indian Polity and Governnce Part 4Document114 pagesIndian Polity and Governnce Part 4jhaashu2001No ratings yet
- VISION IAS सरकारी योजनाए कॉम्प्रिहेंसिव 2023 भाग 2Document131 pagesVISION IAS सरकारी योजनाए कॉम्प्रिहेंसिव 2023 भाग 2surjeetcharan55No ratings yet
- Mco-07 (H) 20-21Document14 pagesMco-07 (H) 20-21ArunNo ratings yet