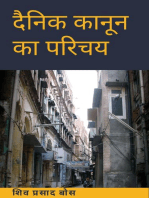Professional Documents
Culture Documents
Judicial Activism
Judicial Activism
Uploaded by
taishwarya200 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views9 pagesArticle on Judicial Activism
Original Title
Judicial activism
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentArticle on Judicial Activism
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views9 pagesJudicial Activism
Judicial Activism
Uploaded by
taishwarya20Article on Judicial Activism
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 9
न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ते कदम
(WHEN JUDGES LEGISLATE)
संदर्भ
हाल के कई निर्णयों से ऐसा माना जा रहा है
कि सर्वोच्च न्यायालय कानून निर्माण करने में
अति सक्रिय भूमिका निभा रहा है। न तो राज्य
के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट
पृथक्करण है और न ही कानून संरक्षित किया
जा रहा है।
इसका तात्पर्य है कि संविधान में राज्य के तीन
अंगों (विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका) के बीच शक्तियों का स्पष्ट
पृथक्करण होना चाहिये और एक अंग को
दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना
चाहिये। यदि ऐसा होता है, तो संविधान के
नाजुक संतुलन को हानि पहुँचेगी और
अराजकता फै लेगी।
न्यायिक सक्रियता क्या है?
न्यायपालिका संवैधानिक प्रणाली के तहत
संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने के
लिये सक्रिय भूमिका निभाती है।
‘न्यायिक सक्रियता’ शब्द न्यायाधीशों के निर्णय को
संदर्भित करता है। न्यायिक समीक्षा को एक सिद्धांत
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके
तहत न्यायपालिका द्वारा विधायिका और
कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है।
उल्लेखनीय है कि न्यायिक समीक्षा को विधायी कार्यों
की समीक्षा, न्यायिक फै सलों की समीक्षा और
प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के तीन आधारों पर
तीन श्रेणियों में वर्गीकृ त किया जा सकता है।
न्यायालय, न्यायिक समीक्षा द्वारा कार्यपालिका और
विधायिका दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं।
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
विभिन्न प्रावधानों के तहत संविधान ने विधायिका
और न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्यप्रणाली में
अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये स्पष्ट रूप से
रेखा खींची है।
जहाँ अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को अपने
कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायाधीश के
आचरण पर चर्चा करने से मना करते हैं, वहीं दूसरी
तरफ, अनुच्छेद 122 और 212 अदालतों को
विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से
रोकते हैं।
इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105
(2) और 194 (2) विधायकों को उनकी भाषण की
स्वतंत्रता और वोट देने की आजादी के संबंध में
अदालतों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं।
न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क
न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को उन मामलों में
अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर
प्रदान करती है जहाँ कानून संतुलन प्रदान करने में
विफल रहा।
इसके अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भी मुद्दों में
अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, यही कारण है कि यह
स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में त्वरित
विश्वास कायम करती है।
कई बार सार्वजनिक शक्ति लोगों को नुकसान
पहुँचाती है, इसलिये न्यायपालिका के लिये
सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को जाँचना आवश्यक
हो जाता है।
यह तेज़ी से उन विभिन्न मुद्दों पर समाधान प्रदान
करने का एक अच्छा विकल्प है, जहाँ विधायिका
बहुमत के मुद्दे पर फँ स जाती है।
न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क
न्यायाधीश किसी भी मौजूदा कानून को ओवरराइड
कर सकते हैं। इसलिये यह स्पष्ट रूप से संविधान
द्वारा तैयार की गई सीमा रेखा का उल्लंघन करता है।
न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर शासन
करने के लिये मानक बन जाती है। इसके अतिरिक्त
निर्णय निजी या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं
जो जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकते
हैं।
अदालतों के बार-बार हस्तक्षेप के कारण लोगों का
विश्वास सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता, अखंडता
और दक्षता के प्रति कम हो जाता है।
न्यायिक सक्रियता
एक अग्रगामी कदम
जब विधायिका बदलते समय के अनुरूप आवश्यक
कानून बनाने में विफल रहती है और सरकारी
एजेंसियाँ ईमानदारी से अपने प्रशासनिक कार्यों को
निष्पादित करने में बुरी तरह विफल हो जाती हैं तो
संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में नागरिकों के
आत्मविश्वास का क्षरण होता है।
ऐसे परिदृश्य में न्यायपालिका आमतौर पर
विधायिका और कार्यपालिका के लिये निर्धारित क्षेत्रों
में कदम उठाती है तो परिणाम न्यायिक कानून और
न्यायपालिका द्वारा सरकार के रूप में सामने आते हैं।
यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन
सरकार या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता
है, तब न्यायाधीश स्वयं नागरिकों की सहायता करने
का कार्य कर सकते हैं।
भारत में न्यायिक सक्रियता को किस तरह से
परिभाषित किया जा सकता है?
a) न्यायपालिका एक निष्क्रिय भूमिका निभाती
है और के वल कानूनों के अनुरूप व्याख्या करती
है
b) न्यायपालिका सार्वजनिक हित के मामलों में
सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है ताकि नागरिकों
के अधिकारों की रक्षा और न्याय हो सके
c) न्यायपालिका सरकार द्वारा नियंत्रित होती है
और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखती है
d) कोई भी नहीं
You might also like
- Judicial Activism in IndiaDocument5 pagesJudicial Activism in IndiamydeargorgeousoneNo ratings yet
- Independence of Supreme CourtDocument3 pagesIndependence of Supreme CourtmydeargorgeousoneNo ratings yet
- Nyaya PalikaDocument39 pagesNyaya Palikaajaydce05100% (1)
- 12 SepDocument1 page12 Sepvaishnavi classesNo ratings yet
- Hindi Project, 7th SemesterDocument13 pagesHindi Project, 7th SemesterAstha DehariyaNo ratings yet
- Law NotesDocument79 pagesLaw NotesSAURABH KOHLI D100% (1)
- CEALSCEPhD03Comparative Constitutional Adjudication Ism19b.en - HiDocument17 pagesCEALSCEPhD03Comparative Constitutional Adjudication Ism19b.en - HiALEEMNo ratings yet
- SC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILDocument7 pagesSC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILALEEMNo ratings yet
- Jurisprudence-Notes in HindiDocument8 pagesJurisprudence-Notes in HindiAjay PandeyNo ratings yet
- GS 2 2023 For Learners 1Document72 pagesGS 2 2023 For Learners 1UtkarshNo ratings yet
- Adminstrative LawDocument128 pagesAdminstrative LawDhaval PatelNo ratings yet
- राक्षसी प्रक्रिया judicial process common law criminal lawDocument12 pagesराक्षसी प्रक्रिया judicial process common law criminal lawALEEMNo ratings yet
- ManualDocument2 pagesManualramesh chaohanNo ratings yet
- Task 1 Feb TranslatedDocument7 pagesTask 1 Feb TranslatedKavitaNo ratings yet
- The Right To PrivacyDocument10 pagesThe Right To Privacytaishwarya20No ratings yet
- Fundamental Rights DiaryDocument143 pagesFundamental Rights DiaryDhanauri DhanauriNo ratings yet
- Mini Training On Constitution Day2Document14 pagesMini Training On Constitution Day2ISNo ratings yet
- भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएंDocument12 pagesभारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएंsolankinaina32No ratings yet
- 356 PDFDocument3 pages356 PDFJoy HappyNo ratings yet
- JUDICIARY न्यायपालिकाDocument26 pagesJUDICIARY न्यायपालिकाamriteshrajtetri1811No ratings yet
- धार्मिक मामलों पर न्यायिक हस्तक्षेप-धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा - secularism धर्म निरपेक्षताDocument9 pagesधार्मिक मामलों पर न्यायिक हस्तक्षेप-धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा - secularism धर्म निरपेक्षताALEEMNo ratings yet
- Legal HindiDocument14 pagesLegal Hindisanskrati116-20No ratings yet
- प्रशासनिक अधिकरनDocument6 pagesप्रशासनिक अधिकरनGaurav SharmaNo ratings yet
- क़ानून की व्याख्या के नियम - वह सब जो आप जानना चाहते हैंDocument15 pagesक़ानून की व्याख्या के नियम - वह सब जो आप जानना चाहते हैंsarveshchaubey4744No ratings yet
- - राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Document2 pages- राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Pradeep KumarNo ratings yet
- - राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Document2 pages- राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Pradeep KumarNo ratings yet
- DemocracyDocument3 pagesDemocracyshaun prakashNo ratings yet
- Om Namah Shivay Second PaperDocument41 pagesOm Namah Shivay Second PaperashishNo ratings yet
- भारत का संविधा भाग 9 धार्मिक स्वतंत्रता Hindi article 25Document6 pagesभारत का संविधा भाग 9 धार्मिक स्वतंत्रता Hindi article 25ALEEMNo ratings yet
- Yojna Daily Current Affairs Hindi Med 22 Feb 2024Document6 pagesYojna Daily Current Affairs Hindi Med 22 Feb 2024sakshisirsagar14No ratings yet
- लोक अदालतDocument7 pagesलोक अदालतagarwalassociate12No ratings yet
- 153 - Dicey-Rule of Law PDFDocument3 pages153 - Dicey-Rule of Law PDFrk4978503No ratings yet
- Administrative Tribunal Notes - 240326 - 170421.en - HiDocument6 pagesAdministrative Tribunal Notes - 240326 - 170421.en - Hiyadavnitin421No ratings yet
- एक देश - एक चुनावDocument3 pagesएक देश - एक चुनावAbhinavSinghNo ratings yet
- Public Administration ShrikantDocument21 pagesPublic Administration ShrikantNeeraj KurmiNo ratings yet
- 05. मौलिक अधिकारDocument2 pages05. मौलिक अधिकारAnuj Singh BadamiNo ratings yet
- JETIR2110354 Research in Academic Law Students .En - HiDocument37 pagesJETIR2110354 Research in Academic Law Students .En - HiALEEMNo ratings yet
- Court Contempt PresentationDocument7 pagesCourt Contempt Presentationharshakoshre6No ratings yet
- धयेय IAS - Best UPSC IAS CSE Online Coaching Best UPSC Coaching Top IAS Coaching in Delhi Top CSEDocument3 pagesधयेय IAS - Best UPSC IAS CSE Online Coaching Best UPSC Coaching Top IAS Coaching in Delhi Top CSEAditya GuptaNo ratings yet
- - hindi - to-the-points - paper4 - corruption-in-india - print - manual# - ~ - text=साथ ही 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा,में 40 अंक प्राप्त किये।Document6 pages- hindi - to-the-points - paper4 - corruption-in-india - print - manual# - ~ - text=साथ ही 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा,में 40 अंक प्राप्त किये।kgz881887No ratings yet
- Preamble and Salient Features of The Constitution Hindi Reviewed 1 50Document9 pagesPreamble and Salient Features of The Constitution Hindi Reviewed 1 50Aniruddha SoniNo ratings yet
- Ilovepdf MergedDocument15 pagesIlovepdf Mergedmahendrasingh366789No ratings yet
- Vision IAS Classroom Study Material Indian PolityDocument475 pagesVision IAS Classroom Study Material Indian PolityraviNo ratings yet
- Judicial-Creativity-Essay en HiDocument5 pagesJudicial-Creativity-Essay en HiALEEMNo ratings yet
- TRANSLATIONDocument14 pagesTRANSLATION1815I UTKARSH SHUBHAMNo ratings yet
- Assignment-Subject 6-Constitutional LawDocument14 pagesAssignment-Subject 6-Constitutional Lawmahendrasingh366789No ratings yet
- 1640680343Document5 pages1640680343Amit Kumar PyenNo ratings yet
- 1. लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों - WatermarkDocument16 pages1. लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों - Watermarkjimaurya431No ratings yet
- Uwais Chauhan TranslationDocument3 pagesUwais Chauhan Translationporetic617No ratings yet
- Hindi ProjectDocument8 pagesHindi ProjectRehaan AhmedNo ratings yet
- Additional Notes For ApproachesDocument2 pagesAdditional Notes For Approachessantosh kumarNo ratings yet
- Extant of PolityDocument6 pagesExtant of Polityshivankur sharmaNo ratings yet
- 11 भारतीय संविधान एवं शासन Part 3 24913 unlockedDocument107 pages11 भारतीय संविधान एवं शासन Part 3 24913 unlockedashish singhNo ratings yet
- PlatoDocument2 pagesPlatoAastha AroraNo ratings yet
- Girdhari LalDocument13 pagesGirdhari LalSarik KhanNo ratings yet
- प्लेटो का न्याय का सिद्धांत - iPleaders सामाजिक न्याय social justiceDocument11 pagesप्लेटो का न्याय का सिद्धांत - iPleaders सामाजिक न्याय social justiceALEEMNo ratings yet
- राजव्यवस्था 28: Daily Class Notes - - (संकल्प UPSC 2024 हिन्दी माध्यम)Document6 pagesराजव्यवस्था 28: Daily Class Notes - - (संकल्प UPSC 2024 हिन्दी माध्यम)rajankarangiya2499No ratings yet
- पाठ योजना 2Document10 pagesपाठ योजना 2DBMS COLLEGE OF EDUCATIONNo ratings yet
- सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ - विकिपीडिया right to information rtiDocument8 pagesसूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ - विकिपीडिया right to information rtiLaw OfficeNo ratings yet