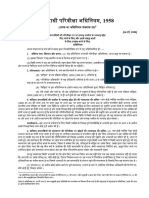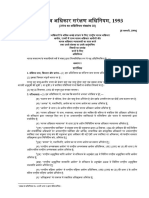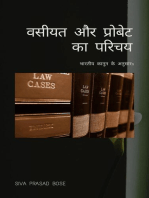Professional Documents
Culture Documents
आईपीसी के तहत मृत्यु दंड दण्ड
आईपीसी के तहत मृत्यु दंड दण्ड
Uploaded by
ALEEMCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
आईपीसी के तहत मृत्यु दंड दण्ड
आईपीसी के तहत मृत्यु दंड दण्ड
Uploaded by
ALEEMCopyright:
Available Formats
फ़ाइल कॉपीराइट ऑनलाइन (https://www.legalserviceindia.com/copyright/register.
htm) -
दिल्ली में आपसी तलाक
फ़ाइल करें (https://www.legalserviceindia.com/helpline/mutual_consent_divorce.htm) -
ऑनलाइन कानूनी
सलाह (https://www.legalserviceindia.com/consult/advice.htm) - भारत में वकील
(https://www.legalserviceindia.com/lawyers/lawyers_home.htm)
आईपीसी के तहत दंड
सैंड्रा द्वारा | दृश्य 123546 (author-18725-sandra.html)
52
9
30
ब्लॉगर 12
WHATSAPP 77
जेब 22
डिग 12
कानून के तहत, गलत करने वाले को फिर से अपराध करने से रोकने के लिए सजा का प्रावधान है। सजा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गलत
काम का परिणाम या परिणाम है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 53 और अध्याय 3 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। यह
धारा विभिन्न प्रकार के दंडों को परिभाषित करती है जिनके लिए अपराधी भारतीय दंड संहिता के तहत उत्तरदायी हैं। धारा 53 के तहत दी गई
सज़ा के वल इस संहिता के तहत दिए गए अपराधों पर लागू होती है।
भारत में सज़ा देने के लिए सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया जाता है। दी जाने वाली सज़ा न तो इतनी कठोर होनी चाहिए और न ही इतनी
आसान होनी चाहिए कि वह अपराधी पर प्रभाव डालने और दूसरों की आंखें खोलने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाए। यह माना
जाता है कि सज़ा ऐसी प्रकृ ति की होनी चाहिए जिससे उनमें सुधार आए। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और सोच.
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार की सज़ाओं का प्रावधान है।
1. मृत्यु दंड
2. आजीवन कारावास
3. कै द होना
a. कठिन
b. सरल
4. संपत्ति की जब्ती
5. अच्छा
मृत्यु दंड
मृत्युदंड को मृत्युदंड भी कहा जाता है। इस सजा के तहत व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती।
किसी अपराध की सज़ा के रूप में अधिकार द्वारा अपराधी को मृत्युदंड देना या उसका जीवन छीन लेना मृत्युदंड या मृत्युदंड है। भारत में यह
दुर्लभतम मामलों में प्रदान किया जाता है।
इसे निम्नलिखित अपराधों में सज़ा के रूप में दिया जा सकता है:
a. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना (धारा 121)
b. वास्तव में प्रतिबद्ध पारस्परिक अपराध को बढ़ावा देना (धारा 132)
c. झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाए (धारा 194)
d. हत्या (धारा 302)
e. आजीवन दोषियों द्वारा हत्या (धारा 303)
f. किसी नाबालिग या पागल या नशे में धुत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना (धारा 305)
g. हत्या के साथ डकै ती (धारा 396)
h. फिरौती के लिए अपहरण (धारा 364ए)
निर्णय विधि
1. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1980 SC 898,1980) ने
मृत्युदंड की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन अदालत ने के वल दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड के प्रावधान को सीमित कर दिया। यदि
मामला इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो मृत्युदंड दिया जा सकता है।
2. जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973 एआईआर 947,1973 एससीआर (2)541)
मृत्युदंड असंवैधानिक है और इसलिए सजा के रूप में अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को वैध माना। यह माना गया कि जीवन
से वंचित करना संवैधानिक रूप से वैध है यदि यह कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
आजीवन कारावास
1955 के अधिनियम XXVI द्वारा आजीवन कारावास शब्द को जीवन भर के लिए परिवहन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। इसके
सामान्य अर्थ में आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के प्राकृ तिक जीवन की शेष पूरी जीवन अवधि के लिए कारावास है। धारा 57 के
अनुसार आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। लेकिन के वल सजा की शर्तों के अंशों की गणना के लिए
आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। लेकिन अन्यथा आजीवन कारावास की सजा अनिश्चित अवधि की होती
है।
निर्णय विधि
1. भागीरथ और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन (1985 एआईआर 1050)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास को दोषी के शेष प्राकृ तिक जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया।
यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है, तो उसे कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम शेष जीवन जेल में रहना होगा।
2. नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (एआईआर 1986 एससी 2192)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि और आईपीसी की धारा 55 के साथ भ्रम को दूर कर दिया। अदालत ने
कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला कोई भी व्यक्ति 14 साल जेल में रहने के बाद अपनी रिहाई का दावा नहीं कर
सकता। आजीवन कारावास कै दी की मृत्यु तक जारी रहता है। इसका एकमात्र अपवाद रूपान्तरण और छू ट है।
कारावास
कारावास का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेना और उसे कारागार में डाल देना।
आईपीसी की धारा 53 के अनुसार, दो प्रकार के दंड हैं:
a. सरल: यह एक ऐसी सज़ा है जिसमें अपराधी को के वल जेल तक ही सीमित रखा जाता है और कोई कठोर श्रम नहीं किया जाता है।
निम्नलिखित कु छ अपराध हैं जो साधारण कारावास से दंडनीय हैं:
गलत संयम (धारा 341)
किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई आवाज या इशारा करना (धारा 509)
शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर दुराचार (धारा 510)
मानहानि (धारा 500,501,502)
संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग (धारा 403)
b. कठोर:
इस मामले में अपराधी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जैसे मकई पीसना, खुदाई करना, लकड़ी काटना आदि। निम्नलिखित कु छ
अपराध हैं जिनके लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है:
हत्या के लिए अपहरण (धारा 364)
डकै ती (धारा 392)
डकै ती (धारा 395)
मौत से दंडनीय अपराध करने के लिए घर में तोड़फोड़ करना (धारा 449)
निर्णय विधि
1. गौतम दत्ता बनाम. झारखंड राज्य (10 फरवरी 2016)
आतिफ मुस्तफा नाम के लड़के का जानबूझकर अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने खुद को आपराधिक मुकदमे से
बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया। एमडी सफीक पहले से ही कोर्ट ट्रायल में है। अदालत में
सुनवाई के दौरान अदालत को अपने 3 दोस्तों के साथ एक लड़के का अपहरण करने के उसके दूसरे अपराध के बारे में पता चला।
अदालत ने उन्हें ढूंढा और अपहरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया जो आईपीसी की धारा 364ए, 120बी के तहत दंडनीय है।
2. मो.मुन्ना बनाम. भारत संघ और अन्य (एआईआर 2005 एससी 3440)
रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता को हत्या का दोषी पाया गया। वहीं इससे पहले
उसे 21 साल की उम्रकै द की सजा मिल चुकी है. इसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आजीवन कारावास 20 साल के बराबर होना
चाहिए और आगे कानून के तहत स्वीकार्य छू ट के अधीन होना चाहिए।
संपत्ति की ज़ब्ती
ज़ब्ती का तात्पर्य अभियुक्त की संपत्ति की हानि से है। इस सज़ा के तहत राज्य अपराधी की संपत्ति जब्त कर लेता है। यह उस व्यक्ति द्वारा किए
गए गलत काम या चूक का नतीजा होता है। जब्त की गई संपत्ति चल या अचल हो सकती है।
दो प्रावधानों में संपत्ति की ज़ब्ती को समाप्त कर दिया गया है:
1. धारा 126 के तहत भारत सरकार के साथ शांति वाले क्षेत्रों में लूटपाट करने के लिए।
2. आईपीसी की धारा 126 में उल्लिखित युद्ध या लूटपाट के दौरान ली गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए धारा 127 के तहत।
जुर्माना
जुर्माने को सीधे तौर पर आर्थिक दंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सज़ा देने से जुड़ी लगभग सभी धाराओं में सज़ा के तौर पर
जुर्माना भी शामिल है. हालाँकि धारा 63 कहती है कि जहाँ राशि व्यक्त की गई है जिससे जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने की वह राशि
जिसके लिए अपराधी उत्तरदायी है, असीमित है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी।
निर्णय विधि
पालनियप्पा गौंडर बनाम। तमिलनाडु राज्य (1977 AIR 1323)
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा दी गई सजा अपराध की प्रकृ ति के अनुपात में होगी जिसमें जुर्माने की सजा भी शामिल है।
और सज़ा अनावश्यक रूप से अत्यधिक नहीं होगी.
निष्कर्ष
हमने विभिन्न दंडों पर चर्चा की है जो अलग-अलग अपराधों में अलग-अलग लगाए जाते हैं, अवधि, प्रकृ ति, आदि प्रत्येक मामले और अपराधों
में और अदालतों के अनुसार भी भिन्न होती है। सभी दंड प्रकृ ति में प्रतिशोधी, सुधारात्मक और निवारक हैं। यह कहा गया है कि सजा के लिए
एक सुधारात्मक दृष्टिकोण आपराधिक कानून का उद्देश्य होना चाहिए।
पुरस्कार विजेता लेख द्वारा लिखा गया है: सुश्री सांद्रा पी राफी
You might also like
- H195820Document5 pagesH195820Jay TiwariNo ratings yet
- जानिए मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने के दंड का निष+ प्राणदंड के कार्यान्वयन में देरीDocument7 pagesजानिए मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने के दंड का निष+ प्राणदंड के कार्यान्वयन में देरीALEEMNo ratings yet
- कैदियों के अधिकार Prisoners Right जेल में बंद कैदियों के अधिकार GgdyijjDocument4 pagesकैदियों के अधिकार Prisoners Right जेल में बंद कैदियों के अधिकार GgdyijjALEEMNo ratings yet
- Girdhari LalDocument13 pagesGirdhari LalSarik KhanNo ratings yet
- Bailable and Non Bailable OffencesDocument4 pagesBailable and Non Bailable OffencesmydeargorgeousoneNo ratings yet
- The Family Courts Act 1984 HINDIDocument6 pagesThe Family Courts Act 1984 HINDIshubh dewanganNo ratings yet
- H1974 02Document214 pagesH1974 02himanjalimishra1010No ratings yet
- Gunda Act HindiDocument9 pagesGunda Act HindiShubhanshu TripathiNo ratings yet
- Indian Penal Code - HindiDocument99 pagesIndian Penal Code - HindidreamachivrsNo ratings yet
- H186045Document99 pagesH186045RAHUL PASTORNo ratings yet
- Top 100 Landmark Judgement - 2023Document23 pagesTop 100 Landmark Judgement - 2023Krishna KishoreNo ratings yet
- सम्पूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता PDFDocument47 pagesसम्पूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता PDFRajul agnihotri88% (8)
- ConstitutionDocument102 pagesConstitutionshrivastavavaibhav575No ratings yet
- Nanavati JudgementDocument94 pagesNanavati JudgementYashi bhardwajNo ratings yet
- 13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989Document27 pages13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989GAURAV SINGHNo ratings yet
- Legal Current Hindi 17.01.24Document5 pagesLegal Current Hindi 17.01.24sonika palNo ratings yet
- भारतीय न्याय संहिता 2023 Press Release 1Document10 pagesभारतीय न्याय संहिता 2023 Press Release 1cilenas236No ratings yet
- NDPS Act Bail जमानत के प्रावधानDocument6 pagesNDPS Act Bail जमानत के प्रावधानALEEMNo ratings yet
- H 195443Document19 pagesH 195443bhumidharpantanti6No ratings yet
- मानव अधिकार और मौलिक अधिकार के मध्य शरीर व आत्मा का संबंध हैDocument3 pagesमानव अधिकार और मौलिक अधिकार के मध्य शरीर व आत्मा का संबंध हैTwin PrajapatiNo ratings yet
- कल्प - संविदाDocument3 pagesकल्प - संविदाselbb1456No ratings yet
- CRPC HindiDocument207 pagesCRPC Hindiabdurrehman1366No ratings yet
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973Document207 pagesदण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973sumit kumarNo ratings yet
- CRPC HindiDocument207 pagesCRPC Hindiking donNo ratings yet
- महिला उत्तराधिकार पर विधि आयोग की रिपोर्टDocument7 pagesमहिला उत्तराधिकार पर विधि आयोग की रिपोर्टms.rhythmsinghNo ratings yet
- DR - Haniraj L Chulani Vs Bar Council of MaharastraDocument15 pagesDR - Haniraj L Chulani Vs Bar Council of MaharastraSarik KhanNo ratings yet
- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारीDocument9 pagesभारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारीPankaj KumarNo ratings yet
- H199410Document12 pagesH199410Vijay ParmarNo ratings yet
- Important Judgments PDF in HindiDocument9 pagesImportant Judgments PDF in Hindidimpi aryaNo ratings yet
- H187201 1Document46 pagesH187201 1Puran PatelNo ratings yet
- Complete Polity For One Day ExamsDocument44 pagesComplete Polity For One Day Examsmaheshsinghms7383No ratings yet
- Extant of PolityDocument6 pagesExtant of Polityshivankur sharmaNo ratings yet
- २८.मुलुकी अपराध संहिता २०७४Document151 pages२८.मुलुकी अपराध संहिता २०७४Anil KhanalNo ratings yet
- All State Indian Penal Code Mains Previous Year Questions: T.me/linkinglaws Linking LawsDocument34 pagesAll State Indian Penal Code Mains Previous Year Questions: T.me/linkinglaws Linking LawsRavinder ThakurNo ratings yet
- भारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFDocument161 pagesभारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFAKSHAJ RANENo ratings yet
- भारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFDocument161 pagesभारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFGauravNo ratings yet
- भारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFDocument161 pagesभारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFluckyNo ratings yet
- Ipc HindiDocument161 pagesIpc HindijinNo ratings yet
- Act 1860 0045 PDF F689 HindiDocument161 pagesAct 1860 0045 PDF F689 Hindihimanjalimishra1010No ratings yet
- भारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFDocument161 pagesभारतीय दण्ड संहिता 1860 PDFs a kharadiNo ratings yet
- Fundamental Rights DiaryDocument143 pagesFundamental Rights DiaryDhanauri DhanauriNo ratings yet
- H198933Document6 pagesH198933Vijay ParmarNo ratings yet
- Assistant Prosecution Officer Apo Exam Paper I Law 2015 609Document16 pagesAssistant Prosecution Officer Apo Exam Paper I Law 2015 609fab movie KhatriNo ratings yet
- Dowry Prohibiton - HindiDocument13 pagesDowry Prohibiton - HindiParinita SinghNo ratings yet
- Cr.P.C-Unit-2 DetailedDocument14 pagesCr.P.C-Unit-2 DetailedgogoNo ratings yet
- Transfer of Property Act 1882 - HindiDocument38 pagesTransfer of Property Act 1882 - HindidreamachivrsNo ratings yet
- 19Document38 pages19SHUBHAM GANDHINo ratings yet
- Transfer of Property Act 1882 - HindiDocument38 pagesTransfer of Property Act 1882 - HindiSHREE Music StudioNo ratings yet
- किन अपराधों में जमानत नहीं होती और कौन से अपराध में हो सकती है आपकी जमानत जानकारी के लिए हमारा यह लेख जरूर पढ़ें। - अलौकिक लेख समस्या आपकी सुझाव हमाराDocument3 pagesकिन अपराधों में जमानत नहीं होती और कौन से अपराध में हो सकती है आपकी जमानत जानकारी के लिए हमारा यह लेख जरूर पढ़ें। - अलौकिक लेख समस्या आपकी सुझाव हमाराAbdul Jabbar ShaikhNo ratings yet
- CCI (Settlement) Regulations, 2024Document15 pagesCCI (Settlement) Regulations, 2024Rajkumar MathurNo ratings yet
- 17Document12 pages17MAKE OF JOKE :Laughter Club, Fun Zone, Tension FreeNo ratings yet
- Specific Relief Act 1963 - HindiDocument12 pagesSpecific Relief Act 1963 - HindiSHREE Music StudioNo ratings yet
- Limitation Act PDFDocument20 pagesLimitation Act PDFshishir duwediNo ratings yet
- Limitation Act - HindiDocument20 pagesLimitation Act - HindiSHREE Music StudioNo ratings yet
- Miyad Adhiniyam ActDocument20 pagesMiyad Adhiniyam Actkuldeep singhNo ratings yet
- SC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILDocument7 pagesSC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILALEEMNo ratings yet
- CCI (Commitment) Regulations, 2024Document12 pagesCCI (Commitment) Regulations, 2024Rajkumar MathurNo ratings yet
- Ram Nath Kovind On Simultaneous ElectionsDocument5 pagesRam Nath Kovind On Simultaneous ElectionsvenkannaNo ratings yet
- Aman Internal Hindi ProjectDocument14 pagesAman Internal Hindi Projectaman rajaNo ratings yet
- निर्वचन के मूल सिद्धांत निर्वचन अर्थान्वयन मे अन्तरDocument23 pagesनिर्वचन के मूल सिद्धांत निर्वचन अर्थान्वयन मे अन्तरALEEMNo ratings yet
- Religious and Charitable Endowments Under Hindu Law - En.hiDocument8 pagesReligious and Charitable Endowments Under Hindu Law - En.hiALEEMNo ratings yet
- 2.2 उपयोगितावादी नैतिकता उपयोगितावाद, utilitarian traditionDocument6 pages2.2 उपयोगितावादी नैतिकता उपयोगितावाद, utilitarian traditionALEEMNo ratings yet
- Hindu Law Notes Religious Endowment - En.hiDocument13 pagesHindu Law Notes Religious Endowment - En.hiALEEMNo ratings yet
- SC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILDocument7 pagesSC & HC क्षेत्राधिकार judicial review PILALEEMNo ratings yet
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग ररDocument1 pageकेन्द्रीय सतर्कता आयोग ररALEEMNo ratings yet
- Essentials of Religious and Charitable Trust Under Hindu Law 3.en - HiDocument18 pagesEssentials of Religious and Charitable Trust Under Hindu Law 3.en - HiALEEMNo ratings yet
- Hindu Religious and Endowment Essential All Answer (200-300) - VVVVVVVVVVVVVVV - En.hi PDFDocument101 pagesHindu Religious and Endowment Essential All Answer (200-300) - VVVVVVVVVVVVVVV - En.hi PDFALEEMNo ratings yet
- डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और एन.आर. बनाम मध्य प्रदेश Protective discrimination is part of compensatory justiceDocument2 pagesडॉ. प्रीति श्रीवास्तव और एन.आर. बनाम मध्य प्रदेश Protective discrimination is part of compensatory justiceALEEMNo ratings yet
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग लDocument2 pagesकेन्द्रीय सतर्कता आयोग लALEEMNo ratings yet
- PROTECTIVE DISCRIMINATION UNDER THE CONSTITUTION OF INDIA Protective Discrimination Is Part of Compensatory JusticeDocument5 pagesPROTECTIVE DISCRIMINATION UNDER THE CONSTITUTION OF INDIA Protective Discrimination Is Part of Compensatory JusticeALEEMNo ratings yet
- अनु 15 16 सुरक्षात्मक भेदभाव सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय पर नई न्यायिक प्रवृत्तियाँ Protective discriminationDocument17 pagesअनु 15 16 सुरक्षात्मक भेदभाव सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय पर नई न्यायिक प्रवृत्तियाँ Protective discriminationALEEMNo ratings yet
- - सुरक्षात्मक भेदभाव और समानता Protective discrimination is part of compensatory justiceDocument9 pages- सुरक्षात्मक भेदभाव और समानता Protective discrimination is part of compensatory justiceALEEMNo ratings yet
- - न्यायिक प्रक्रिया - बनाम - न्यायिक प्रक्रिया -Document3 pages- न्यायिक प्रक्रिया - बनाम - न्यायिक प्रक्रिया -ALEEMNo ratings yet
- (पीडीएफ) आपराधिक मामले में कानूनी मूल्य और न्याय की खोज में जज के कानूनी तर्क judicial reasoningDocument13 pages(पीडीएफ) आपराधिक मामले में कानूनी मूल्य और न्याय की खोज में जज के कानूनी तर्क judicial reasoningALEEMNo ratings yet
- हितप्रद निर्वचन-WPS OfficeDocument1 pageहितप्रद निर्वचन-WPS OfficeALEEMNo ratings yet
- civil procedure code question paper आम4 cpcDocument6 pagescivil procedure code question paper आम4 cpcALEEMNo ratings yet
- परिसीमा 3 - MpgkDocument5 pagesपरिसीमा 3 - MpgkALEEMNo ratings yet
- समझौता पत्र कैसDocument3 pagesसमझौता पत्र कैसALEEMNo ratings yet
- LL.B 5 Sem FormatDocument1 pageLL.B 5 Sem FormatALEEMNo ratings yet