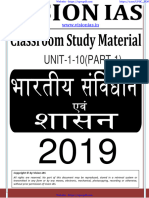Professional Documents
Culture Documents
भारत की श्रम नीति
भारत की श्रम नीति
Uploaded by
r.k.sir78560 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views3 pagesभारत की श्रम नीति का वर्णन करें।
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentभारत की श्रम नीति का वर्णन करें।
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views3 pagesभारत की श्रम नीति
भारत की श्रम नीति
Uploaded by
r.k.sir7856भारत की श्रम नीति का वर्णन करें।
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 3
ममर नीति का वर्णन करें।
भारत की र
Answer: स्वतन्त्रता— प्राप्ति के पचात् त्
श्चायह महसूस किया गया कि
श्रम—नीति सी हो जो कर्मकारों में आत्मविश्वास (Self reliance) पैदा
कर सके । स्वतन्त्रता—प्राप्ति श्चातथा सन् 1954 तक जबकि श्री
के पचात् त्
वी.वी. गिरि श्रम—मंत्री थे, सभी सरकारी प्राख्यान (Official
pronouncements) श्रमिकों के आत्मविश्वासी बनाने हेतु किये गये।
इस विचार धारा को सरकार द्वारा भी समर्थन मिला जिससे एक नई
विचार—धारा को बल मिला, जिसे 'त्रिपक्षीय.
—नीति' के नाम से जाना गया। यह 'त्रिपक्षीय' नीति सन्
मर
रम 1954 तक
केन्द्र—बिदु बन चुकी थी। इस सत्र के दौरान सरकार ने तीन पक्षों
द्वारा सम्मिलित प्रयास को आधार बनाया और वे तीन पार्टियाँ थीं—
व्यवसाय संघ जो कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती थीं, नियोजक तथा
सरकार। इस प्रकार के प्रयास में प्रतिनिधि स्वयं तो कोई निर्णय
नहीं लेते थे। उनका कार्य सलाह—सुझाव देने तक ही सीमित था। इन
तीनों पक्षों में सरकार का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है।
वार्षिक श्रम—सम्मेलनों तथा स्थायी श्रम—समितियों (Standing Labour
Committees) ने इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा की। सम्मेलनों
में कर्मकारों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने, कर्मकारों की शिक्षा,
कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी जैसे विधानों पर बल दिय गया।
सन्1958 के सोलहवें श्रम—सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया
गया, जिसके तहत उद्योग में अनु सन सनशासंहिता के प्रयोग को स्वीकारा
गया।
इस संहिता में व्यवस्था की गयी कि कोई भी पक्ष बिना सूचना दिये
हड़ताल या तालाबन्दी न करे तथा एकपक्षीय कार्यवाही को त्याग कर
सामूहिक रूप में ऐच्छिक विवाचन (Voluntary arbitration) द्वारा
अपनी समस्याओं का समाधान करे। यह भी व्यवस्था की गई कि अवपीड़न
(Ceorcion) (Victimisation) जैसी क्रियाओं का
तथा उत्पीड़न
सहारा न लिया जाय एवं अंशत: हड़ताल या तालाबन्दी को त्याग कर
शिकायत—प्रक्रिया (Grievance procedure) को स्वीकारा जाये।
त्रिपक्षीय नीति एक ऐसी प्रणाली है जो श्रम एवं पूँजी के बीच
निहित हितों की पहचान पर बल देती है। उत्पादन में तथा राष्ट्रीय
अर्थ—व्यवस्था को बनाने में श्रम एवं पूँजी दोनों एक दूसरे के
भागीदार हैं।
श्रम—नीति इस तथ्य पर आगे बढ़ी है कि पूरा समाज तथा व्यक्तिगत
नियोजन कर्मकारों के कल्याण की सुरक्षा के दायित्वाधीन हैं तथा
उन्हें ध्यान में रखना होगा कि कर्मकारों को आर्थिक लाभ का उचित
अंश मिल रहा है अथवा नहीं। इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 को संसद् में पारित किया, जिसमें
कर्मकारों को बोनस दिये जाने सम्बन्धी नियम बनाये गये हैं—
भारतीय श्रम—नीति के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं—
(1) राज्य को परिवर्तन एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए
उत्प्रेरक के रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक के रूप
में मान्यता देना।
(2) न्याय न दिये जाने की स्थिति में कर्मकारों के शान्तिपूर्ण ढंग से
अपने विरोध को प्रकट करने के अधिकार को मान्यता देना।
(3) आपसी समझौता (mutual settlement), सामूहिक सौदेबाजी
(Collective bargaining) एवं ऐच्छिक विवाचन (Valuntary
arbitration) को प्रोत्साहन देना।
(4) कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा
हस्तक्षेप।
(5) औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने को प्राथमिकता देना।
(6) नियोजक एवं नियोजित के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना।
(7) उचित मजदूरी मानदण्डों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
(8) उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु सहयोग देना।
(9) विधानों का समुचित प्रवर्तन।
(10) कर्मकारों की स्थिति को ऊँचा उठाना।
(11) त्रिपक्षीय सलाह मशविरा।
You might also like
- Class 11 Political ScienceDocument83 pagesClass 11 Political ScienceASHIF KHANNo ratings yet
- 8 April 2024 News Paper DiscussionDocument7 pages8 April 2024 News Paper DiscussionFaltu timeNo ratings yet
- एनसीईआरटी शोर्ट नोट्स - भारतीय अर्थव्यवस्था - स्टडी नोट्सDocument113 pagesएनसीईआरटी शोर्ट नोट्स - भारतीय अर्थव्यवस्था - स्टडी नोट्सshivaysinghrajputofficialNo ratings yet
- Bhic 110 HM 2022 23@7736848424Document10 pagesBhic 110 HM 2022 23@7736848424Rohan KumarNo ratings yet
- Judicial Activism in IndiaDocument5 pagesJudicial Activism in IndiamydeargorgeousoneNo ratings yet
- एडिटोरियल (02 Jan, 2023)Document5 pagesएडिटोरियल (02 Jan, 2023)Mayank PratapNo ratings yet
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - विकिपीडियाDocument18 pagesऔद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - विकिपीडियाVinod KumarNo ratings yet
- Code of Conduct V S Code of EthicsDocument2 pagesCode of Conduct V S Code of Ethics9236563265No ratings yet
- राज्य के नीति निदेशक तत्व PDFDocument6 pagesराज्य के नीति निदेशक तत्व PDFvinayyadavxyfNo ratings yet
- Sol - Development and Social MovementDocument136 pagesSol - Development and Social MovementLekhrajNo ratings yet
- Public Policy in IndiaDocument69 pagesPublic Policy in IndiaAmbrish TiwariNo ratings yet
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाDocument15 pagesपूंजीवादी अर्थव्यवस्थाAditya MahakalNo ratings yet
- EssayDocument32 pagesEssayDEBENDRA NATH CHOUDHURYNo ratings yet
- लक्ष्मीकांत बुक सारDocument580 pagesलक्ष्मीकांत बुक सारNirm alaNo ratings yet
- 5 6213004290580021516 PDFDocument336 pages5 6213004290580021516 PDFAshish AgarwalNo ratings yet
- - राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Document2 pages- राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Pradeep KumarNo ratings yet
- - राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Document2 pages- राजनीतिक सिद्धांत उदाश्य और उपोगियता का वर्णन करे। - ... कार के विभिन्न सिद्धांतो का वर्णन करे In Hindi -Pradeep KumarNo ratings yet
- Concept of Good Governance PDFDocument14 pagesConcept of Good Governance PDFvishalkumar6691No ratings yet
- 11 Polscie Hindi 2023 24Document3 pages11 Polscie Hindi 2023 24vk1433090No ratings yet
- Preamble प्रस्तावनाDocument6 pagesPreamble प्रस्तावनाamriteshrajtetri1811No ratings yet
- Ilovepdf MergedDocument15 pagesIlovepdf Mergedmahendrasingh366789No ratings yet
- Indian National CongressDocument5 pagesIndian National Congresskittu4478No ratings yet
- DPSPDocument12 pagesDPSPNadeem SiddiquiNo ratings yet
- Legal HindiDocument7 pagesLegal HindisomyaNo ratings yet
- 11 भारतीय संविधान एवं शासन Part 3 24913 unlockedDocument107 pages11 भारतीय संविधान एवं शासन Part 3 24913 unlockedashish singhNo ratings yet
- Mini Training On Constitution Day2Document14 pagesMini Training On Constitution Day2ISNo ratings yet
- औद्योगिक नीतिDocument23 pagesऔद्योगिक नीतिAditya MahakalNo ratings yet
- ThaDocument47 pagesThacryptowalaNo ratings yet
- Globalization Sem 6 One Shot VideoDocument32 pagesGlobalization Sem 6 One Shot Videodelguru.eduNo ratings yet
- Basics of Economy Overview of Indian Economy Hindi Corrected 18Document9 pagesBasics of Economy Overview of Indian Economy Hindi Corrected 18Alok MishraNo ratings yet
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन #margdarshanDocument33 pagesगुटनिरपेक्ष आन्दोलन #margdarshanrenjaiswalNo ratings yet
- सहकारिता 2Document8 pagesसहकारिता 2skrajput.08071993No ratings yet
- (Introduction of Labour Economics) : ST TH RDDocument16 pages(Introduction of Labour Economics) : ST TH RDAli RazaNo ratings yet
- भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य - विकिपीडियाDocument60 pagesभारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य - विकिपीडियाAbhay ShuklaNo ratings yet
- Fundamental Rights DiaryDocument143 pagesFundamental Rights DiaryDhanauri DhanauriNo ratings yet
- Vision IAS Classroom Study Material Indian PolityDocument475 pagesVision IAS Classroom Study Material Indian PolityraviNo ratings yet
- Fundamental Rights 1692736378751Document41 pagesFundamental Rights 1692736378751Sanvi 2914No ratings yet
- PS Unit 3+4+5Document29 pagesPS Unit 3+4+5governmentjobnotification.277No ratings yet
- GS 2 2023 For Learners 1Document72 pagesGS 2 2023 For Learners 1UtkarshNo ratings yet
- संविधान की प्रस्तािनाDocument6 pagesसंविधान की प्रस्तािनाjinNo ratings yet
- Additional NotesDocument8 pagesAdditional Notessantosh kumarNo ratings yet
- Module 1 History of Life Insurance HindiDocument9 pagesModule 1 History of Life Insurance HindiravandkumarNo ratings yet
- Module 1 History of Life Insurance Hindi PDFDocument9 pagesModule 1 History of Life Insurance Hindi PDFAnilPanchalNo ratings yet
- MSW08 PDFDocument197 pagesMSW08 PDFshersinghb12No ratings yet
- Polity Notes1 Hindi VisionDocument239 pagesPolity Notes1 Hindi Visionyogeshsosa5050No ratings yet
- Panchayat I RajDocument5 pagesPanchayat I Rajshahrachit91No ratings yet
- समान नागरिक कानूनDocument12 pagesसमान नागरिक कानूनmanishahealingsNo ratings yet
- Business Organization Notes Unit 1.en - HiDocument8 pagesBusiness Organization Notes Unit 1.en - HiShashi RajpootNo ratings yet
- Samajik Rohit YadavDocument16 pagesSamajik Rohit YadavRohit YadavNo ratings yet
- 11 ST SetDocument3 pages11 ST SetashishNo ratings yet
- 1690169993Document1 page1690169993Awyaan KaushikNo ratings yet
- Olive: BoardDocument34 pagesOlive: BoardAnmol SolankiNo ratings yet
- 1. भारतीय संविधान - WatermarkDocument11 pages1. भारतीय संविधान - Watermarkjimaurya431No ratings yet
- मानव अधिकार और मौलिक अधिकार के मध्य शरीर व आत्मा का संबंध हैDocument3 pagesमानव अधिकार और मौलिक अधिकार के मध्य शरीर व आत्मा का संबंध हैTwin PrajapatiNo ratings yet
- 7th Pay Commission ReportDocument899 pages7th Pay Commission Reportmech_lalit2k77856100% (1)
- Seven CPC ReportDocument899 pagesSeven CPC ReportVigneshwar Raju PrathikantamNo ratings yet
- Modi Sarkar Naye Prayog Naye Vichar (मोदी सरकार नए प्रयोग, नए विचार)From EverandModi Sarkar Naye Prayog Naye Vichar (मोदी सरकार नए प्रयोग, नए विचार)No ratings yet